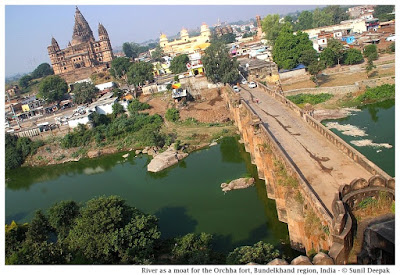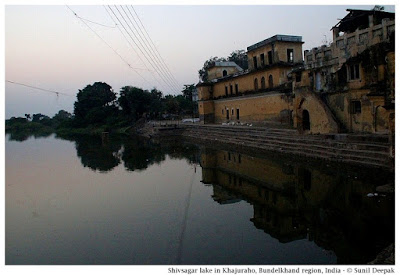Narsimha Dudhai
Vishavarupa Darshan of the NaraHari
tararashana makara kundala manindraih
bhushitam-ashesha-nilayam tava vapurme
chotasi chakasta narasimha narasimha
O Lord Nrisimha, O Lord Nrisimha, Your transcendental body, which is the ultimate shelter of everything. Is decorated with a beautiful golden crown, a forest garland, shark-like earrings, various excellent jewels and an out projecting wide tongue. (Sri Nrisimhashtakam)
The cattle-track drive to Dudhai earlier in the day was partly through a forest road built in the British era. There were times when the track became so bad that I thought of turning back. But I soldiered on; I was glad I did. The Narasimha needs to be talked about.
The statue stands more than 30ft high and in the true spirit of the myth it represents, it has across its thighs the figure of the demon Hiranyakashipu being torn apart. It is not beautiful, but then this incarnation of Vishnu was never meant to be so. In terms of detailing it has some exceptional aspects. The lines of rock have been drawn to a fine point and some articles of clothing and a necklace stand out. The ferocity of the Narasimha-avatar is typified by the teeth drawn back in a snarl. The statue, created out of the rock it stands in, has near perfect camouflage and is nearly invisible unless seen from a relatively close distance.
Research on the statue proved quite futile with the complete absence of documented material on this site. Most Narasimha-centric places of worship are located in south India with just a few scattered sites in the north and central India. Given the lack of material, it was difficult to pin down the time of its creation. However, circumstantial evidence drawn from other sites in the same geographic region points to the Gupta period, when the worship of Vishnu was at a high. The Dashavatara temple at nearby Deogarh and the huge standing Varaha statue in the Udaygiri caves in Madhya Pradesh are two cases in point.
Both date to the Gupta period and both are classic examples of the iconography that was used to depict the incarnations of Vishnu. That the Dudhai Narasimha would belong to this period can only be taken as a logical conclusion, though more research is needed to find a more precise date.
In the Lalitpur district of Uttar Pradesh is the ancient village of Dudhai, which is home to an astounding murti of Lord Nrsimhadeva. Cut into the rock face of a hillside way off the beaten track, relatively few pilgrims search out this hidden treasure. Although it is listed as a sacred site by the Archaeological Survey of India, little documentation is available about the sculpture. Lord Nrsimhadeva's lips are pulled back in a snarl, revealing his fearsome teeth and tongue. The lines of rock have been used advantageously, bringing certain elements of the design to a fine point. The Lord's clothing and ornaments, for example, are very distinct in some places, while in some places the lines of the sculpture have been blurred by water and weather. A split column is beautifully executed in the murti, and the sculptor took full advantage of the natural colors in the rock face, which emphasize certain aspects of the murti design. Overall, this massive image is so camouflaged by its natural surroundings as to be almost invisible, until one gets relatively close, and views it from the right angle.
ओरछा के मंदिर
Temples of Orcha - ओरछा के मंदिर
ओरछा के मंदिर
कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले लोगों ने बुंदेलखंड में रहना शुरू किया था। यही वजह है कि इस इलाके के हर गांव और शहर के पास सुनाने को कई कहानियां हैं। बुंदेलखंड की दो खूबसूरत और दिलचस्प जगहें हैं ओरछा और कुंढार। भले ही दोनों जगहों में कुछ किलोमीटर का फासला हो, लेकिन इतिहास के धागों से ये दोनों जगहें बेहद मजबूती से जुड़ी हुई हैं। ओरछा झांसी से लगभग आधे घंटे की दूरी पर स्थित है।
इतिहास
इसका इतिहास 8वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने इसकी स्थापना की थी। इस जगह की पहली और सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है। दरअसल, यह मंदिर भगवान राम की मूर्ति के लिए बनवाया गया था, लेकिन मूर्ति स्थापना के वक्त यह अपने स्थान से हिली नहीं। इस मूर्ति को मधुकर शाह के राज्यकाल (1554-92) के दौरान उनकी रानी गनेश कुवर अयोध्या से लाई थीं। चतुर्भुज मंदिर बनने से पहले इसे कुछ समय के लिए महल में स्थापित किया गया। लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उसके स्थान से हिला नहीं पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। आज इस महल के चारों ओर शहर बसा है और राम नवमी पर यहां हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वैसे, भगवान राम को यहां भगवान मानने के साथ यहां का राजा भी माना जाता है, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर न होकर महल की ओर है।
मंदिर व आस पास
मंदिर के पास एक बगान है जिसमें स्थित काफी ऊंचे दो मीनार (वायू यंत्र) लोगों के आकर्षण का केन्द्र हैं। जि्न्हें सावन भादों कहा जाता है कि इनके नीचे बनी सुरंगों को शाही परिवार अपने आने-जाने के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करता था। इन स्तंभों के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि वर्षा ऋतु में हिंदु कलेंडर के अनुसार सावन के महीने के खत्म होने और भादों मास के शुभारंभ के समय ये दोनों स्तंभ आपस में जुड़ जाते थे। हालांकि इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं हैं। इन मीनारों के नीचे जाने के रास्ते बंद कर दिये गये हैं एवं अनुसंधान का कोई रास्ता नहीं है।
इन मंदिरों को दशकों पुराने पुल से पार कर शहर के बाहरी इलाके में 'रॉयल एंक्लेव' (राजनिवास्) है। यहां चार महल, जहांगीर महल, राज महल, शीश महल और इनसे कुछ दूरी पर बना राय परवीन महल हैं। इनमें से जहांगीर महल के किस्से सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जो मुगल बुंदेला दोस्ती का प्रतीक है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने अबुल फज़ल को शहजादे सलीम (जहांगीर) को काबू करने के लिए भेजा था, लेकिन सलीम ने बीर सिंह की मदद से उसका कत्ल करवा दिया। इससे खुश होकर सलीम ने ओरछा की कमान बीर सिंह को सौंप दी थी। वैसे, ये महल बुंदेलाओं की वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं। खुले गलियारे, पत्थरों वाली जाली का काम, जानवरों की मूर्तियां, बेलबूटे जैसी तमाम बुंदेला वास्तुशिल्प की विशेषताएं यहां साफ देखी जा सकती हैं।
अब बेहद शांत दिखने वाले ये महल अपने जमाने में ऐसे नहीं थे। यहां रोजाना होने वाली नई हलचल से उपजी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इन्हीं में से एक है हरदौल की कहानी, जो जुझार सिंह (1627-34) के राज्य काल की है। दरअसल, मुगल जासूसों की साजिशभरी कथाओं के कारण् इस राजा का शक हो गया था कि उसकी रानी से उसके भाई हरदौल के साथ संबंध हैं। लिहाजा उसने रानी से हरदौल को ज़हर देने को कहा। रानी के ऐसा न कर पाने पर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हरदौल ने खुद ही जहर पी लिया और त्याग की नई मिसाल कायम की।
बुंदेलाओं का राजकाल 1783 में खत्म होने के साथ ही ओरछा भी गुमनामी के घने जंगलों में खो गया और फिर यह स्वतंत्रता संग्राम के समय सुर्खियों में आया। दरअसल, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद यहां के एक गांव में आकर छिपे थे। आज उनके ठहरने की जगह पर एक स्मृति चिन्ह भी बना है।
जहांगीर महल
बुन्देलों और मुगल शासक जहांगीर की दोस्ती की यह निशानी ओरछा का मुख्य आकर्षण है। महल के प्रवेश द्वार पर दो झुके हुए हाथी बने हुए हैं। तीन मंजिला यह महल जहांगीर के स्वागत में राजा बीरसिंह देव ने बनवाया था। वास्तुकारी से दृष्टि से यह अपने जमाने का उत्कृष्ट उदाहरण है।
राज महल
यह महल ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में एक है। इसका निर्माण मधुकर शाह ने 17 वीं शताब्दी में करवाया था। राजा बीरसिंह देव उन्हीं के उत्तराधिकारी थे। यह महल छतरियों और बेहतरीन आंतरिक भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महल में धर्म ग्रन्थों से जुड़ी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं।
रामराजा मंदिर
यह मंदिर ओरछा का सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण मंदिर है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि राजा मधुकर को भगवान राम ने स्वप्न में दर्शन दिए और अपना एक मंदिर बनवाने को कहा।
राय प्रवीन महल
यह महल राजा इन्द्रमणि की खूबसूरत गणिका प्रवीणराय की याद में बनवाया गया था। वह एक कवयित्री और संगीतकारा थीं। मुगल सम्राट अकबर को जब उनकी सुंदरता के बार पता चला तो उन्हें दिल्ली लाने का आदेश दिया गया। इन्द्रमणि के प्रति प्रवीन के सच्चे प्रेम को देखकर अकबर ने उन्हें वापस ओरछा भेज दिया। यह दो मंजिला महल प्राकृतिक बगीचों और पेड़-पौधों से घिरा है। राय प्रवीन महल में एक लघु हाल और चेम्बर है।
लक्ष्मीनारायण मंदिर
यह मंदिर 1622 ई. में बीरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। मंदिर ओरछा गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना है। मंदिर में सत्रहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के चित्र बने हुए हैं। चित्रों के चटकीले रंग इतने जीवंत लगते हैं जसे वह हाल ही में बने हों। मंदिर में झांसी की लड़ाई के दृश्य और भगवान कृष्ण की आकृतियां बनी हुई हैं।
चतुर्भुज मंदिर
राज महल के समीप स्थित चतुभरुज मंदिर ओरछा का मुख्य आकर्षण है। यह मंदिर चार भुजाधारी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1558 से 1573 के बीच राजा मधुकर ने करवाया था। अपने समय की यह उत्कृष्ठ रचना यूरोपीय कैथोड्रल से समान है। मंदिर में प्रार्थना के लिए विस्तृत हॉल है जहां कृष्ण
भक्त एकत्रित होते हैं।
फूलबाग
बुन्देल राजाओं द्वारा बनवाया गया यह फूलों का बगीचा चारों ओर से दीवारों से घिरा है। पालकी महल के निकट स्थित यह बाग बुन्देल राजाओं का आरामगाह था। वर्तमान में यह पिकनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। फूलबाग में एक भूमिगत महल और आठ स्तम्भों वाला मंडप है। यहां के चंदन कटोर से गिरता पानी झरने के समान प्रतीत होता है।
सुन्दर महल
इस महल को राजा जुझार सिंह के पुत्र धुरभजन के बनवाया था। राजकुमार धुरभजन को एक मुस्लिम लड़की से प्रेम था। उन्होंने उससे विवाह कर इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया। धीर-धीर उन्होंने शाही जीवन त्याग दिया और स्वयं को ध्यान और भक्ति में लीन कर लिया। विवाह के बाद उन्होंने सुन्दर महल त्याग दिया। धुरभजन की मृत्यु के बाद उन्हें संत से रूप में जाना गया। वर्तमान में यह महल काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है।
छतरियां
छतरियों का अर्थ है शाही समाधियाँ जो ओरछा में नदी के किनारे एक अनोखा आकर्षण उत्पन्न करती हैं। बेतवा नदी के कंचन घाट पर ऐसे 14 स्मारक हैं। ओरछा के शासकों की याद में बनवाये गये ये स्मारक 17वीं और 18वीं शताब्दी के हैं। ये छतरियाँ बुन्देल राजाओं के सम्मान में हैं और खास बुन्देलखण्ड शैली में बनी हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जिस काल में इनका निर्माण वह एक “स्वर्णिम युग” था। सूर्यास्त के दौरान नदी में इन स्मारकों का प्रतिबिम्ब देखते ही बनता है। खम्भों पर बने उँचे मंच पर स्थित ये छतरियाँ अपने जादुई आकर्षण से हर वर्ष भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इन छतरियों को एक संकरे पुल से सबसे बेहतर देखा जा सकता है और ओरछा आने वाले लोगों को इन्हें अवश्य देखना चाहिये। नदी के किनारे बने इस स्थल पर पर्यटकों को भरपूर आनन्द प्राप्त होता है।
बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट पर बीर सिंह बुंदेला की छतरी है, यह छतरी तीन मंजिला है। बुदेंलों के इतिहास में वीर सिंह का कार्यकाल स्वर्णयुग कहलाता है। इनके कार्यकाल में ही जहाँगीर महल, नौबतखाना, फ़ूलबाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं हमाम जैसी भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। यह छतरी तीन मंजिली है तथा बुंदेला स्थापत्य के आधार पर ही इसका निर्माण हुआ है। मेहराबों से छतों को सहारा देकर मध्यम में गुम्बद का निर्माण किया गया है। पवित्र पावन बेतवा नदी इसके अधिष्ठान को छूते हुए बहती है।
इसके साथ इन्हें छतरियों का समूह भी कहा जा सकता है। बेतवा के किनारे अन्य पन्द्रह छतरियां भी निर्मित हैं। यहाँ की अधिकांश छतरियां तीन मंजिली है, सूचना फ़लक पर मधुकर शाह, बीरसिंह देव, जसवंत सिंह, उद्वैत सिंह, पहाड़ सिंह आदि का नाम अंकित है। ये छतरियां पंचायतन शैली के मंदिरों जैसी बनी हुई हैं। चौकोर चबुतरे के मध्य में गर्भगृह एवं उसके चारों कोणों में खाली स्थान है, ऊपर जाकर यही अष्टकोणीय हो जाते हैं। इनमें गुंबद विशेष स्थान रखता है।
ओरछा झांसी से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से यहां भोपाल शताब्दी-एक्सप्रेस के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है।
ओरछा का नजदीकी हवाई अड्डा खजुराहो है जो 163 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एयरपोर्ट दिल्ली, वाराणसी और आगरा से नियमित फ्लाइटों से जुड़ा है।
झांसी ओरछा का नजदीकी रेल मुख्यालय है। दिल्ली, आगरा, भोपाल, मुम्बई, ग्वालियर आदि प्रमुख शहरों से झांसी के लिए अनेक रेलगाड़ियां हैं। वैसे ओरछा तक भी रेलवे लाइन है जहां पैसेन्जर ट्रैन से पहुंचा जा सकता है।
ओरछा झांसी-खजुराहो मार्ग पर स्थित है। नियमित बस सेवाएं ओरछा और झांसी को जोड़ती हैं। दिल्ली, आगरा, भोपाल, ग्वालियर और वाराणसी से यहां से लिए नियमित बसें चलती हैं।
दशावतार मंदिर, देवगढ़
दशावतार का विष्णु मंदिर
देवगढ़ का इतिहास में बहुत ही ख़ास स्थान रहा है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके अन्य दर्शनीय स्थलों में मुख्य हैं- सैपुरा ग्राम से 3 मील (लगभग 4.8 कि.मी.) पश्चिम की ओर पहाड़ी पर एक चतुष्कोण कोट, नीचे मैदान में एक भव्य विष्णु का मंदिर, यहाँ से एक फलांग पर वराह मंदिर, पास ही एक विशाल दुर्ग के खंडहर, इसके पश्चात दो और दुर्गों के भग्नावशेष, एक दुर्ग के विशाल घेरे में 31 जैन मंदिरों और अनेक भवनों के खंडहर।
देवगढ़ में सब मिला कर 300 के लगभग अभिलेख मिले हैं, जो 8वीं शती से लेकर 18वीं शती तक के हैं। इनमें ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा अंकित अठारह लिपियों का अभिलेख तो अद्वितीय ही है। चंदेल नरेशों के अभिलेख भी महत्त्वपूर्ण हैं। देवगढ़ बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तट के निकट पहाड़ी पर 24 मंदिरों के अवशेष हैं, जो 7वीं शती ई. से 12वीं शती ई. तक बने थे।
देवगढ़ का शायद सर्वोत्कृष्ट स्मारक ‘दशावतार का विष्णु मंदिर’ है, जो अपनी रमणीय कला के लिए भारत भर के उच्च कोटि के मंदिरों में गिना जाता है। इसका समय छठी शती ई. माना जाता है, जब गुप्त वास्तु कला अपने पूर्ण विकास पर थी। मंदिर का समय भग्नप्राय अवस्था में है, किन्तु यह निश्चित है कि प्रारम्भ में इसमें अन्य गुप्त कालीन देवालयों की भांति ही गर्भगृह के चतुर्दिक पटा हुआ प्रदक्षिणा पथ रहा होगा।
इस मंदिर के एक के बजाए चार प्रवेश द्वार थे और उन सबके सामने छोटे-छोटे मंडप तथा सीढ़ियां थीं। चारों कोनों में चार छोटे मंदिर थे। इनके शिखर आमलकों से अलंकृत थे, क्योंकि खंडहरों से अनेक आमलक प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक सीढ़ियों की पंक्ति के पास एक गोखा था। मुख्य मंदिर के चतुर्दिक कई छोटे मंदिर थे, जिनकी कुर्सियाँ मुख्य मंदिर की कुर्सी से नीची हैं। ये मुख्य मंदिर के बाद में बने थे।
इनमें से एक पर पुष्पावलियों तथा अधोशीर्ष स्तूप का अलंकरण अंकित है। यह अलंकरण देवगढ़ की पहाड़ी की चोटी पर स्थित मध्ययुगीन जैन मंदिरों में भी प्रचुरता से प्रयुक्त है। दशावतार मंदिर में गुप्त वास्तु कला के प्रारूपिक उदाहरण मिलते हैं, जैसे, विशाल स्तम्भ, जिनके दंड पर अर्ध अथवा तीन चौथाई भाग में अलंकृत गोल पट्टक बने हैं। ऐसे एक स्तम्भ पर छठी शती के अंतिम भाग की गुप्त लिपि में एक अभिलेख पाया गया है, जिससे उपर्युक्त अलंकरण का गुप्त कालीन होना सिद्ध होता है।
इस मंदिर की वास्तु कला की दूसरी विशेषता चैत्य वातायनों के घेरों में कई प्रकार के उत्कीर्ण चित्र हैं। इन चित्रों में प्रवेश द्वार या मूर्ति रखने के अवकाश भी प्रदर्शित हैं। इनके अतिरिक्त सारनाथ की मूर्तिकला का विशिष्ट अभिप्राय स्वस्तिकाकार शीर्ष सहित स्तम्भयुग्म भी इस मंदिर के चैत्यवातायनों के घेरों में उत्कीर्ण है। दशावतार मंदिर का शिखर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संरचना है। पूर्व गुप्त कालीन मंदिरों में शिखरों का अभाव है
यह विश्व का इकलौता मंदिर है, जहां भगवान विष्णु के दशावतारों को एक ही मंदिर में पिरोया गया है। इसी वजह से
इसे दशावतार पुकारा गया। दशावतार मंदिर को इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहां रामायण और महाभारत की देव प्रतिमाओं का अनूठा संगम है। मूर्तियों में जहां द्रौपदी और पांडव एक साथ दर्शाए गए हैं, वहीं हाथी की पुकार पर सब कुछ छोड़ विष्णु प्रतिमा का भी एक-एक भाव अपने आप में नायाब है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, जो पंच ललित कलाएं हैं, जिनके आधार पर हमारी संपूर्ण कलाएं समाहित की जाती हैं, उन सभी कलाओं का यहां की मूर्तियों में दर्शन मिलता है। यहां की मूर्तियों में भारतीय दर्शन के सभी प्राचीन धार्मिक चिन्हों- हाथी, शंख पुष्प, कमल आदि का भी समावेश किया गया है, जो देश के दूसरे हिस्सों की शिल्पकृतियों में नहीं मिलता। कई मूर्ति शिल्पकारों का तो यहां तक कहना है कि देवगढ़ में हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ कला का नमूना देखने को मिलता है।
इतिहासकारों के मुताबिक, पुरातात्विक महत्व के हिसाब से जो वैष्णव कला से संबंधित मूर्ति शिल्प है उसके चंद मंदिर ही विश्व में बचे हैं जो अंकोरवाट, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया में हैं। इनके अलावा सिर्फ दशावतार मंदिर ही इस श्रंखला की आखिरी कड़ी है।
यहां की मूर्तियों में सबसे लोकप्रिय गजेंद्र की मोक्ष मुद्रा इतनी वास्तविक और सजीव है कि उसे देखते ही पता चलता है कि भगवान विष्णु बहुत ही हड़बड़ी में आए हैं। उन्होंने पादुकाएं भी नहीं पहनी हैं। नंगे पैर हैं और ऐसे भाग रहे हैं जैसे किसी आपात स्थिति में जा रहे हों। इसके अलावा जिस हाथी का उद्धार करने विष्णु साक्षात आए, उसकी मुद्रा भी बेहद अहम है। हाथी को देखने से लगता है कि वह मृतप्राय स्थिति में है और उसे भगवान विष्णु के अलावा कोई उद्धारक नहीं दिखाई दे रहा। उसके चेहरे पर पीड़ा की जो रेखाएं हैं उसे मूर्ति शिल्प के जरिये इतने वास्तविक तरीके से उकेरा गया है कि उसे देखकर प्रतीत होता है कि यह मूर्ति न होकर साक्षात हाथी खड़ा हो गया हो। इसके अलावा शेषसाही प्रतिमा पर अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि जो एक व्यक्ति शयन की स्थिति में होता है तो बहुत ही आरामदेह मुद्रा में होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह सारी चिंताओं से मुक्त होकर शयन कर रहा है।
इसी तर्ज पर भगवान विष्णु के चेहरे के जो भाव मूर्ति शिल्पकार ने उकेरे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आराम की मुद्रा में भगवान हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं।
इतिहासकारों के मुताबिक, 15वीं शताब्दी के बाद की मूर्तियों में ये खासियत देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मुगलकाल से जो मूर्तिकला का क्षरण शुरू हुआ, उसके बाद मूर्ति शिल्प में न वह हुनर रह गया है और न वह कौशल रह गया है, और न ही वह परंपरा जीवित रह पाई।
माँ वनखंडी देवी का इतिहास
शेष जी भी अपने सहस्र मुख से जिसका वर्णन नहीं कर सकते, शंकर जिसको अपने पंचमुख से नहीं कह सकते,चारो वेदों के ज्ञाता, जगत के रचनाकार ब्रम्ह चार मुख से, सर्वज्ञ विष्णु,एवं कार्तिकेय छः मुख से विघ्नहर्ता-सर्वसिद्धिकर्ता गणेश योगिन्द्रो के गुरु भी जिसकी शक्ति का बखान नही कर पाते, जिनके गुणों के वर्णन में सरस्वती भी जड़ीभूत हो जाती हैं, सनत्कुमार,धर्म,सनंदन,सनातन ,सनक,कपिल, सूर्य,एवं ब्रम्हा के अन्य श्रेष्ठ एवं सिद्ध पुत्र श्री जिनके गुण नही कह सकते तो दुसरे जड़ बुद्धियों की क्या कहें| ब्रम्हा, विष्णु, शिव आदि जिनके चरण कमलो का ध्यान करते हैं,जो भक्तो के लिए ही साध्य है एवं दूसरो के लिए दुर्लभ हैं | कोई कोई ही जिनके गुणों का कुछ-कुछ वर्णन-कीर्तन जानते हैं,उनसे अधिक ज्ञानियों के गुरु गणेश जानते हैं एवं सबसे अधिक सर्वज्ञ शंकर जानते हैं |
परमात्मा की वह चित्त रूपिणी शक्ति जो कालक्रमानुसार विभिन्न रूप धारण करती है तथा ब्रम्हा,विष्णु,महेश जिसकी कृपा से रक्षा करते हैं वह त्रिदेवों की चित्त रूपिणी शक्ति माँ वनखंडी कालपी धाम में निवास करती हैं | भक्तो के हितार्थ शक्ति स्वरूपा माँ विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कालों में अनेक लीलाओं द्वारा अपने स्वरुप का दर्शन कराती हैं | सृष्टि के प्रारंभ से निराकार स्वरुप में प्रतिष्ठित यह शक्तिपुंज जो वर्तमान में वनखंड में विराजत होने के कारण वनखंडी तथा अच्छे-अच्छे शूरमाओं अभिमानिओं एवं विघ्नों का खंडन करने के कारण बलखंडी नाम से जानी जाती हैं |
प्राचीन काल में सुधांशु नाम के एक ब्राह्मण थे जिनके कोई संतान नही थी | एक बार देवर्षि नारद मृत्युलोक में घूमते हुए उनके घर के सामने से निकले | अपने घर के बहार उन्होंने सुधांशु ब्राम्हण को दुखी: अवस्था में बैठे हुए देखा | उस अवस्था में बोथे देख देवर्षि को उसपर दया आयी | उन्होंने उससे दुखी होने का कारन पुछा | ब्राम्हण ने संतान सुख न होने की अपनी व्यथा कही एवं संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना की | नारद ने कहा की वह उसकी बात को भगवान से कहकर उसके दू:ख को मिटाने की प्रार्थना करेंगे | उस ब्राम्हण की बात को सुनकर नारद जी विष्णुलोक पहुंचे एवं भगवान् विष्णु से उस ब्राम्हण की बात कही | भगवान् एन कहा कि इस जन्म में उसके कोई संतान योग नही है | यही बात नारद जी ने ब्रम्हा एवं भगवान् शंकर से पूछी | उन्होंने ने भी यही जवाब दिया | यह बात नारद जी वापस लौटकर उस ब्राम्हण को बताई | निसंतान ब्राम्हण यह सुनकर दू:खी हुआ पर भावी को कौन बदल सकता है | कुछ वर्षोपरांत एक दिन सात वर्ष कि एक कन्या उसके द्वार के सामने सेः कहते हुए निकली कि ” जो कोई मुझे हलुआ-पूड़ी का भोजन कराएगा वह मनवांछित वर पायेगा |” यह बात उस सुधांशु ब्राम्हण की पत्नी ने सुनीं तो दौड़कर बहार आयी | ब्राम्हण पत्नि ने उस कन्या को बुलाया, उस आदर से बैठाकर पूछा कि ” मै यदि आपको हलुआ-पूड़ी खिलाऊं तो क्या मेरी मनोकामना पूर्ण होगी ?” “हाँ अवश्य पूर्ण होगी |” ऐसा उस कन्या ने कहा | तत्पश्चात उस ब्राम्हण पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ उस कन्या को हलुआ-पूड़ी का भोजन कराया | भोजनोपरांत ब्राम्हण पत्नी ने कहा- देवी मेरे कोई संतान नही है ,कृपया मुझे संतान सु:ख का वर दीजिये | कन्या ने ब्राम्हण पत्नी से “तथास्तु” कहा | इसके बाद ब्राम्हण पत्नी ने उस कन्या से उसका नाम व धाम के बारे में पूछा | उस कन्या ने अपना नाम जगदम्बिका तथा अपना धाम अम्बिकावन बताया | समय पर ब्राम्हण को पुत्र प्राप्ति हुई | पुत्र धीरे-धीरे जब कुछ बड़ा हुआ कुछ समय पश्चात एक दिन देवर्षि नारद जी का पुन: आगमन हुआ | नारद जी ने उस ब्राम्हण से पूछा ये पुत्र किसका है ? तो ब्राम्हण ने बताया कि यह पुत्र मेरा है | नारद जी को पहले तो विश्वास नही हुआ, फिर उस ब्राम्हण कि बात सुनकर भगवान् विष्णु के लोक में जाकर उनसे ब्राम्हण पुत्र के बारे में चर्चा की | भगवान् ने कहा ऐसा हो ही नही सकता की ब्राम्हण को कोई संतान हो | यही बात ब्रम्हा और भगवान् शंकर ने भी कही | तब नारद जी ने त्रिदेवों से स्वयं चलकर देखने के लिए प्रार्थना की | नारद जी की प्रार्थना पर त्रिदेव नारद जी के साथ ब्राम्हण के यहाँ पधारे | ब्राम्हण से पुत्र प्राप्ति का सम्पूर्ण वृतांत जानकार त्रिदेव नारद जी एवं वह ब्राम्हण के साथ अम्बिकावन को प्रस्थान किये | अम्बिकावन में उन्हें वह देवी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई दिखी | उस समय सर्दी का मौसम था एवं शीत लहर ले साथ वर्षा भी हो रही थी | अत्यंत शीत लहर के कारण इन्हें ब्राम्हण के साथ-साथ सर्दी का बहुत तेजी से अनुभव हो रहा था | ये सभी उस देवी को देख कर पहुंचे तो देखा कि देवी के सिर पर बहुत बड़ा जूड़ा बंधा हुआ है एवं पास में ही एक पात्र में घृत(घी) रखा हुआ है | उस कन्या ने इन्हें ठण्ड से कांपते हुए देखा तो पास में रखे हुए घी को अपने बालों में लगाकर उसमे अग्नि प्रज्ज्वलित कर दी ताकि इनकी ठण्ड दूर हो सके | परन्तु यह दृश्य देखकर सभी अत्यतेंन भयभीत हो गए एवं देवी से अग्नि शांति हेतु प्रार्थना करने लगे, तब देवी ने अग्नि को शांत कर पुछा , की आप किस लिए यहाँ आये हुए हैं ? त्रिदेव अपने आने का सम्पूर्ण कारन बताते हुए बोले; “देवी हम सब कुछ जान चुके हैं कि आप सर्व समर्थ हैं | जो हम नही कर सकते है वो आप कर सकती हैं | यह अम्बिका वन ही अपना कालपी धाम है और माता जगदम्बिका ही माँ वनखंडी हैं | कोई-कोई इन्हें योग माया के नाम से जानते हैं | ”वर्तमान काल में झांसी कानपुर रेलवे लाइन ब्रिटिश काल के समय जब बिछाई जा रही थी , उस समय के अंग्रेज अधिकारी तथा कालपी के पटवारी कानूगो आदि उस स्थान का सर्वेक्षण कर रहे थे उस समय ब्रिटिश अधिकारी को दो सफ़ेद शेर दिखाई दिए | ब्रिटिश अधिकारी ने उनका शिकार करना चाहा तो साथ के लोगो ने ऐसा न करने का विनय किया | उनकी बात सुनकर कुछ क्षण के लिए अधिकारी हिचका इतने में वो शेर आगे निकल गए | किन्तु अधिकारी का मन नही माना एवं उसने उन शेरों का पीछा किया | अधिकारी के साथ दुसरे अन्य लोग भी उनके साथ चले | जंगल में विचरते हुए वे शेर एक झड़ी की तरफ आकर गम हो गए | जब सभी लोग घूम कर उस घनी झाडी के सामने आये तो वे शेर पत्थर के बने हुए वहां पर बैठे थे |
उनके (शेरों के) पीछे झाड़ियों के अन्दर माँ की पिण्डी का दर्शन हो रहा था | उस समय यह पूरा क्षेत्र घनघोर जंगल के रूप में था माँ की पिण्डी झाड़ियों में एक टीले के ऊपर दबी हुई थी | जो अपना हल्का सा आभास दे रही थी | उस दृश्य को देखकर वह अंग्रेज अधिकारी एवं उनके साथ के सभी लोग भयभीत एवं चकित हो गए एवं आश्चर्य-चकित अवश्था में उलटे पैरों वापस लौट पड़े |जिस विवरण को उस समय के पटवारी ने अपनी दैनिक डायरी में लिपिबद्ध किया | कुछ समय तक यह घटना चन्द ही लोगो तक रही लेकिन उसी समय एक और घटना घटी | आस-पास क्षेत्र के चरवाहे जंगल में अपने जानवर चराया करते थे | उनमे से एक चरवाहे की गाय जो बछड़े को जन्म देने के उपरांत जंगल में चरने को आती थी किन्तु शाम को जब पहुँचती तो उसके थानों में दूध नही रहता था | चरवाहा इस बात को देख कर कुछ दिन हैरान रहा | उसके बाद इसकी जांच करने का निश्चय किया कि इस गाय का दूध कौन निकाल लेता है | यह सोच कर दुसरे दिन उसने जंगल में चरते समय उस गाय का पीछा किया | तो उसने देखा की गाय एक टीले पर जाकर झाड़ियों के बीच में खड़ी हुई तथा उस टीले पर दिखाई दे रहे एक पत्थर पर गाय के थनों से दूध निकल कर बहने लगा|
जैसे वह गाय उस दूध से उस पत्थर का अभिषेक कर रही हो | उस दृश्य को देखकर चरवाहा अत्यतेंन आश्चर्य-चकित हुआ एवं उसने अपने साथियों को बुला कर यह दृश्य दिखाया | उन सबने यह दृश्य देख कर उस पत्थर को निकलना चाह किन्तु जितना वो खोदते उतना ही वो पत्थर गहरा होता जाता था | अंत में उस पत्थर को उसी स्थान पर छोड़ दिया गया एवं सभी अपने-अपने घर को आ गए | रात्री में उस चरवाहे को माँ ने स्वप्न में बताया कि मैं जगतजननी जगदम्बा हूँ| तथा वह मेरा ही स्थान है | वहां पर जो कोई भी हलुआ-पूड़ी का मुझे भोग लगाएगा उसकी सभी अभिलाषाओं की मैं पूर्ति करुँगी |
When Shivaji Maharaj met Bundelkhand Kesri Chatrsaal
When Shivaji Maharaj met Bundelkhand Kesri Chatrsaal
The meeting is a monumental event in India’s history. It laid the foundations of Hindu rule in Bundelkhand – a pivotal and strategically very important province.
The content of what Maharaja Chhatrasal said to Shivaji is brought out beautifully by Lal Kavi (actual name Gorelal Purohit) in Chhatraprakash.
Chhatrasal Bundela said
पिता हमारे सुबा दोडे I तुर्कन पर अजमेय खांडे I
तिन चम्पती के नंद हम, ससि नववाई काहि I
हम भूले सियो वृथा, हितु जानी कै वाहि I
एड एक शिवराज निबाही I करे अपने चित कि चाही I
आठ पातशाही झुक झोरे, सुबनी बांधी डआंड ले छओरे I
ऐसे गुण सिवराज के I बसे चित में आई I
मिलिवोई मन में धन्यो I मनसी मत जो बनाई I
Loosely translated it means: “My father (Champat Rai) ravaged the province and rose against the Turks (Mughals). But his three sons have not been able to live up to his ideals. Only Shivaji has been able to follow what is correct and do what his heart says. Eight rulers have been defeated by him.
“I am much inspired by these deeds of Shivaji. Hence I want to meet Shivaji and obey whatever is asked of him.”
Chhatrasal Bundela intended to join the growing armies of Chhatrapati Shivaji, but Shivaji gave a beautiful reply, in which he tried to stir Chhatrasal’s patriotic feelings for the liberation of his own Bundelkhand from tyrannical Mughal rule. He wanted Chhatrasal Bundela to free and work for the prosperity of his rayat in Bundelkhand, rather than just be a sardar in the Maratha army in the Deccan.
Shivaji’s reply is also found in Lal Kavi’s Chhatraprakash –
सिवा किसा सुनि कैकही तुमि छत्री सिरताज I
जीत अपनी भूम को, करो देश को राज I
करो देश को राज छतोरे, हम तुमतै कबहुं नाही न्यारे I
दैरी देस मुगलानको मारो, दबटी दिली के दल संहारौ I
तुरकन की परतीत न मानो I तुम केहार तुरकन गज जानो I
तुरकन में ना विवेक विलोक्यो I मिलन गये उन्हे तुम रोकयो I
Translation: Chhatrasal, you are like the crown jewel of kshatriyas. You should fight and win back your lands and rule over them. I am not different than you. Fight and defeat the Mughals. Make their armies run away. Do not trust the Turkis (Mughals). You are a lion, and the Turks are elephants. They are untrustworthy, you go to meet them, they will put hurdles in front.
Thus, inspired by Chhatrapati Shivaji, Maharaja Chhatrasal Bundela returned to his Bundelkhand. Then began the long struggle to liberate Bundelkhand from the despotic rule of the Mughals. It is said that Chhatrapati Shivaji also granted Maharaja Chhatrasal Bundela, a sword.
Dudhai Varhaavtaar – An Unknown Gem from Chandela
"During the end of twelfth century and start of thirteenth century, two brothers Devpat and Khovpat were residing at Devgadh. As per legends, they had access to the philosopher’s stone (paras mani), which made them very rich. They constructed various temples in and around Devgadh, including Dudhai. As per a legend, the Badi and Choti Barat temples at Dudhai were constructed by them. The old name of Dudhai was Maholi (as mentioned in “Bharat ke Digambar Jain Tirth”) & Dugdhakupya (as mentioned in “Epigraphia Indica vol I, page 214”)"
- Ruchira Shrivastava
The definitive history of the town can be traced from the Mughal period when it attained certain importance. Abul Fazl mentions that Lalitpur and Dudhai were parganas under the Chanderi Sarkar which in turn was one of the Sarkar under the Malwa suba. The first scholarly reference of Dudhai comes from Alexander Cunningham in his survey reports. He visited the town in 1874-75 and described its monuments in details. He tells that the village was situated on the ridge to the north of the Ram Sagar, a large artificial lake. He further tells that with construction of roads connecting with other villages, the people of Dudhai who earlier emigrated had started to return. He also touched upon the legends and traditions on the history of the place. The next reference is from A Fuhrer however he merely repeated what was mentioned in Cunningham’s reports. In 1889, Keilhorn, in Indian Antiquary vol. XVIIII, edited the inscriptions at a temple in Dudhai. However he remained silent on the monuments of the place. 1889 also sees an attempt from P C Mukherji who described the antiquities of Lalitpur in great details. This was an important work from the scholar as it contained a good number of plates providing plans and sketchings of the monuments and ruins. The Imperial Gazetteer of India for United Provinces of Agra and Oudh, prepared in 1905, refers Dudhai as a ruined town standing on the bank of an artificial tank. The same position is taken in the Jhansi Gazetteer, prepared in 1909, where Dudhai is referred as a decayed village. The Gazetteer of the North-Western Provinces ascribed these monuments to the ancient Gonds however the people were unanimous in referring them to Raja Jalandhar Chandel.
The ASI (Archaeological Survey of India) website mentions thirteen protected monuments at Dudhai village. These can be put into three different regions around the village. The first region is where we find larger and lesser Surang with few other temples including Jain temples. The second region is where rock-cut Narasimha is found and the third region is where are found Bania ki Barat and few other ruins. Larger and Lesser Surang
Lesser Surang (Choti Sarai) – It is called lesser surang as its spire does not reach very high in comparison to the other temple, known as larger surang. However in plan and dimensions, it would be a larger temple than the latter. Cunningham mentions that this was a Brahma temple however it is a tri-kuta (triple shrines) temple consisting of three cells, dedicated to Brahma, Shiva and Vishnu. Only two cells have survived, the one dedicated to Vishnu is no more intact. The temple would have been dedicated to Shiva in most probability as evident from its design and orientation.
Larger Surang (Badi Sarai) – This temple is built on a jagati (platform) and is a twin temple consisting of two back to back shrines. These shrines face opposite directions, east and west. Both these shrines share a common tower which is now in very bad state of preservation. The temple can be entered through its two entrances, from east and west. The temple is consisted of a mandapa, maha-mandapa and garbha-grhas.
Lintel of Shiva Cell
Shiva The three cells (garbha-grhas) were connected to a common mandapa, roof of which has not survived the toll of time. There is no antarala (vestibule) in front of these cells as these all open directly to the common mandapa. The lintel of the garbha-grha doorways are adorned with various images including Nava-grhas (nine planets) and Sapta-matrikas (seven mothers) along with the images of dedicatory deity. The lintel of the grabha-grha of Brahma shows Brahma on the lalata-bimba while Gayatri and Savitri on its terminals. The lintel of the Shiva cell shows dancing Shiva at lalata-bimba with Vishnu and Brahma on its terminals.
Lintel of Brahma Cell
Brahma A Shivalinga is placed inside the cell dedicated to Shiva while the cell dedicated to Brahma is empty. There would have been individual towers above three individual cells however only the tower above the Brahma cell has survived but in very bad shape of preservation. The temple would have been raised above a high rising jagati (platform) which was approached through a flight of steps. Six inscriptions are found in this temple and from these it can be fairly stated that the temple was constructed during the Chandela period of first decade of the eleventh century, under the reign of prince Devalabdhi, nephew of the Chandela king Yashoverman.
North-west view The central portion consists of two rooms with a doorway between them, so that there is no back wall against which a statue could be placed. In the absence of any large figure or any other distinguishing feature, it is very hard to determine to whom this elegant temple was dedicated. Also this peculiar plan of back to back shrines is indeed a rare design.
Shiva Temple Linga or Mahadev Temple – Only the garbha-grha of this temple remains now. It houses a Shivalinga inside.
Varaha
Varaha with serpent in front
Varaha Back This large Varaha is installed near the large and lesser Surang. This Varaha is carved on the very similar lines as of the famous Varaha image at Khajuraho. All the body of the animal is carved with multitude of images. Among the other images, we find the dashavatara (ten incarnations) of Vishnu on its back.
Secrets of Bundelkhand - Neelkantheswar Temple Pali
Neelkantheswar Temple Pali
Neelkantheswar, is a famous temple dedicated to Lord Shiva. It is said to be the oldest temple of Lord Shiva near in Pali area of Lalitpur district, about 25 km from Lalitpur.
The idol of Lord Shiva in this temple is unique in that it has three heads, and it is considered to be one and only Avatar of Lord Shiva. Pali .
This temple is situated amid dense forests on a hillock and this place is also famous for betel growing.
The temple dates back to the Chandela period, and legend has it that the idol came out in its own from the mountain and the temple was built around it.
A very huge fair (mela) is held here every year during the Maha Shivratri festival. A procession of devotees can be witnessed on this day.
यहाँ के राजा आज भी भगवन श्री राम चंद्र हैं
ओरछा का राज न सिर्फ राम के नाम पर चलता है, बल्कि मंदिर में विराजे राम सरकारी गार्ड आफ ऑनर के साथ ही जागते-सोते हैं.
'दिवस ओरछा रहत हैं, रेन अयोध्या बास'. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में जन्में राम देश-दुनिया में भले ही भगवान के रूप में पूजे जाते हैं,लेकिन ओरछा में रियासत काल से ही राम को 'भगवान' के साथ-साथ 'राजा'माना गया है. यही कारण है कि आजादी के बाद से सरकार के सेनानी रोज इन्हें राजा के रूप में चार बार सलामी देते हैं. गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था सरकार ने की है.
यह मिथक है कि ओरछा रियासत काल में रानी कुंवरगनेश अयोध्या से भगवान राम को पुत्र की भांति ओरछा लाई थीं. यहां उन्होंने राम को पुत्रवत मान राजतिलक कराया और फिर तभी से मंदिर में विराजे राम भगवान के साथ-साथ राजा के रूप में स्वीकार किए गए.
देश और दुनिया में अकेले ओरछा ही ऐसा मंदिर है, जहां भगवान राम राजा के रूप में मान्य हैं. सरकार ने भी 'भगवान' को 'राजा' माना है. राजा की सुरक्षा और सम्मान में सरकार ने यहां मंदिर में सेनानी तैनात किए हैं. मंदिर के मुख्यद्वार पर पहरेदार के रूप में सेनानी 24 घंटे में चार बार सलामी देता है.
गार्ड ऑफ ऑनर यानी सलामी का वक्त सुबह 8 बजे, दोपहर 12.30 बजे, रात 8 बजे और देर रात 1.00 बजे नियत है. इन चारों वक्त मंदिर में आरती होती है.
मंदिर के पुजारी रमाकांत शरण बताते हैं कि यहां अयोध्या के भगवान राम राजा के रूप में विराजित हैं. वे कहते हैं- "ओरछा में आज भी राम राजा की ही सरकार चलती है."
यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि ओरछा नगरी की सीमा में किसी भी नेता अथवा अधिकारी को सलामी नहीं दी जाती और न ही कोई यहां अपने वाहन पर लगी बत्ती को जलाकर आता है. जून 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ओरछा आईं तो यह सुन कर हतप्रभ रह गईं कि यहां राम को राजा के रुप में मान्यता मिली हुई है, इसलिए यहां राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को सलामी नहीं दी जाती.झाँसी का नाम पहले बलवंत नगर था या शंकर गढ़ या मंजमहल ??????
Untold tales from Mahabharata
The Mahabharat is one of the two major epics in Sanskrit of ancient India. It contains over one lakh couplets and is thrice as long as the Bible. However, only a fraction of the narration actually deals with the main story with the rest containing additional myths and teachings. It clearly states: “what is found here may be found elsewhere but what is not found here cannot be found elsewhere.” Take a look at some untold and unknown stories from this great scripture…
2/25
2
1. The story of five golden arrows
As Kaurawas were losing the battle of Mahabharata, Duryodhana approached Bhisma one night and accused him of not fighting the Mahabharata war to his full strength because of his affection for Pandavas. Bhisma greatly angered, immediately picked up 5 golden arrows and chanted mantras declaring tomorrow he will kill 5 pandavas with the 5 golden arrows. Duryodhana not having faith in his words asked Bhisma to give custody of 5 golden arrows saying that he will keep them and will return them next morning.
3/25
3
A flash back
Long back before the Mahabharata war, Pandavas were living in exile in a forest. Duryodhana placed his camp on the opposite side of the pond where Pandavas were staying. Once while Duryodhana was taking bath in that pond, the heavenly prince Gandharvas also came down. Duryodhana picked a fight with them only to be deafeted and captured. Arjuna saved Duryodhana and set him free. Duryodhana was ashamed but being a Kshatriya, told Arjuna to ask for a boon. Arjuna replied he would ask for the honour gift later when he needed it.
4/25
4
Arjuna asks for his gift
It was during that night of Mahabharata war, when Krishna reminded Arjuna of his unsatisfied boon and told him to go to Duryodhana and ask for 5 golden arrows. When Arjuna asked for the arrows Duryodhana was shocked but being a kshatriya and bound by his promise he had to honour his words. He asked who told you about golden arrows, Arjuna replied who else other than Lord Krishna. Duryodhana again went to Bhisma and requested for another five golden arrows. To this Bhisma laughed and replied that is not possible.
5/25
5
2. The birth of Dronacharya
The birth of Dronacharya, the Guru of the Pandavas and Kauravas in the Mahabharata, is very interesting. It would not be wrong to say that Dronacharya is the first test tube baby in the world. Rishi Bharadwaja is the father of Dronacharya and mother is an Apasara name Krithaji. One evening Rishi Bharadwaja was getting ready to do his evening prayers. He went to the Ganga River to take his usual bath but was amazed to find a beautiful woman bathing at his usual spot in the river.
6/25
6
First test tube baby?
On seeing Rishi Bharadwaja, the beautiful Apsara Krithaji got out of the Ganga River wearing a single loin cloth. Rishi Bharadwaja was moved by the heavenly beauty of the Apsara. Overpowered by the moment, the sage involuntarily emitted his semen. The Rishi collected this sperm in a clay pot and stored it in a dark place in his Ashram. Drona was born in this pot. 'Dronam' means pot and 'Dronar' is one who was born from the pot.
7/25
7
3. Sehdeva ate his father’s brain, literally!
When Pandu, the father of the Pandavas, was about to die, he wished for his sons to partake of his brain so that they inherit his wisdom and knowledge. Only Sahadeva paid heed, though; it is said that with the first bite of his father’s brain, he gained knowledge of all that had happened in the universe. With the second he gained knowledge of the present happenings, and with the third he came to know of all that would occur in the future.
8/25
8
A vow of silence
Sahadeva, often relegated to silence in the story along with his brother Nakul, is known for his prescience. He is said to have known all along that a great war would come to cleanse the land, but he did not announce it lest that would bring it about. As it happened, staying silent about it did not help either.
9/25
9
4. When Duryodhan approached Sahadeva
Sahadeva who had eaten the flesh of his father Pandu after his death could not only see past, and future but also had a great knowledge in Astrology. This is the reason why Shakuni sent Duryodhana to Sahadeva to ask the mahurat (right time) of the Mahabharat War. Sahadeva being honest had disclosed it to Duryodhan in spite knowing the fact that Duryodhan was his real enemy in the battle.
10/25
10
5. Balarama was Abhimanyu’s father–in–law
Abhimanyu ‘s wife Vatsala was the daughter of Balarama. Balarama wanted that Vatsala should marry Laxman, Duryodhana’s son. Abhimanyu and Vatsala both loved each other and wanted to get married. Abhimanyu took the help of his brother Ghatotkacha (a daitya) who tricked Laxman and terrified him. Ghatotkach then flew away with Vatsala and went to his brother Abhimanyu. Laxman was very upset from all this and he vowed that he will not marry throughout his life.
11/25
11
6. The sacrifice of Iravan
Iravan, the son of Arjun and naga princess Uloopi, sacrificed himself to goddess Kali to ensure the victory of his father and his team in the Kurukshetra war. He however, had a last wish – He wanted to marry a girl before he died. Now, getting a girl who knew her husband would die in few days was a tricky task. So, Lord Krishna took the form of Mohini, married Iravan and even wept like a widow after her husband died.
12/25
12
7. Dhritarashtra had a son with his maid servant
Yuyutsu was born to Sauvali, a maid servant who attended Dhritarashtra and looked upon the royal household. Sauvali was not kshatriya but belonged to the Vaishya class. She was appointed to look after Dhritarashtra when Gandhari was declared pregnant. Dhritarashtra was mesmerized by the maid’s charm and used her, both for his physical and sexual gratification. Thus, was born Yuyutsu, the dasi putra of Dhritarashtra.
13/25
13
8. Duryodhana’s dilemmas
Duryodhan is lying in the battle field, awaiting death, badly bruised by the wounds inflicted by Bhima. He kept his three fingers in a raised position and is unable to speak. All the efforts made by his men to understand the meaning proved to be futile. Seeing his plight Krishna approached him and said "I know what issues occupied your mind. I will address them".
14/25
14
Questions and their answers
Krishna identified the issues as - not building a fort around Hastinapur, not persuading Vidur to fight the battle, not making Aswathama the commander-in-chief after the death of Dronacharya. Krishna explained further that if you would have built a fort, I would have asked Nakul to mount the horse and destroy the fort; if you would have succeeded in persuading Vidur to participate in the battle, I would also fought the battle and if Aswathama was made the commander-in-chief, I would have made Yudhistir angry.
15/25
15
Duryodhana could peacefully die
On hearing this Duryodhan closed all the fingers and within seconds he left his body. Many of us do not know that Nakul can drive his horse even in heavy rain without getting wet. He travels with such a speed between a drop and another drop, without getting wet. Only Nakul can do this among Kaurav and Pandav warriors. It also seems that if Yudhistir gets angry, everything that falls within the range of his eye sight will be burnt.
16/25
16
9. How Udupi fed the Kurukshetra warriors
Five thousand years ago, the Kurukshetra war, between the Pandavas and the Kauravas, was the mother of all battles. All the kings – hundreds of them – aligned themselves on one side or the other. The king of Udupi however chose to remain neutral. He spoke to Krishna and said, ‘Those who fight battles have to eat. I will be the caterer for this battle.’ Many of the Udupi people are caterers even today.
17/25
17
No wastage
The battle lasted 18 days, and every day, thousand soldiers died. So the Udupi king had to cook that much less food, otherwise it would go waste. The amazing thing was that every day, the food was exactly enough for all the soldiers and no food was wasted. After a few days, people were amazed, ‘How is he managing to cook the exact amount of food!’ No one could know how many people had died on any given day.
18/25
18
Krishna’s maya
When someone asked the kind of Udupi, ‘How do you manage this?’ the king replied, ‘Every night I go to Krishna’s tent. Krishna likes to eat boiled groundnuts in the night so I peel them and keep them in a bowl. After he is done I count how many nuts has he eaten. If it’s 10 peanuts, I know tomorrow 10,000 people will be dead. So the next day when I cook lunch, I cook for 10,000 people less.
19/25
19
10. Karna's Last Test
Karna was lying on the battlefield gasping for breath in his last moments. Krishna assumed the form of an indigent Brahmin and approached him wanting to test his generosity. Krishna exclaimed: "Karna! Karna!" Karna asked him: "Who are you, Sir?" Krishna (as the poor Brahmin) replied: "For a long time I have been hearing about your reputation as a charitable person. Today I came to ask you for a gift." "Certainly, I shall give you whatever you want", replied Karna.
20/25
20
Krishna asks for gold
"I want a small quantity of gold", said Krishna. Karna opened his mouth, showed the gold fillings for his teeth and said: "I shall give this to you. You can take them". Assuming a tone of revulsion, Krishna said: “Do you expect me to break your teeth and take the gold from them? How can I do such a wicked deed?” Karna picked up a stone, knocked out his teeth and offered them to the "Brahmin".
21/25
21
A step further
Krishna in his guise as Brahmin wanted to test Karna further. "What? Are you giving me as gift teeth dripping with blood? I cannot accept this. I am leaving", he said. Karna pleaded: "Swami, please wait." Even while he was unable to move, Karna took out his arrow and aimed it at the sky. Immediately rain dropped from the clouds. Cleaning the teeth with the rainwater, Karna offered the teeth with both his hands.
22/25
22
Krishna reveals himself
Karna asked: "Who are you, Sir"? Krishna said: "I am Krishna. I admire your spirit of sacrifice. In any circumstance you have never given up your spirit of sacrifice. Ask me what you want." Beholding Krishna's beauteous form, Karna said with folded hands: "Krishna! To have the vision of the Lord before one's passing is the goal of human existence. You came to me and blessed me with your form. This is enough for me. I offer my salutations to you."
23/25
23
11. A tale of true friendship
Once Duryodhana's wife Bhanumathi and Karna were playing a game of dice. As the game progressed, it was evident that Karna was winning and Bhanumathi was losing. Just then Duryodhana entered his queen's chamber. Karna had his back to the door while Bhanumathi was facing it. Seeing her husband coming, she was about to stand up. As she was just rising, Karna, thinking that she was trying to get away, snatched at her drape, studded with pearls.
24/25
24
The thread snapped
Tugged at by Karna's powerful hands, the thread snapped and all the pearls rolled on the floor. Queen Bhanumathi was stunned and did not know what to say or do. She was afraid that, for no fault of hers, she would be misunderstood by her husband because of Karna's offensive and insensitive behavior. Seeing her shocked state and sensing that something was wrong, Karna turned round and saw his friend Duryodhana. He was also deeply shocked and distressed beyond words.
25
A strong bond
Here he was, in the royal chamber, playing a game of dice with his friend's wife and, as if this was not enough, he had the audacity to catch her clothes, thus embarrassing and endangering her chaste reputation. He stood dumbfounded and transfixed. As both Bhanumathi and Karna look down sheepishly, unable to meet Duryodhana's eyes, the Kaurava scion only asks, "Should I just collect the beads, or string them as well."
Bundelkhand Kesri Chatrsal - महाराजा छत्रसाल
‘‘इत जमना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस।
छत्रसाल से लरन की रही न काह होंस।’’
मध्यकालीन भारत में विदेशी आतताइयों से सतत संघर्ष करने वालों में छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और बुंदेल केसरी छत्रसाल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, परंतु जिन्हें उत्तराधिकार में सत्ता नहीं वरन ‘शत्रु और संघर्ष’ ही विरासत में मिले हों, ऐसे बुंदेल केसरी छत्रसाल ने वस्तुतः अपने पूरे जीवनभर स्वतंत्रता और सृजन के लिए ही सतत संघर्ष किया। उन्होंने विस्तृत बुंदेलखंड राज्य की गरिमामय स्थापना ही नहीं की थी, वरन साहित्य सृजन कर जीवंत काव्य भी रचे। छत्रसाल ने अपने 82 वर्ष के जीवन और 44 वर्षीय राज्यकाल में 52 युद्ध किये थे। शौर्य और सृजन की ऐसी उपलब्धि बेमिसाल है वीरों और हीरोंवाली माटी के इस लाड़ले सपूत ने कलम और करवाल को एक-सी गरिमा प्रदान की थी। मूल ऊर्जा का केंद्रः ओरछा बुंदेलखंड में सन 1531 से गढ़ कुंडार के उतरांत ओरछा ही राज्य के रूप में मूल ऊर्जा केंद्र रहा है। हेमकर्ण की वंश परंपरा में सन 1501 में ओरछा में रुद्रप्रताप सिंह राज्यारूढ़ हुए, जिनके पुत्रों में ज्येष्ठ भारतीचंद्र 1539 में ओरछज्ञ के राजा बने तब बंटवारे में राव उदयजीत सिंह को महेबा (महोबा नहीं) का जागीरदार बनाया गया, इन्ही की वंश परंपरा में चंपतराय महेबा गद्दी पर जिन परिस्थितियों में आसीन हुए उसके बारे में लाल कवि ने ‘छत्रप्रकाश’ में कहा है-‘‘प्रलय पयोधि उमंग में ज्यों गोकुल जदुदाय त्यों बूड़त बुंदेल कुल राख्यों चंपतराय।’’
किंतु पूरे जीवनभर विदेशी मुगलों से संघर्ष करते हुए इस रणबांकुरे बुंदेला को अपने ही विश्वासघातियों के कारण सन 1661 में अपनी वीरांगना रानी लालकुंआरि के साथ आत्माहुति देनी पड़ी।
छत्रसाल के पिता चंपतराय जब मुग़ल सेना से घिर गये तो उन्होंने अपनी पत्नी 'रानी लाल कुंवरि' के साथ अपनी ही कटार से प्राण त्याग दिये, किंतु मुग़लों को स्वीकार नहीं किया। छत्रसाल उस समय चौदह वर्ष की आयु के थे। अपने बड़े भाई 'अंगद राय' के साथ वह कुछ दिनों मामा के घर रहे, किंतु उनके मन में सदैव मुग़लों से बदला लेकर पितृ ऋण से मुक्त होने की अभिलाषा थी। बालक छत्रसाल मामा के यहाँ रहता हुआ अस्त्र-शस्त्रों का संचालन और युद्ध कला में पारंगत होता रहा।
दस वर्ष की अवस्था तक छत्रसाल कुशल सैनिक बन गए थे। अंगद राय ने जब सैनिक बनकर राजा जयसिंह के यहाँ कार्य करना चाहा तो छोटे भाई छत्रसाल को यह सहन नहीं हुआ। छत्रसाल ने अपनी माता के कुछ गहने बेचकर एक छोटी सा सैनिक दल तैयार करने का विचार किया। छोटी सी पूंजी से उन्होंने 30 घुड़सवार और 347 पैदल सैनिकों का एक दल बनाया और मुग़लों पर आक्रमण करने की तैयारी की। 22 वर्ष की आयु में छत्रसाल युद्ध भूमि में कूद पड़े।
'बुंदेलखंड के शिवाजी' के नाम से प्रख्यात छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल 3 संवत 1706 विक्रमी तदनुसार दिनांक 17 जून, 1648 ईस्वी को एक पहाड़ी ग्राम में हुआ था। अपने पराक्रमी पिता चंपतराय की मृत्यु के समय वे मात्र 12 वर्ष के ही थे। वनभूमि की गोद में जन्में, वनदेवों की छाया में पले, वनराज से इस वीर का उद्गम ही तोप, तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ। पांच वर्ष में ही इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु अपने मामा साहेबसिंह धंधेर के पास देलवारा भेज दिया गया था। माता-पिता के निधन के कुछ समय पश्चात ही वे बड़े भाई अंगद राय के साथ देवगढ़ चले गये। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए छत्रसाल ने पंवार वंश की कन्या देवकुंअरि से विवाह किया।
जिसने आंख खोलते ही सत्ता संपन्न दुश्मनों के कारण अपनी पारंपरिक जागीर छिनी पायी हो, निकटतम स्वजनों के विश्वासघात के कारण जिसके बहादुर मां-बाप ने आत्महत्या की हो, जिसके पास कोई सैन्य बल अथवा धनबल भी न हो, ऐसे 12-13 वर्षीय बालक की मनोदशा की क्या आप कल्पना कर सकते हैं? परंतु उसके पास था बुंदेली शौर्य का संस्कार, बहादुर मां-माप का अदम्य साहस और ‘वीर वसुंधरा’ की गहरा आत्मविश्वास। इसलिए वह टूटा नहीं, डूबा नहीं, आत्मघात नहीं किया वरन् एक रास्ता निकाला। उसने अपने भाई के साथ पिता के दोस्त राजा जयसिंह के पास पहुंचकर सेना में भरती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया।
राजा जयसिंह तो दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य कर रहे थे अतः औंरगजेब ने जब उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा तो छत्रसाल को इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर मिला। मइ्र 1665 में बीजापुर युद्ध में असाधारण वीरता छत्रसाल ने दिखायी और देवगढ़ (छिंदवाड़ा) के गोंडा राजा को पराजित करने में तो छत्रसाल ने जी-जान लगा दिया। इस सीमा तक कि यदि उनका घोड़ा, जिसे बाद में ‘भलेभाई’ के नाम से विभूषित किया गयाउनकी रक्षा न करता तो छत्रसाल शायद जीवित न बचते पर इतने पर भी जब विजयश्री का सेहरा उनके सिर पर न बांध मुगल भाई-भतीजेवाद में बंट गया तो छत्रसाल का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने मुगलों की बदनीयती समझ दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी।
इन दिनों राष्ट्रीयता के आकाश पर छत्रपति का सितारा चमचमा रहा था। छत्रसाल दुखी तो थे ही, उन्होंने शिवाजी से मिलना ही इन परिस्थितियों में उचित समझा और सन 1668 में दोनों राष्ट्रवीरों की जब भेंट हुई तो शिवाजी ने छत्रसाल को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियेां का आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना की मंत्रणा दी एवं समर्थ गुरु रामदास के आशीषों सहित ‘भवानी’ तलवार भेंट की-
करो देस के राज छतारे हम तुम तें कबहूं नहीं न्यारे। दौर देस मुगलन को मारो दपटि दिली के दल संहारो। तुम हो महावीर मरदाने करि हो भूमि भोग हम जाने। जो इतही तुमको हम राखें तो सब सुयस हमारे भाषे।
छत्रसाल बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने ऐसे लोगों को पहले हटाया जो मुग़लों की मदद कर रहे थे।
शिवाजी से स्वराज का मंत्र लेकर सन 1670 में छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि लौट आयी परंतु तत्कालीन बुंदेल भूमि की स्थितियां बिलकुल मिन्न थीं। अधिकाश रियासतदार मुगलों के मनसबदार थे, छत्रसाल के भाई-बंधु भी दिल्ली से भिड़ने को तैयार नहीं थे। स्वयं उनके हाथ में धन-संपत्ति कुछ था नहीं। दतिया नरेश शुभकरण ने छत्रसाल का सम्मान तो किया पर बादशाह से बैर न करने की ही सलाह दी।
ओरछेश सुजान सिंह ने अभिषेक तो किया पर संघर्ष से अलग रहे। छत्रसाल के बड़े भाई रतनशाह ने साथ देना स्वीकार नहीं किया तब छत्रसाल ने राजाओं के बजाय जनोन्मुखी होकर अपना कार्य प्रारंभ किया। कहते हैं उनके बचपन के साथी महाबली तेली ने उनकी धरोहर, थोड़ी-सी पैत्रिक संपत्ति के रूप में वापस की जिससे छत्रसाल ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी-सी सेना तैयार कर ज्येष्ठ सुदी पंचमी रविवार वि.सं. 1728 (सन 1671) के शुभ मुहूर्त में शहंशाह आलम औरंगजेब के विरूद्ध विद्रोह का बिगुल बजाते हुए स्वराज्य स्थापना का बीड़ा उठाया। छत्रसाल की प्रारंभिक सेना में राजे-रजवाड़े नहीं थे अपितु तेली बारी, मुसलमान, मनिहार आदि जातियों से आनेवाले सेनानी ही शामिल हुए थे। चचेरे भाई बलदीवान अवश्य उनके साथ थे। छत्रसाल का पहला आक्रमण हुआ अपने माता-पिता के साथ विश्वासघात करने वाले सेहरा के धंधेरों पर। मुगल मातहत कुंअरसिंह को ही कैद नहीं किया गया बल्कि उसकी मदद को आये हाशिम खां की धुनाई की गयी और सिरोंज एवं तिबरा लूट डाले गये। लूट की सारी संपत्ति छत्रसाल ने अपने सैनिकों में बांटकर पूरे क्षेत्र के लोगों को उनकी सेना में सम्मिलित होने के लिए आकर्षित किया। कुछ ही समय में छत्रसाल की सेना में भारी वृद्धि होने लगी और उन्हेांने धमोनी, मेहर, बांसा और पवाया आदि जीतकर कब्जे में कर लिए।
ग्वालियर-खजाना लूटकर सूबेदार मुनव्वर खां की सेना को पराजित किया, बाद में नरवर भी जीता। सन 1671 में ही कुलगुरु नरहरि दास ने भी विजय का आशीष छत्रसाल को दिया। ग्वालियर की लूट से छत्रसाल को सवा करोड़ रुपये प्राप्त हुए पर औरंगजेब इससे छत्रसाल पर टूट-सा पड़ा। उसने सेनपति रणदूल्हा के नेतृत्व में आठ सवारों सहित तीस हजारी सेना भेजकर गढ़ाकोटा के पास छत्रसाल पर धावा बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ पर दणदूल्हा (रुहल्ला खां) न केवल पराजित हुआ वरन भरपूर युद्ध सामग्री छोड़कर जन बचाकर उसे भागना पड़ा। इस विजय से छत्रसाल के हौसले काफी बुलंद हो गये।
सन 1671-80 की अवधि में छत्रसाल ने चित्रकूट से लेकर ग्वालियर तक और कालपी से गढ़ाकोटा तक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। दक्षिण भारत में जो स्थान समर्थगुरु रामदास का है वही स्थान बुन्देलखंड में 'प्राणनाथ' का रहा है, जिस प्रकार समर्थ गुरु रामदास के कुशल निर्देशन में छत्रपति शिवाजी ने अपने पौरुष, पराक्रम और चातुर्य से मुग़लों के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक उसी प्रकार गुरु प्राणनाथ के मार्गदर्शन में छत्रसाल ने अपनी वीरता से, चातुर्यपूर्ण रणनीति से और कौशल से विदेशियों को परास्त किया था। प्राणनाथ छत्रसाल के मार्ग दर्शक, अध्यात्मिक गुरु और विचारक थे।
सन 1675 में छत्रसाल की भेंट प्रणामी पंथ के प्रणेता संत प्राणनाथ से हुई जिन्होंने छत्रसाल को आशीर्वाद दिया-
छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होय जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होय। इसी अवधि में छत्रसाल ने पन्ना के गौड़ राजा को हराकर, उसे अपनी राजधानी बनाया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1744 की गोधूलि बेला में स्वामी प्राणनाथ ने विधिवत छत्रसाल का पन्ना में राज्यभिषेक किया। विजय यात्रा के दूसरे सोपान में छत्रसाल ने अपनी रणपताका लहराते हुए सागर, दमोह, एरछ, जलापुर, मोदेहा, भुस्करा, महोबा, राठ, पनवाड़ी, अजनेर, कालपी और विदिशा का किला जीत डाला। आतंक के मारे अनेक मुगल फौजदार स्वयं ही छत्रसाल को चैथ देने लगे। बघेलखंड, मालवा, राजस्थान और पंजाब तक छत्रसाल ने युद्ध जीते। परिणामतः यमुना, चंबल, नर्मदा और टोंस मे क्षेत्र में बुंदेला राज्य स्थापित हो गया। सन 1707 में औरंगजेब का निध्न हो गया। उसके पुत्र आजम ने बराबरी से व्यवहार कर सूबेदारी देनी चाही पर छत्रसाल ने संप्रभु राज्य के आगे यह अस्वीकार कर दी। महाराज छत्रसाल पर इलाहाबाद के नवाब मुहम्मद बंगस का ऐतिहासिक आक्रमण हुआ। इस समय छत्रसाल लगभग 80 वर्ष के वृद्ध हो चले थे और उनके दोनों पुत्रों में अनबन थी। जैतपुर में छत्रसाल पराजित हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में उन्हेांने बाजीराव पेशवा को पुराना संदर्भ देते हुए सौ छंदों का एक काव्यात्मक पत्र भेजा जिसकी दो पंक्तियां थीं
"जो गति गज और ग्राह की सो गति भई है आज बाजी जात बुन्देल की राखौ बाजी लाज।"
फलतः बाजीराव की सेना आने पर बंगश की पराजय ही नहीं हुई वरन उसे प्राण बचाकर अपमानित हो, भागना पड़ा। छत्रसाल युद्ध में टूट चले थे, लेकिन मराठों के सहयोग से उन्हेांने कलंक का टीका सम्मान से पोंछ डाला। यहीं कारण था छत्रसाल ने अपने अंतिम समय में जब राज्य का बंटवारा किया तो बाजीराव को तीसरा पुत्र मानते हुए बुंदेलखंड झांसी, सागर, गुरसराय, काल्पी, गरौठा, गुना, सिरोंज और हटा आदि हिस्से के साथ राजनर्तकी मस्तानी भी उपहार में दी।
कतिपय इतिहासकार इसे एक संधि के अनुसार दिया हुआ बताते हैं पर जो भी हो अपनी ही माटी के दो वंशों, मराठों और बुंदेलों ने बाहरी शक्ति को पराजित करने में जो एकता दिखायी, वह अनुकरणीय है। छत्रसाल ने अपने दोनों पुत्रों ज्येष्ठ जगतराज और कनिष्ठ हिरदेशाह को बराबरी का हिस्सा, जनता को समृद्धि और शांति से राज्य-संचालन हेतु बांटकर अपनी विदा वेला का दायित्व निभाया।
4 अप्रैल 1729 को छत्रसाल ने विजय उत्सव मनाया। इस विजयोत्सव में बाजीराव का अभिनन्दन किया गया और बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र स्वीकार कर अपने राज्य का तीसरा भाग बाजीराव पेशवा को सौंप दिया। प्रथम पुत्र हृदयशाह पन्ना, मऊ, गढ़कोटा, कालिंजर, एरिछ, धामोनी इलाका के ज़मींदार हो गये जिसकी आमदनी 42 लाख रू. थी। दूसरे पुत्र जगतराय को जैतपुर, अजयगढ़, चरखारी, नांदा, सरिला, इलाका सौपा गया जिसकी आय 36 लाख थी। बाजीराव पेशवा को काल्पी, जालौन, गुरसराय, गुना, हटा, सागर, हृदय नगर मिलाकर 33 लाख आय की जागीर सौपी गयी। छत्रसाल का राज्य प्रसिद्ध चंदेल महाराजा कीर्तिवर्धन से बड़ा था। छत्रसाल तलवार के धनी थे और कुशल शस्त्र संचालक भी थे। वह शस्त्रों का आदर करते थे। वह अपनी सभा में विद्वानों को सम्मानित करते थे। वह स्वयं भी बहुत विद्वान् थे। वह कवि थे, शांति के समय में कविता करना छत्रसाल का प्रिय कार्य रहा है। शौर्य और सृजन की ऐसी उपलब्धि बेमिसाल है
राज्य संचालन के बारे में उनका सूत्र उनके ही शब्दों मेंः राजी सब रैयत रहे, ताजी रहे सिपाहि छत्रसाल ता राज को, बार न बांको जाहि।
यही कारण था कि छत्रसाल को अपने अंतिम दिनों में वृहद राज्य के सुप्रशासन से एक करोड़ आठ लाख रुपये की आय होती थी। उनके एक पत्र से स्वष्ट होता है कि उन्होंने अंतिम समय 14 करोड़ रुपये राज्य के खजाने में (तब) शेष छोड़े थे। प्रतापी छत्रसाल ने पौष शुक्ल तृतीया भृगुवार संवत् 1788 (दिसंबर 1731) को छतरपुर (नौ गांव) के निकट मऊ सहानिया के छुवेला ताल पर अपना शरीर त्यागा और विंध्य की अपत्यिका में भारतीय आकाश पर सदा-सदा के लिए जगमगाते सितारे बन गये। छत्रसाल की तलवार जितनी धारदार थी, कलम भी उतनी ही तीक्ष्ण थी। वे स्वयं कवि तो थे ही कवियों का श्रेष्ठतम सम्मान भी करते थे। अद्वितीय उदाहरण है कि कवि भूषण के बुंदेलखंड में आने पर आगवानी में जब छत्रसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा लगा दिया तो भूषण कह उठेः
और राव राजा एक चित्र में न ल्याऊं- अब, साटू कौं सराहौं, के सराहौं छत्रसाल को।।
The Temples of Bundelkhand - Neelkanth Temple
The Temples of Bundelkhand - Neelkanth Temple
One whose Throat is Blue
I bow to Nilakantha [who has] ten arms, three eyes,
is sky-clad [and] lord of the directions,
dark-eyed and adorned by/with poison.
— Translated by Rohini Bakshi
One of the most famous legends, which has been described in the Bhagavata Purana, the Mahabharata, and the Vishnu Purana, is that of samudra manthan, or churning of the ocean. It is about the time when the gods and demons fought and the demons often got the upper hand. On being appealed to, Lord Vishnu advised the gods to solve the problem diplomatically, which resulted in an alliance between the gods and demons to churn the sea of milk for the nectar of immortality, which they would divide equally between them.
Lord Vishnu assured the gods that he would ensure that they alone got the nectar of immortality. During the churning, many objects came up. One was the halahala, a pot of potent poison which could destroy everyone. Again, on Lord Vishnu’s advice, the gods approached Lord Shiva, who was the only one capable of swallowing it without being affected. Lord Shiva swallowed the poison while his consort Goddess Parvati, it is said, held his neck to prevent it from going into his stomach. The poison turned his throat blue, which is why he’s called Neelkanth, or the one with a blue throat. Though the poison didn’t harm him, Lord Shiva’s throat was burning and he came to earth to rest.
According to legend, that place was Kalinjar where the Chandela rulers, who were Shiva bhakts, built in the 10th century a magnificent Neelkanth temple. The Chandela rulers of Bundelkhand also built the Kalinjar fort, which lives up to its name, ‘The destroyer of time’, between the 9th and 13th centuries. It is one of the few forts that stood against the invasions of Mahmud of Ghazni. It lies on a hilly plateau, 1,203 ft above the plains in the Vindhya range.
The entrance to the fort and the palaces inside are impressive, but it was Neelkanth temple that took my breath away. It was the best part of my trip to Bundelkhand. From the top, the 165 steps that lead down to it in a long and winding route look daunting, but don’t let that deter you. It’s worth every bit of the effort.
Though the scenery accompanying the journey down the steps is enough to refresh tired feet, it was the first sight of the Grecian altar-looking 16-pillared yagna mandap from the top that was enough to give us a sense of purpose. We continued with renewed vigour. The mandap, which is said to have once been covered, now stands under the open sky as a testimony to time.
There are carvings and statues on the rocks all along the route. At the museum of Kalinjar fort, the Archaeological Survey of India officer said that out of the 874 specimens of sculpture they had there, most were found during excavations of the temple. I can well believe him after seeing the riches there. A door leads to the village. On the way, an adorable Ganesha statue keeps guard. On the rock, just a little way above the mandap, are spectacular statues of Chamundi Devi. Behind the mandap is a small shrine cut into the rock itself, with a tall Shivling installed in it. The unique feature of the Shivling is that it is always wet near the throat portion, even if there is a drought or famine in this area.
The door of the cave is a massive stone shutter-like thing, which the pujari told me used to move, but they no longer know the secret lever. To the right of the temple, a few steps down, is the most amazing statue of Kal Bhairav (incarnation of Lord Shiva) carved in the rocks. This is easy to miss as most people return from the mandap area. It is 24 ft high, 17 ft wide, has 18 arms, and is garlanded by skulls. The statue is majestic and stunning, and gave us the feel of the power of destiny, for which it is worshipped. Just above the temple is a natural water source that never dries up.
Water continually drips onto the Shivling, keeping the neck moist. Thirty-five steps lead up to the sarovar cut in the mountains behind the temple. It is said that this contains treasure, and there are some indications written on its walls. I don’t know how true this is, for surely someone must have found it if it was material treasure. To my mind, it’s treasure of the spiritual kind, for I felt a great sense of peace here.
नीलकंठ महादेव मन्दिर, कालिंजर
नीलकंठ महादेव मन्दिर, कालिंजर
नीलकंठ महादेव मन्दिर, कालिंजर
- वामन पुराण में कालिंजर को नीलकण्ठ का निवास स्थल माना गया है:
| “ | कालन्जरे नीलकण्ठं सरश्वामनुत्तम॥ हंसयुक्तं महाकोश्यां सर्वपाप प्रणाशनम॥ | ” | ||||||
| ||||||||
कालिंजर किले के पश्चिमी भाग में कालिंजर के अधिष्ठाता देवता नीलकंठ महादेव का एक प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर को जाने के लिए दो द्वारों से होकर जाते हैं। रास्ते में अनेक गुफ़ाएँ तथा चट्टानों को काट कर बनाई शिल्पाकृतियाँ बनायी गई हैं। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह मंडप चंदेल शासकों की अनोखी कृति है। मंदिर के प्रवेशद्वार पर परिमाद्र देव नामक चंदेल शासक रचित शिवस्तुति है व अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मन्दिर के ऊपर ही जल का एक प्राकृतिक स्रोत है, जो कभी सूखता नहीं है। इस स्रोत से शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक तरीके से होता रहता है।
बुन्देलखण्ड का यह क्षेत्र अपने सूखे के कारण भी जाना जाता है, किन्तु कितना भी सूखा पड़े, यह स्रोत कभी नहीं सूखता है। चन्देल शासकों के समय से ही यहाँ की पूजा अर्चना में लीन चन्देल राजपूत जो यहाँ पण्डित का कार्य भी करते हैं, वे बताते हैं कि शिवलिंग पर उकेरे गये भगवान शिव की मूर्ति के कंठ का क्षेत्र स्पर्श करने पर सदा ही मुलायम प्रतीत होता है। यह भागवत पुराण के सागर मंथन के फलस्वरूप निकले हलाहल विष को पीकर, अपने कंठ में रोके रखने वाली कथा के समर्थन में साक्ष्य ही है।
मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग से पसीना भी निकलता रहता है। ऊपरी भाग स्थित जलस्रोत हेतु चट्टानों को काटकर दो कुञ्ड बनाए गए हैं जिन्हें स्वर्गारोहण कुञ्ड कहा जाता है। इसी के नीचे के भाग में चट्टानों को तराशकर बनायी गई काल-भैरव की एक प्रतिमा भी है। इनके अलावा परिसर में सैकड़ों मूर्तियाँ चट्टानों पर उत्कीर्ण की गई हैं।शिवलिंग के समीप ही भगवती पार्वती एवं भैरव की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं।
प्रवेशद्वार के दोनों ही ओर ढेरों देवी-देवताओं की मूर्तियां दीवारों पर तराशी गयी हैं। कई टूटे स्तंभों के परस्पर आयताकार स्थित स्तंभों के अवशेष भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कि इन पर छः मंजिला मन्दिर का निर्माण किया गया था। इसके अलावा भी यहाँ ढेरों पाषाण शिल्प के नमूने हैं, जो कालक्षय के कारण जीर्णावस्था में हैं।
कालिंजर का किला
कालिंजर का उल्लेख अनेक युगों से होता आया है। इसका वर्णन व उल्लेख करने वाले कुछ ग्रन्थ इस प्रकार से हैं:
- ऋगवेद में इसके वर्णन के अनुसार इसे चेदिदेश का अंग माना गया था।
| “ | यथा चिच्चैद्यः कशुः शतमुष्ट्रानां ददत्सहस्रा दश गोनाम् ॥३७॥ यो मे हिरण्यसंदृशो दश राज्ञो अमंहत ।अधस्पदा इच्चैद्यस्य कृष्टयश्चर्मम्ना अभितो जनाः ॥३८॥ | ” |
- विष्णु पुराण में इसका परिक्षेत्र विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियों के अन्तर्गत्त माना गया है:
| “ | महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः॥ विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः ॥ | ” |
- गरुड़ पुराण में कालिंजर के महत्त्व को स्वीकारते हुए इसे महातीर्थ एवं परमतीर्थ की संज्ञा दी गई है।
| “ | गौवर्णं परमं तीर्थ, तीर्थ माहिष्मती पुरी॥ कालंजर महातीर्थ, शुक्रतीर्थ मनुत्तमम्॥ | ” |
- तथा सम्पूर्ण प्रकार के पापों से मुक्त कर मोक्ष दिलाने वाला बताया गया है:
| “ | कृते शोचे मुक्तिदश्च शांर्ग्ङ्गधारीतन्दिके॥ विरजं सर्वदं तीर्थ स्वर्णाक्षंतीर्थमुतमम्॥ | ” |
- वायु पुराण के अनुसार विषपान पश्चात भगवान शिव का कण्ठ नीला पड़ गया और काल को भस्म करने के कारण यहाँ का नाम कालिंजर पड़ गया।
| “ | तत्र कालं जरिष्यामि तथा गिरिवरोत्तमे॥ तेन कालंजरो नाम भविष्यति स पर्वतः॥ | ” |
- वायु पुराण में ही कहा गया है कि जो व्यक्ति कालन्जर में श्राद्ध करता है, उसे पुण्य लाभ होता है।:
| “ | कालन्जरे दशार्णायं नैमिषै कुरुजांगले॥ वाराणस्या तु नगर्या तुदेयं तु यन्ततः॥ | ” |
- कूर्म पुराण में शिव जी के यहाँ काल को जीर्ण करने का उल्लेख है, इसलिये भविष्य में इसका नाम कालंजर होगा।:
| “ | काले महेश निहते लोकनाथः पितामहः। अचायत वरं रुद्रम सजीवो यं भवित्वति॥ इत्थेतत्परम तीर्थ कालंजर मितिशृतम। गत्वाम्यार्च्य महादेवं गाआणपत्यं स विन्द्यति॥ | ” |
- वामन पुराण में कालिंजर को नीलकण्ठ का निवास स्थल माना गया है:
| “ | कालन्जरे नीलकण्ठं सरश्वामनुत्तम॥ हंसयुक्तं महाकोश्यां सर्वपाप प्रणाशनम॥ | ” |
- वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामचन्द्र जी ने एक कुत्ते के कहने पर ब्राह्मण को कालिंजर का कुलपति नियुक्त किया।
| “ | कालन्जरे महाराज कौलपत्य प्रतीप्ताम॥ एतत्छुत्वा तुरामेण कालेपत्यं भिषेचितः॥ | ” |
- महाभारत में वेद व्यास ने इस क्षेत्र को वेदों का ही अंश माना है, व कहा है कि इसकी सीमाएं कुरु, पांचाल, मत्स्य, दशार्ण, आदि से जुड़ी हुई हैं।
| “ | सन्ति रम्याजनपदा वहवन्ना: पारितः कुरुन। पांचालश्च-चेदि-मत्स्याश्च शूरसेनाः पटच्चरा॥११॥ दशार्णा: नवराष्ट्रश्च मल्लः सात्वा, युगन्धराः। कुन्ति राष्ट्र सुविस्तीर्ण सुराष्ट्रावन्त्यस्तथा॥ | ” |
- इनके अलावा भविष्य पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण एवं कालिंजर महात्म्य नामक ग्रन्थों में भी इस क्षेत्र की महिमा का वर्णन है।
कालिञ्जर अर्थात समय का विनाशक – काल: अर्थात समय, एवं जय : अर्थात विनाश। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार सागर मन्थन उपरान्त भगवान शिव ने सागर से उत्पन्न हलाहल विष का पान कर लिया था एवं अपने कण्ठ में ही रोक लिया था, जिससे उनका कण्ठ नीला हो गया था, अतः वे नीलकण्ठ कहलाये।तब वे कालन्जर आये व यहाँ काल पर विजय प्राप्त की। इसी कारण से कालिन्जर स्थित शिव मन्दिर को नीलकंठ भी कहते हैं।तभी से इस पहाड़ी को ही पवित्र तीर्थ माना जाता है।
पद्म पुराण में इस क्षेत्र को नवऊखल यानि सात पवित्र स्थलों में से एक बताया गया है।इसे विश्व का सबसे प्राचीन स्थल बताया गया है। मत्स्य पुराण में इस क्षेत्र को अवन्तिका एवं अमरकंटक के साथ अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। जैन धर्म के ग्रंथों तथा बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में इसे कालगिरि कहा गया है। कालिंजर तीर्थ की महिमा ब्रह्म पुराण (अ.६३) में भी वर्णित है।इस घाटी क्षेत्र को घने वन तथा घास के खुले मैदान, दोनों ही घेरे हुए हैं। यहाँ का प्राकृतिक वैभव इस स्थान को तप करने व ध्यान लगाने जैसे आध्यात्मिक कार्यों के लिये एक आदर्श स्थान बनाता है।
कालिन्जर शब्द (कालञ्जर) प्राचीन पौराणिक हिन्दू ग्रन्थों में उल्लेख तो पाता है, किन्तु इस किले का सही सही उद्गम स्रोत अभी अज्ञात ही है, किन्तु जनश्रुतियों के अनुसार इसकी स्थापना चन्देल वंश के संस्थापक चंद्र वर्मा ने की थी वहीं कुछ इतिहासवेत्ताओं का मानना है कि इसकी स्थापना केदारवर्मन द्बारा द्वितीय-चौथी शताब्दी में करवायी गई थी। एक अन्य मान्यता अनुसार औरंगज़ेब ने इसके कुछ द्वारों का निर्माण कराया था। हिन्दू पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार इस स्थान का नाम सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेतायुग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंहलगढ़ और कलियुग में कालिंजर के नाम से विख्यात रहा है।
१६वीं शताब्दी के फारसी इतिहासवेत्ता फिरिश्ता के अनुसार, कालिन्जर नामक शहर की स्थापना किसी केदार राजा ने ७वीं शताब्दी में की थी। उसमें यह दुर्ग चन्देल शासन से प्रकाश में आया। चन्देल-काल की कथाओं के अनुसार दुर्ग का निर्माण एक चन्देल राजा ने करवाया था।चन्देल शासकों द्वारा कालिन्जराधिपति ("कालिन्जर के अधिपति ") की उपाधि का प्रयोग उनके द्वारा इस दुर्ग को दिये गए महत्त्व को दर्शाता है।
कालिञ्जर, उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बांदा जिले में कलिंजर नगरी में स्थित एक पौराणिक सन्दर्भ वाला, ऐतिहासिक दुर्ग है जो इतिहास में सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा है। यह विश्व धरोहर स्थल प्राचीन मन्दिर नगरी-खजुराहो के निकट ही स्थित है। कलिंजर नगरी का मुख्य महत्त्व विन्ध्य पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर इसी नाम के पर्वत पर स्थित इसी नाम के दुर्ग के कारण भी है। यहाँ का दुर्ग भारत के सबसे विशाल और अपराजेय किलों में एक माना जाता है।
इस पर्वत को हिन्दू धर्म के लोग अत्यंत पवित्र मानते हैं, व भगवान शिव के भक्त यहाँ के मन्दिर में बड़ी संख्या में आते हैं। प्राचीन काल में यह जेजाकभुक्ति (जयशक्ति चन्देल) साम्राज्य के अधीन था। इसके बाद यह दुर्ग यहाँ के कई राजवंशों जैसे चन्देल राजपूतों के अधीन १०वीं शताब्दी तक, तदोपरांत रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा। इन राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमांयू जैसे प्रसिद्ध आक्रांताओं ने आक्रमण किए लेकिन इस पर विजय पाने में असफल रहे।
अनेक प्रयासों के बाद भी आरम्भिक मुगल बादशाह भी कालिंजर के किले को जीत नहीं पाए। अन्तत: मुगल बादशाह अकबर ने इसे जीता व मुगलों से होते हुए यह राजा छत्रसाल के हाथों अन्ततः अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। इस दुर्ग में कई प्राचीन मन्दिर हैं, जिनमें से कई तो गुप्त वंश के तृतीय -५वीं शताब्दी तक के ज्ञात हुए हैं। यहाँ शिल्पकला के बहुत से अद्भुत उदाहरण हैं।
इस दुर्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ढेरों युद्धों एवं आक्रमणों से भरी पड़ी है। विभिन्न राजवंशों के हिन्दू राजाओं तथा मुस्लिम शासकों द्वारा इस दुर्ग पर वर्चस्व प्राप्त करने हेतु बड़े-बड़े आक्रमण हुए हैं, एवं इसी कारण से यह दुर्ग एक शासक से दूसरे के हाथों में चलता चला गया। किन्तु केवल चन्देल शासकों के अलावा,कोई भी राजा इस पर लम्बा शासन नहीं कर पाया।
सतयुग में कालिंजर चेदि नरेश राजा उपरिचरि बसु के अधीन रहा व इसकी राजधानी सूक्तिमति नगरी थी।त्रेता युग में यह कौशल राज्य के अन्तर्गत्त आ गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तब कोसल नरेश राम ने इसे किन्ही कारणों से भरवंशीय ब्राह्मणों को दे दिया था। द्वापर युग में यह पुनः चेदि वंश के अधीन आ गया एवं तब इसका राजा शिशुपाल था। उसके बाद यह मध्य भारत के राजा विराट के अधीन आया। कलियुग में कालिंजर के किले पर सर्वप्रथम उल्लिखित नाम दुष्यंत- शकुंतला के पुत्र भरत का है।
इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार उसने चार किले बनवाए थे जिसमें कालिंजर का सर्वाधिक महत्त्व है। तदोपरांत महात्मा बुद्ध (५६३-४८० ई.पू.) के समय यहाँ चेदि वंश का आधिपत्य रहा। महात्मा बुद्ध की यात्रा के वर्णन में उनके कालिंजर आने का भी उल्लेख है। इसके बाद यह मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गया व विंध्य-आटवीं नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात शुंग वंश तथा कुछ वर्ष पाण्डुवंशियों का आधिपत्य रहा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र का विन्ध्य आटवीं नाम से उल्लेख है। इनके बाद यह वर्धन साम्राज्य के अधीन भी रहा।
गुर्जर प्रतिहारों के शासन में यह उनके अधिकार में आया एवं नागभट्ट द्वितीय के समय तक रहा। तब चन्देल शासक उनहीं के माण्डलिक राजा हुआ करते थे। तब के लगभग हरेक ग्रन्थ या अभिलेखों में कालिन्जर का उल्लेख मिलता है।२४९ ई. में यहाँ हैहय वंशी कृष्णराज का शासन था, एवं चतुर्थ शताब्दी में नागों का अधिकार हुआ, जिन्होंने यहाँ नीलकंठ महादेव का मन्दिर बनवाया। तत्पश्चात सत्ता गुप्त वंश को हस्तांतरित हुई।प्राचीन काल में यह जेजाकभुक्ति (जयशक्ति चन्देल) साम्राज्य के अधीन था।
९वीं से १५वीं शताब्दी तक यहाँ चन्देल शासकों का शासन था। चन्देल राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमांयू ने आक्रमण किए लेकिन जीतने में असफल रहे।[9][3] १०२३ में महमूद गज़नवी ने कालिंजर पर आक्रमण कर यहाँ से लूट का माल ले गया था, किन्तु किले पर अधिकार नहीं किया था। इसके बाद अनेक प्रयासों के बाद भी आरम्भिक मुगल कालिंजर के किले को जीत नहीं पाए।
मुगल आक्रांता बाबर इतिहास में एकमात्र ऐसा सेनाधिपति रहा, जिसने १५२६ में राजा हसन खां मेवातपति से वापस जाते हुए दुर्ग पर आधिपत्य प्राप्त किया किन्तु वह भी उसे रख नहीं पाया। शेरशाह सूरी महान योद्धा था, किन्तु इस दुर्ग का अधिकार वह भी प्राप्त नहीं पर पाया। इसी दुर्ग के अधिकार हेतु चन्देलों से युद्ध करते हुए २२ मई १५४५ में उसकी उक्का नामक आग्नेयास्त्र(तोप) से निकले गोले के दुर्ग की दीवार से टकराकर वापस सूरी पर गिरकर फटने से उसकी मृत्यु हुई थी। अन्तत: बड़े संघर्ष एवं प्रयास के बाद १५६९ में अकबर ने यह दुर्ग जीता और अपने नवरत्नों में एक बीरबल को उपहारस्वरूप प्रदान किया।
बाबर एवं अकबर, आदि के द्वारा किये गए प्रयत्नों के विवरण बाबरनामा, आइने अकबरी, आदि ग्रन्थों में मिलते हैं।बीरबल के बाद यह दुर्ग बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। छत्रसाल के बाद इस किले पर पन्ना के शासक हरदेव शाह ने अधिकार कर लिया। १८१२ ई. में यह दुर्ग अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया।१८५७ के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी कालिंजर दुर्ग की प्रधान भूमिका रही थी। तब इस पर एक छोटी ब्रिटिश टुकड़ी का अधिकार था। १८१२ ई. में ब्रिटिश टुकड़ियां बुन्देलखण्ड पहुंचीं। काफ़ी संघर्ष के उपरान्त उन्हें दुर्ग पर अधिकार मिला। कालिंजर दुर्ग पर ब्रिटिश शासन की अधीनता इसके लिये एक महत्त्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई।
पुराने अभिजात वर्ग के हाथों से निकल कर अब यह नये नौकरशाहों के हाथों में आ गया था, जिन लोगों ने ब्रिटिश प्रशासन को अपनी स्वामिभक्ति के प्रदर्शन करने हेतु इस दुर्ग के कई भागों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। दुर्ग को पहुंचाये गए नुक्सान के चिह्न अभी भी इसकी दीवारों एवं अन्दर के खुले प्रांगण में देखे जा सकते हैं।
दुर्ग एवं इसके नीचे तलहटी में बसा कस्बा, दोनों ही इतिहासकारों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ मन्दिरों के अवशेष, मूर्तियां, शिलालेख एवं गुफ़ाएं, आदि सभी उनके रुचि के साधन हैं। कालिंजर दुर्ग में कोटि तीर्थ के निकट लगभग २० हजार वर्ष पुरानी शंख लिपि स्थित है जिसमें रामायण काल में वनवास के समय भगवान राम के कालिंजर आगमन का भी उल्लेख किया गया है।
इसके अनुसार श्रीराम, सीता कुंड के पास सीता सेज में ठहरे थे। कालिंजर शोध संस्थान के तत्कालीन निदेशक अरविंद छिरौलिया के कथनानुसार इस दुर्ग का विवरण अनेक हिन्दु पौराणिक ग्रन्थों जैसे पद्म पुराण व वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसके अलावा बुड्ढा-बुड्ढी सरोवर व नीलकंठ मंदिर में नौवीं शताब्दी की पांडुलिपियां संचित हैं, जिनमें चंदेल-वंश कालीन समय का वर्णन मिलता है। दुर्ग के प्रथम द्वार में १६वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा लिखवाई गई प्रशस्ति की लिपि भी है।
दुर्ग के समीपस्थ ही काफिर घाटी है। इसमें शेरशाह सूरी के भतीजे इस्लाम शाह की १५४५ई० में लगवायी गई प्रशस्ति भी यहाँ उपस्थित है। इस्लाम शाह ने अपना दिल्ली पर राजतिलक होने के बाद यहाँ के कोटि तीर्थ में बने मन्दिरों को तुड़वाकर उनके सुन्दर नक्काशीदार स्तंभों का प्रयोग यहाँ बनी मस्जिद में किया था। इसी मस्जिद के बगल में एक चबूतरा (ख़ुतबा) बनवाया था, जिसपर बैठकर उसने ये शाही फ़रमान सुनाया था, कि अब से कालिन्जर कोई तीर्थ नहीं रहेगा, एवं मूर्ति-पूजा को हमेशा के लिये निषेध कर दिया था। इसका नाम भी बदल कर शेरशाह की याद में शेरकोह (अर्थात शेर का पर्वत) कर दिया था।
बी डी गुप्ता के अनुसार कालिंजर के यशस्वी राजा व रानी दुर्गावती के पिता कीर्तिवर्मन सहित उनके ७२ सहयोगियों की हत्या भी उसी ने करवायी थी।[3] दुर्ग में ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्व के ढेरों शिलालेख जगह-जगह मिलते हैं, जिनमें से अनेक लेख हजारों वर्ष पूर्व अति प्राचीन काल के भी हैं
कालिंजर दुर्ग विंध्याचल की पहाड़ी पर ७०० फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुर्ग की कुल ऊंचाई १०८ फ़ीट है। इसकी दीवारें चौड़ी और ऊंची हैं। इनकी तुलना चीन की दीवार से की जाये तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। कालिंजर दुर्ग को मध्यकालीन भारत का सर्वोत्तम दुर्ग माना जाता था। इस दुर्ग में स्थापत्य की कई शैलियाँ दिखाई देती हैं, जैसे गुप्त शैली, प्रतिहार शैली, पंचायतन नागर शैली, आदि।प्रतीत होता है कि इसकी संरचना में वास्तुकार ने अग्नि पुराण, बृहद संहिता तथा अन्य वास्तु ग्रन्थों के अनुसार की है।
किले के बीचों-बीच अजय पलका नामक एक झील है जिसके आसपास कई प्राचीन काल के निर्मित मंदिर हैं। यहाँ ऐसे तीन मंदिर हैं जिन्हें अंकगणितीय विधि से बनाया गया है। दुर्ग में प्रवेश के लिए सात दरवाजे हैं और ये सभी दरवाजे में एक दूसरे से भिन्न शैलियों से अलंकृत हैं। यहाँ के स्तंभों एवं दीवारों में कई प्रतिलिपियां बनी हुई हैं, जिनमें मान्यता के अनुसार यहाँ के छुपे हुए खजाने की जगह का रहस्य भी छुपा हुआ है।
इसका उल्लेख करते कुछ मध्यकालीन ग्रन्थ इस प्रकार से हैं: चन्देल काल के अनेक विद्वानों ने इसका वर्णन अनेक ग्रन्थों में किया है, जिनमेम से कुछ प्रमुख हैं: प्रबोध चन्द्रोदय, रूपकषटकम, आल्हखण्ड, आदि।
पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चन्दबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में कालिंजर की प्रशंसा की है। मध्य काल (१६वीं शताब्दी) में यह सुल्तानों के अधीन हो गया। तब की लिखी पुस्तकों में भी इसका उल्लेख मिलता रहा है।
मुगल काल में इसका उल्लेख बाबरनामा एवं आइने अकबरी में आता है। बाद में बुन्देलों के अधिकार में रहा। लाल कवि विरचित छत्रप्रकाश में इसका वर्णन आता है।
यहाँ की भूमि पर बैठकर ही अनेक ऋषियों-मुनियों ने वेदों की ऋचाओं का सृजन किया था। यहीं नारद संहिता, बृहस्पति सूत्र, आदि की रचना हुई। आदि कवि वाल्मीकि ने यहीं वाल्मीकि रामायण का सृजन किया व महाकवि व्यास ने वेदों की रचना, तथा कालांतर में गोस्वामी तुलसीदास ने भी निकट ही रामचरितमानस की रचना भी यहीं की थी।
जगनिक ने आल्हखण्ड ग्रंथ का सृजन किया, चन्देल नरेश गण्ड ने अनेक काव्यों का भावनात्मक सृजन यहीं किया, जिनके द्वारा महमूद गजनवी भी मित्र रूप में परिवर्तित हो गया। महान कवि पद्माकर यहीं थे, व संस्कृत ग्रन्थ प्रबोधचन्द्रोदय के रचयिता भी यहीं हुए थे। कालीदास व बाणभट्ट जैसे साहित्यकार विन्ध्य आटवीं से प्रभावित होकर यहाँ का वर्णन अपने ग्रन्थों में करते रहे। बुन्देलखण्ड के कवि घासीराम व्यास, कृष्णदास ने भी यहाँ के भावनात्मक एवं कलात्मक वर्णन किये हैं।
महाराज छत्रसाल व भी उत्तम कोटि के कवि रहे हैं। उन्होंने व सुप्रसिद्ध लालकवि ने भी यहाँ के उल्लेख अपनी कविताओं के माध्यम से किये हैं। महाकवि भूषण ने इस क्षेत्र का उल्लेख किया है। तत्कालीन सोलंकी राजा ने ही उन्हें भूषण की पद्वी से विभूषित किया था। लिखते हैं:
“दुज कन्नौज कुल कश्यपी, रत्नाकर सुतधीर। बसत त्रिविक्रमपुर सदा, तरनि तनुजा तीर॥
वीर बीरबर से जहाँ, उपजे कवि अरु भूप। देव बिहारीश्वर जहां, विश्वेश्वर तद्रूप॥
कुलकलंक चितकूटपति, साहस शील समुद्र। कवि भूषण पद्वी दई, हृदयराम सुत रुद्र॥”
इनके अलावा प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने रानी दुर्गावती नामक उपन्यास में रानी दुर्गावती को कालिंजर नरेश कीर्तिसिंह की पुत्री बताया है। रानी ने दलपत शाह से प्रेम विवाह किया था व अकबर की सेना से युद्ध करते हुए काम आ गयीं। अब्रिहा नामक ग्रन्थ में जेजाकभुक्ति का उल्लेख मिलता है, जिसकी व्याख्या अंग्रेज़ विद्वान रोनाल्ड ने की है व बताया है कि कालिंजर इसका ही एक भाग था। अरब विद्वान यात्री इब्न बतूता ने यहाँ का भ्रमण किया था व विस्तार से उल्लेख किया है। जैन विद्वानों ने इसे जैन तीर्थ माना है व उसे कल्याण-कटक नाम से बताया है। बौद्ध ग्रन्थों में इसे कंचन पर्वत, कारगीक पर्वत एवं चित्रकूट नाम से लिखा है। टॉलमी के भौगोलिक मानचित्र में प्रसाइके को यमुना नदी के दक्षिण में दिखाया गया है, जिसकी राजधानी कालिंजर बतायी है। तबकात-ए-नासिरी में दिल्ली के सुल्तान अल्तमश के १२३३ ई. में कालिंजर पर आक्रमण के उद्देश्य से बढ़ने के बारे में उल्लेख है। यहाँ का राजा तब डर के भाग गया व इस क्षेत्र को खूब लूटा गया को तत्कालीन हिसाब से २५ लाख से अधिक था।
The Forts of Bundelkhand - Mysterious Kalinjar Fort
He also wrote about ‘Kāliñjara Mahātmya’ in this book. It was then visited by Maisey in 1848 A.D. and he described the antiquities of whole Kāliñjara fort including this temple in detail. After Maisey, Cunningham visited the fort and wrote about the antiquities found in this temple. Later, Fuhrer described the antiquities of this place. Krishna Dev also visited this place. Then in 1976 A.D. Krishna Kumar documented all the antiquities of the fort but did not publish any exclusive account of this temple. After this Sushil Kumar Sullere visited this place and described the antiquities in detail.
The Forts of Bundelkhand - Orcha , First of the Prince of Bundelkhand
Orchha, which is located about 320 km NW of Rewa, has remained obscure for years, hidden as it was beneath a veil of thick vegetation. Located about 15 km NW of Jhansi (Uttar Pradesh), it is a quick drive from the cradle of Rani Lakshmibai.
Even today, it is only beginning to be discovered as an interesting place by the discerning traveller.
Last September (year 2014), we got an opportunity to visit this historical wonder, which is teeming with tales-each worth telling.
Situated on the banks of the beatific Betwa1 river, Orchha is a medieval city steeped in the legacy of the Bundela dynasty. It had the distinction of being the capital of an eponymous princely state-one of the largest and most powerful kingdoms of Central India.
Orchha State (also known as Urchha, Ondchha and Tikamgarh) was a princely state of the Bundelkhand region of British India. It was located within what is now the state of Madhya Pradesh.
Still retaining much of its pristine splendour in the form of enchanting palaces and temples, Orchha was founded in 1501 AD by the Bundela chieftain Rudra Pratap Singh. He moved his capital from Garh Kundar to Orchha city in 1531 and died in the same year.
Rudra Pratap Singh was succeeded by his son, Bharati Chand, who died without leaving an heir in 1554 and was in turn succeeded by his younger brother, Madhukar Shah.
Bharatichand and Madhukar Shah had to face attacks conducted by the Afghan Islam Shah Suri and the Mughal Akbar in the 16th century. Events involving Bharti Chand were recorded by the court poet Keshavdas, and those referring to Madhukar Shah in Akbarnama. Madhukar Shah had to relinquish lands to Akbar in 1577 and 1588. His position had become so precarious in the 1570s that he agreed to Orchha becoming a tributary state and to enlistment of himself and his family in the service of the Mughal Empire. However, another near-contemporary historian-`Abd al-Qadir Bada’uni, records him as a rebel in 1583.
During the reign of the Mughal emperor Jahangir, his vassal, Vir Singh Deo (also written as Bir Singh Deo), was the ruler of the Orchha area. According to historians, Orchha scaled heights of architectural glory during this period, with the construction of the Jahangir Mahal in 1605 and the Sawan Bhadon Mahal.
In the early-17th century, Raja Jhujhar Singh rebelled against the Mughal emperor Shah Jahan, whose armies devastated the state and occupied Orchha from 1635 to 1641. The conquerors installed his brother on the throne. It will be interesting to note that Orchha was the only Bundela state not entirely subjugated by the Marathas in the 18th century.
Tehri, a town about 84 km south of Orchha, became the capital of Orchha state in 1783. Tehri was the site of the fort of Tikamgarh, eventually taking the name of the fort.
In 1811, during the period of Company Rule in India, Orchha became part of theBundelkhand Agency within the Central India Agency.
During the British Raj, Hamir Singh, was elevated to the title of Maharaja in 1865. During his reign the allied forces of Orchha and Datia invaded Jhansi in 1857 with the intention of dividing the Jhansi territory between them. However they were defeated by Rani Lakshmibai’s army and her allies in August 1857.
Maharaja Pratap Singh, who succeeded Hamir Singh in 1874, stressed on the development of the state, himself designing most of the engineering and irrigation works that were executed during his reign.
In 1908, the boundaries of the state lay between 24° 26′ and 25° 40′ North and 78° 26′ and 79° 21′ East, forming an area of 5,400 sq km.
With a 15 gun salute, Orchha was the oldest and highest in rank of all the Bundela states. The state’s maharajas bore the hereditary title First of the Prince of Bundelkhand.
After India’s Independence in 1947, Vir Singh, Pratap Singh’s successor, it acceded the state to the Union of India on 1 January 1950.The district became part of Vindhya Pradesh state, which was merged into the state of Madhya Pradesh in 1956.
Present day Orchha is a charming farming town in the Tikamgarh district of Madhya Pradesh, where the glory of the past ages lives on in its historical sites and temples.

Situated on an island in the Betwa River, the Orchha Fort Complex was the brainchild of Raja Rudra Pratap Singh, who began work on the palace building in 1525 AD; and was completed by his successor Bharti Chand.
The imposing fort complex is divided into several connected buildings which were erected at different times. Significant among these are the Raj Mahal, Jehangir Mahal, and Rai Praveen Mahal.
Situated to the right of the quadrangle, the Raj Mahal is the first palace on entering the complex. It was built in the 17th century by Raja Madhukar Shah. The plain exteriors, crowned by chhatris, give way to interiors with colourful murals, boldly colourful on a variety of religious themes, including this one depicting the Samudra Manthan from Hindu mythology.

Built by Raja Bir Singh Ju Deo in the 17th century to commemorate the visit of Emperor Jehangir to Orchha, the Jehangir Mahal is considered to be a singularly beautiful specimen of Mughal architecture. It will be interesting to mention here that Jehangir’s mother-Jodha-was also a Rajput.

The Jehangir Mahal which offers a breathtaking view of Orchha city, particularly the soaring temple spires and cenotaphs.

Below is a picture of the ‘purva dwaar’ (eastern gate) which overlooks the Betwa river.

Rai Praveen Mahal is a tribute to the poetess and musician-Rai Parveen-the paramour of Raja Indramani (1672- 76). She was sent to the court of the Mughal Emperor who was captivated by her. However, she so impressed the Great Mughal with the purity of her love for Indramani that he sent her back to Orchha.
The Sheesh Mahal (Glass Palace) is another section of the palace which has been converted into a heritage hotel by Madhya Pradesh Tourism Development Corporation.
Orchha is also home to some beautiful places of worship such as the Chaturbhuj Temple, Raja Ram Temple, and Laxminarayan Temple.
Dedicated to the Hindu deity-Vishnu-Chaturbhuj Temple was constructed at the behest of the Queen of Orchha, Ganeshi Bai, during the reign of Raja Madhukar Shah. Termed by some as an ‘almost’ temple, it was specially constructed to enshrine the image of Ram. Legend has it that the Raja Madhukar Shah (1554-92) brought an idol of Ram from Varanasi and housed it in his queen’s palace while the Chaturbhuj Temple was being built. However, when the temple was completed and the time to shift the idol came, it could not be moved. The palace where the idol was placed became the Ram Raja temple where it stands till today, with the Chaturbhuj resembling an empty cathedral.
A blend of religious and secular styles taken from temple and fort architecture, the east facing Chaturbhuj Temple is richly ornamented with lotus symbols.


Painted in subtle hues of pink and yellow, Ram Raja Temple is the centre around which the life of Orchha revolves.

The presiding Deity here is Lord Ram, who is worshipped as a king and not as avatar of Vishnu. A Guard of Honour is held everyday, with police personnel designated as Guards at the temple. It is believed that Lord Ram rules Ayodhya during the day and travels to Orchha at night.
A short walk on a flagstone path from behind the Ram Raja temple leads to the Lakshminarayan Temple.

Unpretentious on the outside, the interiors of this temple are akin to an art gallery, housing intricate murals on a variety of spiritual and secular subjects.


An interesting piece of information, is that the milkcake is the most ubiquitous prasad item in this temple town. Prasad is a devotional offering made to God, usually food which is later shared among devotees.

Visit to the cluster of 14 Chhatris (cenotaphs or memorials to the rulers of Orchha), grouped along the Kanchan Ghat of the river Betwa on the south end of town. Built in Rajput style, the memorials are a blend of Hindu and Mughal style architecture.


Imposing and poignant at the same time, these chhatris imprint a lingering impact on the visitor.
The Son et lumière in the evening at the Raja Mahal is a fascinating experience which provides one an opportunity to relive the pages of history speckled with the rise and fall of mighty kings, riveting romances, and feats of valour.

Places to stay: A highly recommended place to stay in Orchha is The Orhha Resort. It is being single-handedly operated by Mr. Anoop Khullar, former Food and Beverage Head at Taj, Mumbai and now Vice President of Oswal Motels & Resorts Pvt Ltd. At past seventy, this man is a livewire – full of energy, high spirits, positive vibes and sound advice. The Orchha Resort which has been built in heritage style and offers excellent hospitality complete with a bansuri (flute) player et al.
The group has a new venture – The Orchha Palace – a 300 room lavish hotel on 50 acres of land which is coming up nearby and is expected to be completed by 2016.
Another interesting place to stay while in Orchha is the Amar Mahal Hotel which is the brainchild of Brijendra Singh Rathore – former Member of the Legislative Assembly of India and Member of the Vidhan Sabha of Madhya Pradesh Assembly from Prithvipur.
It is a treat to explore the by lanes of this city whose history I now know by heart. Though, I wish the monuments be protected by the Archaeological Survey of India (ASI); currently they are under the aegis of the Madhya Pradesh state tourism department.
______________________________________________________________________________________
- The Betwa or Betravati, is a tributary of the Yamuna river in Northern India. It is also known as Yetravati in Sanskrit. Rising in the Vindhya Range, just north of Hoshangabad in Madhya Pradesh, the Betwa flows north-east through Madhya Pradesh and Orchha to Uttar Pradesh. Almost half of its course, which is not navigable, runs over the Malwa Plateau. The confluence of the Betwa and the Yamuna Rivers is Hamirpur in Uttar Pradesh.
- The word Orchha means ‘hidden’. The region was so named because it was completely hidden amidst dense forests.
- Historians trace the origin of the Bundela dynasty in the 11th century to a Rajput prince who offered himself as a sacrifice to Vindhyavasini-the goddess of the Vindhya Mountains. Pleased with his sense of devotion, she stopped him and named him ‘Bundela’ (one who offered blood). The Bundela dynasty ruled over the area between the Yamuna and Narmada rivers. In the 14th century Sahanpal Bundela, with Parmars and Chauhans, captured Garh Kundar, near Damoh from a Khangar king. When the Tughlaqs, who were ruling Delhi in the 15th century, pushed the Bundelkhand Rajas out of Garh Kundar (the then Bundela capital), they retreated to distant Orchha.
- Prior to Company Rule, the rulers of Orchha all held the title of Raja. They were: Rudra Pratap (1501-1531), Bharatichand (1531-1554), Madhukar Shah (1554-1592), Ram Shah (1592-1605), Vir Singh Deo (also spelled Bir Singh Deo) (1605–1626/7), Jhujhar Singh (1626/7-1635) (brother of Hardaul Singh), Devi Singh (1635-1641) (brother of Jhujhar Singh), Pahar Singh (1641-1653), Sujan Singh (1653-1672), Indramani Singh (1672-1675), Jaswant Singh (1675-1684), Bhagwat Singh (1684-1689), Udwat Singh (1689-1735), Prithvi Singh (1735-1752), Sanwant Singh (1752-1765), Hati Singh (1765–1768), Man Singh (1768–1775), Bharti Singh (1775–1776)
- During the British era, the title of Raja was in use until 1865, when it was replaced with that of Maharaja. The rulers were: Vikramajit Mahendra (1796–1817), Dharam Pal (1817–1834), Taj Singh (1834–1842), Surjain Singh (1842–1848), Hamir Singh (raja 1848-1865; maharaja 1865-1874), Pratap Singh (1874-1930), Vir Singh II (4 March 1930-acceded 1 January 1950)
- Bundelkhand is a geographic region in Central India, now divided between the states of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, with the larger portion lying in the latter.
- Chhatris are elevated, dome-shaped pavilions used as an element in Indian architecture. Chhatris are widely used in palaces and forts, or to demarcate funerary sites. They bear their origins in Rajasthani architecture where they were memorials for kings and royalty. The term ‘chhatri’ means umbrella or canopy.
- A cenotaph is an ‘empty tomb’ or a monument in honour of a person or group of people who are interred elsewhere. It can also be an initial tomb for a person whose remains are reinterred elsewhere. The word is derived from the Greek ‘kenotaphion’ (kenos means ‘being empty’ and taphos means ‘tomb’). Although most cenotaphs are erected in honour of individuals, several noted cenotaphs are dedicated to the memories of groups of individuals, such as the lost soldiers of a country/empire.
- The name Chaturbhuj is derived from the Sanskrit words ‘chatu’ which means four and ‘bhuja’ which means means one who has four arms and refers to Vishnu.
- Ghat is a Hindi word derived from the Sanskrit ‘ghattah’ which means ‘a flight of steps leading down to a river.’
The Secrets of Bundelkhand - Birth Place of Bhakt Prahalad
The Secrets of Bundelkhand - Birth Place of Bhakt Prahalad
Erachh
Bhakt Prahlad was born in Erich and Holika Dehan first took place Erich. The names of a number of rulers of Erich during the post-Maurya period are found from the coins issued by them. They are Sahasamitra, Ishvaramitra, Sahasrasena, Mitrasena, Amitasena The names of a number of rulers of Erich during the post-Maurya period are found from the coins issued by them. They are Sahasamitra, Ishvaramitra, Sahas
Erachh (airach ) The town of Erachh (Jhansi District), with remains of mosques and tombs, seen on the left bank of the river Betwa, which recedes in the middle into the distance. Erich is a town and a nagar panchayat in Jhansi district in the state of Uttar Pradesh, India. In ancient period it was known as Erikachha or Erakachha and according to a Buddhist text, the Petavatthu it was one of the major cities of the Dasanna janapada.
The Largest Hindu temple in Indonesia - Prambanan
The Largest Hindu temple in Indonesia - Prambanan
Prambanan Temple
Prambanan temple , dedicated to the Trimurti, the expression of God as the Creator (Brahma), the Preserver (Vishnu) and the Destroyer (Shiva) has three main temples in the primary yard, namely Vishnu, Brahma, and Shiva temples. Those three temples are symbols of Trimurti in Hindu belief. All of them face to the east. Each main temple has accompanying temple facing to the west, namely Nandini for Shiva, Angsa for Brahma, and Garuda for Vishnu. Besides, there are 2 flank temples, 4 kelir temples and 4 corner temples. In the second area, there are 224 temples.
Prambanan temple is extraordinarily beautiful building constructed in the tenth century during the reigns of two kings namely Rakai Pikatan and Rakai Balitung. Soaring up to 47 meters (5 meters higher than Borobudur temple), the foundation of this temple has fulfilled the desire of the founder to show Hindu triumph in Java Island. This temple is located 17 kilometers from the city center, among an area that now functions as beautiful park.
According to the Shivagrha inscription of 856 CE, the temple was built to honor Lord Shiva, and its original name was Shiva-grha (the House of Shiva) or Shiva-laya (the Realm of Shiva). According to the Shivagrha inscription, a public water project to change the course of a river near Shivagrha Temple was undertaken during the construction of the temple. The river, identified as the Opak River, now runs north to south on the western side of the Prambanan temple compound.
Historians suggest that originally the river was curved further to east and was deemed too near to the main temple.The project was done by cutting the river along a north to south axis along the outer wall of the Shivagrha Temple compound. The former river course was filled in and made level to create a wider space for the temple expansion, the space for rows of pervara (complementary) temples.
There is a legend that Javanese people always tell about this temple. As the story tells, there was a man named Bandung Bondowoso who loved Roro Jonggrang. To refuse his love, Jonggrang asked Bondowoso to make her a temple with 1,000 statues only in one-night time. The request was nearly fulfilled when Jonggrang asked the villagers to pound rice and to set a fire in order to look like morning had broken. Feeling to be cheated, Bondowoso who only completed 999 statues cursed Jonggrang to be the thousandth statue.
The inner zone or central compound is the holiest among the three zones. It is the square elevated platform surrounded by a square stone wall with stone gates on each four cardinal points. This holiest compound is assembled of eight main shrines or candi. The three main shrines, called Trimurti ("three forms"), are dedicated to the three Gods: Brahma the Creator, Vishnu the Keeper, and Shiva the Destroyer.
The Shiva temple is the tallest and largest structure in Prambanan Loro Jonggrang complex; it measures 47 metres tall and 34 metres wide. The main stairs are located on the eastern side. The eastern gate of Shiva temple is flanked by two small shrines, dedicated to guardian gods, Mahakala and Nandhisvara. The Shiva temple is encircled with galleries adorned with bas-reliefs telling the story of Ramayana carved on the inner walls of the balustrades.
To follow the story accurately, visitors must enter from the east side and began to perform pradakshina or circumambulating clockwise. The bas-reliefs of Ramayana continue to the Brahma temple galleries.
The Shiva shrine is located at the center and contains five chambers, four small chambers in every cardinal direction and one bigger main chamber in the central part of the temple. The east chamber connects to the central chamber that houses the largest temple in Prambanan, a three-metre high statue of Shiva Mahadeva (the Supreme God).
The statue bears Lakçana (attributes or symbol) of Shiva such as skull and sickle (crescent) at the crown, and third eye on the forehead; also four hands that holds Shiva's symbols: prayer beads,
feather duster, and trisula (trident). Some historians believe that the depiction of Shiva as Mahadeva was also meant to personify king Balitung as the reincarnation of Shiva. So, when he died, a temple was built to commemorate him as Shiva. The statue of Shiva stands on a lotus pad on a Yoni pedestal that bears the carving of Nāga serpents on the north side of the pedestal.
The other three smaller chambers contain statues of Hindu Gods related to Shiva: his consort Durga, the rishi Agastya, and Ganesha, his son. A statue of Agastya occupies the south chamber, the west chamber houses the statue of Ganesha, while the north chamber contains the statue of Durga Mahisasuramardini depicting Durga as the slayer of the Bull demon. The shrine of Durga is also called the temple of Rara Jonggrang (Javanese: slender virgin), after a Javanese legend of princess Rara Jonggrang.Brahma temple contains the statue of Brahma and Vishnu temple houses the statue of Vishnu. Brahma and Vishnu temple measures 20 metres wide and 33 metres tall.
On the outside-facing walls of the Shiva temple's central cella there are a total of 24 relief panels. Eight of these figures collectively represent a group of Deities called the Lokapalas -- the guardians of the eight directions of space.
Vedic cosmology associates six of the eight Lokapalas with six of the planets of ancient astronomy: Kubera (Venus), Varuna (Mercury), Yama (Mars), Agni (Saturn), Issana (Moon) and Indra (Jupiter). In addition, the Lokapalas Nirriti and Vayu were assigned stations in the sky that corresponded with certain star signs of Vedic astronomy, called the nakshatras.
In Vishnu temple, to the north of Shiva temple, you will find only one room with Vishnu statue in it. In Brahma temple, to the south of Shiva temple, you find only room as well with Brahma statue in it.
Quite attractive accompanying temple is Garuda temple that is located close to Vishnu temple. This temple keeps a story of half-bird human being named Garuda. Garuda is a mystical bird in Hindu mythology. The figure is of golden body, white face, red wings, with the beak and wings similar to eagle's. It is assumed that the figure is Hindu adaptation of Bennu (means 'rises' or 'shines') that is associated with the god of the Sun or Re in Old Egypt mythology or Phoenix in Old Greek mythology. Garuda succeeded in saving his mother from the curse of Aruna (Garuda's handicapped brother) by stealing Tirta Amerta (the sacred water of the gods).
Its ability to save her mother made many people admire it to the present time and it is used for various purposes. Indonesia uses the bird as the symbol of the country. Other country using the same symbol is Thailand, with the same reason but different form adaptation and appearance. In Thailand, Garuda is known as Krut or Pha Krut.
Prambanan also has panels of relief describing the story of Ramayana. Experts say that the relief is similar to the story of Ramayana that is told orally from generation to generation. Another interesting relief is Kalpataru tree that - in Hindu - the tree is considered tree of life, eternity and environment harmony. In Prambanan, relief of Kalpataru tree is described as flanking a lion. The presence of this tree makes experts consider that Javanese society in the ninth century had wisdom to manage its environment.
Just like Garuda, Kalpataru tree is also used for various purposes. In Indonesia, Kalpataru is used as the logo of Indonesian Environment Institution. Some intellectuals in Bali even develop "Tri Hita Karana" concept for environment conservation by seeing Kalpataru relief in this temple. This tree of life is also seen in the gunungan (the puppet used as an opening of traditional puppet show or wayang kulit). This proves that relief panels in Prambanan have been widely known throughout the world.
If you see the relief in detail, you will see many birds on them; they are real birds as we can see on the earth right now. Relief panels of such birds are so natural that biologists can identify their genus. One of them is the relief of the Yellow-Crest Parrot (Cacatua sulphurea) that cites unanswered question. The reason is that the bird only exists in Masakambing Island, an island in the middle of Java Sea. Then, did the bird exist in Yogyakarta? No body has succeeded in revealing the mystery.
You can discover many more things in Prambanan. You can see relief of Wiracarita Ramayana based on oral tradition. If you feel tired of enjoying the relief, you can take a rest in the beautiful garden in the complex.
It was likely started by Rakai Pikatan as the Hindu Sanjaya Dynasty's answer to the Buddhist Sailendra Dynasty's Borobudur
Enjoy the moments on Twitter -
https://twitter.com/i/moments/852024018278391809
Hinduism In Bali
Hinduism was already prevalent in most of Indonesia way before Islam came, spread by monks on trading ships from India, with the locals later forming societies and kingdoms based around this culture
A while after that, though Islam came, also from traders, and the religion appealed more to the locals and they welcomed it warmly, partly because it lacks the caste system which Hinduism has. Islam spread wider and wider until Indonesia become what it is now.
So Hinduism already exists in Bali, and it can be presumed that the locals did not accept Islam, and instead remaining in Hinduism.
There's never been a significant presence of Muslim community there since barely anybody from where they all hail ever came to Bali to spread the religion. By the time Majapahit began to loose its dominance over the archipelago, most of its spin-offs underwent the Islamization but retained its maritime culture. Bali didn't. Unlike Java, Bail didn't (and doesn't) posses any major trading port. Elusive as it might be, no significant spice grew in Bali as well. Traders from South Asia and Near East sailed to Malacca, Java or Borneo -- marrying locals while introducing Islamism to local nobles -- and making contact with people from the East (lesser Sunda, Moluccas and Buru), while passing Bali altogether.
Bali remained isolated and undisturbed for 300 hundred years since the fall of Majapahit. It allied the Franco-Dutch bloc during Napoleonic wars, ensuring its sovereignty in the wake of European scrambles of every corner of earth. All that while retaining Hinduism as state religion. Thus, Bali and Aceh were the last places in Indonesian Archipelago to have not yet fallen into full Dutch control in the wake of twentieth century. By the time the Dutch army was invading the southern Balinese kingdoms (where Denpasar lies) in 1908, almost all of local hereditary rulers were acting as either a vassal, a puppet ruler or just a symbol of a local Dutch-administered sub-colonial entity.
Balinese say that their ancestors where from India, some say Indian Hindu rulers during 8th century ruled the island and gave the Hindu religion to its inhabitants. May be this is the reason why the ocean got its name "The Indian ocean", an ocean ruled by Indians.
Today almost 90% of Bali population is Hindu, and the masses love to flaunt their religion. Major road crossing squares posses giant statues of mythological hero's Rama, Krishna ,bhima , Arjuna and many more. Unlike India people out here are more religious and ardent believer of Hinduism. Their temple doesn't contain idol as they strongly claim they are not idol worshipers, and support their statement with its mention in holy vedas inscriptions, which again contradicts Hinduism of india.
May be this is how Hinduism was back then in 8th century across the ocean. No idol worship ,no discrimination among classes and no superstitious belifes. But then after 8th century the religion took different courses in two different lands, in India it evolved to what it is today we follow in India, whereas it remained the very same in Bali the way it was back in 8th century.
Today Balinese believes in the trinity , bramha ,Vishnu , Mahesh . the creator - protector - destroyer. They believe in each and every aspect of Hinduism and practices it religiously. There temple contains trinity without any idol inside. They follow Vedas and the epic stories ardently. For them their heroes are the one from the great epic stories Ramayana and Mahabharata. Their traditional costumes still have traces of our Indian wear ,sari, apparently their ethnic wear resembles very much to the costumes in southern india under the rule of pallava and chola dynasties.
Today in front of Balinese you as a Indian Hindu might feel inadequate in calling yourself a Hindu. Hinduism has been complicated by we indians in last 10 centuries. May the changes made in our customs where need of the hour back then.
May be this is what Hinduism is all about Making yourself comfortable in the surrounding. Actually Hinduism isn't a religion but way of life. One need to mould him self as per the socio-politico condition of the surrounding. In last decade of centuries we indians have witnessed many invasions, change of power and crises which left some serious stains leading to letting Indian
Bali has also evolved in away, for its survival it has accepted tourism industry. Tourists are the first citizens of Bali , yes its true. You can apparently feel it once you land in the island. The ever smiling faces of Balinese make you fall in love with this beautiful community. They will adore you and help you in discovering their island. When in Bali you shall not bother about crossing the heavily trafficked road, because unlike any other place in the planet, whole traffic will stop for you to cross the road that too with a smiling face by the waiting car drivers. Yes its true am not making this up, me and my wife have actually experienced this in Bali on couple of occasions. And this and few similar incidents made me make this statement " Bali must be the only province on earth where visitors/ tourists are its first citizens ".
And I strongly believe this evolution amongst the local masses has a reason too, during the recent blasts, in 2002 and 2005 which took place at the crowded pubs near kuta beach left Bali with sorrows of down time in tourist industry. Even today people out here get upset while discussing about event and its aftereffects. It was a season of draught for the tourism industries, and Balinese would never even dream of such experience in future. Thus tourist are the focal of attention for them.
Balinese Hinduism (Indonesian: Hindu Dharma) is the form of Hinduism practiced by the majority of the population of Bali. This is particularly associated with the Balinese people residing on the island and represents a distinct form of Hindu worship incorporating local animism, ancestor worship or Pitru Paksha and reverence for Buddhist saints or Bodhisattava. Although the population of Indonesia is predominantly Muslim and Christian, 83% of the people on Bali identify as Hindu. The fundamental principle underlying Hinduism is that there is order in the cosmos, known as dharma. There is also a disordering force, adharma. Hindus seek balance and harmony between these two forces, thus freeing themselves from the never-ending cycle of reincarnation, attaining a state called moksa.
Balinese Hinduism divides the cosmos into three layers. The highest level is heaven, or suarga, the abode of the gods. Next is the world of man, buwah. Below this is hell or bhur, where the demons live and where people's spirits are punished for misdeeds on earth. This tripartite division is mirrored in the human body (head, body and feet) and the shrines found outside Balinese buildings.
Along with the traditional Hindu gods such as Brahma, Vishnu and Siva, Balinese Hindus worship a range of deities unique to their branch of the religion. Sang Hyang Widhi (also known as Acintya or Sang Hyang Tunggal) is the designation for one God in Balinese Hinduism. In the concept of Balinese tradition of Hinduism, Acintya or Sang Hyang Widhi is associated with the concept of Brahman. Balinese Hindu belief in a single God is in line with the first principle of the Indonesian state philosophy Pancasila.
The empty chair at the top of the padmasana shrine found outside houses and temples is for Sang Hyang Widhi Wasa According to Balinese Hindu precepts, there are many manifestations of Sang Hyang Widhi Wasa in the form of gods such as Dewi Sri, the goddess of rice, and many other gods associated with mountains, lakes and the sea.
Balinese Hindus built Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, the second largest temple in Indonesia after Pura Besakih in Bali, dedicated to Hindu Sundanese King Sri Baduga Maharaja.
Sang Ratu Jaya Dewata. Pura Aditya Jaya is the largest temple in Indonesian capital Jakarta.
At least one Balinese Hindu temple exists in Europe. A padmasana exists in Hamburg, Germany in front of the Museum of Ethnology, Hamburg.
The Island Of Gods - Bali
The Island Of Gods - Bali
The Island Of Gods - Bali
Bali is a province of Indonesia which is located between the islands of Java and Lombok island, Bali island is also commonly referred to as The Island Of Thousands Temples, The Island of Gods, and Bali Dwipa, Bali also has several small islands are also included in the province of Bali, including the island of Nusa Penida, Nusa Lembongan Island, Nusa Ceningan island, Serangan Island and Menjangan Island.
The capital of Bali is Denpasar, located in the south of the island, the island of Bali is renowned as a world tourism destination with unique art and culture. Bali island is the best place for a holiday with the world class accommodation.
The history of Bali covers a period from the Paleolithic to the present, and is characterized by migrations of people and cultures from other parts of Asia. In the 16th century, the history of Bali started to be marked by Western influence with the arrival of Europeans, to become, after a long and difficult colonial period under the Dutch, an example of the preservation of traditional cultures and a key tourist destination.
Balinese culture was strongly influenced by Indian, Chinese, and particularly Hindu culture, beginning around the 1st century AD. The name Bali Dwipa ("Bali island") has been discovered from various inscriptions, including the Blanjong pillar inscription written by Sri Kesari Warmadewa in 914 AD and mentioning "Walidwipa".
It was during this time that the complex irrigation system Subak was developed to grow rice. Some religious and cultural traditions still in existence today can be traced back to this period. The Hindu Majapahit Empire (1293–1520 AD) on eastern Java founded a Balinese colony in 1343. When the empire declined, there was an exodus of intellectuals, artists, priests, and musicians from Java to Bali in the 15th century.
Bali being part of the Sunda shelf, the island had been connected to the island of Java many times through history. Even today, the two islands are only separated by a 2.4 km Bali Strait. The ancient occupation of Java itself is accredited by the findings of the Java man, dated between 1.7 and 0.7 million years old, one of the first known specimens of Homo erectus.
Bali also was inhabited in Paleolithic times (1 my BCE to 200.000 BCE), testified by the finding of ancient tools such as hand axes were found in Sembiran and Trunyan villages in Bali. A Mesolithic period (200.000-3.000 BCE) has also been identified, characterized by advanced food gathering and hunting. This period yields more sophisticated tools, such as arrow points, and also tools made of animal or fish bones. They lived in temporary caves, such as those found in the Pecatu hills of the Badung regency, such as the Selanding and the Karang Boma caves.
From around 3000 to 600 BCE, a Neolithic culture emerges, characterized by a new wave of inhabitants bringing rice-growing technology and speaking Austronesian languages.These Austronesian peoples seem to have migrated from South China, probably through the Philippines and Sulawesi. Their tools included rectangular adzes and red slipped decorated pottery.
A Bronze Age period follows, from around 600 BCE to 800 CE. Between the 8th and 3rd century BCE, the island of Bali acquired the "Dong Son" metallurgical techniques spreading from Northern Vietnam. These techniques involved sophisticated casting from moulds, with spiral and anthropomorphic motifs.
As mould fragments have been found in the area of Manuaba in Bali, it is thought that such implements were manufactured locally rather than imported. The raw material to make bronze (copper and tin) had to be imported however, as it is not available on Bali.
Numerous bronze tools and weapons were made (axes, cooking tools, jewellery), and ceremonial drums from that period are also found in abundance, such as the "Moon of Pejeng", the largest ceremonial drum yet found in Southeast Asia, dated to around 300 BCE
The ancient historical period is defined by the appearance of the first written records in Bali, in the form of clay pallets with Buddhist inscriptions. These Buddhist inscriptions, found in small clay stupa figurines (called "stupikas") are the first known written inscriptions in Bali and date from around the 8th century CE. Such stupikas have been found in the regency of Gianyar, in the villages of Pejeng, Tatiapi and Blahbatuh
The Majapahit Empire rule over Bali became complete when Gajah Mada, Prime Minister of the Javanese king, defeated the Balinese king in Bedulu in 1343.The Majapahit capital in Bali was established at Samprangan and later Gelgel. Gelgel remained the paramount kingdom on Bali until the second half of the 17th century.
With the rise of Islam in the Indonesian archipelago, the Majapahit empire finally fell, and Bali became independent at the end of the 15th or beginning of the 16th century, with much of the Javanese aristocracy finding refuge in Bali, bringing an even stronger influx of Hindu arts, literature and religion. According to later chronicles the dynasty of Majapahit origins, established after 1343, continued to rule Bali for 5 more centuries until 1908, when the Dutch eliminated it in the Dutch intervention in Bali (1908).
In the 16th century, the Balinese king Dalem Baturenggong even expanded in turn his rule to East Java, Lombok and western Sumbawa. Around 1540, together with the Islamic advance, a Hindu reformation movement took place, led by Dang Hyang Nirartha, leading to the introduction of the Padmasana shrine in honour of the "Supreme God" Acintya, and the establishment of the present shape of Shiva-worshipping in Bali. Nirartha also established numerous temples, including the spectacular temple at Uluwatu.
The first European contact with Bali is thought to have been made in 1585 when a Portuguese ship foundered off the Bukit peninsula and left a few Portuguese in the service of Dewa Agung. In 1597 the Dutch explorer Cornelis de Houtman arrived at Bali and, with the establishment of the Dutch East India Company in 1602, the stage was set for colonial control two and a half centuries later when Dutch control expanded across the Indonesian archipelago throughout the second half of the nineteenth century (see Dutch East Indies).
Dutch political and economic control over Bali began in the 1840s on the island's north coast when the Dutch pitted various distrustful Balinese realms against each other. In the late 1890s, struggles between Balinese kingdoms in the island's south were exploited by the Dutch to increase their control.
The Dutch mounted large naval and ground assaults at the Sanur region in 1906 and were met by the thousands of members of the royal family and their followers who fought against the superior Dutch force in a suicidal Puputan defensive assault rather than face the humiliation of surrender. Despite Dutch demands for surrender, an estimated 1,000 Balinese marched to their death against the invaders.
In the Dutch intervention in Bali (1908), a similar massacre occurred in the face of a Dutch assault in Klungkung. Afterward, the Dutch governors were able to exercise administrative control over the island, but local control over religion and culture generally remained intact. Dutch rule over Bali came later and was never as well established as in other parts of Indonesia such as Java and Maluku. In the 1930s, anthropologists Margaret Mead and Gregory Bateson, and artists Miguel Covarrubias and Walter Spies, and musicologist Colin McPhee created a western image of Bali as "an enchanted land of aesthetes at peace with themselves and nature", and western tourism first developed on the island. Imperial Japan occupied Bali during World War II. Bali Island was not originally a target in their Netherlands East Indies Campaign, but as the airfields on Borneo were inoperative due to heavy rains the Imperial Japanese Army decided to occupy Bali, which did not suffer from the comparable weather. The island had no regular Royal Netherlands East Indies Army (KNIL) troops. There was only a Native Auxiliary Corps Prajoda (Korps Prajoda) consisting of about 600 native soldiers and several Dutch KNIL officers under command of KNIL Lieutenant Colonel W.P. Roodenburg. On 19 February 1942, the Japanese forces landed near the town of Senoer (Sanur). The island was quickly captured. During the Japanese occupation a Balinese military officer, I Gusti Ngurah Rai, formed a Balinese 'freedom army'. The lack of institutional changes from the time of Dutch rule, however, and the harshness of war requisitions made Japanese rule little better than the Dutch one. Following Japan's Pacific surrender in August 1945, the Dutch promptly returned to Indonesia, including Bali, immediately to reinstate their pre-war colonial administration. This was resisted by the Balinese rebels now using Japanese weapons. On 20 November 1946, the Battle of Marga was fought in Tabanan in central Bali. Colonel I Gusti Ngurah Rai, by then 29 years old, finally rallied his forces in central Bali at Marga Rana, where they made a suicide attack on the heavily armed Dutch. The Balinese battalion was entirely wiped out, breaking the last thread of Balinese military resistance. In 1946 the Dutch constituted Bali as one of the 13 administrative districts of the newly proclaimed State of East Indonesia, a rival state to the Republic of Indonesia which was proclaimed and headed by Soekarno and Hatta. Bali was included in the "Republic of the United States of Indonesia" when the Netherlands recognized Indonesian independence on 29 December 1949.
Temples of Bali
Temples of Bali
Bali was inhabited by around 2000 BC by Austronesian peoples who migrated originally from Taiwan through Maritime Southeast Asia. Culturally and linguistically, the Balinese are thus closely related to the peoples of the Indonesian archipelago, Malaysia, the Philippines, and Oceania. Stone tools dating from this time have been found near the village of Cekik in the island's west. In ancient Bali, nine Hindu sects existed, namely Pasupata, Bhairawa, Siwa Shidanta, Waisnawa, Bodha, Brahma, Resi, Sora, and Ganapatya. Each sect revered a specific deity as its personal Godhead.
Balinese culture was strongly influenced by Indian, Chinese, and particularly Hindu culture, beginning around the 1st century AD. The name Bali Dwipa ("Bali island") has been discovered from various inscriptions, including the Blanjong pillar inscription written by Sri Kesari Warmadewa in 914 AD and mentioning "Walidwipa". Bali’s highlands and coasts are home to many ancient temples. Several of them have become the island’s most iconic landmarks, featuring magnificent centuries-old architecture and set against the exotic backdrops. Lively processions, ornate decorations and festivity take place during temple anniversaries, which come around twice a Gregorian year based on a local 210-day calendar. On any other day, they are great places to visit at least once during your visits to Bali. Each temple is unique. Be it the cloudy peaks of Mount Agung at the Besakih ‘mother temple’, the mysterious ruins of Goa Gajah, or the golden sunsets and silhouettes of Uluwatu and Tanah Lot. Proper conduct and temple attire comprising a waist cloth (sarong) and sash are required, available for rental or donation fees at all sites.
Tanah Lot Temple
Tanah Lot Temple is one of Bali’s most important landmarks, famed for its unique offshore setting and sunset backdrops. An ancient Hindu shrine perched on top of an outcrop amidst constantly crashing waves; Tanah Lot Temple is simply among Bali’s not-to-be-missed icons. The onshore site is dotted with smaller shrines alongside visitors’ leisure facilities that comprise restaurants, shops and a cultural park presenting regular dance performances. The temple is located in the Beraban village of the Tabanan regency, an approximate 20km northwest of Kuta, and is included on most tours to Bali’s western and central regions.
Legend of Tanah Lot Dang Hyang Nirartha, a high priest from the Majapahit Kingdom in East Java who travelled to Bali in 1489 to spread Hinduism, arrived at the beautiful area and established a site honouring the sea god, Baruna. Here, he shared his teachings to Beraban villagers, only to face opposition from the village chief who soon gathered his loyal followers to dispel Nirartha. The priest resisted, incredibly shifting a large rock he meditated upon out to sea while transforming his sashes into sea snakes to guard at its base.
The rock’s original name, Tengah Lod, means ‘in the sea’. Acknowledging Nirartha’s powers, the humbled chief vowed allegiance. Before setting off, Nirartha gifted him a holy kris dagger, which is now among the sanctified heirlooms of the Kediri royal palace. Pilgrims bring these relics each Kuningan day by foot on an 11km pilgrimage to the Luhur Pakendungan temple, the priest’s former meditational site.
Although you cannot enter the temple grounds, the panoramic views and cultural offerings are highlights to enjoy. On the holy day of Kuningan, five days prior to the temple’s anniversary date, the heirloom pilgrimage is one of Bali’s festive parades worth witnessing. Tanah Lot’s piodalan falls on every Wednesday that follows each Kuningan on Bali’s 210-day Pawukon calendar. Dress and act respectfully as on any temple visit in Bali.
Uluwatu Temple
Uluwatu Temple or Pura Luhur Uluwatu, one of six key temples believed to be Bali's spiritual pillars, is renowned for its magnificent location, perched on top of a steep cliff approximately 70 metres above sea level. This temple also shares the splendid sunset backdrops as that of Tanah Lot Temple, another important sea temple located in the island's western shores. Pura Luhur Uluwatu is definitely one of the top places on the island to go to for sunset delights, with direct views overlooking the beautiful Indian Ocean and daily Kecak dance performances. Balinese architecture, traditionally-designed gateways, and ancient sculptures add to Uluwatu Temple's appeal.
Without a doubt, what makes Uluwatu Temple spectacular is its cliff-top setting at the edge of a plateau 250 feet above the waves of the Indian Ocean. 'Ulu' means the ‘top’ or the ‘tip’ and 'watu' means a ‘stone’ or a ‘rock’ in Balinese. Several archaeological remains found here prove the temple to be of megalithic origin, dating back to around the 10th century. There are two entrances to Uluwatu Temple, from the south and the north. A small forest lies at the front and hundreds of monkeys dwell here. They are believed to guard the temple from bad influences. The serpentine pathway to the temple is fortified by concrete walls on the cliff side. It takes about an hour to get from one end to another as there are several fenced points along the way to stop. The views from the bottom of the water surging up against rocks and the ocean horizon are remarkable. The Balinese Hindus believe that the three divine powers of Brahma, Vishnu, and Siva become one here. That belief results in making Uluwatu Temple a place of worship of Siva Rudra, the Balinese Hindu deity of all elements and aspects of life in the universe. Pura Uluwatu is also dedicated to protect Bali from evil sea spirits.
Inscriptions mention that Uluwatu Temple was instigated by Mpu Kunturan, a Majapahit monk who also participated in establishing several other important temples in Bali such as Pura Sakenan in Denpasar, about 1,000 years ago. A holy priest from eastern Java, Dhang Hyang Dwijendra, then chose Uluwatu Temple to be his spiritual journey's final worshiping place. Balinese Hindu devotees believe that he reached the highest spiritual point of oneness with deities by a strike of lightning and completely disappeared. Legend, however, says that Dhang Hyang Dwijendra (also frequently referred to by name as Danghyang Nirartha) was the architect of Uluwatu Temple and several other temples in Bali, Lombok, as well as Sumbawa. Until 1983, Pura Uluwatu was hardly accessible and a lightning strike in 1999 set some parts of the temple on fire. The temple has had some restorations since it was first built.
Behind the main shrine in one of the courtyards of Uluwatu Temple lies a Brahmin statue facing the Indian Ocean, considered as a representation of Dhang Hyang Dwijendra. The two entrances to the temple area are split gates with leaves and flowers carvings. In front of each of them are a couple of sculptures shaped like a human body with an elephant head. A heritage of the 10th century is the one-piece winged stone gate to the inside courtyard of Pura Uluwatu. Winged gates are not commonly found on the island. An addition to Pura Uluwatu in the 16th century is Pura Dalem Jurit. There are three statues in it, one of them is of Brahma. There are two stone troughs in the temple area. If both of them are joined, they create a sarchopagus (Megalithic coffin). Uluwatu Beach, below the cliff, is one of Bali's best internationally-known surfing spots.
Every six months according to the Balinese 210-day Pawukon cycle, big temple anniversary celebrations are held at the temple. The temple's keeper, the royal family of Jro Kuta from Denpasar, are patrons for the event. Precautionary signs warn visitors of the monkeys grabbing attractive items such as sunglasses and cameras. However, they can be calmer when approached with peanuts or bananas, lending an opportunity to retake stolen possessions. There hasn't been any significant erosion on the shoreline underneath the temple's towering cliff. Believers regard it as a manifestation of the divine power that protects Pura Uluwatu. Public facilities are available, but not in the temple area. Unlike some other tourist destinations in Bali, Uluwatu Temple area has limited amounts of hassling vendors. Visitors must wear a sarong and a sash, as well as appropriate clothes common for temple visits. They can be hired here.
The best time to visit is just before sunset. A Kecak dance is performed everyday at the adjacent cliff-top stage at 18:00 to 19:00. Visitors are charged a nominal fee. What makes it the most favourite venue to watch a Kecak dance is the sunset background of the performance. There's no public transportation to get here and going back in to town will be difficult without any prearranged ride or taxi. A guide is not necessary, though helpful. The service offered is hassle-free at very minimum prices.
Besakih Temple
Besakih Temple known as Bali’s ‘Mother Temple’ for over 1,000 years, sits 1,000 metres high on the southwestern slopes of Mount Agung. Besakih is an artistic and unique complex that comprises at least 86 temples which include the main Pura Penataran Agung (the Great Temple of State) and 18 others. Besakih is the biggest and holiest of the island's temples and is surrounded by breathtaking and scenic rice paddies, hills, mountains, streams, and more.
To the Balinese, visiting the temple sanctuaries is a special pilgrimage. Mount Agung’s high location gives it an almost mystical quality. Many stairs lead up to the sacred mountain, leading to the many temples that vary according to types, status, and functions. Pura Besakih features three temples dedicated to the Hindu trinity. Pura Penataran Agung in the centre has white banners for Shiva, the destroyer; Pura Kiduling Kreteg on the right side is with red banners for Brahma, the creator; and Pura Batu Madeg represents Vishnu, the preserver, with its black banners. You can visit other temples in Pura Besakih, but many of their inner courtyards are closed to the public as they’re reserved for pilgrims. Pura Besakih is the only temple open to every devotee from any caste groups. This is because of its nature as the primal centre of all ceremonial activities.
Pura Batu Madeg, containing a central stone, indicates that the area of Pura Besakih was already regarded a holy place since ancient times. In the 8th century, a Hindustani monk had revelations to build homes for people during his isolation. Throughout the process, many of his followers died due to illness and accidents. On its completion it was called ‘Basuki’, referring to the dragon deity ‘Naga Besukian’, believed to inhabit Mount Agung. The name eventually evolved into ‘Besakih’. Other shrines were gradually built and Pura Besakih was made the main temple during the conquering of Bali by the Majapahit Empire in 1343. Since then, Pura Besakih has had several restorations as earthquakes in 1917 and Mount Agung’s series of eruptions in 1963 damaged the complex. The lava flow passed by Pura Besakih and it is believed to be a miraculous signal from the deities that they wanted to demonstrate their power without completely destroying the holy complex their devotees had built for them.
The largest temple in the complex, Pura Penataran Agung, has different areas representing seven layers of the universe, each with their own shrines. Pura Pasimpangan on the downstream side (on the east of the main street) and Pura Pangubengan upstream are approximately three kilometres apart. Located on higher ground, the closest to Mount Agung's peak, Pura Pangubengan has great vistas and it’s about a 30-minute walk from the main Pura Penataran Agung. Around 10 minutes to the east of Pura Pangubengan is Pura Batu Tirtha. It is where holy water is sourced for the ‘karya agung’ ceremonies at Pura Besakih and Pekraman villages. Four temples in the complex reflect four forms of God at compass points: Pura Batu Madeg in the north, Pura Kiduling Kreteg to the south, Pura Gelap in the east, and Pura Ulun Kulkul in the west. ‘Batu ngadeg’, literally ‘standing stone’, is found in the shrine of Meru Tumpang Sebelas at Pura Batu Madeg. This is where Vishnu is believed to descend. Still in the courtyard of Pura Batu Madeg, in front of Meru Tumpang Sebelas is the Pesamuan shrine (quadrangle-shaped with two lines of 16 poles) as a symbol of how Vishnu’s power interrelates with the world. At least 20 minutes to the northwest from Pura Batu Madeg, down the footpath to the valley and along the river, is Pura Peninjoan – erected on a tiny hill. The beautiful views from here include all the shrines of Pura Penataran Agung, beaches and southern Bali in the distance. On the west is Pura Ulun Kulkul, famous for the main and most precious ‘kulkul’ (Balinese wooden slit gong) on the island. Kulkul is a signaling device to summon or convey special messages. On the northern side of Pura Ulun Kulkul is Pura Merajan Selonding where the 'Bredah' inscription mentions a king in Besakih, and a set of ancient gamelan called ‘Selonding’ are kept. Pura Gua, located on the eastern side of the main street, is the home of the dragon deity.
There’s a big cave at the canyon of the river on the east that has its mouth closed due to erosion, but people still sometimes practise yoga there. Pura Jenggala, southwest of Pura Penataran Agung, is also often called Pura Hyang Haluh by the local devotees. The ‘Setra Agung’ burial grounds is south of the temple. Here are sacred ancient stone statues in the form of the mythical garuda bird. Pura Basukian Puseh Jagat is located southeast of Pura Penataran Agung, the main foundation of Pura Besakih.
Pura Besakih was nominated as a World Heritage Site in 1995, but as yet remains unvested. There are at least 70 ceremonies or religious celebrations held each year here, as each shrine has its own anniversary, plus the big holidays based on the 210-day Balinese Hindu calendar system. Pura Basukian, Pura Penataran Agung, and Pura Dalem Puri are the mother of all village’ temples, namely Pura Puseh, Pura Desa, and Pura Dalem. Their shrines contain religious literature referring how a temple must be built. During the daytime Besakih becomes a crowded tourist trap, with self-professed ‘temple guards’, touts, hawkers, and more. Bear in mind that you should wear a proper top, a sarong, and a sash.
The best visiting times of the day are in the early morning and in the evening as the complex is much quieter during these hours. The official guides are easily identifiable with their symmetrically patterned traditional Batik shirts. The service is not free, though not expensive at all either considering how big the complex is. There's no obligation to hire a guide for tours around the complex. Sarongs and sashes are available for rent. They’re also available for purchase at the many stalls outside, and bargaining is recommended. Women on their periods are forbidden entry. Don’t forget to change money in the more urban areas as the rates here are not reliable.
Ulun Danu Beratan
The Ulun Danu Beratan Temple is both a famous picturesque landmark and a significant temple complex located on the western side of the Beratan Lake in Bedugul, central Bali. The whole Bedugul area is actually a favorite cool upland weekend and holiday retreat for locals and island visitors alike from the southern and urban areas, as it is strategically located, connecting the island’s north and south. Ulun Danu Beratan, literally ‘the source temple of Lake Beratan’, is easily the island’s most iconic sanctuary sharing the scenic qualities with the seaside temples of Uluwatu and Tanah Lot. The smooth reflective surface of the lake surrounding most of the temple’s base creates a unique floating impression, while the mountain range of the Bedugul region encircling the lake provides the temple with a scenic backdrop.
The temple was built in the 17th century in worship of the main Hindu trinity, Brahma-Vishnu-Shiva, as well as the lake goddess, Dewi Danu. The sight and cool atmosphere of the Bali uplands have made the lake and this temple a favourite sightseeing and recreational spot as well as a frequently photographed site.
The history of the Ulun Danu temple can be traced back to the rise of the Mengwi kingdom. The ‘floating’ temple complex is comprised of four groups of shrines, including the prominent Lingga Petak shrine to its east. There are four gates facing each of the four points of the compass. The second group is located in the west and pays homage to another temple in the hill of Puncak Mangu and is regarded as the symbol of soil fertility. The ‘puncak’ or hilltop of Mangu is northeast of Lake Beratan.
Entering the temple gates, instantly noticeable are the typical Balinese architectural features and the tiered shrines. Inside the complex, the three main shrines are dedicated to the worship of god Vishnu which boasts 11 tiers, god Brahma with seven 7 tiers and Shiva with three tiers. As the temple complex occupies a rather low lying side of the lake, the floating effect is thus featured when the lake’s water levels rise.
This is the time for the most perfect photo opportunities. Besides a silent witness and historical site of the golden days of the Mengwi kingdom, this temple complex is also home to a megalithic artifact in the form of a sarcophagus and stone tablet. This has led to the assumption that it was a consecrated site before the Hindu temple was built.
Ulun Danu Beratan temple’s anniversary ceremony or Piodalan takes place every Kliwon Julungwangi Tuesday on the Pawukon Balinese calendar cycle which occurs every 210 days. Also a grander Piodalan Agung takes place every 420 days. However, on any other regular day the serene lake views and cool uplands are an experience itself.
Visits to the Ulun Danu Beratan temple are subject to an entrance fee of IDR 7,500 for domestic tourists and IDR 10,000 for foreigners. Those who want more than scenery may hire traditional jukung outriggers to tour the lake as well as motorized boats for a quicker ride. The other side of the Beratan Lake also offers various water sports such as parasailing and jet-skis. Close to the temple complex visitors can hire fishing gear and bait to pass the time away on the lakeside. The Eka Karya Botanical Gardens is also a highlight of the Bedugul region, with access located nearby.
Goa Gajah
Goa Gajah’s name is slightly misleading, lending the impression that it’s a gigantic dwelling full of elephants. Nevertheless, Goa Gajah ‘Elephant Cave’ is an archaeological site of significant historical value that makes it a special place to visit. Located on the cool western edge of Bedulu Village, six kilometres out of central Ubud, you do not need more than an hour to descend to its relic-filled courtyard and view the rock-wall carvings, a central meditational cave, bathing pools and fountains.
Goa Gajah dates back to the 11th century, built as a spiritual place for meditation. The main grounds are down a flight of steps from the roadside and parking area, which is lined with various art and souvenir shops and refreshment kiosks. Upon reaching the base you will come across a large ‘wantilan’ meeting hall and an assortment of large old stone carvings, some restored to their former full glory. The pool, excavated in 1954, features five out of supposedly seven statues depicting Hindu angels holding vases that act as waterspouts. Various structures reveal Hindu influences dating back to the 10th century, and some relics feature elements of Buddhism dating even earlier to the 8th century.
The cave is shallow; inside are three stone idols each wrapped in red, yellow and black cloths. Black soot lines the cave’s walls as result from the current-day incense burning. Several indentations show where meditating priests once sat. The northern side of the complex is dominantly Buddhist while south across the river it’s mostly Shivaite. At the southern end are beautiful rice fields and small streams that lead to the Petanu River – another natural site entwined in local legends.
Goa Gajah was built on a hillside and as two small streams met here forming a campuhan or ‘river junction’, the site was considered sacred and was built for hermetic meditation and prayers. What’s in the name? Even though the site’s name translates into ‘Elephant Cave’, you won’t find any pachyderms here. Various theories suggest the origin of the name, such as back in time the Petanu River was originally called ‘Lwa Gajah’, meaning the ‘River Gajah’, before it came to be called Petanu River. Other sources state that the ‘Gajah’ or elephant aspect came from the stone figure inside the cave depicting the Hindu lord Ganesh, who is characterised by an elephant’s head. Ancient inscriptions also allude to the name Antakunjarapada, which roughly translates to ‘elephant’s border’.
The cave’s entrance shows a menacing giant face with its wide open mouth as the door. Various motifs depicting the forest and animals are carved out of the outer rock face. The giant face was considered to be that of an elephant’s. When to visit The complex is open daily 08:00 - 16.00. As with any temple in Bali, women during their periods are forbidden entrance and wearing a sarong and waist sash is a must. These are available for rent at the entrance. Goa Gajah temple celebrates its 'piodalan' temple anniversary on an 'Anggara Kasih Prangbakat' Tuesday on the Balinese 210-day Pawukon calendar, corresponding to different dates on the Gregorian calendar each year (consult a local). Entry tickets are 15,000 rupiah for adults and 7,500 for children.
Tirta Empul temple
Pura Tirta Empul is a Hindu Balinese water temple located near the town of Tampaksiring, Bali, Indonesia. The temple compound consists of a petirtaan or bathing structure, famous for its holy spring water, where Balinese Hindus go to for ritual purification. The temple pond has a spring which gives out fresh water regularly, which Balinese Hindus consider to be holy or amritha.Tirta Empul means Holy Spring in Balinese.
Tirta Empul Temple was founded around a large water spring in 962 A.D. during the Warmadewa dynasty (10th-14th centuries).The name of the temple comes from the ground water source named “Tirta Empul”. The spring is the source of the Pakerisan river.The temple is divided into three sections: Jaba Pura (front yard), Jaba Tengah (central yard) and Jeroan (inner yard). Jaba Tengah contains 2 pools with 30 showers which are named accordingly: Pengelukatan, Pebersihan and Sudamala dan Pancuran Cetik (poison).
The temple is dedicated to Vishnu, another Hindu god name for the supreme consciousness Narayana.On a hill overlooking the temple, a modern villa was built for President Sukarno’s visit in 1954. The villa is currently a rest house for important guests.
आल्हा-ऊदल की कहानी - The Story of Two Brave-Hearts Aalha-Udal
आल्हा-ऊदल की कहानी - The Story of Two Brave-Hearts Aalha-Udal
बड़े लडइया महोबेवाला जिनके बल को वार न पार
"जौन घड़ी यहु लड़िका जन्मो दूसरो नाय रचो करतार सेतु बन्ध और रामेश्वर लै करिहै जग जाहिर तलवार किला जीती ले यह माडू का बाप का बदला लिहै चुकाय जा कोल्हू में बाबुल पेरे जम्बे को ठाडो दिहे पिराय किला किला पर परमाले की रानी दुहाई दिहे फिराय सारे गढ़ो पर विजय ये करिके जीत का झंडा दिहे गडाय तीन बार गढ दिल्ली दाबे मारे मान पिथौरा क्यार नामकरण जाको ऊदल है भीमसेन क्यार अवतार" जिस बालक के पैदा होने पर जब ज्योतिषियों ने ये कहा हो तो उसे गौरव पुरुष होना ही था l
पं० ललिता प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रन्थ आल्हखण्ड की भूमिका में आल्हा को युधिष्ठिर और ऊदल को भीम का साक्षात अवतार बताते हुए लिखा है - "यह दोनों वीर अवतारी होने के कारण अतुल पराक्रमी थे। ये प्राय: १२वीं विक्रमीय शताब्दी में पैदा हुए और १३वीं शताब्दी के पुर्वार्द्ध तक अमानुषी पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गये।
ऐसा प्रचलित है की ऊदल की पृथ्वीराज चौहान द्वारा हत्या के पश्चात आल्हा ने संन्यास ले लिया और जो आज तक अमर है और गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवनदान दे दिया था ,पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र संजम भी महोबा की इसी लड़ाई में आल्हा उदल के सेनापति बलभद्र तिवारी जो कान्यकुब्ज और कश्यप गोत्र के थे उनके द्वारा मारा गया था l
वह शताब्दी वीरों की सदी कही जा सकती है और उस समय की अलौकिक वीरगाथाओं को तब से गाते हम लोग चले आते हैं। आज भी कायर तक उन्हें (आल्हा) सुनकर जोश में भर अनेकों साहस के काम कर डालते हैं। यूरोपीय महायुद्ध में सैनिकों को रणमत्त करने के लिये ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को भी इस (आल्हखण्ड) का सहारा लेना पड़ा था। आल्ह-खण्ड लोक कवि जगनिक द्वारा लिखित एक वीर रस प्रधान काव्य हैं जिसमें आल्हा और ऊदल की ५२ लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन हैं। जगनिक कालिंजर के चन्देल राजा परमार्दिदेव (परमाल ११६५-१२०३ई.) के आश्रयी कवि (भाट) थे। इन्होने परमाल के सामंत और सहायक महोबा के आल्हा-ऊदल को नायक मानकर आल्हखण्ड नामक ग्रंथ की रचना की जिसे लोक में 'आल्हा' नाम से प्रसिध्दि मिली। इसे जनता ने इतना अपनाया और उत्तर भारत में इसका इतना प्रचार हुआ कि धीरे-धीरे मूल काव्य संभवत: लुप्त हो गया।
विभिन्न बोलियों में इसके भिन्न-भिन्न स्वरूप मिलते हैं। अनुमान है कि मूलग्रंथ बहुत बड़ा रहा होगा। १८६५ ई. में फर्रूखाबाद के कलक्टर सर चार्ल्स इलियट ने 'आल्ह खण्ड' नाम से इसका संग्रह कराया जिसमें कन्नौजी भाषा की बहुलता है। आल्ह खण्ड जन समूह की निधि है। रचना काल से लेकर आज तक इसने भारतीयों के हृदय में साहस और त्याग का मंत्र फूँका है. राजपूतों के नैतिक नियमों में केवल वीरता ही नहीं थी बल्कि अपने स्वामी और अपने राजा के लिए जान देना भी उसका एक अंग था। आल्हा और ऊदल की जिन्दगी इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। सच्चा राजपूत क्या होता था और उसे क्या होना चाहिये इसे लिस खूबसूरती से इन दोनों भाइयों ने दिखा दिया है, उसकी मिसाल हिन्दोस्तान के किसी दूसरे हिस्से में मुश्किल से मिल सकेगी।
कहते है कि आल्हा को युद्ध से घृणा थी और न्यायपूर्ण ढंग से रहना विशेष पसंद था । इनके पिता जच्छराज (जासर) और माता देवला थी। ऊदल इनका छोटा भाई था। जच्छराज और बच्छराज दो सगे भाई थे जो राजा परमा के यहाॅ रहते थे। परमाल की पत्नी मल्हना थी और उसकी की बहने देवला और तिलका से महाराज ने अच्छराज और बच्छराज की शादी करा दी थी। मइहर की देवी से आल्हा को अमरता का वरदानल मिला था। युद्ध में मारे गये वीरों को जिला देने की इनमें विशेशता थी। लाार हो कर कभी-कभी इन्हें युद्ध में भी जाना पड़ता था। जिस हाथी पर ये सवारी करते थे उसका नाम पष्यावत था। इन का विवाह नैनागढ़ की अपूर्व सुन्दरी राज कन्या सोना से हुआ था। इसी सोना के संसर्ग से ईन्दल पैदा हुआ जो बड़ा पराक्रमी निकला। शायद आल्हा को यह नही मालूम था कि वह अमर है। इसी से अपने छोटे एवं प्रतापी भाई ऊदल के मारे जाने पर आह भर के कहा है-
पहिले जानिति हम अम्मर हई, काहे जुझत लहुरवा भाइ । (कहीं मैं पहले ही जानता कि मैं अमर हूँ तो मेरा छोटा भाई क्यों जूझता)
ऊदल का जन्म 12 वी शादी में जेठ दशमी दशहरा के दिन हुआ था इनके पिता देशराज राजा जम्बे माडोगढ़ वर्तमान मांडू जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है द्वारा युद्ध में मारे गये थे जिनकी मा का नाम देवल था जी अहीर जाति के थी बड़ी बहादुर और ज्ञानी थी जिनकीमृत्यु पर आल्हा ने विलाप करते हुए कहा कि"मैय्या देवे सी ना मिलिहै भैया न मिले वीर मलखान पीठ परन तो उदय सिंह है जिन जग जीत लई किरपान" राजा परिमाल की रानी मल्हना ने ऊदल का पालन पोषण पुत्र की तरह किया इनका नाम उदय सिंह रखा ऊदल बचपन से ही युद्ध के प्रति उन्मत्त रहता था इसलिए आल्हखण्ड में लिखा है "कलहा पूत देवल क्यार " अस्तु जब उदल का जन्म हुआ उस समय का वर्त्तान्त अलह खण्ड में दिया है.
ऊदल , आल्हा का छोटा भाई, युद्ध का प्रेमी और बहुत ही प्रतापी था। अधिकांष युद्धों का जन्मदाता यही बतलाया जाता है। इसके घेड़े का नमा बेंदुल था। बेंदुल देवराज इन्द्र के रथ का प्रधान घोड़ा था। इसक अतिरिक्त चार घोड़े और इन्द्र के रथ में जोते जाते थे जिन्हे ऊदल धरा पर उतार लाया था। इसकी भी एक रोचक कहानी है। - ‘‘कहा जाता है कि देवराज हन्द्र मल्हना से प्यार करता था। इन्द्रसान से वह अपने रथ द्वारा नित्य रात धरती पर आता था। ऊदल ने एक रात उसे देख लिया और जब वह रथ लेकर उड़ने को हुआ , ऊदल रथ का धुरा पकड़ कर उड़ गया। वहां पहुंच कर इन्द्र जब रथ से उतरा, ऊदल सामने खड़ा हो गया। अपनी मर्यादा बचाने के लिए इन्द्र ने ऊदल के ही कथ्नानुसार अपने पांचों घोडे़ जो उसके रथ में जुते थे दे दिये। पृथ्वी पर उतर कर जब घोड़ों सहित गंगा नदी पार करने लगा तो पैर में चोट लग जाने के कारण एक घोड़ा बह गया। उसका नाम संडला था और वह नैनागढ़ जिसे चुनार कहते है किले से जा लगा। वहां के राजा इन्दमणि ने उसे रख लिया। बाद में वह पुनः महोबे को लाया गया और आल्हा का बेटा ईन्दल उस पर सवारी करने लगा। ऊदल वीरता के साथ-साथ देखने में भी बड़ा सुन्दर था। नरवरगढ़ की राज कन्या फुलवा कुछ पुराने संबंध के कारण सेनवा की शादी में नैनागढ़ गयी थी। द्वार पूजा के समय उसने ऊदल को दख तो रीझ गयी। अन्त में कई बार युद्ध करने पर ऊदल को उसे अपना बनाना पड़ा । ऊदल में धैर्य कम था। वह किसी भी कार्य को पूर्ण करने के हतु शीघ्र ही शपथ ले लेता था। फिर भी अन्य वीरों की सतर्कता से उसकी कोई भी प्रतिज्ञा विफल नही हुई। युद्ध में ही इसका जीवन समाप्त हो गया। इसका मुख्य अस्त्र तलवार था।
आल्हा और ऊदल के मार्के और उसको कारनामे एक चन्देली कवि ने शायद उन्हीं के जमाने में गाये, और उसको इस सूबे में जो लोकप्रियता प्राप्त है वह शायद रामायण को भी न हो। यह कविता आल्हा ही के नाम से प्रसिद्ध है और आठ-नौ शताब्दियॉँ गुजर जाने के बावजूद उसकी दिलचस्पी और सर्वप्रियता में अन्तर नहीं आया। आल्हा गाने का इस प्रदेश मे बड़ा रिवाज है। देहात में लोग हजारों की संख्या में आल्हा सुनने के लिए जमा होते हैं। शहरों में भी कभी-कभी यह मण्डलियॉँ दिखाई दे जाती हैं।
बड़े लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण में यह किस्सा अधिक लोकप्रिय है। किसी मजलिस में जाइए हजारों आदमी जमीन के फर्श पर बैठे हुए हैं, सारी महाफिल जैसे बेसुध हो रही है और आल्हा गाने वाला किसी मोढ़े पर बैठा हुआ आपनी अलाप सुना रहा है। उसकी आवज आवश्यकतानुसार कभी ऊँची हो जाती है और कभी मद्धिम, मगर जब वह किसी लड़ाई और उसकी तैयारियों का जिक्र करने लगता है तो शब्दों का प्रवाह, उसके हाथों और भावों के इशारे, ढोल की मर्दाना लय उन पर वीरतापूर्ण शब्दों का चुस्ती से बैठना, जो जड़ाई की कविताओं ही की अपनी एक विशेषता है, यह सब चीजें मिलकर सुनने वालों के दिलों में मर्दाना जोश की एक उमंग सी पैदा कर देती हैं।
बयान करने का तर्ज ऐसा सादा और दिलचस्प और जबान ऐसी आमफहम है कि उसके समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। वर्णन और भावों की सादगी, कला के सौंदर्य का प्राण है।
इसी किस्से की एक बानगी देखिये --
राजा परमालदेव चन्देल खानदान का आखिरी राजा था। तेरहवीं शाताब्दी के आरम्भ में वह खानदान समाप्त हो गया। महोबा जो एक मामूली कस्बा है उस जमाने में चन्देलों की राजधानी था। महोबा की सल्तनत दिल्ली और कन्नौज से आंखें मिलाती थी।
आल्हा और ऊदल इसी राजा परमालदेव के दरबार के सम्मनित सदस्य थे। यह दोनों भाई अभी बच्चे ही थे कि उनका बाप जसराज एक लड़ाई में मारा गया। राजा को अनाथों पर तरस आया, उन्हें राजमहल में ले आये और मोहब्बत के साथ अपनी रानी मलिनहा के सुपुर्द कर दिया। रानी ने उन दोनों भाइयों की परवरिश और लालन-पालन अपने लड़के की तरह किया। जवान होकर यही दोनों भाई बहादुरी में सारी दुनिया में मशहूर हुए। इन्हीं दिलावरों के कारनामों ने महोबे का नाम रोशन कर दिया है।
आल्हा और ऊदल राजा परमालदेव पर जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रानी मलिनहा ने उन्हें पाला, उनकी शादियां कीं, उन्हें गोद में खिलाया। नमक के हक के साथ-साथ इन एहसानों और सम्बन्धों ने दोनों भाइयों को चन्देल राजा का जॉँनिसार रखवाला और राजा परमालदेव का वफादार सेवक बना दिया था। उनकी वीरता के कारण आस-पास के सैकडों घमंडी राजा चन्देलों के अधीन हो गये। महोबा राज्य की सीमाएँ नदी की बाढ़ की तरह फैलने लगीं और चन्देलों की शक्ति दूज के चॉँद से बढ़कर पूरनमासी का चॉँद हो गई।
यह दोनों वीर कभी चैन से न बैठते थे। रणक्षेत्र में अपने हाथ का जौहर दिखाने की उन्हें धुन थी। सुख-सेज पर उन्हें नींद न आती थी। और वह जमाना भी ऐसा ही बेचैनियों से भरा हुआ था। उस जमाने में चैन से बैठना दुनिया के परदे से मिट जाना था। बात-बात पर तलवांरें चलतीं और खून की नदियॉँ बहती थीं। यहॉँ तक कि शादियाँ भी खूनी लड़ाइयों जैसी हो गई थीं। लड़की पैदा हुई और शामत आ गई। हजारों सिपाहियों, सरदारों और सम्बन्धियो- की जानें दहेज में देनी पड़ती थीं। आल्हा और ऊदल उस पुरशोर जमाने की यच्ची तस्वीरें हैं और गोकि ऐसी हालतों ओर जमाने के साथ जो नैतिक दुर्बलताएँ- और विषमताएँ पाई जाती हैं, उनके असर से वह भी बचे हुए नहीं हैं, मगर उनकी दुर्बलताएँ- उनका कसूर नहीं बल्कि उनके जमाने का कसूर हैं।
आल्हा का मामा माहिल एक काले दिल का, मन में द्वेष पालने वाला आदमी था। इन दोनों भाइयों का प्रताप और ऐश्वर्य उसके हृदय में कॉँटे की तरह खटका करता था। उसकी जिन्दगी की सबसे बड़ी आरजू यह थी कि उनके बड़प्पन को किसी तरह खाक में मिला दे। इसी नेक काम के लिए उसने अपनी जिन्दगी न्यौछावर कर दी थी। सैंकड़ों वार किये, सैंकड़ों बार आग लगायी, यहॉँ तक कि आखिरकार उसकी नशा पैदा करनेवाली मंत्रणाओं ने राजा परमाल को मतवाला कर दिया। लोहा भी पानी से कट जाता है। एक रोज राजा परमाल दरबार में अकेले बैठे हुए थे कि माहिल आया। राजा ने उसे उदास देखकर पूछा, भइया, तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ है। माहिल की आँखों में आँसू आ गये। मक्कार आदमी को अपनी भावनाओं पर जो अधिकार होता है वह किसी बड़े योगी के लिए भी कठिन है। उसका दिल रोता है मगर होंठ हँसते हैं, दिल खुशियों के मजे लेता है मगर आँखें रोती हैं, दिल डाह की आग से जलता है मगर जबान से शहद और शक्कर की नदियॉँ बहती हैं। माहिल बोला-महारा- , आपकी छाया में रहकर मुझे दुनिया में अब किसी चीज की इच्छा बाकी नहीं मगर जिन लोगों को आपने धूल से उठाकर आसमान पर पहुँचा दिया और जो आपकी कृपा से आज बड़े प्रताप और ऐश्वर्यवाल- बन गये, उनकी कृतघ्रता और उपद्रव खड़े करना मेरे लिए बड़े दु:ख का कारण हो रही है। परमाल ने आश्चर्य से पूछा- क्या मेरा नमक खानेवालों में ऐसे भी लोग हैं? माहिल- महाराज, मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका हृदय कृपा का सागर है मगर उसमें एक खूंखार घड़ियाल आ घुसा है। -वह कौन है? -मैं।
परमाल ने आश्चर्य से पूछा-तुम! माहिल- हॉँ महाराज, वह अभागा व्यक्ति मैं ही हूँ। मैं आज खुद अपनी फरियाद लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अपने सम्बन्धियो- के प्रति मेरा जो कर्तव्य है वह उस भक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं जो मुझे आपके प्रति है। आल्हा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उसका मांस मेरा मांस और उसका रक्त मेरा रक्त है। मगर अपने शरीर में जो रोग पैदा हो जाता है उसे विवश होकर हकीम से कहना पड़ता है। आल्हा अपनी दौलत के नशे में चूर हो रहा है। उसके दिल में यह झूठा खयाल पैदा हो गया है कि मेरे ही बाहु-बल से यह राज्य कायम है। राजा परमाल की आंखें लाल हो गयीं, बोला-आल्हा को मैंने हमेशा अपना लड़का समझा है। माहिल - लड़के से ज्यादा। परमाल - वह अनाथ था, कोई उसका संरक्षक न था। मैंने उसका पालन-पोषण किया, उसे गोद में खिलाया। मैंने उसे जागीरें दीं, उसे अपनी फौज का सिपहसालार बनाया। उसकी शादी में मैंने बीस हजार चन्देल सूरमाओं का खून बहा दिया। उसकी मॉँ और मेरी मलिनहा वर्षों गले मिलकर सोई हैं और आल्हा क्या मेरे एहसानों को भूल सकता है?
माहिल , मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता। माहिल का चेहरा पीला पड़ गया। मगर सम्हलकर बोला- महाराज, मेरी जबान से कभी झूठ बात नहीं निकली। परमाल - मुझे कैसे विश्वास हो? महिल ने धीरे से राजा के कान में कुछ कह दिया। आल्हा और ऊदल दोनों चौगान के खेल का अभ्यास कर रहे थे। लम्बे-चौड़- मैदान में हजारों आदमी इस तमाशे को देख रहे थे। गेंद किसी अभागे की तरह इधर-उधर ठोकरें खाता फिरता था। चोबदार ने आकर कहा-महाराज ने याद फरमाया है। आल्हा को सन्देह हुआ। महाराज ने आज बेवक्त क्यों याद किया? खेल बन्द हो गया। गेंद को ठोकरों से छुट्टी मिली। फौरन दरबार मे चौबदार के साथ हाजिर हुआ और झुककर आदाब बजा लाया। परमाल - ने कहा- मैं तुमसे कुछ मॉँगूँ? दोगे? आल्हा ने सादगी से जवाब दिया फरमाइए
आल्हा - ने कनखियों से माहिल की तरफ देखा समझ गया कि इस वक्त कुछ न कुछ दाल में काला है। इसके चेहरे पर यह मुस्कराहट क्यों ? गूलर में यह फूल क्यों लगे ? क्या मेरी वफादारी का इम्तहान लिया जा रहा है ?
जोश से बोला महाराज , मैं आपकी जबान से ऐसे सवाल सुनने का आदी नहीं हूँ। आप मेरे संरक्षक, मेरे पालनहार, मेरे राजा हैं। आपकी भँवों के इशारे पर मैं आग में कूद सकता हूँ और मौत से लड़ सकता हूँ। आपकी आज्ञा पाकर में असम्भव को सम्भव बना सकता हूँ आप मुझसे ऐसे सवाल न करें।
परमाल - शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद है। आल्हा- मुझे क्या हुक्म मिलता है ?
परमाल- तुम्हारे पास नाहर घोड़ा है ?
आल्हा ने ‘जी हॉँ’ कहकर माहिल की तरफ भयानक गुस्से भरी हुई आँखों से देखा। परमाल- - अगर तुम्हें बुरा न लगे तो उसे मेरी सवारी के लिए दे दो। आल्हा कुछ जवाब न दे सका, सोचने लगा, मैंने अभी वादा किया है कि इनकार न करूँगा। मैंने बात हारी है। मुझे इनकार न करना चाहिए। निश्चय ही इस वक्त मेरी स्वामीभक्ति की परीक्षा ली जा रही है। मेरा इनकार इस समय बहुत बेमौका और खतरनाक है। इसका तो कुछ गम नहीं। मगर मैं इनकार किस मुँह से करूँ, बेवफा न कहलाऊँगा? मेरा और राजा का सम्बन्ध केवल स्वामी और सेवक का ही नहीं है, मैं उनकी गोद में खेला हूँ। जब मेरे हाथ कमजोर थे, और पॉँव में खड़े होने का बूता न था, तब उन्होंने मेरे जुल्म सहे हैं, क्या मैं इनकार कर सकता हूँ ? विचारो की धारा मुड़ी- माना कि राजा के एहसान मुझ पर अनगिनती हैं मेरे शरीर का एक-एक रोआँ उनके एहसानों के बोझ से दबा हुआ है मगर क्षत्रिय कभी अपनी सवारी का घोड़ा दूसरे को नहीं देता। यह क्षत्रियों- का धर्म नहीं। मैं राजा का पाला हुआ और एहसानमन्द हूँ। मुझे अपने शरीर पर अधिकार है। उसे मैं राजा पर न्यौछावर कर सकता हूँ। मगर राजपूती धर्म पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उसे मैं नहीं तोड़ सकता।
जिन लोगों ने धर्म के कच्चे धागे को लोहे की दीवार समझा है, उन्हीं से राजपूतों का नाम चमक रहा है। क्या मैं हमेशा के लिए अपने ऊपर दाग लगाऊँ? आह! माहिल ने इस वक्त मुझे खूब जकड़ रखा है। सामने खूंखार शेर है; पीछे गहरी खाई। या तो अपमान उठाऊँ या कृतघ्न कहलाऊँ। या तो राजपूतों के नाम को डुबोऊँ या बर्बाद हो जॉँऊ। खैर, जो ईश्वर की मर्जी, मुझे कृतघ्न कहलाना स्वीकार है, मगर अपमानित होना स्वीकार नहीं। बर्बाद हो जाना मंजूर है, मगर राजपूतों के धर्म में बट्टा लगाना मंजूर नहीं। आल्ह- सर नीचा किये इन्हीं खयालों में गोते खा रहा था। यह उसके लिए परीक्षा की घड़ी थी जिसमें सफल हो जाने पर उसका भविष्य निर्भर था। मगर माहिल के लिए यह मौका उसके धीरज की कम परीक्षा लेने वाला न था। वह दिन अब आ गया जिसके इन्तजार में कभी आँखें नहीं थकीं। खुशियों की यह बाढ़ अब संयम की लोहे की दीवार को काटती जाती थी। सिद्ध योगी पर दुर्बल मनुष्य की विजय होती जाती थी। एकाएक परमाल ने आल्हा से बुलन्द आवाज में पूछा- किस दुविधा में हो? क्या नहीं देना चाहते?
आल्हा ने राजा से आंखें मिलाकर कहा-जी नहीं। परमाल- को तैश आ गया, कड़ककर बोला-क्यों?- आल्हा ने अविचल मन से उत्तर दिया-यह राजपूतों का धर्म नहीं है। परमाल-कया मेरे एहसानों का यही बदला है? तुम जानते हो, पहले तुम क्या थे और अब क्या हो? आल्हा-जी हॉँ, जानता हूँ। परमाल- तुम्हें मैंने बनाया है और मैं ही बिगाड़ सकता हूँ। आल्हा से अब सब्र न हो सका, उसकी आँखें लाल हो गयीं और त्योरियों पर बल पड़ गये। तेज लहजे में बोला- महाराज, आपने मेरे ऊपर जो एहसान किए, उनका मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। क्षत्रिय कभी एहसान नहीं भूलता। मगर आपने मेरे ऊपर एहसान किए हैं, तो मैंने भी जो तोड़कर आपकी सेवा की है। सिर्फ नौकरी और नामक का हक अदा करने का भाव मुझमें वह निष्ठा और गर्मी नहीं पैदा कर सकता जिसका मैं बार-बार परिचय दे चुका हूँ। मगर खैर, अब मुझे विश्वास हो गया कि इस दरबार में मेरा गुजर न होगा। मेरा आखिरी सलाम कबूल हो और अपनी नादानी से मैंने जो कुछ भूल की है वह माफ की जाए। माहिल की ओर देखकर उसने कहा- मामा जी, आज से मेरे और आपके बीच खून का रिश्ता टूटता है। आप मेरे खून के प्यासे हैं तो मैं भी आपकी जान का दुश्मन हूँ। आल्हा की मॉँ का नाम देवल देवी था। उसकी गिनती उन हौसले वाली उच्च विचार स्त्रियों में है जिन्होंने हिन्दोस्तान के पिछले कारनामों को इतना स्पृहणीय बना दिया है। उस अंधेरे युग में भी जबकि आपसी फूट और बैर की एक भयानक बाढ़ मुल्क में आ पहुँची थी, हिन्दोस्तान में ऐसी ऐसी देवियॉँ पैदा हुई जो इतिहास के अंधेरे से अंधेरे पन्नों को भी ज्योतित कर सकती हैं। देवल देवी से सुना कि आल्हा ने अपनी आन को रखने के लिए क्या किया तो उसकी आखों भर आए। उसने दोनों भाइयों को गले लगाकर कहा- बेटा ,तुमने वही किया जो राजपूतों का धर्म था। मैं बड़ी भाग्यशालिन हूँ कि तुम जैसे दो बात की लाज रखने वाले बेटे पाये हैं । उसी रोज दोनों भाइयों महोबा से कूच कर दिया अपने साथ अपनी तलवार और घोड़ो के सिवा और कुछ न लिया। माल –असबाब सब वहीं छोड़ दिये सिपाही की दौलत और इज्जत सबक कुछ उसकी तलवार है। जिसके पास वीरता की सम्पति है उसे दूसरी किसी सम्पति की जरुरत नहीं। बरसात के दिन थे, नदी नाले उमड़े हुए थे। इन्द्र की उदारताओं से मालामाल होकर जमीन फूली नहीं समाती थी । पेड़ो पर मोरों की रसीली झनकारे सुनाई देती थीं और खेतों में निश्चिन्तत की शराब से मतवाल किसान मल्हार की तानें अलाप रहे थे । पहाड़ियों की घनी हरियावल पानी की दर्पन –जैसी सतह और जगंली बेल बूटों के बनाव संवार से प्रकृति पर एक यौवन बरस रहा था।
मैदानों की ठंडी-ठडीं मस्त हवा जंगली फूलों की मीठी मीठी, सुहानी, आत्मा को उल्लास देनेवाली महक और खेतों की लहराती हुई रंग बिरंगी उपज ने दिलो में आरजुओं का एक तूफान उठा दिया था। ऐसे मुबारक मौसम में आल्हा ने महोबा को आखिरी सलाम किया । दोनों भाइयो की आँखे रोते रोते लाल हो गयी थीं क्योंकि आज उनसे उनका देश छूट रहा था । इन्हीं गलियों में उन्होंने घुटने के बल चलना सीखा था, इन्ही तालाबों में कागज की नावें चलाई थीं, यही जवानी की बेफिक्रियो- के मजे लूटे थे।
इनसे अब हमेशा के लिए नाता टूटता था। दोनो भाई आगे बढते जाते थे , मगर बहुत धीरे-धीरे । यह खयाल था कि शायद परमाल ने रुठनेवालों- को मनाने के लिए अपना कोई भरोसे का आदमी भेजा होगा। घोड़ो को सम्हाले हुए थे, मगर जब महोबे की पहाड़ियो का आखिरी निशान ऑंखों से ओझल हो गया तो उम्मीद की आखिरी झलक भी गायब हो गयी। उन्होनें जिनका कोई देश नथा एक ठंडी सांस ली और घोडे बढा दिये।
उनके निर्वासन का समाचार बहुत जल्द चारों तरफ फैल गया। उनके लिए हर दरबार में जगह थीं, चारों तरफ से राजाओ के सदेश आने लगे। कन्नौज के राजा जयचन्द ने अपने राजकुमार को उनसे मिलने के लिए भेजा। संदेशों से जो काम न निकला वह इस मुलाकात ने पूरा कर दिया। राजकुमार की खातिदारिया और आवभगत दोनों भाइयों को कन्नौज खींच ले नई। जयचन्द आंखें बिछाये बैठा था। आल्हा को अपना सेनापति बना दिया।
आल्हा और ऊदल के चले जाने के बाद महोबे में तरह-तरह के अंधेर शुरु हुए। परमाल कमजी शासक था। मातहत राजाओं ने बगावत का झण्डा बुलन्द किया। ऐसी कोई ताकत न रही जो उन झगड़ालू लोगों को वश में रख सके। दिल्ली के राज पृथ्वीराज की कुछ सेना सिमता से एक सफल लड़ाई लड़कर वापस आ रही थी। महोबे में पड़ाव किया। अक्खड़ सिपाहियों में तलवार चलते कितनी देर लगती है। चाहे राजा परमाल के मुलाजियों की ज्यादती हो चाहे चौहान सिपाहियों की, तनीजा यह हुआ कि चन्देलों और चौहानों में अनबन हो गई। लड़ाई छिड़ गई।
चौहान संख्या में कम थे। चंदेलों ने आतिथ्य-सत्कार के नियमों को एक किनारे रखकर चौहानों के खून से अपना कलेजा ठंडा किया और यह न समझे कि मुठ्ठी भर सिपाहियों के पीछे सारे देश पर विपत्ति आ जाएगी। बेगुनाहों को खून रंग लायेगा। पृथ्वीराज को यह दिल तोड़ने वाली खबर मिली तो उसके गुस्से की कोई हद न रही। ऑंधी की तरह महोबे पर चढ़ दौड़ा और सिरको, जो इलाका महोबे का एक मशहूर कस्बा था, तबाह करके महोबे की तरह बढ़ा। चन्देलों ने भी फौज खड़ी की। मगर पहले ही मुकाबिले में उनके हौसले पस्त हो गये। आल्हा-ऊदल के बगैर फौज बिन दूल्हे की बारात थी। सारी फौज तितर-बितर हो गयी। देश में तहलका मच गया।
अब किसी क्षण पृथ्वीराज महोबे में आ पहुँचेगा, इस डर से लोगों के हाथ-पॉँव फूल गये। परमाल अपने किये पर बहुत पछताया। मगर अब पछताना व्यर्थ था। कोई चारा न देखकर उसने पृथ्वीराज से एक महीने की सन्धि की प्रार्थना की। चौहान राजा युद्ध के नियमों को कभी हाथ से न जाने देता था। उसकी वीरता उसे कमजोर, बेखबर और नामुस्तैद दुश्मन पर वार करने की इजाजत न देती थी। इस मामले में अगर वह इन नियमों को इतनी सख्ती से पाबन्द न होता तो शहाबुद्दीन के हाथों उसे वह बुरा दिन न देखना पड़ता। उसकी बहादुरी ही उसकी जान की गाहक हुई।
उसने परमाल का पैगाम मंजूर कर लिया। चन्देलों की जान में जान आई। अब सलाह-मशविरा होने लगा कि पृथ्वीराज से क्योंकर मुकाबिला किया जाये। रानी मलिनहा भी इस मशविरे में शरीक थीं। किसी ने कहा, महोबे के चारों तरफ एक ऊँची दीवार बनायी जाय ; कोई बोला, हम लोग महोबे को वीरान करके दक्खिन को ओर चलें। परमाल जबान से तो कुछ न कहता था, मगर समर्पण के सिवा उसे और कोई चारा न दिखाई पड़ता था।
तब रानी मलिनहा खड़ी होकर बोली : ‘चन्देल वंश के राजपूतो, तुम कैसी बच्चों की-सी बातें करते हो? क्या दीवार खड़ी करके तुम दुश्मन को रोक लोगे? झाडू से कहीं ऑंधी रुकती है ! तुम महोबे को वीरान करके भागने की सलाह देते हो। ऐसी कायरों जैसी सलाह औरतें दिया करती हैं। तुम्हारी सारी बहादुरी और जान पर खेलना अब कहॉँ गया? अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि चन्देलों के नाम से राजे थर्राते थे। चन्देलों की धाक बंधी हुई थी, तुमने कुछ ही सालों में सैंकड़ों मैदान जीते, तुम्हें कभी हार नहीं हुई। तुम्हारी तलवार की दमक कभी मन्द नहीं हुई। तुम अब भी वही हो, मगर तुममें अब वह पुरुषार्थ नहीं है।
वह पुरुषार्थ बनाफल वंश के साथ महोबे से उठ गया। देवल देवी के रुठने से चण्डिका देवी भी हमसे रुठ गई। अब अगर कोई यह हारी हुई बाजी सम्हाल सकता है तो वह आल्हा है। वही दोनों भाई इस नाजुक वक्त में तुम्हें बचा सकते हैं। उन्हीं को मनाओ, उन्हीं को समझाओं, उन पर महोते के बहुत हक हैं। महोबे की मिट्टी और पानी से उनकी परवरिश हुई है। वह महोबे के हक कभी भूल नहीं सकते, उन्हें ईश्वर ने बल और विद्या दी है, वही इस समय विजय का बीड़ा उठा सकते हैं।’ रानी मलिनहा की बातें लोगों के दिलों में बैठ गयीं। जगना भाट आल्हा और ऊदल को कन्नौज से लाने के लिए रवाना हुआ। यह दोनों भाई राजकुँवर लाखन के साथ शिकार खेलने जा रहे थे कि जगना ने पहुँचकर प्रणाम किया। उसके चेहरे से परेशानी और झिझक बरस रही थी। आल्हा ने घबराकर पूछा—कवीश्वर, यहॉँ कैसे भूल पड़े? महोबे में तो खैरियत है? हम गरीबों को क्योंकर याद किया? जगना की ऑंखों में ऑंसू भर जाए, बोला—अगर खैरियत होती तो तुम्हारी शरण में क्यों आता। मुसीबत पड़ने पर ही देवताओं की याद आती है। महोबे पर इस वक्त इन्द्र का कोप छाया हुआ है। पृथ्वीराज चौहान महोबे को घेरे पड़ा है। नरसिंह और वीरसिंह तलवारों की भेंट हो चुके है। सिरकों सारा राख को ढेर हो गया। चन्देलों का राज वीरान हुआ जाता है। सारे देश में कुहराम मचा हुआ है।
बड़ी मुश्किलों से एक महीने की मौहलत ली गई है और मुझे राजा परमाल ने तुम्हारे पास भेजा है। इस मुसीबत के वक्त हमारा कोई मददगार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी किम्मत बॅंधाये। जब से तुमने महोबे से नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हिम्मत बँधाये। जब से तुमने महोबे से नाता तोड़ा है तब से राजा परमाल के होंठों पर हँसी नहीं आई। जिस परमाल को उदास देखकर तुम बेचैन हो जाते थे उसी परमाल की ऑंखें महीनों से नींद को तरसती हैं।
रानी महिलना, जिसकी गोद में तुम खेले हो, रात-दिन तुम्हारी याद में रोती रहती है। वह अपने झरोखें से कन्नैज की तरफ ऑंखें लगाये तुम्हारी राह देखा करती है। ऐ बनाफल वंश के सपूतो ! चन्देलों की नाव अब डूब रही है। चन्देलों का नाम अब मिटा जाता है। अब मौका है कि तुम तलवारे हाथ में लो। अगर इस मौके पर तुमने डूबती हुई नाव को न सम्हाला तो तुम्हें हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा क्योंकि इस नाम के साथ तुम्हारा और तुम्हारे नामी बाप का नाम भी डूब जाएगा।
आल्हा ने रुखेपन से जवाब दिया—हमें इसकी अब कुछ परवाह नहीं है। हमारा और हमारे बाप का नाम तो उसी दिन डूब गया, जब हम बेकसूर महोबे से निकाल दिए गए। महोबा मिट्टी में मिल जाय, चन्देलों को चिराग गुल हो जाय, अब हमें जरा भी परवाह नहीं है। क्या हमारी सेवाओं का यही पुरस्कार था जो हमको दिया गया? हमारे बाप ने महोबे पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिये, हमने गोड़ों को हराया और चन्देलों को देवगढ़ का मालिक बना दिया। हमने यादवों से लोहा लिया और कठियार के मैदान में चन्देलों का झंडा गाड़ दिया।
मैंने इन्ही हाथों से कछवाहों की बढ़ती हुई लहर को रोका। गया का मैदान हमीं ने जीता, रीवॉँ का घमण्ड हमीं ने तोड़ा। मैंने ही मेवात से खिराज लिया। हमने यह सब कुछ किया और इसका हमको यह पुरस्कार दिया गया है? मेरे बाप ने दस राजाओं को गुलामी का तौक पहनाया। मैंने परमाल की सेवा में सात बार प्राणलेवा जख्म खाए, तीन बार मौत के मुँह से निकल आया। मैने चालीस लड़ाइयॉँ लड़ी और कभी हारकर न आया। ऊदल ने सात खूनी मार्के जीते। हमने चन्देलों की बहादुरी का डंका बजा दिया। चन्देलों का नाम हमने आसमान तक पहुँचा दिया और इसके यह पुरस्कार हमको मिला है? परमाल अब क्यों उसी दगाबाज माहिल को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाते जिसकों खुश करने के लिए मेरा देश निकाला हुआ था !
जगना ने जवाब दिया—आल्हा ! यह राजपूतों की बातें नहीं हैं। तुम्हारे बाप ने जिस राज पर प्राण न्यौछावर कर दिये वही राज अब दुश्मन के पांव तले रौंदा जा रहा है। उसी बाप के बेटे होकर भी क्या तुम्हारे खून में जोश नहीं आता? वह राजपूत जो अपने मुसीबत में पड़े हुए राजा को छोड़ता है, उसके लिए नरक की आग के सिवा और कोई जगह नहीं है। तुम्हारी मातृभूमि पर बर्बादी की घटा छायी हुई हैं। तुम्हारी माऍं और बहनें दुश्मनों की आबरु लूटनेवाली निगाहों को निशाना बन रही है, क्या अब भी तुम्हारे खून में जोश नहीं आता? अपने देश की यह दुर्गत देखकर भी तुम कन्नौज में चैन की नींद सो सकते हो?
देवल देवी को जगना के आने की खबर हुई। असने फौरन आल्हा को बुलाकर कहा—बेटा, पिछली बातें भूल जाओं और आज ही महोबे चलने की तैयारी करो। आल्हा कुछ जबाव न दे सका, मगर ऊदल झुँझलाकर बोला—हम अब महोबे नहीं जा सकते। क्या तुम वह दिन भूल गये जब हम कुत्तों की तरह महोबे से निकाल दिए गए? महोबा डूबे या रहे, हमारा जी उससे भर गया, अब उसको देखने की इच्छा नहीं हे। अब कन्नौज ही हमारी मातृभूमि है।
राजपूतनी बेटे की जबान से यह पाप की बात न सुन सकी, तैश में आकर बोली—ऊदल, तुझे ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए शर्म नहीं आती ? काश, ईश्वर मुझे बॉँझ ही रखता कि ऐसे बेटों की मॉँ न बनती। क्या इन्हीं बनाफल वंश के नाम पर कलंक लगानेवालों के लिए मैंने गर्भ की पीड़ा सही थी? नालायको, मेरे सामने से दूर हो जाओं। मुझे अपना मुँह न दिखाओं। तुम जसराज के बेटे नहीं हो, तुम जिसकी रान से पैदा हुए हो वह जसराज नहीं हो सकता।
यह मर्मान्तक चोट थी। शर्म से दोनों भाइयों के माथे पर पसीना आ गया। दोनों उठ खड़े हुए और बोले- माता, अब बस करो, हम ज्यादा नहीं सुन सकते, हम आज ही महोबे जायेंगे और राजा परमाल की खिदमत में अपना खून बहायेंगे। हम रणक्षेत्र में अपनी तलवारों की चमक से अपने बाप का नाम रोशन करेंगे। हम चौहान के मुकाबिले में अपनी बहादुरी के जौहर दिखायेंगे और देवल देवी के बेटों का नाम अमर कर देंगे।
दोनों भाई कन्नौज से चले, देवल भी साथ थी। जब वह रुठनेवाले अपनी मातृभूमि में पहुँचे तो सूखें धानों में पानी पड़ गया, टूटी हुई हिम्मतें बंध गयीं। एक लाख चन्देल इन वीरों की अगवानी करने के लिए खड़े थे। बहुत दिनों के बाद वह अपनी मातृभूमि से बिछुड़े हुए इन दोनों भाइयों से मिले। ऑंखों ने खुशी के ऑंसू बहाए। राजा परमाल उनके आने की खबर पाते ही कीरत सागर तक पैदल आया। आल्हा और ऊदल दौड़कर उसके पांव से लिपट गए। तीनों की आंखों से पानी बरसा और सारा मनमुटाव धुल गया।
दुश्मन सर पर खड़ा था, ज्यादा आतिथ्य-सत्कार का मौकर न था, वहीं कीरत सागर के किनारे देश के नेताओं और दरबार के कर्मचारियों की राय से आल्हा फौज का सेनापति बनाया गया। वहीं मरने-मारने के लिए सौगन्धें खाई गई। वहीं बहादुरों ने कसमें खाई कि मैदान से हटेंगे तो मरकर हटेंगें। वहीं लोग एक दूसरे के गले मिले और अपनी किस्मतों को फैसला करने चले। आज किसी की ऑंखों में और चेहरे पर उदासी के चिन्ह न थे, औरतें हॅंस-हँस कर अपने प्यारों को विदा करती थीं, मर्द हँस-हँसकर स्त्रियों से अलग होते थे क्योंकि यह आखिरी बाजी है, इसे जीतना जिन्दगी और हारना मौत है।
उस जगह के पास जहॉँ अब और कोई कस्बा आबाद है, दोनों फौजों को मुकाबला हुआ और अठारह दिन तक मारकाट का बाजार गर्म रहा। खूब घमासान लड़ाई हुई। पृथ्वीराज खुद लड़ाई में शरीक था। दोनों दल दिल खोलकर लड़े। वीरों ने खूब अरमान निकाले और दोनों तरफ की फौजें वहीं कट मरीं। तीन लाख आदमियों में सिर्फ तीन आदमी जिन्दा बचे-एक पृथ्वीराज, दूसरा चन्दा भाट तीसरा आल्हा। प्रथ्वीराज के शब्द भेदी बाण से उदल की मौत हुई ।
उदल की मौत से आल्हा समझ गया की इस धरती से जाने का समय आ गया है। उसने अपने गुरू गोरखनाथ जी का दिया हुया बिजुरिया नामक दिव्याश्त्र हाथ मे लेकर प्रथ्वीराज को मारने चल पड़े। आल्हा को आता देखकर प्रथ्वीराज का सेनापति चंदरबरदई ने प्रथ्वीराज से कहा राजा आल्हा के समान इस धरती पर कोई दूसरा वीर नहीं है यदि ज़िंदा रहना चाहते हो तो आल्हा के सामने हतियार मत उठाना। प्रथ्वीराज ने आल्हा के सामने हाथ जोड़ लिए ।
इसी समय वहाँ पर गुरु गोरखनाथ आगाए उन्होने आल्हा से कहा ये दिव्यास्त्र धरती के साधारण मनुस्यों पर चलाने के लिए नहीं है और बे आल्हा को अपने साथ सा शरीर स्वर्ग ले गए।
इसका असली लुत्फ़ सुनकर ही आ सकता है
आल्हा ऊदल का वीडियो सुनिए यहाँ पर
बैरागढ़ अकोढ़ी गाँव ज़िला जालौन मे आल्हा की गाड़ी हुई एक सांग आज भी है। जो माता शारदा के मंदिर के प्रांगड़ मे है। माता के मंदिर मे आज भी सुबह पुजारियों को दरवाजे खोलने पर दो फूल चढ़े मिलते है। कहते है ये फूल आल्हा चढ़ाते है। काफी लोगों ने सच्चाई पता करने की कोसिस की। लेकिन जो रात मे मंदिर मे रुका बो सुबह ज़िंदा नहीं मिला। आप भी जाकर सच्चाई पता कर सकते है।
ऐसी भयानक अटल और निर्णायक लड़ाई शायद ही किसी देश और किसी युग में हुई हो। दोनों ही हारे और दोनों ही जीते। चन्देल और चौहान हमेशा के लिए खाक में मिल गए क्योंकि थानेसर की लड़ाई का फैसला भी इसी मैदान में हो गया। चौहानों में जितने अनुभवी सिपाही थे, वह सब औरई में काम आए। शहाबुद्दीन से मुकाबला पड़ा तो नौसिखिये, अनुभवहीन सिपाही मैदान में लाये गये और नतीजा वही हुआ जो हो सकता था।
दक्षराज और देवल देवी के बड़े पुत्र आल्हा को पौराणिक परंपराओं में युधिष्ठिर का अवतार माना गया है। अतुलित बल के स्वामी होने के बावजूद उन्होंने अपने बल का कभी अमर्यादित प्रदर्शन नहीं किया। आल्हा जिस युग की उपज थे, उसे परंपरागत रूप से सामंती काल कहा जाता है, और ‘जाकर कन्या सुंदर देखी तापर जाइ धरी तरवार’ इस युग का कटु सत्य था, लेकिन इसके बावजूद आल्हा एकपत्नी व्रती रहे।
यहां तक कि चुनारगढ़ की लड़ाई के समय जब राजा नैपाली के पुत्रों जोगा और भोगा ने छल-छद्म से आल्हा को बंदी बना लिया तो राजकुमारी सोनवॉ ने आल्हा के समक्ष चुपके से भाग चलने का प्रस्ताव रखा, जिसे आल्हा ने अस्वीकार कर दिया और एक कुमारी कन्या के हाथ से भोजन ग्रहण करना भी अनुचित समझा। यद्यपि यही सोनवॉ कालांतर में आल्हा की पत्नी बनीं और उनका एक नाम मछला भी प्रचलन में आया, क्योंकि वो रोज मछलियों को दाना खिलाती थीं।
आल्हा और वीर भूमि महोबा एक दूसरे के पर्याय हैं। यहां की सुबह आल्हा से शुरू होती है और उन्हीं से खत्म। यहां नवजात बच्चों के नामकरण भी आल्हखंड के नायकों के नाम पर रखे जाते हैं। कोई भी सामाजिक संस्कार आल्हा की पंक्तियों के बिना पूर्ण नहीं होता। यहां का अपराध जगत भी बहुत कुछ आल्ह खंड से प्रभावित होता है।
कुछ वषरें पहले एक व्यक्ति ने किसी आल्हा गायक को गाते सुना कि ‘जाके बैरी सम्मुख ठाड़े, ताके जीवन को धिक्कार’ तो उसने रात में ही जाकर अपने दुश्मन को गोली मार दी। आल्हा का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि 800 वर्षो के बीत जाने के बावजूद वह आज भी बुंदेलखंड के प्राण स्वरूप हैं।
बुंदेलखंड का जन-जन आज भी चटकारे लेकर गाता है- बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में पानीदार यहां का घोड़ा, आग यहां के पानी में आल्हा-ऊदल गढ़ महुबे के, दिल्ली का चौहान धनी जियत जिंदगी इन दोनों में तीर कमानें रहीं तनी बाण लौट गा शब्दभेद का, दाग लगा चौहानी में पानीदार यहां का पानी, आग यहां के पानी में आल्हा की तरह उनके अनुज ऊदल भी अप्रतिम योद्धा थे।
उन्हें भीम का अवतार माना गया है। संपूर्ण आल्हखंड उनके साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है। उनकी वीरता को देखकर उन्हें बघऊदल कहा जाता है।बैरागढ़ के मैदान में पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडराय, जिसे आल्हखंड में चौड़ा कहा गया है, ने धोखे से ऊदल की हत्या कर दी थी। ऊदल की हत्या के बाद ही चौहान सेना चंदेल योद्धाओं का वध करने में सफल हुई थी। महोबा में इस वीर योद्धा के नाम से एक चौक का नाम ऊदल चौक रखा गया है। ऊदल को आदर देते हुए आज भी लोग इस चौक पर घोड़े से सवार होकर नहीं जाते हैं।
महोबा के अंग्रेज प्रशासक जेम्स ग्रांट ने लिखा है कि ‘एक बार बारात जा रही थी और दूल्हा घोड़े पर बैठा था। जैसे ही बारात ऊदल चौक पहुंची घोड़ा भड़क गया और उसने दूल्हे को उठाकर पटक दिया। मैं परंपरागत रूप से सुनता आया हूं कि ऊदल चौक पर कोई घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकता और आज मैने उसे प्रत्यक्ष देख लिया।’
आल्हा-ऊदल के नाम पर महोबा शहर के ठीक बीचों-बीच दो चौक बनाए गए हैं। यहां आल्हा-ऊदल की दो विशालकाय प्रतिमाएं हैं। आल्हा अपने वाहन गज पशचावद पर सवार हैं। ऊदल अपने उड़न घोड़े बेदुला पर सवार हैं। ये दोनों प्रतिमाएं इतनी भीमकाय और जीवंत हैं कि इन्हें देखने लोग दूर-दूर से आते हैं। कीरत सागर के किनारे आल्हा की चौकी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां आल्हा के गुल्म के सैनिक रहते थे। ऐसी ढेर सारी चौकियां महोबा में आबाद हैं जो सामंती परिवेश की याद दिलाती हैं। आल्हा के पुत्र इंदल की चौकी मदन सागर के बीचों-बीच हैं। इसका संपर्क अथाह जलराशि के नीचे सुरंग के माध्यम से किले से था।
प्रशासन ने अब इस सुरंग को बंद कर दिया है। आल्हखंड के अनुसार इंदल भी अपने पिता आल्हा की तरह अमर माने गए हैं। यह कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने जब यह देखा कि आल्हा अपने दिव्य अस्त्रों से पृथ्वीराज का बध कर देगा तो वे उसे और इंदल लेकर कदली वन चले आए। इस कदली वन की पहचान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तराखंड के तराई इलाकों से की है। आल्हा की उपास्य चंडिका और मनियां देव आज भी महोबा में उसी प्रकार समादृत हैं। चंडिका देवी की उपासना महोबा वासी ही नहीं अपितु संपूर्ण बुंदेलखंड करता है। नवरात्र के अवसर पर यहां सारा बुंदेलखंड उमड़ पड़ता है। आल्हा की सुमरनी इन्हीं चंडिका मां से प्रारंभ होती है।
बुंदेलखंड में विवाह अथवा अन्य मांगलिक कार्यो का प्रथम निमंत्रण मां चंडिका को ही दिया जाता है। चंदेल नरेशों ने महोबा में तीन देवी पीठ बनाए थे- बड़ी चंडिका, छोटी चंडिका और मनियां देव का मंदिर। ये तीनों आज भी उसी प्रकार उपास्य हैं। बड़ी चंडिका इसमें सर्वाधिक भव्य और आदरणीय हैं। इस मंदिर के प्रांगण में शिव कंठ, नृत्यरत गणेश, पंचदेव चौकी और पचास से अधिक सती चिन्ह अन्य आकर्षण हैं। आल्हा का महोबा बारिश में अत्यंत आकर्षक हो जाता है। सावन में गली-कूचे आल्हा की तान से गुंजायमान हो जाते हैं। लेकिन महोबा में सर्वाधिक भीड़ होती है रक्षाबंधन के पर्व पर। यह पर्व यहां कजली महोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
यह उस क्षण की स्मृति है जब महोबा के रणबांकुरों ने पृथ्वीराज को हराकर भगाने पर मजबूर कर दिया था। इस विजय के बाद ही महोबा में बहनों ने भाइयों को राखी बांधी थी। उस घटना को 800 वर्ष बीत गए लेकिन आज भी महोबा में रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा के दिन न मनाकर एक दिन बाद परेवा को मनाया जाता है। इस दिन सारा बुंदेलखंड महोबा में एकत्र हो जाता है। होटलों और धर्मशालाओं की बात छोडि़ए, लोगों के घर भी हाउसफुल हो जाते हैं। यह बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। हवेली दरवाजा, जहां पर 1857 में बागियों को फांसी दी गई थी, वहां से एक जुलूस निकलकर कीरत सागर के तट पर समाप्त होता है, जहां विजय के उपरांत महोबा की बहनों ने आल्हा-ऊदल और अन्य योद्धाओं को राखी बांधी थी।
कीरत सागर के किनारे आल्हा की चौकी जो इस समय एक मंच का रूप ले लेती है और सात दिन तक अहर्निश इस मंच पर बुंदेली नृत्य और गायन का प्रस्तुतीकरण होता रहता है। इस समय खजुराहो में जो विदेशी पर्यटक रहते हैं, वो भी महोबा आ जाते हैं। रहिलिया सागर का सूर्य मंदिर, शिव तांडव, महोबा का दुर्ग, पीर मुबारक भाह की मजार महोबा के अन्य आकर्षण हैं। पीर की मजार पर जियारत के करने के लिए हिंदुस्तान के कोने-कोने से जायरीन आते हैं। जैसे- महोबा का पुरातत्व निखर कर सामने आ रहा है, वैसे-वैसे आल्हा का महोबा खजुराहो और कालिंजर के साथ एक नए पर्यटन त्रिकोण के रूप में उभर रहा है।
जनता में अब तक यही विश्वास है कि वह जिन्दा है। लोग कहते हैं कि वह अमर हो गया। यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि आल्हा सचमुच अमर है अमर है और वह कभी मिट नहीं सकता, उसका नाम हमेशा कायम रहेगा।
कालिंजर के किले का रहस्य
कालिंजर के किले का रहस्य
इतिहास के उतार-चढ़ावों का प्रत्यक्ष गवाह बांदा जनपद का कालिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है। इस किले के नाम जरुर बदलते गये हैं। सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेतायुग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंहलगढ़ और कलियुग में कालिंजर के नाम से ख्याति पायी है।कालिंजर का अपराजेय किला प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति साम्राज्य के अधीन था। जब चंदेल शासक आये तो इस पर मुगल शासक महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने आक्रमण कर इसे जीतना चाहा पर कामयाब नहीं हो पाये। अंत में अकबर ने १५६९ में यह किला जीतकर बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया। बीरबल के बाद यह किला बुंदेले राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। इनके बाद किले पर पन्ना के हरदेव शाह का कब्जा हो गया। १८१२ में यह किला अंग्रेजों के अधीन हो गया।
इस दुर्ग के निर्माण का नाम तो ठीक-ठीक साक्ष्य कहीं नहीं मिलता पर जनश्रुति के मुताबिक चंदेल वंश के संस्थापक चंद्र वर्मा द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कतिपय इतिहासकारों के मुताबिक इस दुर्ग का निर्माण केदार वर्मन द्वारा ईसा की दूसरी से सातवीं शताब्दी के मध्य कराया गया था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इसके द्वारों का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। कालिंजर दुर्ग में प्रवेश के लिए सात द्वार थे। इनमें आलमगीर दरवाजा, गणेश द्वार, चौबुरजी दरवाजा, बुद्धभद्र दरवाजा, हनुमान द्वार, लाल दरवाजा और बारा दरवाजा थे। अब हालत यह है कि समय के साथ सब कुछ बदलता गया। दुर्ग में प्रवेश के लिए तीन द्वार कामता द्वार, रीवां द्वार व पन्नाद्वार है। पन्नाद्वार इस समय बंद है।
छठी शताब्दी और आज २०१७ ...करीब पंद्रह सौ साल का वक़्त गुजर चुका है. इतने लंबे अरसे में तो यादों पर भी वक़्त की गर्द चढ़ जाती है. पर यहां जिस राज़ की बात की जा रही है, वो पंद्रह सौ साल बाद भी जिंदा है.
एक किला, जो पहाड़ों पर सीना ताने खड़ा है, इस किले में रहस्य है. सन्नाटे को चीरती घुंघरुओं की चीख़ है, तो कहीं तिलिस्मी चमत्कार. कई ख़ौफ़नाक हवेलियों और किले के क़िस्से अब तक सुने गए हैं. ऐसी कोई भी हवेली या किला नहीं था, जहां कोई रहता हो, इसलिए दास्तान कितनी सच है, कितनी झूठ, ये शक़ हमेशा बना रहता था. मगर इस किले में 'वो' रहती है और साथ में रहती है उसकी घुंघरुओं का आवाज़. जी हां...'वो', जिसे मरे १५०० साल बीत चुके हैं.
कभी किसी महल जैसा रहा शानदार किला आज खंडहर में तब्दील हो गया है. मगर यहां की ज़िंदगी यहां के क़िरदारों के साथ आज भी ज़िंदा नज़र आती है. यहां के वीराने आज भी किसी के जिंदा होने का अहसास कराते हैं और जब दिन थककर सो जाता है, तो यहां रात की तनहाई अक्सर घुंघरुओं की छनकती आवाजों से टूट जाती है.
कालिंजर के इस दुर्ग में काली गुफाओं के कई रहस्यमई तिलिस्म हैं. रात होते ही इन गुफाओं में एक अजीब हलचल होती है. दिन के वक्त ये किला जितना खामोश नज़र आता है, रात के वक्त उतना ही खौफनाक. किले की ८०० फुट की ऊंचाई पर पानी की धार नीचे से ऊपर की ओर बहती है.
बांदा में ज़मीन से 800 फुट ऊंची पहाड़ियों पर बना है कालिंजर का किला. कालिंजर दुर्ग को किसी ने चमत्कार कहा तो किसी ने अनोखा तिल्सिम करार दिया.
कालिंजर किले में दाखिल होते ही कई रहस्यमयी छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई देती हैं वो गुफाएं जिसका ओर तो है, लेकिन छोर का पता ही नहीं चलता. यानी गुफाएं शुरू तो होती हैं, लेकिन खत्म कहां जाकर होती हैं, यह कोई नहीं जानता.
गुफाओं में जगह जगह मकड़ी के जाले और घूरती बिल्लियों की निगाहे रोंगटे खड़े देती हैं, लेकिन इन सबके बावजूद खामोशी बिखरी पड़ी है चारों ओर
इन अंधेरी गुफाओं के बीच ये टप टप गिरता पानी हमारे जिस्म में सिहरन पैदा कर देता है . इन अंधेरी गुफाओं में चमगादड़ों ने अपना आशियाना बना रखा है. आगे की जगह को पातालगंगा कहते है.
इस किले में एक दो नहीं बल्कि कई तरह की गुफाए बनी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल उस काल में सीमाओं की हिफाजत के लिए होता था. किले के पश्चमी छोर पर ही एक और रहस्मयी गुफा थी. इस गुफा में घना अंधेरा रहता है और इसके अंदर अजीब तरह की आवाजें आती रहती हैं
कालिंजर के रहस्मयी किले में सात दरवाजे है. इन सात दरवाजों में एक दरवाजा ऐसा है, जो सिर्फ रात के सन्नाटे में खुलता है और यहां से निकला एक रास्ता रानीमहल ले जाता है जहां रात की खामोशी को घुंघरुओं की आवाज़ें तोड़ देती हैं और इन्ही घुंघरुओं की आवाज़ सुनने के लिए अब हमें शाम ढलने का का इंतज़ार करना पड़ता है
दरअसल कालिंजर किले में मौजूद रानी महल है. एक दौर था जब इस महल में हर रात महफिलें सजा करती थीं. कहने वाले कहते हैं कि आज १५०० साल बाद भी शाम ढलते ही एक नर्तकी के कदम यहां उसी तरह थिरकने लगते हैं. बस फर्क यह है कि अब इन घुंघरुओं की आवाज दिल बहलाती नहीं बल्कि दिल दहला जाती है.
घुंघरू की आवाज उस नर्तकी की है जिसका नाम पद्मावती था. गज़ब की खूबसूरत इस नर्तकी की जो भी एक झलक देख लेता वही उसका दीवाना बन बैठता. कहते हैं जब उसके घुंघरू से संगीत बहता तो चंदेल राजा उसमें बंधकर रह जाते. पद्मावती भगवान शिव की भक्त थी. लिहाजा खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो पूरी रात दिल खोल कर नाचती थी.
पद़माती अब नहीं है, पर हैरानी की बात ये है कि हज़ारों साल बाद आज भी ये किला पद्मावती के घुघरुओं की आवाज़ से आबाद है. खुद इतिहासकार भी इस सच को मानते हैं. रिसर्च के दौरान एक बार उन्हें देर रात इस महल में रुकना पड़ा और फिर रात की खामोशी में अचानक उन्हें वही घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी.
हजारों साल पुराने इस किले का इतिहास कुछ ऐसा है कि लोग फिर भी इन वीरान खंड्हरों की ओर खिंचे चले आते हैं. ये किला दरअसल चंदेल साम्रज्य की मिलकियत हुआ करता था. मगर किले के इतिहास से अलग लोगों को ज्यादा दिलचस्पी है किले में छुपे खजाने से. इस किले ने अब तक जितनी भी लड़ाइयां झेली वो सब खजाने को लेकर ही हुईं. अफवाहें हैं कि कालिंजर के किले में हीरे-जवाहरातों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है.
पहाडी़ पर मौजूद इस किले में चित्रकारी और पत्थरों पर हुई नक्काशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किले में काफी धन दौलत रही होगी. ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि कालिंजर के किला पर छठी शताब्दी से लेकर १५वी शताब्दी तक चंदेलों का शासन रहा. इस किले को गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने इनसे जीतना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए.
इस चमत्कारी किले को इतिहास के हर युग में अलग अलग नाम से जाना गया, जिसका बाकायदा हिन्दू ग्रन्थों में जिक्र भी किया गया है. दरअसल कालिंजर का मतलब होता है काल को जर्जर करने वाला.
यहां के मुख्य आकर्षणों में नीलकंठ मंदिर है। इसे चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। मंदिर में १८ भुजा वाली विशालकाय प्रतिमा के अलावा रखा शिवलिंग नीले पत्थर का है। मंदिर के रास्ते पर भगवान शिव, काल भैरव, गणेश और हनुमान की प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गयीं हैं।
रोमांच और चमत्कार से हटकर कालिंजर का पौराणिक महत्व शिव के विषपान से भी है. समुद्र मंथन में मिले कालकूट के पान के बाद शिव ने इसी कालिंजर में विश्राम करके काल की गति को मात दी थी, इसलिए इस जगह का नाम कालिंजर पड़ा.शिवलिंग की खासियत यह है कि उससे पानी रिसता रहता है। इसके अलावा सीता सेज, पाताल गंगा, पांडव कुंड, बुढ्डा-बुढ्डी ताल, भगवान सेज, भैरव कुंड, मृगधार, कोटितीर्थ व बलखंडेश्वर, चौबे महल, जुझौतिया बस्ती, शाही मस्जिद, मूर्ति संग्रहालय, वाऊचोप मकबरा, रामकटोरा ताल, भरचाचर, मजार ताल, राठौर महल, रनिवास, ठा. मतोला सिंह संग्रहालय, बेलाताल, सगरा बांध, शेरशाह शूरी का मकबरा हुमायूं की छावनी आदि हैं।
नीलकंठ मंदिर के ऊपर ही पहाड़ के अंदर एक और कुंड है, जिससे स्वर्गा कहा जाता है. इसे भी धर्म से जोड़ा जाता है. पहाड़ों पर सीना ताने खड़े इस कालिंजर के किले में कहीं रहस्य है, तो कही घुंघरुओं का खौफ़. कहीं तिलिस्मी चमत्कार है, तो कहीं अंधेरी गुफाओं का रोमांच. यह ही वजह है कि कला औऱ शिल्प की अदभुत मिसाल अभी तक बाइज़्ज़त कायम हैं. रही बात ख़ौफ़ की, तो इस किले की ख़ूबसूरती की रोशनी में ख़ौफ़ का साया भी धुंधला पड़ता ही नज़र आता है.
बेतवा का इतिहास
एक कवि ने नदियों के बारे में कहा है कि-
शुचि सोन केन बेतवा निर्मल जल धोता कटि सिर वक्ष स्थल,
पद रज को फिर श्रद्धापूर्वक धोता गंगा, यमुना का जल।
वनमालिन सुन्दर सुमनों से तुव रूप सँवारे ले विराम।
बेतवा प्राचीन नदियों में से एक मानी गयी है। बेतवा नदी घाटी की नागर सभ्यता लगभग पाँच हजार वर्ष पुरानी है। एक समय निश्चित ही बंगला की तरह इधर भी जरूर बेंत (संस्कृत में वेत्र) पैदा होता होगा, तभी तो नदी का नाम वेत्रवती पड़ा होगा। बेतवा तथा धसान बुन्देलखण्ड के पठार की प्रमुख नदियाँ हैं जिसमें बेतवा उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश की सीमा रेखा बनाती है। इसे बुन्देलखण्ड की गंगा भी कहा जाता है। इसका जन्म रायसेन जिले के कुमरा गाँव के समीप विन्ध्याचल पर्वत से होता है। यह अपने उद्गम से निकलकर उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर बहती है। इतना ही नहीं बेतवा नदी पूर्वी मालवा के बहुत से हिस्सों का पानी लेकर अपने पथ पर प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियाँ बीना और धसान दाहिनी ओर से और बायीं ओर से सिंध इसमें मिलती हैं। सिन्ध गुना जिले को दो समान भागों में बाँटती हुई बहती है। बेतवा की सहायक बीना नदी सागर जिले की पश्चिमी सीमा के पास राहतगढ़ कस्बे के समीप भालकुण्ड नामक 38 मीटर गहरा जलप्रपात बनाती है। गुना के बाद बेतवा की दिशा उत्तर से उत्तर-पूर्व हो जाती है। यह नदी मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश की सीमा बनाती हुई माताटीला बाँध के नीचे झरर घाट तक बहती है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर झाँसी में बेतवा 17 किलोमीटर तक प्रवाहमान रहती है। जालौन जिले के दक्षिणी सीमा पर सलाघाट स्थान पर बेतवा नदी का विहंगम दृश्य दर्शनीय है।
इसका जलग्रहण क्षेत्र प्रायः पूर्वी मालवा है। इसी क्षेत्र का यह जल ग्रहण करते हुए उत्तर की ओर गमन करती है। 380 किमी की जीवन यात्रा में यह विदिशा, सागर, गुना, झाँसी एवं टीकमगढ़ जिले की उत्तरी-पश्चिमी सीमा के समीप से बहती हुई हमीरपुर के पास यमुना नदी में अपनी इहलीला समाप्त कर देती है।
संस्कृत के महाकवि बाणभट्ट ने कादम्बरी और कालिदास ने मेघदूत में इसका उल्लेख किया है। बेतवा का प्राचीन नाम बेत्रवती है। महाकवि कालिदास ने इसे बेत्रवती सम्बोधन करते हुए लिखा है कि-
तेषां दिक्षु प्रथित विदिसा लक्षणां राजधानीम्
गत्वा सद्यः फलं विकलं कामुकत्वस्य लब्धवा।
तीरोपान्तस्तनितसुभगं पस्यसि स्वादु दस्मात्,
संभ्रु भंगमुखमिव पदो वेत्रवत्याश्चलोर्मि।।
हे मेघकुम्भ! विदिशा नामक राजधानी में पहुँचकर शीघ्र ही रमण विलास का सुख प्राप्त करोगे, क्योंकि यहाँ बेत्रवती नदी बह रही है। उसके तट के उपांग भाग में गर्जनपूर्वक मनहरण हरके उसका चंचल तरंगशाली सुस्वादु जल प्रेयसी के भ्रुभंग मुख के समान पान करोगे।
बेतवा के उद्गम स्थान पर विभिन्न दिशाओं से तीन नाले एक साथ मिलते हैं। हालाँकि यह नाले गर्मी में सूख जाते हैं। 1 मीटर व्यास का एक गड्ढा यहां सदाबहार पानी से भरा रहता है। एक जो इसका मूल उद्गम है। बेत्रवती के नाम के पीछे एक मान्यता यह भी हो सकती है कि इस स्थान पर पहले कभी बेत (संस्कृत नाम) पैदा हुआ है, यहाँ बेत के सघन वन होंगे। इसीलिए इसका नाम बेत्रवती पड़ा है। बेतवा की तुलना पं. बनारसी दास चतुर्वेदी ने जर्मन की राइन नदी से की है।
पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार- ‘सिंह द्वीप नामक एक राजा ने देवराज इन्द्र से शत्रुता का बदला लेने के लिए कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण की स्त्री वेत्रवती मानुषी नदी का रूप धारण कर उसके पास आयी और बोली- मै वरुण की स्त्री वेत्रवती आपको प्राप्त करने आयी हूँ। स्वयं भोगार्थ अभिलिषित आयी हुई स्त्री को पुरुष स्वीकार नहीं करता, वह नरकगामी और घोर ब्रह्मपातकी होता है। इसलिए हे महाराज! कृपया मुझे स्वीकार कीजिये।’ राजा ने वेत्रवती की प्रार्थना स्वीकार कर ली तब वेत्रवती के पेट से यथा समय 12 सूर्यों के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जो वृत्रासुर नाम से जाना गया। जिसने देवराज इन्द्र को परास्त करके सिंह द्वीप राजा की मनोकामना पूर्ण की।
कभी नहीं सूखी है न सूखेगी बेत्रवती की धार,
ये कलिगंगा भगीरथी बुन्देलखण्ड का अनुपम प्यार।
युगों-युगों से भोले-भाले, ऋषि-मुनि भक्त अनन्य हुए, विदिशा और ओरछा जिसके तट पर बसकर धन्य हुए।
जगदीश्वर
बेतवा नदी के किनारे प्रसिद्ध स्थान विदिशा (साँची), झाँसी, ओरछा, गुना और चिरगाँव बसे हुए हैं। साँची में विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है, जहाँ विश्वभर के बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भक्त यहाँ आराधना, साधना और दर्शन लाभ के लिए आते हैं। सांची के पुरावशेषों की खोज सर्वप्रथम 1818 में जनरल टेलर ने की थी। साँची को काकणाय, काकणाद वोट, वोटश्री पर्वत भी कहा जाता है। मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी श्रीदेवी विदिशा की निवासी थीं, जिनकी इच्छा के मुताबिक यहाँ सम्राट अशोक ने एक स्तूप विहार और एकाश्म स्तम्भ का निर्माण कराया था। साँची में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान के पुरावशेष भी हैं।
शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने विदिशा पर शासन किया था। जिसकी राजधानी कुशावती थी। मौर्य सम्राट अशोक ने विदिशा के महाश्रेष्ठि की पुत्री श्रीदेवी से विवाह किया था, जिससे उसे पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा प्राप्त हुए थे। अशोक ने साँची (विदिशा), भरहुत (सतना) एवं कसरावद (निमाड़) में स्तूप तथा रूपनाथ (जबलपुर), वंसनगर, पवाया, एरण, रामगढ़ (अम्बिकापुर) में स्तम्भ स्थापित कराये थे। हिन्द-यूनानी एण्टायलकीड्स के दूत हेलियाडोरस ने विदिशा में एक विष्णु स्तम्भ स्थापित कराया था जिसमें उसने स्वयं को ‘परम भागवत’ कहा है। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप का विस्तार कराया था। सातवाहन वंश एवं भारशिव वंश के राजाओं ने विदिशा पर राज किया।
ओरछा
ओड़छो वृन्दावन सो गांव,
गोवर्धन सुखसील पहरिया जहाँ चरत तृन गाय,
जिनकी पद-रज उड़त शीश पर मुक्ति मुक्त है जाय।
सप्तधार मिल बहत बेतवा, यमुना जल उनमान,
नारी नर सब होत कृतारथ, कर-करके असनान।
जो थल तुण्यारण्य बखानो, ब्रह्म वेदन गायौ,
सो थल दियो नृपति मधुकर कौं,
श्री स्वामी हरिदास बतायौ।
-महाराजा मधुकर शाह
ओरछा बुन्देली शासकों के वैभव का प्रमुख केन्द्र रहा है यहाँ जहाँगीर महल, लक्ष्मीनारायण मंदिर, बुन्देलकालीन छतरियाँ, तुंगारण्य, कवि केशव का निवास स्थान, महात्मा गांधी भस्मि विसर्जन स्थल, चन्द्रशेखर आजाद गुफा, रायप्रवीण महल, शीश महल, दीवाने आम, पालकी महल, छारद्वारी एवं बजरिया के हनुमान मंदिर आदि अन्य स्थान देखने योग्य हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने ओरछा का गुणगान इन शब्दों में किया है-
कहाँ आज यह अतुल ओरछा, हाय! धूलि में धाम मिले।
चुने-चुनाये चिन्ह मिले कुछ, सुने-सुनाये नाम मिले।
फिर भी आना व्यर्थ हुआ क्या तुंगारण्य? यहाँ तुझमें?
नेत्ररंजनी वेत्रवती पर हमें हमारे राम मिले।
ओरछा के अन्य दर्शनीय स्थलों में जहाँगीर महल-जिसे जहाँगीर ने अपने विश्राम के लिए ओरछा के दुर्ग में एक सुन्दर महल बनवाया था जिसे जहाँगीर महल कहते हैं। यह बेतवा के मनोरम तट पर स्थित एक भव्य और ऐतिहासिक महल है।
ओरछा दुर्ग
मानिकपुर झाँसी रेल-मार्ग पर बेतवा नदी पर बुन्देलवंशीय राजाओं ने यह महल बनवाया था। जो राजाओं के शौर्य, पराक्रम और वीरतापूर्ण गौरव गाथाओं का गुणगान कर रहा है। ओरछा महल के भीतर अनेक प्राचीन मन्दिर हैं जिनमें चतुर्भुज मंदिर, रामराजा मन्दिर और लक्ष्मीनारायण मन्दिर बुन्देला नरेशों की कलाप्रियता के प्रतिमान हैं।
बेतवा को पुराणों में ‘कलौ गंगा बेत्रवती भागीरथी’ कहा गया है। आचार्य क्षितीन्द्र मोहन सेन ‘हमारी बुन्देलखण्ड की यात्रा’ नामक लेख में कहते हैं कि- ‘बेत्रवती ने अपने चंचल प्रवाहों से सारे बुन्देलखण्ड को सिक्त कर रखा है।’
ओरछा सात मील के परकोटे पर बसा पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगर है। जो सोलहवीं शताब्दी में बुन्देला राजाओं की राजधानी था।
कंचना घाट
बेतवा का कंचना घाट नाम इस कारण पड़ा क्योंकि इस घाट पर स्त्रियों के स्नान करने पर उनके स्वर्ण आभूषणों के क्षरण से प्रतिदिन लगभग सवा मन सोना घिसकर बह जाता था।
ओरछा के रामराजा मन्दिर में आज भी बाल भोग लगता है और भोग के रूप में पान का बीड़ा, इत्र का फाहा एवं मिष्टान्न भक्तों को प्रदान किया जाता है। राम को राजा मानकर प्रतिदिन प्रातः एवं संध्याकाल में शासकीय तौर पर उन्हें तोपों से सलामी दी जाती है तथा पुलिस इस मंदिर में हमेशा तैनात रहती है। यहाँ राम वनवासी रूप में न होकर राजा के रूप में अपने दरबार में विराजमान हैं। इसलिए यह रामराजा मंदिर कहलाता है। राजा के रूप में देश में राम के मंदिर बहुत कम हैं।
वास्तव में यह स्थान मंदिर के वास्तु शास्त्र के आधार पर निर्मित नहीं है। यह गणेश कुँवरि रानी का महल था जो एक जनश्रुति के आधार पर मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसी मान्यता है कि रामराजा सरकार को गणेश कुँवरि अयोध्या की सरयू नदी की जलराशि के मध्य से पुष्य नक्षत्र में पैदल चलकर अपनी गोद में लेकर ओरछा आयी थीं।
रामलला रानी के साथ तीन शर्तों के आधार पर आये थे। पहली शर्त पुष्य नक्षत्र में लेकर चलने की थी। दूसरी शर्त-अगर रानी उन्हें किसी स्थान पर रख देंगी तो वे फिर वहाँ से उठेंगे नहीं और अन्तिम शर्त थी ओरछा में आने के बाद वहाँ के राजा राम ही होंगे। दूसरी शर्त के आधार पर रानी ने रामलला को मंदिर के बजाय भूलवश अपने महल में रख दिया था। अतः वे वहीं प्रतिस्थापित हो गये।
ऐसी जनश्रुति है कि अकबर बादशाह मधुकर शाह से प्रेरित होकर माथे पर तिलक लगाते थे तथा वे मधुकर शाह को गुरुवत मानते थे। ऐसी मान्यता भी है कि हरदौल मरणोपरान्त अपनी बहन कुन्जावती की पुत्री के विवाह में बारातियों से मिले थे और भात भी खाया था। इसी स्मृति स्वरूप बुन्देलखण्ड में विवाह के अवसरों पर हरदौल को खिचड़ी चढ़ाने की प्रथा भी बरकरार है। हरदौल यहाँ जन-जन के देवता माने जाते हैं। जिनकी मढ़ियाँ गाँव-गाँव में हैं। विवाहोपरान्त इन मढ़ियों में दूल्हा-दूल्हन के हाथे लगते हैं और लोग मन्नतें मानते हैं। ओरछा के रामराजा मंदिर परिसर में हरदौल विषपान स्थल है। जिसे बुन्देलखण्डवासी श्रद्धा और भक्तिपूर्वक अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहीं पर हरदौल बैठका, पालकी महल, सावन-भादों स्तम्भ, कटोरा, फूलबाग चौक आदि भी दर्शनीय हैं।
चंदेरी
इस नगर से बेतवा और उर्वशी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चंदेरी समुद्र तल से 1700 फुट की ऊँचाई पर स्थित अशोक नगर जिला से 50 किलोमीटर दूर है। महाभारत के हैहयवंशी शिशुपाल चेदि नरेश ने इसे बसाया था। इसी कारण शायद यह चंदेरी कहलाया होगा। इस ऐतिहासिक नगर ने प्राचीनकाल में अनेक आक्रमण झेले, जैसे-महमूद गजनवी, नसरुद्दीन खिलजी के सेनापति अमिलमुल, फिरोजशाह तुगलक, सिकन्दर और बाबर आदि। यहाँ की साड़ियाँ और जरी की कारीगरी का कार्य जग-जाहिर है।
देवगढ़
उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिले से 33 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा के तट पर विन्ध्याचल की दक्षिण-पश्चिम पर्वत श्रृँखला पर देवगढ़ स्थित है। इसका प्राचीन नाम लुअच्छागिरि है। पहले प्रतिहारों और बाद में चंदेलों ने इस पर शासन किया। देवगढ़ में ही बेतवा के किनारे 19 मान स्तम्भ और दीवालों पर उत्कीर्ण 200 अभिलेख हैं। जैन मंदिरों के ध्वंसावशेष यहाँ बहुतायत में विद्यमान हैं। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर भी दर्शनीय हैं। यहाँ बहुतायत में विद्यमान हैं। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर भी दर्शनीय हैं यहाँ 41 जैन मंदिर हैं। यहाँ प्रतिहार, कल्चुरि और चंदेलों के शासनकाल की प्रतिमाएँ और अभिलेख बिखरे पड़े हैं। पुरातत्व की दृष्टि से देवगढ़ जग प्रसिद्ध है। बिखरी हुई मूर्तियों को संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। बेतवा तट पर तीसरा स्थान रणछोड़ जी है। यह स्थल धौर्रा से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। रणछोड़ जी मंदिर में विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमाएं हैं। यहाँ हनुमान जी की भव्य मुर्ति भी है। लेकिन यह मंदिर शिखरहीन है। इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ और भी मंदिरों के पुरावशेष हैं जो हमारी समृद्धि का कहानी कहते हैं। देवगढ़ पुरातत्वविदों का एक महत्वपूर्ण कला केंद्र है। पुरातत्व सम्पदा से सम्पन्न है देवगढ़। इसे बेतवा नदी का आइसलैण्ड कहा जाता है।
बुन्देलखण्ड के पठारी प्रदेश की प्रमुख नदी बेतवा है जो मालवा का जल अपने साथ प्रवाहित कर नरहर कगार को देवगढ़ के पास काटकर एक सुन्दर गुफा का निर्माण करती है। इस पठार प्रदेश से सिंध, केन, पहुज और धसान नदियाँ प्रवाहित होती है।
15 जनवरी 1941 की मधुकर पत्रिका के एक लेख पं. बनारसी दास चतुर्वेदी लिखते हैं कि- ‘बेतवा यमुना की सखी है, बहन है। इसलिए यमुना मैया के सपूत हम चौबों के लिए बेतवा मौसी हुई। वह आगे कहते हैं कि बेत्रवती के तीन रूप अपनी जीवन यात्रा में हैं। उसके मायके में यानी भोपाल में उसके उद्गम स्थान पर चिरगाँव के निकट बाँध पर संयत जीवन बिताते हुए और ओरछा में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में जब-जब हमने बेतवा को देखा है उसके विचित्र प्रभाव से हम प्रभावित हुए हैं। वे कहते हैं कि बेतवा की यह जन्मभूमि वस्तुतः हमारे जैसे श्रांत पथिक के लिए एक अद्भुत, आनन्ददायक सुखकर भूमि थी।’ बाणभट्ट ने कादम्बरी में विन्ध्याटवी का अद्भुत वर्णन किया है-
मज्जन मालवविलासिनी कुचतट स्फालन
जर्ज्जरितोर्मि मालयाजवालव गाहनावतारित,
जय कुन्जर सिंदूर सन्ध्यामान सलिलया
उन्मद कलहंस कुल-कोलाहल मुखरित कूलया।
विदिशा के चारों तरफ बहती बेत्रवती नदी में स्नान के समय विलासिनियों के कुचतट के स्फालन (हिलने) से उसकी तरंग श्रेणी चूर्ण-विचूर्ण हो जाती थी और रक्षकों द्वारा स्नानार्थ आनीत विजाता स्त्रियों के अग्रभाग में लिप्त सिंदूर के फैलने से सांध्य आकाश की भाँति उसका पानी लाल हो जाया करता था और उसका तट देश उन्मत कलहंस मण्डली के कोलाहल से सदा मुखरित रहता था।
वीरांगना झलकारी बाई - Jhalkari Bai
वीरांगना झलकारी बाई - Jhalkari Bai
वीरांगना झलकारी बाई
ग्वालियर रोड से भोजला गाँव नजदीक था। खेतों में हरी-भरी चने की फसल लहरा रही थी। चारों तरफ रंग-बिरंगे फूल खिले थे। प्रकृति अपने अनोखे श्रृंगार में थी। उन्हीं की अनुपम छटा निहारते हुए राहगीर सड़क से उतरकर छोटे रास्ते पर आ गया था। दिन का समय था। चारों तरफ धूप फैली थी। गाँव की विराट संस्कृति का अनूठा सौन्दर्य अपनी अस्मिता और पहचान के साथ सर्वत्र दिखाई देता था। अलग-बगल से गुजरते हुए लोग। राहगीर कुछ के लिए अपना था और अन्य के लिए पराया, पर अजनबी नहीं था। जमीन की गन्ध जितनी बाहर थी उतनी ही उसके भीतर भी। खेत पार कर अचानक राहगीर की निगाहें छः सात वर्षीय एक लड़की की ओर उठ गई। उसका रंग थोड़ा साँवला था। आँखों में ढेर सारी चमक, बिखरे बाल। राहगीर ने पलभर सोचा। उसे ध्यान आया। पहले इस लडकी को कहीं देखा है। वह व्यक्ति गाँव में दो-तीन बरस पहले भी आ चुका था। उसी व्यक्ति ने मन में सोचा। कहीं यह सदोवा की मोड़ी तो नहीं है। राहगीर पास आया, तो पूछ बैठा वह, ‘‘बिन्नू का कर रई ?’’ मिट्टी के ढेर पर बैठी लड़की के कानो में अनजाने व्यक्ति की आवाज पड़ी तो चौंक-सी उठी वह। उसने देखा अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आकर ठहर गया था। लड़की के होंठों पर हल्की मूँछें थीं। सिर पर सफेदी बिखरी हुई थी। शरीर पर मटमैला कुर्ता और धोती, पाँव में साधारण जूतियाँ, जो धूल-मिट्टी से अटी हुई थीं। लगता था जैसे वह काफ़ी दूर से पैदल चलकर आया हो। बिना किसी हिचकिचाहट के तपाक से उसने कहा था, ‘‘किलौ बनाई रई हूँ।’’ पूछने वाले के मुँह से आश्चर्य से निकला, ‘‘क्या ?’’ झलकारी फिर बोली, ‘‘किलौ, तोय सुनाई नई दैरयौ।’’ उसके स्वर में थोड़ी तुर्शी थी। सुनने वाले को बुरा लगा। थोड़ा नाराजगी के स्वर में बोला, ‘‘बिन्नू तैं तो भौतई खुन्नस खा रई। य्य तो बतला, कौन की मोड़ी है तू ?’’ झलकारी इस बार धीरे से बोली, ‘‘सदोवा मूलचन्द्र की।’’ सुनकर आगन्तुक जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि वह पूछ बैठी, ‘‘हमाय बारे में पूछ लयो अपने बारे में नई बताओ कछु। इतिहास जब भी लिखा गया है, राजाओं को केन्द्र में रखकर लिखा गया है। राजा उस देश का प्रथम पुरुष होता है। इसलिए राजा का स्थान इतिहास में शीर्ष पर होता है। इतिहासकारों, कवियों, लेखकों के द्वारा उनका वर्णन नायक के रूप में किया जाता है। किन्तु द्वितीय लाइन के नायकों का वर्णन कम ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि इतिहास ने बिल्कुल ही उन्हें नकारा हो। भगवान राम का जहाँ भी उल्लेख आता है, हनुमान जी को भी उतनी ही श्रद्धा और आदर-भाव से याद किया जाता है।
इसी प्रकार झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिलाओं की एक शाखा थी। जिसकी सेनापति वीरांगना झलकारी बाई थीं। बुंदेलखण्ड की प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान ने केवल महारानी लक्ष्मीबाई का ही गुणगान किया है। उनकी कविता में झलकारी बाई का कहीं नाम नहीं आया है। किन्तु राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने झलकारी की बहादुरी को निम्न प्रकार पंक्तिबद्ध किया है - जा कर रण में ललकारी थी, वह तो झाँसी की झलकारी थी । गोरों से लडना सिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी ।। झलकारी बाई का जन्म 22 नवम्बर 1830 को झांसी के पास के भोजला गाँव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थीं तब उनकी माँ की मृत्यु के हो गयी थी और उसके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला था। उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया गया था। उन दिनों की सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया था। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं के रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में उसकी मुठभेड़ एक तेंदुए के साथ हो गयी थी, और झलकारी ने अपनी कुल्हाड़ी से उस जानवर को मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गाँव के एक व्यवसायी पर हमला किया तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। उसकी इस बहादुरी से खुश होकर गाँव वालों ने उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया, पूरन भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी।
एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गाँव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झाँसी के किले मे गयीं, वहाँ रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देख कर अवाक रह गयी क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखतीं थीं। अन्य औरतों से झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुईं। रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी की प्रशिक्षण लिया। यह वह समय था जब झांसी की सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था लार्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के चलते, ब्रिटिशों ने निःसंतान लक्ष्मीबाई को उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। हालांकि, ब्रिटिश की इस कार्रवाई के विरोध में रानी के सारी सेना, उसके सेनानायक और झांसी के लोग रानी के साथ लामबंद हो गये और उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय ब्रिटिशों के ख़िलाफ़ हथियार उठाने का संकल्प लिया। अप्रैल 1858 के दौरान, लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से, अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा किये कई हमलों को नाकाम कर दिया।
रानी के सेनानायकों में से एक दूल्हेराव ने उसे धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठ अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गईं। झलकारी बाई का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के, ब्रिटिशों को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ मे ले ली। जिसके बाद वह किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज़ के शिविर मे उससे मिलने पहँची।
ब्रिटिश शिविर में पहँचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यूग रोज़ से मिलना चाहती है। रोज़ और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्ज़े में है। जनरल ह्यूग रोज़ जो उसे रानी ही समझ रहा था, ने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? तो उसने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे फाँसी दो। जनरल ह्यूग रोज़ झलकारी का साहस और उसकी नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ, और झलकारी बाई को रिहा कर दिया गया। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी इस युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुई। एक बुंदेलखंड किंवदंती है कि झलकारी के इस उत्तर से जनरल ह्यूग रोज़ दंग रह गया और उसने कहा कि "यदि भारत की 1% महिलायें भी उसके जैसी हो जायें तो ब्रिटिशों को जल्दी ही भारत छोड़ना होगा"। यदि लक्ष्मीबाई के सेनानायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्राय: अभेद्य था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोकगाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने २२ जुलाई २००१ में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है,उनकी प्रतिमा और एक स्मारक अजमेर, राजस्थान में निर्माणाधीन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थापित की गयी है, साथ ही उनके नाम से लखनऊ मे एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी शुरु किया गया है।
बुंदेलखंड के पकवान
महुआ और बेर बुंदेलखंड के लोगों का सबसे प्रिय भोजन है। ये दोनों वृक्ष इस जगह के लोकप्रिय वृक्ष हैं। यहाँ महुआ को मेवा, बेर को कलेवा (नास्ता) और गुलचुल का सबसे बढ़िया मिष्ठान माना जाता है, जैसा कि इस पंक्ति से स्पष्ट होता है
मउआ मेवा बेर कलेवा गुलचुल बड़ी मिठाई।
इतनी चीज़ें चाहो तो गुड़ाने करो सगाई।।
चिल्लाह तारा घाट, बुंदेलखंड- 1838
लटा मछुओं को भूनकर और उसके बाद कूट कर उनमें गरी, चिरौंजी आदि मेवा मिला कर छोटी- छोटी कुचैया की तरह बनाया जाता है, यह इस जगह का विशेष भोजन रहा है। यहाँ के लोग बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए इसी भोजन को परोसते थे। यहाँ के लोगों की एक कहावत अधिक प्रचलित हैं कि खानें को मउआ, पैरबै में अमोआ इस बात का संकेत देती है कि स्थानीय लोगों में मउआ और अमोआ दोनों काफ़ी लोकप्रिय रहा है। भोजन के संबंध में अनेक लोक मान्यताएँ प्रचलित हैं:-
चैत मीठी चीमरी बैसाख मीठो मठा
जेठ मीठी डोबरी असाढ़ मीठे लठा।
सावन मीठी खीर- खँड़ यादों भुजें चना,
क्वाँर मीठी कोकरी ल्याब कोरी टोर के।
कातिक मीठी कूदई दही डारो मारे कों।
अगहन खाव जूनरी मुरी नीबू ज़ोर कें।
पूस मीठी खिचरी गुर डारो फोर कों।
मोंव मीठी मीठे पोड़ा बेर फागुन होरा बालें।
समै- समै की मीठी चीज़ें सुगर खबैया खावें।
बुंदेलखंडवासियों में हर मौसम में अलग भोजन खाने का प्रचलन था। ये लोग भोजन खाने में कभी- कभी काफ़ी सावधानी से काम लेते हैं। बुंदेलखंड के लोगों में बेर का बहुत ही विशेष महत्त्व था। यहाँ की एक कहावत है
मुखें बेर, अघाने पोंड़ा ये लोग भोजन खाने से पहले बेर ज़रूर खाते थे।
कनी उर भाला की अनी यहाँ के लोगों का मानना था कि कच्चे चावल की नोंक भाले की नोंक के बराबर हानिकारक होती है।
बुंदेलखंड के लोगों के भोजन का प्रभाव लोक संस्कृति पर दिखाई देता था। इसलिए वह लोग यह मानते थे कि जैसा भोजन किया जाएगा, वैसा ही मन होगा।
जैसो अनजल खाइये, तैसोई मन होये।
जैसो पानी पीजिए, तैसी बानी होय।।
यहां थोड़े से बुन्देलखण्ड के व्यंजनों का उल्लेख किया जा रहा है। आप देखेंगी कि ये बनाने में आसान हैं, सस्ते हैं, और खाने में अत्यन्त स्वादिष्ट हैं।
पूड़ी के लडडू:
ये लड्डू निर्धन परिवारों में बूंदी के लडूओं के स्थानापत्र कहे जा सकते हैं, पर स्वाद में उनसे भिन्न होते हैं। ये त्यौहारों पर या बुलावा (बुलउआ) के लिए बनाये जाते हैं। बेसन की बड़ी एवं मोटी पूड़ियां तेल में सेंककर हाथों से बारीक मीड़ी (मींजी) जाती है। फिर उन्हें चलनी से छानकर थोड़े से घी में भूना जाता है। उसके बाद शक्कर या गुड़ की घटना डाल कर हाथों से बांधा जाता है। शक्कर के लड्डू अधिक स्वादिष्ट बनते हैं, गुड़ के काम चलाऊ होते हैं। कहीं-कहीं पर स्वाद की वृद्धि करने के उद्देश्य से इनमें इलायची या काली मिर्च भी पीसकर मिला दी जाती है।
आँवरिया:
इसे आंवले की कढ़ी भी लोग कहते हैं। सूखे आंवलों की कलियों को घाी या तेल में भूनकर सिल पर पीसा जाता है। बेसन को पानी में घोलकर किसी बर्तन में चूल्हे पर चढ़ा देते हैं और उसी में आंवलों का यह चूर्ण डाल देते हैं। मिट्टी के बर्तन अर्थात हण्डी में अधिक स्वादिष्ट बनता है। लाल मिर्च, जीरा, प्याज एवं लहसुन आदि सामान्य मसाले पीसकर डाले जाते हैं। मसाले पीसकर डाले जाते हैं। मसाले के इस मिश्रण को तेल या धी में भूनकर बेसन को घोल छौंका जाये तो और अच्छा है। नमक अवश्य डाला जाता है।
हिंगोरा:
यह हींग से व्युत्पन्न हुआ है। मटटे के अभाव में बेसन का घोल थोड़ी सी हींग छौंककर पका लेते र्है। साधारण नमक डाल देते है। यह एक प्रकार की मट्ठाविहीन कढ़ी है। यह भी स्वादिष्ट पर भारी होता है।
थोपा:
यह शब्द ‘थोपने’, से बना है। बेसन को पानी में घोलकर कड़ाही में हलुवे की तरह पकाते हैं। उसमें नमक, मिर्च, लहसुन, जीरा एवं प्याज काटकर मिला देते है। जब हलुवा की तरह पककर कुछ गाढ़ा हो जाता है, तब जरा-सा तेल छोड़ देते है। पक जाने पर किसी थाली या हुर से पर तेल लगाकर हाथ से थोप देते हैं। बर्फी या हलुवे की तरह थोप दिये जाने पर छोटी-छोटी कतरी बना दी जाती है। इन्हें ऐसा ही खाया जाता है और मट्ठे में भी। मढ्ढे में डालकर रोटी से भी शाक (साग) की तरह खाते हैं। निर्धन परिवारों का यह नाश्ता भी है।
बफौरी:
यह शब्द ‘वाष्प’ से बना है। बुन्देली में ‘वाष्प’ को बाफ् और भाफ् (कहीं कहीं पर भापु) कहते है। मिट्टी या धातु के बर्तन में पानी भरकर उसके मंुह पर कोई साफ कपड़ा बांध देते है। उसे आग पर खौलाते हैं। जब वाष्प निकलने लगती हैं, तब उस पर बेसन की पकौड़ियां सेंकते हैं। इन पकौड़ियों को कड़ाही में लहसुन, प्याज, धनियां हल्दी एवं मिर्चीदि मसालों के मिश्रण को घी या तेल में छौंक कर पकाया जाता है। यह भी एक प्रकार का शाक है।
ठोंमर:
ज्वार को ओखली में मूसल से कूटकर दलिया बना लेते हैं। फिर इसे धातु या मिट्टी के बर्तन में चूल्हे पर दलिया की तरह मट्ठे में पकाते हैं। थोड़ा सा नमक भी डाल देते है। इसे सादा खाया जाता है। और दूध-गुड़ या दूध शक्कर से भी।
महेरी या महेइ:
यह भी ठोंमर की तरह बनती है। ज्वार का दलिया (पत्थर की चक्की से पिसा हुआ) मट्ठे में चुराया (पकाया) जाता है। जरा-सा नमक डाल देते है। यह मिट्टी के बर्तन में अधिक स्वादिष्ट बनती है। इसे भी सादा या दूध मीठे के साथ खाया जाता है। लोधी एवं अहीर जातियों का यह प्रिय भोजन है। जाड़े की रातों में यह अधिक बनायी जाती है और सुबह खायी जाती है। बासी महेरी अधिक स्वादिष्ट हो जाती है। अन्य मौसम में ताजी ही अच्छी रहती है।
मांडे:
ये मैदा से बनाये जाते हैं। इनके बनाने की विधि रोटी वाली ही है। अन्तर यह है कि रोटी लोहे के तवे पर सेंकी जाती है, जबकि मांड़े मिट्टी के तवों पर, जिन्हें कल्ले कहते हैं, बनाये जाते हैं। तवे कुम्भकार के यहां से बने हुए आते है। मांडे रोटी से आकार में बड़े होते है। इन्हें घी में डुबोया जाता है।
एरसे:
ये त्यौहारों विशेषकर होली या दीपावली, पर बनाये जाते है। ये मूसल से कूटे गए चावलों के आटे से बनाये जाते है। आटे में गुड़ मिला देते हैं और फिर पूड़ियों की तरह घी में पकाते हैं। घी के एरसे ही अधिक स्वादिष्ट होते है। तेल में अच्छे नहीं बनते ।
करार:
मूंग की दाल भिगोकर, उसके छिलके हटाकर एवं उसे पीसकर मट्ठे में घोला जाता है। इसके बाद इस घोल को मसालों के सहित बेसन की कढ़ी की तरह पकाते है। इसी प्रकार हरे चनों (छोले या निघोना) की कढ़ी बनायी जाती है।
फरा:
ये दो प्रकार के होते हैं। गेहूं के आटे को मांड़ कर या तो उसकी छोटी-छोटी रस्सियां बना ली जाती है या पूड़िया। फिर इन्हें खौलते हुए पानी में सेंका जाता है। निर्धन में व्रत के दिन पूडियों के स्थान पर इन्ही का व्यवहार किया जाता है। बड़े कानों के लिए यहां ‘फरा जैसे कान की’ उपमा दी जाती है।
अद्रैनी:
आधा गेहूं का आटा एवं आधा या आधे से कम बेसन मिलाकर जो नमकीन पूड़ी बनायी जाती है, उसे अद्रैनी कहते है। यह तेल या घी में बनती है। इसमें अजवायन का जीरा डाला जाता है। बड़ी स्वादिष्ट होती है।
रसखीर:
गन्ने के रस में पके हुए चावलों को ‘रसखीर’ कहते हैं। इस भोजन के लिए दूसरों को निमन्त्रित भी किया जाता है।
मसेला:
यह कोंहरियों की तरह मूंठा या रोसा की फलियों से दाने निकाल कर बनाया जाता है। इसमंे नमक एवं मिर्चादि मसाले मिलाये जाते है।
बेसन के आलू:
सूखे हुए आंवलों को घी या तेल मंे भून कर और पत्थर पर पीसकर बेसन में मिलाते है। और उस मिश्रण से आलू के समान छोटे-छोटे लड्ड़ू बना लेते है। इन्हें खौलते पानी मंे पकाते है। फिर चाकू से छोटे-छोटे काटकर तेल या घी में भूनते हैं। इसके बाद मसालों के साथ छौंक कर कड़ाही या पतीली में बनाते हैं। ये मांस से भी अधिक स्वादिष्ट बनते है।
he Forts of Bundelkhand - Jhansi
The Forts of Bundelkhand - Jhansi
The Jhansi fort is situated in the outskirts of Jhansi in uttar Pradesh. It was Built in the year 1613 by Raja Bir Singh Deo of Orchha.The fort extends to a sprawling expansion of 15 acres (61,000 m2) and this colossal structure measures about 312m in length and 225m in width. On the whole, there are twenty-two supports with a mammoth strengthening wall cosseted by a moat on both sides.
The fort standing in the hilly area shows how the north Indian style of fort construction differs from that of the south. In the south most of the forts were built on the sea beds like Bekal Fort in Kerala. The granite walls of the fort are between 16 and 20 feet thick and on the south side meet the city walls. The south face of the fort is almost perpendicular.There are 10 gates giving access to the fort. Some of these are Khanderao Gate, Datia Darwaza, Unnao Gate, Jharna Gate, Laxmi Gate, Sagar Gate, Orchha Gate, Sainyar Gate and Chand Gate. Notable sights in the fort are the Shiva temple, Ganesh temple at the entrance, and the Kadak Bijli cannon used in the uprising of 1857. The memorial board reminds one of the hair-raising feat of the Rani Lakshmibai in jumping on horseback from the fort. Nearby is the Rani Mahal, built in the later half of the 19th century where there is now an archaeological museum.
The shattered upholder on the eastern side was rebuild by the British, who also supplemented a floor to Panch Mahal. Every year in the month of Jan-feb a grand occasion is held known as Jhansi Mahotsav many eminent personalities and artist perform their play . The fort proper has occupied an area of 15 acres and measures 312m in length and 225m in width. Altogether, there are twenty-two bastions with a huge fortification wall protected by a moat on two sides. A bastion on the eastern side was destroyed, which was reconstructed by the British, who also added a floor to Panch Mahal.
The fort can be divided in three parts keeping in view the different stages of its constructions:- Baradari, Shankergarh and Panch Mahal. Besides, the fort contains many ancient structures of great importance. The old city wall had ten gates known as Khanderao, Datia, Unnao, Orchcha, Baragaon, Lakshmi, Sagar, Sainyar, Bhander and Jhirna. The first eight still have wooden doors and of the last two, the former is completely closed and the latter is open. A breach in the wall between Sainyar gate and Jhirna gate, which was made by Hugh Rose’s batteries during the assault on the fort in 1858, is still in existence. There are also four khirkis (entrances) made in the walls-Ganpatgir-ki-Khirki, Alighol-ki-Khirki, Sujan khan- ki-Khirki and Sagar Khirki. The main structures within the fort are Baradari, Ganesh mandir, Shahar Darwaza, Bhawani shnakr, Kadak bijali, Grave of Gulam Gaus Khan, Panch Mahal, Siva temple, Execution tower, Kal kothari, etc.
The construction of the fort is ascribed to the Bundela Rajput chief and the ruler of the kingdom of Orchha Veer Singh ju Deo Bundela in 1613.It is one of the strongholds of the Bundelas. In 1728, Mohammed Khan Bangash attacked Maharaja Chattrasal. Peshwa Bajirao [2] helped Maharaja Chattrasal defeat the Mughal army. As a mark of gratitude, Maharaja Chattrasal offered a part of his state, which included Jhansi, to Peshwa Bajirao.
In 1742 Naroshanker was made the subedar of Jhansi. During his tenure of 15 years he not only extended the strategically important Jhansi fort (the extension is called Shankergarh), but also constructed other buildings. In 1757, after Naroshanker was called back by the Peshwa. Madhav Govind Kakirde and then Babulal Kanahai were made the subedars of Jhansi. From 1766 to 1769 Vishwas Rao Laxman served as the subedar of Jhansi. Then Raghunath Rao (II) Newalkar was appointed the subedar of Jhansi. He was a very able administrator, increasing the revenue of the state and building both the MahaLakshmi Temple and the Raghunath Temple.
Notable sights in the fort are the Shiva temple, Ganesh temple at the entrance, and the Kadak Bijli cannon used in the uprising of 1857.
After the death of Shiv Rao his grandson Ramchandra Rao was made subedar of Jhansi. His poorly administered term ended with is death in 1835. His successor Raghunath Rao (III) died in 1838. The British rulers then accepted Gangadhar Rao as the Raja of Jhansi. The inefficient administration of Raghunath Rao (III) left Jhansi in a very poor financial position.
However, he was succeeded by Raja Gangadhar Rao, who was a very good administrator. He was reportedly very generous and sympathetic, and the local population of Jhansi was well satisfied. In 1842 Raja Gangadhar Rao married Manikarnika Tambe who was the given the new name of Lakshmi Bai She gave birth to a boy, later named Damodar Rao, in 1851, who died after four months. The Maharaja adopted a child called Anand Rao, the son of Gangadhar Rao's cousin, who was renamed Damodar Rao, on the day before the Maharaja died.
The adoption was in the presence of the British political officer who was given a letter from the Maharaja instructing that the child be treated with respect and that the government of Jhansi should be given to his widow for her lifetime. After the death of the Maharaja in November 1853, because Damodar Rao (born Anand Rao) was adopted, the British East India Company, under Governor-General Lord Dalhousie, applied the Doctrine of Lapse, rejecting Damodar Rao's claim to the throne and annexing the state to its territories.
In March 1854, Lakshmibai was given an annual pension of Rs. 60,000 and ordered to leave the palace and the fort. In 1857 the revolt broke out and she took the control of the fort and led Jhansi forces against those of the British East India Company.
Jhansi was besieged by the company forces of General Hugh Rose in March and April 1858 and was captured on 4 April 1858. Rani Lakshmi Bai was able to make a daring escape on horseback from the fort and the city before the city was pillaged by Rose's troops.
The fort standing in the hilly area shows how the north Indian style of fort construction differs from that of the south. In the south most of the forts were built on the sea beds like Bekal Fort in Kerala. The granite walls of the fort are between 16 and 20 feet thick and on the south side meet the city walls. The south face of the fort is almost perpendicular. There are 10 gates giving access to the fort. Some of these are Khanderao Gate, Datia Darwaza, Unnao Gate, Jharna Gate, Laxmi Gate, Sagar Gate, Orchha Gate, Sainyar Gate and Chand Gate.
The memorial board reminds one of the hair-raising feat of the Rani Lakshmibai in jumping on horseback from the fort. Nearby is the Rani Mahal, built in the later half of the 19th century where there is now an archaeological museum.
In 1861 the British Government gave the Jhansi fort and Jhansi city to Jiyaji Rao Scindia, the Maharaja of Gwalior, but the British took back Jhansi from Gwalior state in 1868.
Jhansi Rani Laxmi Bai - Original Picture - The Real Story
Jhansi Rani Laxmi Bai - Original Picture - The Real Story
Few Months back one of a member in Jhansi Group posted this photograph of Rani Jhansi and claimed it to be the original and the only available picture of Rani Jhansi Lakshmi Bai.
A Hindi website, which has uploaded the photograph of the Queen, claims it is her only picture available in the world . The website has also uploaded rare and ‘original’ letters written by Rani Lakshmibai — one of the leading figures of the 1857 rebellion against the British.
But a freedom fighter from Belgaum claims that he is in possession of the Original photograph of Rani Laxmibai of Jhansi. “The photograph was taken by Halfman, a British photographer, when the Rani was 15yrs old….”..says Vithal Rao Yalgi, an 86 yr old freedom fighter from Belgaum, Karnataka. Laxmibai was born in the year 1835 and the photograph was taken at the Jhansi palace in 1850. The photograph shows Laxmibai, with her traditional ornaments, which were given to her by Nanasaheb Peshwa of Pune, who also joined her in the freedom struggle against the British.The Rani’s photo was? exhibited in Bhopal on August 19th and the Academicians of the History department of Bhopal University.Vithalrao Yalgi told Indian Express that he received the photograph from a person called Thakur, whose father and grandfather took part in the freedom struggle.
Picture below shows the real Rani Laxmibai
“The authenticity of this photograph is true as per our research,” reads a note on ths website. It also states that those having doubts could consult the Archaeological Survey of India (ASI)"
The story shows a photograph of a woman claiming it to be that of the legendary Rani Laxmibai of Jhansi. It also comes with an explanation of how and when the picture is taken and discovered later. The facts of this story are however mixed. Firstly, the picture can not be that of original Rani Laxmibai, because such a photograph technology was not prevalent in those days. Experts and those familiar with the history of the 1857 mutiny also have their reservations over its genuineness.
“I have seen the photograph… I can’t say it’s a fake, but I have my doubts about its originality,” senior Congress leader and scion of the erstwhile Samthar estate near Jhansi, Raja Ranjit Singh Judeo, said. “The Rani is seen sitting on the throne in regal attire. This seems improbable as Raja Ganga Rao was the ruler at that time (in 1850)… he died in 1853.” Judeo also said that the use of cameras was very rare in that era. “Even the British rarely had cameras,” he explained.
Amaresh Misra, author of The War of 1857, said he neither saw the photograph, nor heard of it during the research for his book. He also said he had never come across any reference about Hoffman.
“If it’s an original, it is a national treasure,” Rajesh Tope, descendant of Tatya Tope, who fought the British alongside the Rani of Jhansi, said. A similar controversy had erupted over a supposedly rare photograph of Tatya Tope, which turned out to be fake.
I am also embedding a Video link from ABP News about this story
If we leave this photograph by Hoffman aside, not much is known about the appearance of Jhansi Ki Rani Lakshmibai. However, a rare account about her looks is available from the contemporary Australian novelist and journalist John Lang who met the Queen in 1854. Later Lang wrote about her in his newspaper, The Mofussilite:
Her face must have been handsome when she was younger (the Rani was about 19 years old when Lang met her), and even now it had many charms. The expression also was very good, and very intelligent. The eyes were particularly fine, and the nose very delicately shaped. She was not very fair, though she was far from black. She had no ornaments, except a pair of gold earrings. Her dress was plain white muslin, so fine in texture, and drawn about her in such a way, and so tightly, that the outline of her figure was plainly discernible – and a remarkably fine figure she had.
This article is based on the facts known insofar. I do not claim that I have verified the veracity of the real photograph of Jhansi Ki Rani Lakshmibai. The primary aim of this article is to hope that the readers will stop circulating the fake photograph of Jhansi Ki Rani published in newspaper.History of Bundelkhand - बुंदेलखंड का इतिहास
History of Bundelkhand - बुंदेलखंड का इतिहास
कहावत है – ‘‘चित्रकूट में रम रहे, रहिमन अवध नरेश जा पर विपदा परत है, सो आवत इही देश’’
भगवान राम अपने वनवास के समय अयोध्या से आकर चित्रकूट में रहे। यहा के कौल भील लोगों के सानिध्य में रहकर अनेक वर्ष चित्रकूट में विताये। बाद में कालिंजर, पदमावती, मालथौल, खिमलासा मालवा अंचल होते हुये दक्षिण के दंण्डकारण्य में पंचवटी गोदावरी के तट पर वर्तमान में नासिक में रहे थे।
इसी समय सम्राट अशोक का प्रभाव क्षेत्र भी बुंदेलखंड (bundelkhand) रहा अशोक जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसने सांची के स्तूप बनवाये विदिशा उसकी ससुराल थी, विदिशा क्षेत्र में तो संस्कृति और कला को काफी प्रोत्साहन मिला
शुंग, कन्व सातवाहन राजाओं के समय विष्णुपुराण, वायुपुराण भागवतपुराणों का लेखन कार्य हुआ, जिनके दशवें और बारहवें स्कन्धों में इन राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कुषाण राजा कनिष्क जो सूर्यदेव का उपासक था दतिया जिले के उन्नाव में प्राचीन सूर्यमंदिर स्थापित हुआ था वो नये परिवेश में आज भी है। पश्चिमी बुंदेलखंड (bundelkhand) में वालाटक ब्राहम्णों का शासन था जिनका मूल ठिकाना वेतवा के तट पर स्थित वाधाट जिला टीकमगढ़(tikamgarh) था। वे बड़े प्रतापी राजा थे। वाकाटकों का बनवाया हुआ मडखेडा में सूर्य मंदिर दर्शनीय है। वाकाटक, गुप्त और नाग राजा समकालीन थे। गुप्त सम्राट समुद्र गुप्त ने नागों की सत्ता को विखंटित कर स्वयं इस क्षेत्र को अपने आधीन कर लिया था। और वैष्ठव धर्म, संस्कृति का प्रचार किया था। बीना नदी के किनारे ऐरण में कुवेर नागा की पुत्री प्रभावती गुप्ता रहा करती थी जिसके समय काव्य, स्तंभ, वाराह और विष्णु की मूर्तिया दर्शनीय है। इसकी समय पन्ना नागौद क्षेत्र में उच्छकल्प जाति कें क्षत्रियों का शासन स्थापित हुआ था जबकि जबलपुर परिक्षेत्र में खपरिका सागर और जालौन क्षेत्र में दांगी राज्य बन गये थे। जिनकी राजधानी गड़पैरा थी दक्षिणी पश्चिमी झाँसी (Jhansi)–ग्वालियर के अमीर वर्ग के अहीरों की सत्ता थी तो धसान क्षेत्र के परिक्षेत्र में मांदेले प्रभावशाली हो गये थे। छटवीं शताब्दी में खजुराहों में जिजोतियां ब्राहम्ण राज्य स्थापित हो गया था.
प्राचीन काल में बुंदलेखंड(bundelkhand) तपस्वीयों की तपो भूमि थी। कालपी में व्यास ऋषि का आश्रम था। चित्रकूट कालिंजर के पास वाल्मिकि ऋषि रहते थे. कालांतर में यहा चेदी राजाओं का राज रहा जो चिदी वंश के थे। तत्पश्चात् नागों का राज्य रहा जिनकी राजधानी नागाभद्र नागौद थी। नागराजा शैव भक्त थे नाग राज्य कला, संस्कृति में उच्च कोटि का था। इनकी सत्ता सिंधु नदी के किनारे शिवपुरी क्षेत्र की थी। सिंधु के किनारे पर पवा इनकी दूसरी राजधानी थी। रामायण काल में यह क्षेत्र रामचंद्र जी के पुत्र कुश के आधीन था, जिसकी राजधानी कुशावती थी वर्तमान में कालिंजर के नदी के पश्चिमी किनारे लव पुरी थी जो रामचंद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र लव के आधीन थी वर्तमान में लौढी महा भारत काल में इस क्षेत्र में कर्वी नगर करूषपुरी के नाम से विख्यात था जहा दलाकी–मलाकी राजाओं का राज्य था तो विराट नगरी भी इसी बुंदेलखंड (bundelkhand) में थी जिसे वर्तमान में राठ कहा जाता है। भगवान कृष्ण के मौसेरे भाई राजा शिशुपाल चंदेरी में राजा थे तो दंतवा के नाम से दतिया प्रसिद्ध था। सेवड़ा जो सिंधु नदी के तट पर है यहा ब्रम्हा के पुत्रों ने तपस्या की थी।
जिझौती शासन काल में बुंदेलखंड (bundelkhand) की जिझौती कहा जाता था। कालांतर में आठवीं सदी के पश्वात् चंदेल राज्य का आभिरभाव हुआ था जिसकी राजधानी महोवा महोत्सवपुरी थी। चंदेलों ने बुंदेलखंड (bundelkhand) क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र के रूप में पहचान दी थी। उन्होने बुंदेलखंड (bundelkhand) क्षेत्र में चंदेली तालाबों का निर्माण कराकर उनके किनारों पर बस्तिया बसाकर बुंदेलखंड (bundelkhand) क्षेत्र को कृषि के क्षेत्र में अग्रसर किया था। उस समय धान, गन्ना, वनोजप और धी को पैदावार खूब होती थी। चंदेरी का एक पानुसाह सेठ अपने टाढे लेकर इस क्षेत्र में व्यापार करने आते थे तभी से जैन व्यवसायी भी इस क्षेत्र में भाये, क्षेत्र में गुड खूब बनाया जाता था। गन्ने की पिराई वाले पत्थर के काल आज भी गांव–गांव में जाने जाते है। चंदेल राजाओं ने मंदिर स्थापत्य कला, मूर्ति स्थापत्य कला, तालाब स्थापत्य कला पर काफी जोर दिया था। गांव–गांव के चंदेली तालाब और खजुराहों(khajuraho) के विश्व प्रसिद्ध मंदिर एवं अजयगढ़(ajaygarh) के महल चंदेल काल की कला के सर्वोच्च नमूने है जो विश्वप्रसिद्ध है।
सन् 1181–82 में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल राज्य सत्ता पर आमण कर उसे वैरागढ़ उरई के मैदान में पराजित कर अस्तित्वहीन कर दिया था। पृथ्वीराज के चंदेलों की सामरिक महत्ता सांस्कृतिक वैभव को विखंटित कर दिया था। इस युद्ध में चंदेल राजा परमालेख के आल्हा–दल मलखान आदि सरदारों के साथ अन्य सभी सरदास वीरगति को प्राप्त हो गये थे। चंदेलों के बाद महोनी से बुंदेली राज सत्ता का आभिरभाव हुआ। महोनी जो जालौन जिले में पहुज नदी के किनारे बुंदेलों का ठिकाना था जहां का अधिपति सोहनपाल था। सोहनपाल को उसके भाइयों ने महोनी से खदेड दिया था। सोहनपाल महोनी छोड़ कर वेतवा के तटवर्तीय वन आच्छादित क्षेत्र में गडकुडार के समीप आया और बुंदेला, परमार, धंधेरे तीन वर्ग के क्षत्रियों का संगठन बनाकर कुठार के किले को खंगारों से छीनकर सन् 1257 में कुडार में अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी।
1257 से 1539 ई. तक बुंदेलों की राजसत्ता कुडार में रही, तत्पश्चात् महाराजा रूद्र प्रताप ने बेतवा नदी के एक टापू पर ओर से छोर तक 1531 ई. में किले की आधारशिला रखी। क्योकि बेतवा के सूढा टापू के ओर से छोर तक किला बनने के बाद उसका नाम भी ओर छोर से ओरछा (orchha) पड़ गया था। ओरछा (orchha) का किला बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। सधन वन के बीच से प्रवाहित बेतवा नदी जिसकी 2 धाराओं के मध्य टापू पर ओरछा (orchha) दुर्ग अजेय रहा है। जो सामरिक महत्व का अजेय किला रहा है।
दुर्ग के रूप में यह वन दुर्ग, जल दुर्ग और गिरिदुर्ग का संयुक्त रूप से मिले जुले रूप का रहा है। राजा रूद्र प्रताप की मृत्यु 1531 ई. के पश्वात् उनके पुत्र भारतीचंद्र ने ओरछा (orchha) दुर्ग एवं नगर वसाहट को पूर्ण कराया और 1539 ई. में कुडार से राजधानी बदलकर ओरछा (orchha) बना ली थी। कालांतर में ओरछा (orchha) राज्य यमुना से नर्मदा तक एवं सिंधु से सतना तक अर्थात सम्पूर्ण बुंदेलखंड (bundelkhand) में फैला हुआ था। समय के साथ साथ ओरछा (orchha) राजवंश के राजकुमारों को जहा जो जागीरों दी गई थी वहा उन्होने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये थे। इस प्रकार दतिया,चंदेरी,अजयगढ़,पन्ना,चरखाई,बांदा,विजावर,जैसे सभी राज्य ओरछा (orchha) राजवंश के फुटान रहे है। ओरछा (orchha) राजवंश का राजवंशीय वटवृक्ष अथवा रिश्तेदार संबंधियों के राज्य अथवा उनके सेनापति कामदारों के द्वारा स्थापित कर लिये राज्यों के निर्माताओं का संबंध किसी न किसी प्रकार से ओरछा (orchha) राजवंश से रहा है.
सन् 1729 ई. छत्रसाल बुंदेला पन्ना के मददगार बनकर मराठा पेशवा वाजीराव प्रथम पूना से जैतपुर आया था सहायता के उपलक्ष में छत्रसाल ने बुंदेलखंड (bundelkhand) का तीसरा भाग देने की शर्त पर सहायता प्राप्त की थी अस्तु बाजीराव पेशवा ने छत्रसाल की मृत्यु 1531 ई. के पश्चात् बलात बलपूर्वक बुंदेलखंड (bundelkhand) का तीसरा हिस्सा जो 36 लाख 5 हजार रूपये आय का था अपने आधीन कर लिया था चूंकि वाजीराव पेशवा पूना महाराष्ट में रहता था तथा बुंदेलखंड (bundelkhand) में उसके कर्मचारी मामल्ददार रहते थे। जो राजस्व वसूली कर पूना भेजते रहते थे चंूकि मराठे गैर क्षेत्रिय थे बुंदेलखंड (bundelkhand) क्षेत्र गैर क्षेत्रीय मराठों के लिये धन आपूर्ति का एक साधन था, मामल्ददार क्षेत्र की राजस्व वसूली के साथ–साथ बुंदेले ओरे देशी राजाओं, अन्य राजाओं से चौथ एवं सरदेशमुखी बसूलकर पेशवा भेजते रहते थे जो राज्य चौथ देने में आनाकानी करता था उसके राज्य और नगर को वे अपनी ताकारी–पिंडारी सेना द्वारा लूट लिया करते थे। गांबों, नगरों को भाग लगा देते थे। झाँसी (Jhansi) का किला जो ओरछा (orchha) राज्य के महाराणा वीरसिंह जू देव प्रथव का वनवाया हुआ था, मराठा मामन्ददार सरदार नारोंशंकर ने अपने कब्जे में कर ओरछा (orchha) के राजा पृथ्वीसिंह के समय ओरछा (orchha) नगर की खूब लूट मार की थी ओरछा (orchha) नगर के सभी लोगों को बलपूर्वक झाँसी (Jhansi) में बसाया था और ओरछा (orchha) को जनहीन कर दिया था मकानों में उसने आग लगा दी थी जब ओरछा (orchha) नगर निवासियों को नागोशंकर बलपूर्वक झाँसी (Jhansi)ले गया तो ओरछा (orchha) में भगवान रामराजा और किला महल आदि शेष रहे थे
महाराजा विमाजीत सिंह ने सन् 1783 ई. में ओरछा (orchha) से भागकर टेहरी टीकमगढ़(tikamgarh) को अपनी राजधानी बना ली थी। महाराजा विमजीत सिंह ने टेहरी पर पहाड़ी पर किला बनवाया। पहाड़ी के पश्चिमी तरफ राजधानी नगर का विस्तार कराया, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। श्री कृष्ण का एक नाम टीकमजी है, तो कृष्ण उफर् टीकमजी के नाम पर टेहरी के किले एवं नगर का नाम टीकमगढ़(tikamgarh) रखा। 1783 से 17 दिसम्बर 1947 तक अर्थात महाराजा विमजीत सिंह से महाराज वीरसिंह जू देव द्वितीय तक ओरछा (orchha) राज्य का संचालन कार्य टीकमगढ़(tikamgarh) राजधानी से हुआ। अंत में प्रजातांत्रिय शासन की मांग बुलंद हुई, जिस कारण 17 दिसम्बर 1947 की महाराजा वीरसिंह देव द्वितीय ने अपने ओरछा (orchha) राज्य सत्ता को जनता के हाथ सौपकर उत्तरदायी शासन दे दिया था और जनता को राजतंत्र से मुक्त कर दिया था
लुप्त होते बुन्देली लोक नृत्य - Dances of Bundelkhand
लुप्त होते बुन्देली लोक नृत्य - Dances of Bundelkhand
सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन के दौर में सक्रमण काल से गुजर रहें बुन्देली भूभाग में लोक नृत्य अब विलुप्त की कगार पर पहुंच गये है बुन्देली लोक नृत्य पंरम्पराओं को बचाने के लिए समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो सैरा नृत्य, डोमरहा नृत्य, जवारा नृत्य, कीर्तन नृत्य, कानड़ा नृत्य, चांचरा या पाइ-डण्डा नृय, झांझिया नृत्य, मोनिया नृत्य, देवी नाच, चमराहा नृत्य, कहारों का नाच, राई नृत्य, ढिमराई नृत्य, कुम्हराई नृत्य, दुलदुल घोड़ी नाच, खशुआ नाच, चांगलिया नाच, सिर्फ अतीत का इतिहास बनकर रह जायेगें। कानडा नृत्य धोवी जाति का परम्परागत नृत्य है।भगवान कृष्ण या कान्हा से सम्बन्धित इस नृत्य को नया जीवन तथा नया सम्बल और पुर्न प्रतिष्ठा दिलाने वाले सागर के लक्ष्मीनारायण रजक ने कहा था कि किसी जमाने में कानड़ा नृत्यकों को समाज में इतना सम्मान और नेंग मिलता था कि उसे और जीवनकोपार्जन के लिए नहीं भटकना पड़ता था पहले विवाह में पग-पग पर कनाडियाई होती थी हल्दी चढ़ाते समय, मैहर का पानी भरते समय, मण्डप छपते समय, बरात विदा होते समय, बारात की अगुवानी में कनाड़ियाई होती थी बिना कनड़ा नृत्य की शादी विवाह नहीं होते थे।
लेकिन आजकल कानड़ा को कोई बुलाते नहीं है पहले कनड़ा विवाह का अनिवार्य अंग था इसलिए कानड़ा के बहुत से कालाकार होते थे लेकिन आजकल कानड़ा नृत्य के स्थान पर विवाह में लोग बैण्ड बाजों या रेकाडिंग से काम निकालने लगंे है, इसलिए कानड़ा नृत्य के कलाकार आज न के बराबर है। अब तो कोई शादी विवाह में कानड़ा करवाते है आर्थिक अभाव के कारण ही कानड़ा नृत्य छूटता जा रहा है केवल सांरगी लोटा से कानड़ा नृत्यों का आज पेट नही भरता, वे कानड़ा को छोड़कर अन्य मजदूरी की तलाश में भटकने लगे इससे हमारे लोक कला जगत की एक महत्वपूर्ण विधा की बहुत बड़ी हानि हुई है।
पहले एक ही विवाह में दो-तीन कानड़ा नृत्यक पहुॅचते थे वहां प्रतिस्पर्धा होती थी प्रत्येक कानड़ा कलाकार अपनी-अपनी कला के माध्यम से श्रेष्टता सिद्ध करता था अब तो गणेश उत्सव या नवरात्रि उत्सव ही कानड़ा नृत्य के अवसर रह गये है कभी-कभी शिशु जन्म पर खुशी से कोई-कोई कनिड़ाई गंवाते नचवाते हैं। ऊॅचे-परे गांव के किसान जैसी कद-काठी वाले जब लक्ष्मीनारायण रजक कानड़ा की पारम्परिक भेश भूषा और सिंगार कुर्ता, बांगा, कंदिया, सेली, सेली, वाजूबंद, पकड़ी, कलगी, लगाए पैरों में घुघरू बांधे हाथ में सांरगी लिये निकलते है तो कानड़ा के इस सज्जन कलाकार को देखकर दर्शक ठगे रह जाते है और जब सारंगी मृदंग लोटा, झूला, कसावरी, टिमकी और खजरी की संगत के साथ कानड़ा गीत में बुन्देली शब्द, बिरहा, रमपुरिया, राई सैरा, दादरों की धुन लय ताल में निकालते है तो कानड़ा नृतक की पैरो की थिरकन और कमर की लचक तथा नृत्य की वृत्तीय गतियां देखते ही बनती है।
लक्ष्मीनारायण रजक कानड़ा के दक्ष कालाकार हैं। जिन्होंने इस नृत्य को नई गति प्रदान की श्री रजक ने कृष्ण लीला, रामचरित महाभारत की कथाओं श्रृगांर तथा सामाजिक विषयों पर कानड़ा की परम्मपरागत धुनों में बुन्देली की कई रचनाएं की और अन्य कवियों के छन्दों को गाना शुरू किया। लेकिन उनके द्वारा पुर्न प्रतिष्ठित यह कला काल के गाल में समाने के लिए धीमे-धीमें जा रही हैं।
बुन्देली लोक बाध्य अलगोजा, मौहर, रमतुला, बीन, डपला, दौंड़, नगाड़ा, खजली, अंजलि, नगडिया, तांसा, चंग, नरगा, इकतारा, कसौरा, जोरी या झांझ, चिमटा आदि बाद्यय बजाने वाले कलाकार धीरे-धीरे सिमट रहें है। लोक संस्कृति विभाग सिर्फ नाम के आयोजन करके भारी धनराशि लोक संस्कृति के नाम पर व्यय तो कर रही है लेकिन इन नृत्यों को बचाने के लिए कुछ सार्थक प्रयास नहीं हो रहें है झांझिया नृतक द्वारा गाये जाने वाला यह गीत ‘‘हरी री चिरैया, तोरे पियेर रे पंख, सो उड़-उड़ जाये, बबुरा तोरी डार’’ की गति हो रही है राई नृत्य करने वाली बेड़नी की हालत अत्यन्त खराब है राई, बुन्देलखण्ड के श्रेष्ठतम लोक नृत्यों में से हैं।
भादों में कृष्ण जन्माष्टमी से प्रारम्भ होकर, यह नृत्य फाल्गुन माह में होली तक चलता है। इस नृत्य का नाम राई क्यों पड़ा, इसका तो कोई निश्चित कारण पता नहीं चल पाया, पर बुन्देलखण्ड की बेड़नियों द्वारा किया जाने वाला और अपनी विशिष्टता में मयूर-मुद्राओ का सौन्दर्य समेटै, यह नृत्य अपने यौवन काल में राज्याश्रृय प्राप्त दरबारी नृत्य रहा हैं अब इसे अन्य लोग भी करने लगे हैं। बेड़नियाॅ यह नृत्य करते हुए, अपने यौवन काल में राज्याश्रृय प्राप्त दरबारी नृत्य रहा है। अब इस अन्य लोग भी करने लगे हैं।
बेड़िनियाॅ यह नृत्य करते हुए, अपनी शरीर को इस प्रकार लोच और रूप देती है कि बादलों की गड़गड़ाहट पर मस्त होकर नाचने वाले मोर की आकृति का आभास मिलता हैं। इसका लहंगा सात गज से लेकर सत्तरह गज तक घेरे का हो सकता है। मुख्य नृत्य मुद्रा में अपने चेहरे को घूॅघट से ढंककर लहंगे को दो सिरों से जब नर्तकी अपेन दोनों हाथों से पृथ्वी के सामानान्तर कन्धें तक उठा लेती है, तो उसके पावों पर से अर्द्ध चन्द्राकार होकर, कन्धे तक उठा यह लहंगा नृत्यमय मयूर के खुले पंखों का आभास देता हैं।
नृत्य में पद संचालन इतना कोमल होता हे कि नर्तकी हवा मेें तैरती सी लगती है। इसमें ताल दादरा होती है। पर अन्त में कहरवा अद्धा हो जाता है साथ में पुरूष वर्ग लोग धुन गाता है। नृत्य की गति धीरे-धीरे तीव्र होती जाती है। राई में ढोलकिया की भी विशिष्ट भूमिका होती है। एक से अधिक छोलकिए भी नृत्य में हो सकते है। ढोलकिए नाचती हुई नर्तकी के साथ ढोलक की थाप पर उसके साथ आगे-पीछें बढ़ते हैं, बैठते हैं, चक्कर लगाते हैं। नृत्य चरम पर ढोलकिया दोनों हाथों के पंजों पर अपनी शरीर का पूरा बोझ सम्भाले हुए, टांगे आकाश की ओर कर, अर्द्धवाकार रेखा बनाकर आगे-पीछे चलता है। इस मुद्रा मे इसे बिच्छू कहा जाता है।
राई नृत्य में नर्तकी की मुख्य पोशाक-लहंगा और ओढ़नी होती है वस्त्र विभिन्न चमकदार रंगों के होते है। दोनों हाथों में रूमाल तथा पंावों में घूॅघरू होते हैं। पुरूष (वादक) बुन्देलखण्डी पगड़ी, सलूका और धोती पहनते हैं राई के मुख्य वाद्य ढोलक, डफला, झींका, मंजीरा, तथा रमतुला है। इस लोक नृत्यों को बचाने के लिए बुन्देलखण्ड में ही लोक संस्कृति केन्द्र की स्थापना जरूरी है। तभी बुन्देली लोक गीत नृत्य, तथा लोक वाद्य सुरक्षित और संरक्षित रह सकेगें।
Rai Dance -- Through the centuries Raai has been the folk dance which has touched its peak as a classical dance. Later, Raai degenerated its aesthetical value and lost its classical expression. Today it remains simply as a folk dance. Raai means a mustard seed. When a mustard seed is thrown into a saucer, the seed starts to swings around. This way mustard seed moves in the saucer, the dancers also swings and when the singers sing the lyrics of the song the dancers follow the beats with foot steps. It is a duet and the competition is between the beats of the drum and foot steps of the dancer. The drummer and the dancer try to win each other and this comp
Badhiya Dance -- Badhaiya is a ceremonial dance. It is performed on child birth, marriages or any other get together to celebrate happiness and joy. The collective moments of dancers show the unique expressions of their faces. With rhythm and movements they greet for the occasion
Ravala Dance -- Ravala dance in Bundelkhand is basically a dance drama. The farm labour community of Bundelkhand performs Ravala during marriages. It is performed with very funny expressions and humorous dialogues. The audiences are entertained by these expressions of dance and the dialogues of drama.
Divari Dance-- This dance in Bundelkhand is performed every year during the festival of light Diwali/Deepawali in the end of October or first week of November according to lunar calendar. In this connection the epic story goes that “in Gokul” when Lord Krishna raised Goverdhan Parvat on his finger to save the local people, they danced in joy. The dancers wear multi-coloured apparels and the chief dancer holds the peacock feathers in his hands and the rest stick those feathers in their half pants. The main instruments used in this dance are ‘Dholak’ and ‘Nagaria’ (both being a form of drums). The male dancers with long sticks show the marshal arts when the beats of drums inspire their energy and emotions. This dance is also performed as a ‘thanks giving’ after harvesting.
Pahunahi Dance This song and dance is performed to welcome the guests in particular.
Khidkiyan of Jhansi Fort
Khidkiyan of Jhansi Fort
The Jhansi fort is situated in the outskirts of Jhansi in uttar Pradesh. It was Built in the year 1613 by Raja Bir Singh Deo of Orchha.The fort extends to a sprawling expansion of 15 acres (61,000 m2) and this colossal structure measures about 312m in length and 225m in width. On the whole, there are twenty-two supports with a mammoth strengthening wall cosseted by a moat on both sides. The shattered upholder on the eastern side was rebuild by the British, who also supplemented a floor to Panch Mahal. Every year in the month of Jan-feb a grand occasion is held known as Jhansi Mahotsav many eminent personalities and artist perform their play .The fort proper has occupied an area of 15 acres and measures 312m in length and 225m in width. Altogether, there are twenty-two bastions with a huge fortification wall protected by a moat on two sides. A bastion on the eastern side was destroyed, which was reconstructed by the British, who also added a floor to Panch Mahal.
There are also four khirkis (entrances) made in the walls-Ganpatgir-ki-Khirki, Alighol-ki-Khirki, Sujan khan- ki-Khirki and Sagar Khirki. The main structures within the fort are Baradari, Ganesh mandir, Shahar Darwaza, Bhawani shnakr, Kadak bijali, Grave of Gulam Gaus Khan, Panch Mahal, Siva temple, Execution tower, Kal kothari, etc. Although, when I discussed with the local people , i came to know about two more khidki , Bahiron Khidki and Billaiya khidki.
Ganpat khidki
AliGol ki khidki
Suje Khan khidki
Sagar Khidki
Bhairon Khidki
Billayia khidki
The Gates in Jhansi City
Jhansi Fort or Jhansi ka Kila is a fortress situated on a large hilltop called Bangra, in Uttar Pradesh, Northern India. It served as a stronghold of the Chandela Kings in Balwant Nagar from the 11th through the 17th century.
In 1728, Mohammed Khan Bangash attacked Chattrasal. and helped Maharaja Chattrasal defeat the Mughal army. As a mark of gratitude, Maharaja Chattrasal offered a part of his state, which included Jhansi, to Mohammed Khan Bangash. In 1742 Naroshanker was made the subedar of Jhansi. During his tenure of 15 years he not only extended the strategically important Jhansi fort (the extension is called Shankergarh), but also constructed other buildings. In 1757, after Naroshanker was called back by the Peshwa. Madhav Govind Kakirde and then Babulal Kanahai were made the subedars of Jhansi. From 1766 to 1769 Vishwas Rao Laxman served as the subedar of Jhansi. Then Raghunath Rao (II) Newalkar was appointed the subedar of Jhansi. He was a very able administrator, increasing the revenue of the state and building both the MahaLakshmi Temple and the Raghunath Temple.
After the death of Shiv Rao his grandson Ramchandra Rao was made subedar of Jhansi. His poorly administered term ended with is death in 1835. His successor Raghunath Rao (III) died in 1838. The British rulers then accepted Gangadhar Rao as the Raja of Jhansi. The inefficient administration of Raghunath Rao (III) left Jhansi in a very poor financial position.
However, he was succeeded by Raja Gangadhar Rao, who was a very good administrator. He was reportedly very generous and sympathetic, and the local population of Jhansi was well satisfied. In 1842 Raja Gangadhar Rao married Manikarnika Tambe who was the given the new name of Lakshmi Bai. Lakshmi Bai ruled Jhansi after the death of her husband and used the fort as her residence. In 1858 she led Jhansi forces against those of the British East India Company.
The fort standing in the hilly area shows how the north Indian style of fort construction differs from that of the south. In the south most of the forts were built on the sea beds like Bekal Fort in Kerala. The granite walls of the fort are between 16 and 20 feet thick and on the south side meet the city walls. The south face of the fort is almost perpendicular.The fort extends to a sprawling 15 acres (61,000 m2) and this colossal structure measures about 312m in length and 225m in width. On the whole, there are twenty-two supports with a mammoth strengthening wall surrounded by a moat on both sides. The shattered upholder on the eastern side was rebuilt by the British, who also added a floor to Panch Mahal.
The Gates in Jhansi City
The old city wall had ten gates known as Khanderao, Datia, Unnao, Orchcha, Baragaon, Lakshmi, Sagar, Sainyar, Bhander and Jhirna. The first eight still have wooden doors and of the last two, the former is completely closed and the latter is open. A breach in the wall between Sainyar gate and Jhirna gate, which was made by Hugh Rose’s batteries during the assault on the fort in 1858, is still in existence. There are also four khirkis (entrances) made in the walls-Ganpatgir-ki-Khirki, Alighol-ki-Khirki, Sujan khan- ki-Khirki and Sagar Khirki.
1.BadaGaon Gate
2.Bhanderi Gate - Bhanderi gate of the fort of Jhansi through which Rani Laxmibai escaped from the fort during the 1857 Indian war of independence.
3.Chand Gate
4.Datiya Gate
5.Khanderao Gate
6.Laxmi Gate
7.Orcha Gate
8.Sagar Gate
9.Saiyer Gate
10.Unnao Gate
The Beauty of Jhansi
Duknu Rock
Duknu rock is on the way from jai academy to dongri
Orcha
Rani Mehal
Rani Mahal of Jhansi was actually the palace of Lakshmi Bai, Rani of Jhansi. The palace of Lakshmi Bai has now been converted in to a museum that treasures the memory of Rani Lakshmi Bai as well as the archeological remains of 9th to 12th century that has been excavated and unearthed recently.
Rani Mahal is the former residence of the Rani of Jhansi that was built in the late 18th century. The palace consists of arched chambers around an open courtyard that looks magnificent and is a welcome break from the typical architectures of Bundelkhand. The palace has been the epicenter of the Great Sepoy Mutiny of 1857 in Bundelkhand region. Various plans for mutiny were hatched in this palace when the British Resident turned down the repeated efforts for reconciliation from Rani’s side.
When the 5th unit of the 12 Native Regiment revolted in the nearby fort, people close to Rani rose in revolt too and massacred every possible European sol of the city.The retaliation was quick and equally ruthless. In a notorious incident at the palace, British troops stormed the building through a rear stable and massacred 50 of the Rani ’s Royal Bodyguards. The only spot worth seeing in the palace apart from the museum is the durbar hall. Located on the 2nd floor, Durbar Hall features an original painted wood-paneled ceiling.
Betwa
The Betwa is a river in Northern India, and a tributary of the Yamuna. Also known as the Vetravati, the Betwa rises in the Vindhya Range just north of Hoshangabad in Madhya Pradesh and flows north-east through Madhya Pradesh and flow through Orchha to Uttar Pradesh. Nearly one-half of its course, which is not navigable, runs over the Malwa Plateau before it breaks into the upland.
A tributary of the Yamuna River, the confluence of the Betwa and the Yamuna Rivers takes place in the Hamirpur town in Uttar Pradesh, in the vicinity of Orchha.
In Sanskrit 'Betwa' is 'Vetravati' which means ‘containing reeds'. This river is mentioned in the epic Mahabharata along with the Charmanwati river. Both are tributaries of Yamuna. Vetravati was also known as Shuktimati. The capital of Chedi Kingdom was on the banks of this river.
 |
| Betwa at Notghat Bridge |
 |
| Betwa at Sukwa Dhukwa |
Barwa Sagar
Barwa Sagar fort was Built by the Bundela Udot Singh in 1705, it has seen its share of bloodshed. In 1744, a brother of Gwalior's Scindia ruler was killed here during a battle with the troops from nearby Orchha. That skirmish seemed like a Sunday school picnic compared to what followed in the melee of 1857-58. Moropant Tambe, the father of Rani Lakshmibai of Jhansi captured the fort by evicting the garrison. Later, it became the setting of a battle in which the British commander Hugh Rose defeated an army under the leadership of Tatya Tope who was on his way to Jhansi to relive the garrison there. The years afterward were peaceful, with the fort becoming a British outpost and, at times, a place for touring officials and surveyors to break journey.
From the top of the tower can also be viewed the sizable water body behind the fort. This is the "sagar" in Barwa Sagar, an artificial lake created by the making of an irrigation dam by the Chandellas. Incredibly, the dam is intact and still in use. In Bundelkhand - a region plagued by chronic water shortages, the water of the lake is used for irrigation, fishing and personal ablutions by the villagers. Maybe our planners need to take a lesson from the Chandellas.
Barua Sagar Tal is a large lake situated in Barua Sagar near Jhansi.It is a large lake and it was created about 260 years ago by Raja Udit Singh of Orchha, who built the embankment.
Jarai-ka-Math
It is a beautiful temple dedicated to goddess Amba in Barua sagar.Jarai-ka-Math was Built during the reign of the Pratiharas. The temple dates backs to approximately 860 AD, this red sandstone temple is a pancharata shrine of the Panchayatan type, in which the main temple is surrounded by four subsidiary shrines at the four corners.
The temple is a repercussion to the vigorous temple-building activity which became a characteristic feature of the Chandellas. The temple is dedicated to Devi (Amba or Durga) whose multifarious forms are represented in the profusely carved sculptures along the temple walls. The temple stands on elevated ground dominating its surroundings. The main image of the deity is missing from the sanctum sanctorum. Only the pedestal, and the jeweled right foot of a female placed on a lotus stalk, remains. This detail is traditionally associated with the goddess Tara or Mateswari.
The placement of a miniature, sixteen-armed image of a goddess on the central lintel of the entrance further supports the conjecture that the temple is dedicated to a goddess. Erotic sculptures, akin to those at Khajuraho, also grace the Jarai-ka-Math.
Ghugua Math, Barwa Sagar taken by an unknown photographer, c. 1890s and forms part of the Archaeological Survey of India Collections. The North-Western Provinces list gives the following information, "...Close to the banks of the lake, is a small unique temple of the early Chandella period, measuring 15 feet by 12 feet, and built of massive blocks of grey granite without mortar. The temple proper consists of four small cells, each of which has a slightly ornamented door, and is capped with a kalasa resting on a low pyramidal row of stones. Over three of the doors is a small figure of Ganesha, whilst the fourth contains a figure of Durga. The portico in front of the temple is supported on five massive pillars, with cruciform capitals, topped by large architraves and massive slabs."
Pahuj Dam
Pahuj River is a river flowing in Bhind District of Madhya Pradesh in central India.
It is tributary of Sindh River, which joins Yamuna River in Etawah Uttar Pradesh state, just after the Chambal River confluences into Yamuna river.
Sukwa-Dhukwa
This dam was constructed on Betwa river during 1905 and is located on
Jhansi Lalitpur Highway. The Dam is about 4000 ft. in length. There is a inspection house here which offers a panoramic view of the dam and its upstream Lake.
Pariccha
Parichha is a town in Jhansi district in Uttar Pradesh.Paricha Dam is about 25 km from Jhansi on the National Highway 25. Built on the Betwa River, its reservoir, a placid stretch of water that runs to Notghat Bridge, is 34 km away. Parichha houses a 640 MW coal based power station (soon to be expanded close to 1140 MW). It is located on Jhansi-Kanpur highway.
Matatila
The Matatila Dam, is a dam in India that was built in 1958 on the Betwa River. Situated 93 km away from Deogarh, this earthern dam is 35 m high.
The catchment area is around 20 sq km with a maximum storage capacity of 1132 mcm.
Nestled between a large numbers of small hills, this place is popular among tourists. Water sports facilities are also available.
RajGhat Dam
The foundation stone for this modern monument was laid by Late Smt. Indira Gandhi in 1971. The catchment area formed by the dam is around 17000 square kilometres, which had led to the submersion of around 70 villages.
The length of the sand barrier constructed is more than 11 kilometres, which is longest sand barrier in any dam in Asia
Deogarh
Deogarh is a small farming village near the town of Lalitpur in Lalitpur district, in the state of Uttar Pradesh."Deogarh" derives from the Sanskrit Deo and garh, "God" and "fort", compounded to mean "fort of the Gods". This term, "House of God", is also widely used as a place name for villages in the vicinity of temples within fort-walls throughout India. it is known for its Gupta monuments, located on and near the hill fort on the right bank of the Betwa River. A number of ancient monuments of Hindu and Jain origins are found within and outside the walls of the fort.

The Gupta temple dedicated to Lord Vishnu, popularly known as the Dashavatara Temple, is the earliest known Panchyatana temple in North India. It depicts ten incarnations of Vishnu. Special features of this ancient temple, which is mostly in ruins, include carved figurines of river goddesses Gangaand Yamuna on the doorway to the sanctum sanctorum, three large carved panels of Vaishnava mythology related to Gajendra Moksha, the Nar NarayanTapasya (meditation), and the Anantshayi Vishnu reclining on a serpent
Deogarh's strategic location on the ancient route to the Deccan Plateau made it a historically important place. Its antiquarian, archaeological and epigraphical importance are linked to the Gupta period, the Gurjara–Prathiharas, the Gonds, the Muslim rulers of Delhi, the Marathas and the British eras.
The fort on the hill is dominated by a cluster of Jain temples on its eastern part, the oldest of these dating to the 8th or 9th century. Apart from Jain temples, the wall frescoes of Jain images of "iconographic and the stylistic variety", are special features of the fort. The three ghats (ghat means "flight of stone steps leading to the river"), which provide approach to the Betwa river edge from the fort — the Nahar Ghat, the Rajghat and the ghat with the Siddiki Ghufa (saints cave) — are also of archeological significance.The fort of Deogarh is in a valley which generally has a gentle slope. The valley is formed by the Betwa River at the western end of the hills of the Vindhya Range. Known earlier as Vetravati (Sanskrit, meaning "containing reeds"), the Betwa River is a tributary of the Yamuna River, and skirts the fort hill on its southern side. The river, flowing at a bend near the fort, has a rocky bed. It flows in a cascade of deep pools with steep rocky banks of sandstone formations. The fort is located on a precipice of the steep cliff, just above the river on its right bank
The Deogarh monuments can be categorized based on their location at valley and fort temples, which are generally built with sand stones of brick-red colour. The valley temples consist mainly of Hindu temples from the Gupta period near the Deogarh village..
Sonagiri Temples
Sonagiri Temple Complex is situated near Jhansi at a distance of 35 km. Actually it is closest (10 Km) to the town of Datia on the Jhansi Gwalior road, which is slated to become a part of the ambitious North – South Highway corridor.
Photograph of the group of Jain temples at Sonagiri, taken by George Edward Herne in 1869. Sonagiri is a sacred place of pilgrimage for the Digambara Jains since the time of Bhagwan Chandraprabhu (the 8th Tirthankara) who attained salvation there.
LORD CHANDRAPRABHU IDOL There are seventy seven beautiful Jain temples in hills and twenty six temples in village.The temple no. fifty seven on hill is the main temple. This temple has attra- ctive artistic spire. In this temple the principal deity is Lord Chandraprabhu, eleven feet in height. Two other beautiful idols of Lord SheetalNath & Parsvnath are installed.There is a column of dignity ( Manstambh ) 43 feet in height and an attractive model of Samavsharan. The samavsharan of Bhagwan Chandraprabhu came here for seventeen times. Nang, Anang, Chintagati, Pooranchand, Ashoksen, Shridatta and many other saints achieved salvation from here. This is the unique place known as Laghu Sammed Shikhar covering the area of 132 acres of two hills.
Photograph of a temple at Datia in Madhya Pradesh from the Album of 'Views of Central India by Deen Dayal, Indore', taken by Deen Dayal in the 1870s. Datia is an ancient town already mentioned in the Mahabharatha as "Daityavakra". .
The town is a pilgrimage centre for the devotees of Siddhapeeth Shri Peetambara Devi. Among the many temples are a temple with Mughal style frescoes and the Gopeshwar Temple. The principal monument is the seven-storeyed palace of Raja Bir Singh Ju Deo, built on a hill overlooking a lake
There are around 77 temples on the hill with tall spires. Those in this view have towers topped with either conical or round domes and are futher elaborated with ornamental pavilions on their flat roofs,
 Sonagiri ( literally, the golden peak) is a place sacred to Digambar Jains.
Sonagiri ( literally, the golden peak) is a place sacred to Digambar Jains.
Portrait of Arjun Singh of Datia, brother of Maharaja Bhawani Singh from the 'Album of cartes de visite portraits of Indian rulers and notables' by Bourne and Shepherd, early 1870s. Datia, located in Madhya Pradesh, was controlled by the descendants of the Bundela Rajput family of Orcha from the start of the eighteenth century. Bhawani Singh (1846-1907) succeeded as Raja of Datia in 1857 but disturbances arose as Arjun Singh, an illegitimate son of the last chief and brother of Maharaja Bhawani Singh aspired to the throne. But he was suppressed by a British force and exiled to Benares.
Watercolour drawing by Frederick Charles Maisey of the gateway of the old fort at Seondah in Madhya Pradesh, from an album of 60 drawings dated 1847-1854. In the 'Descriptive list of drawings of Captain Maisey' the artist wrote, "Syundah, or Syurdah, is a considerable town on the Sind river…in the Datya territory. Besides a modern fort, there is an old one, among the ravines, now quite ruined…The old fort and town, which were probably built at the commencement of the 16th Sambat century, have been entirely ruined by the gradual formation of ravines; of the town and village, scattered stones and bricks alone mark the site: the remains of one of its entrance gateways still exist…The first gate of the Fort is still pretty perfect; it consists of a fine bold archway, not at all Hindu in appearance, with usual loopholed chambers on either side.
Photograph of the Cenotaph and Palace of the Rajah of Datia at Datia in Madhya Pradesh taken by George Edward Herne in 1869. Datia is built on a series of low hills and is famous for the Nrising Dev Palace, also known as the Govind Mandir, built around 1620 by Rajah Bir Singh Deo and considered one of the best surviving examples of early 17th Century Rajput architecture. Just outside the town is the palace of Raja Subha Karan, Rajgarh, possibly the building in the background of the photograph, which now contains government offices. The cenotaph in the foreground is one of many fine examples to be found in the area.
Photograph of a temple at Datia in Madhya Pradesh from the Album of 'Views of Central India by Deen Dayal, Indore', taken by Deen Dayal in the 1870s. Datia is an ancient town already mentioned in the Mahabharatha as "Daityavakra". The town is a pilgrimage centre for the devotees of Siddhapeeth Shri Peetambara Devi. Among the many temples are a temple with Mughal style frescoes and the Gopeshwar Temple. The principal monument is the seven-storeyed palace of Raja Bir Singh Ju Deo, built on a hill overlooking a lake.
Photograph of the Rajgarh Palace at Datia in Madhya Pradesh, from the Lee-Warner Collection: 'Scenes and Sculptures of Central India, Photographed by Lala Deen Diyal, Indore.', taken by Deen Dayal in the 1870s. Datia was the capital of the principality of the same name under the Bundela Rajputs in the 16th and 17th centuries. The Rajgarh Palace, seen in this view, is situated west of the old palace known as Nrising Dev Palace or Govind Mandir (c.1620). It was built by Subhakaran and accomodates governmental offices. This is a view looking across the lake towards the palace on the hillside beyond.
 |
| Narsing Palace |
 |
| Narsing palace |
 |
| RajGarh palace |
Shri Pitambara Peeth
The ashram is located in Datia town of Madhya Pradesh, India approx 75 km from GWALIOR ( Airport) and approx 25 km from Jhansi. It is well connected by train and the ashram is around 3 km from the Datia railway station
Shri Pitambra Peeth is a complex of temples (including an Ashram), which according to many legends was a 'Tapasthali' (place of meditation) of many mythological as well as real life people. The shivlingam of shree Vankhandeswar Shiva is tested and approved by the Archeological Survey of India to be of the same age as that of the Mahabharata. It is primarily a Shakta place of worship (devoted to Mother Goddess).
This shakti peeth has Vankhandeswar Shiva Temple as well which is said to be of the time of Mahabharata.
Pujyapaad was called 'Swamiji'or 'Maharaaj' by the devotees. No one knows from where he came, or his name; nor did he disclose this to anyone. However, he was a Dandi Swami. Living legend who knows about Swamiji is Pt Shri Gaya Prasad Nayak ji (Babuji) of Garhi Malehara. Pujya Swamiji Maharaj and Babuji's Guruji were Gurubhai.
Pujyapaad was a strong devotee of the Goddess Pitambara. He had a natural liking for the Sanskrit language. He was having good knowledge of Urdu, Persian and Arabic, English, Pali, Prakrit languages. He liked the classical music and various great classical musicians of that time used to visit the ashram. Some of the musicians who visited the ashram are Pundit Gundai Maharaj, Siyaram Tiwari, Rajan Sajay Mishra, Dagar Bandhu etc. One of the greatest classical musician Acharaya Brhaspati was follower of Pujyapaad.
Unao Balaji
The Balaji, a famous and rare sun temple of its own unique architecture, is situated in a very small town Unao of Datia district in Madhya Pradesh. The Balaji temple was built in the pre-historic time by the king of Datia.
It is said that a cow used to go to a particular place to get fed in the outskirts of Unao. The cow every day pours her milk at that particular place. The cow was belong to a person of caste "Kachhi", the people of this caste generally used to grow vegetables. The owner of cow was not aware of this incident. Once a person of Lodhi caste saw that the cow is pouring her milk on the earth. The people of this cast have the occupation of assassinating cows. He immediately grabbed the opportunity and assassinated the cow. On the following night, The God Sun comes in the dreams of the king of Datia and told the king to dig him out from the location, where the cow used to pour her milk. Next morning, King called his boys and dug out the place and found a statue of GOD SUN. He built a temple in Unao and established the statue on a brick platform, and as said by the god sun, the owner of that cow has been assigned the Priest. Since then only people belonging to "Kachhi" caste can only sit at the brick platform and offer garlands, prasadas to the deity. While in India, only a person belonging to Brahmin caste can offer worship. The pilgrims and pandas(people belong to Brahmin caste)also take part in the worship of the deity but the main priest is said to be "Kachhi" caste people.
The Balaji temple is situated in the vicinity of Unao. Unao is a small town which falls under Datia district in Madhya Pradesh. Unao is 17 km away from Datia and around 17 km from Jhansi (famous for Jhansi ki Raani, LakshmiBai)Jhansi. Unao, makes a segment of a circle with Datia and Jhansi being the crossing point of the chords in the segment. Unao can be reached by any of the two places.
he Sun Temple at Unao in Madhya Pradesh is unique in its architecture. The Sun God is the main deity of this temple. The Sun God stands on a brick platform covered with black plates. Twenty-one triangles, representing the 21 phases of the Sun are engraved in the shrine. Here, special worship is offered on Sundays. Local belief is that worshippers find relief from skin ailments at this temple.
The deity Balaji is very much famous for curing skin ailments. People from far distant places come and worship the deity. Below the temple, a river Pahooj is also flowing. There are some wells in the river, at the time of summer, people used to have bathe with the water in the wells. It is said that if you have bathe in river and offer water to deity Balaji, all your incurable skin ailments will be cured within few days. Sunday is considered as the day of deity Balaji (Sun). All the inhabitants of Unao and the surrounding region has enormous faith in the deity and also have felt the power of it.
Jhansi - The Evolution - Vintage collection
Jhansi - The Evolution - Vintage collection
Jhansi is a city in the state of Uttar Pradesh. It is about 415 km from Delhi and 292 km from Lucknow, and the gateway to Bundelkhand. Jhansi grew in popularity during the reign of the Marathas because of the heroics of its valiant queen, Rani Lakshmi Bai. She had valiantly fought against the Britishers during the 1857 revolt.
Jhansi, sometimes known as Balwantnagar, was founded by Bir Singh Deo Raja of Orchha who built a fort here on top of a rocky hill in 1613. A town soon developed which remained in possession of the Bundelas until 1742. At this point it was seized by the Marathas who built the great stronghold, Shanker Fort, an extension of the older structure. The rapid growth of Jhansi during this period was partly due to the forcible removable of people from other places. It was subsequently held by Shuja-ud-daula, Nawab of Oudh for a few months and later wrested from him by Anup Giri Gosain of Moth from whom it passed to the Raja of Orchha. In 1766 it was again brought under Maratha rule. The East India Company acquired certain rights over the area in 1805 and in 1853, with the death of Raja Gangadhar Rao, the territory lapsed to the British. The town is notable for its associations with Lakshmi Bai, Rani of Jhansi, a leading figure in the Indian Uprising of 1857.
Jhansi was first known as Shankargarh, when Orchha was the capital of Bundelas. In a bid of strengthening the security of Orchha, its king Raja Bir Singh Ja Deo had constructed a fort on a hill in Shankargarh. And it was when he looked at the site for the new fort from his Orchha palace that he realized the place looked like a jhain-si (blurred shadow). And this is how Jhansi got its present name.
Photograph of the Fort of Jhansi in Uttar Pradesh, from the Lee-Warner Collection: 'Scenes and Sculptures of Central India, Photographed by Lala Deen Diyal, Indore.', taken by Deen Dayal in 1882. The fort of Jhansi was built under the rule of Raja Bir Singh Deo (1605-27) of Orchha in the turbulent area of Bundelkhand. It is situated on a rocky hill in a strategic position. Jhansi remained a small village until 1742 when it was taken by the Maratha general, Naru Shankar who strengthened and enlarged the fort. The territory was later under the control of Peshwas until it passed to the hands of the British East India Company after the death of Raja Gangadhar Rao in 1853. In 1857 a few men of the 12th Bengal Infantry mutinied, shot their European officers and seized the fort. The Rani of Jhansi, Lakshmi Bhai, who had been disposed, tried to take control with no success. In 1858 the British recaptured the town after a very hard fight in which the Rani took part. She finally fell after a heroic fight on 18 June 1858 outside Gwalior and is now considered a heroine of Indian independence.
This fort is none other than the famous Jhansi Fort. Jhansi fort was built in 1613 and today has a wonderful collection of sculptures that depicts the history of Bundelkhand. It is said that Jhansi grew around this fort which crowns a neighboring rock. There are many sculptures of the 9th to 12th centuries found in the Rani Mahal too. The museum of Jhansi houses regional antiques like sculptures, manuscripts, paintings, arms and silver, gold and copper coins.
view from Kemasin ki taoriya
In 1861 the city of Jhansi and a dependent territory was ceded to Gwalior State and the capital of the district was moved to Jhansi Naoabad (Jhansi Refounded), a village without "cantonment" (military camp). Jhansi (the old city) became the capital of a "subah" (provínce) within the state of Gwalior, but in 1886 was returned to British rule as a district of the United Provinces of Agra and Oudh in exchange for the Gwalior Fort and the cantonment of Morar nearby.(It had been given to the Maharaja of Gwalior, but came under British rule in 1886 as the result of a territorial swap.)
The Queen - Lakshmibai, Rani of Jhansi
The Queen - Lakshmibai, Rani of Jhansi
Originally named Manikarnika at birth (nicknamed Manu), she was born on 19 November 1828 at Kashi (Varanasi) to a Maharashtrian brahman family Moropant Tambe and Bhagirathibai Tambe. She was also known as Chulbuli because of her jolly ways & beauty. She lost her mother at the age of four. She was educated at home.
An Old Haveli : the House in Which Laxmibai, Rani of Jhansi was Born
Her father Moropant Tambe worked at the court of Peshwa at Bithur and then travelled to the court of Raja Bal Gangadhar Rao Newalkar, the Maharaja of Jhansi, when Manu was thirteen years old.
Samadhi of Raja Gangadhar Rao ( Image : Atul Gaur )
She was married to Gangadhar Rao, the Raja of Jhansi, at the age of fourteen and was given the new name 'Lakshmi Bai'. Because of her father's influence at court, Rani Lakshmi Bai had more independence than most women, who were normally restricted to the zenana: She studied self defence, horsemanship, archery, and even formed her own army out of her female friends at court.
Rani Lakshmi Bai gave birth to a son in 1851, however this child died when he was about four months old. After the death of their son, the Raja and Rani of Jhansi adopted Anand Rao. However, it is said that her husband the Raja never recovered from his son's death, and he died on 21 November 1853 of a broken heart.
Rani Lakshmibai was accustomed to riding on horseback accompanied by a small escort between the palace and the temple although sometimes she was carried by palanquin.
Image : magictravels
Her horses included Sarangi, Pavan and Badal; according to tradition she rode Badal when escaping from the fort in 1858.
The Rani Mahal, the palace of Rani Lakshmibai, has now been converted into a museum. It houses a collection of archaeological remains of the period between the 9th and 12th centuries AD.
Samadhi of Rani at Gwalior
On 17 June in Kotah-ki-Serai near the Phool Bagh of Gwalior, a squadron of the 8th (King's Royal Irish) Hussars, under Captain Heneage, fought the large Indian force commanded by Rani Lakshmibai which was trying to leave the area. The 8th Hussars charged into the Indian force, killing many Indian soldiers, taking two guns and continuing the charge right through the Phool Bagh encampment. In this engagement, according to an eyewitness account, Rani Lakshmibai put on a sowar's uniform and attacked one of the hussars; she was unhorsed and also wounded, probably by his sabre. Shortly afterwards, as she sat bleeding by the roadside, she recognized the soldier and fired at him with a pistol, whereupon he "dispatched the young lady with his carbine". According to another tradition Rani Lakshmibai, the Queen of Jhansi, dressed as a cavalry leader, was badly wounded; not wishing the British to capture her body, she told a hermit to burn it. After her death a few local people cremated her body.
Everything else is here
Thanks to copsey family for the excellent work on Jhansi Ki Rani.. the best so far by all means.
Orcha - The Vintage collection
Orcha - The Vintage collection
Orchha State was founded in 1501 AD by the Bundela chief, Rudra Pratap Singh, who became its first king. He reigned between 1501-1531, during which time he built the fort at what is now the town of Orchha, on the banks of the river Betwa. He moved his capital from Garhkundar to that town in 1531 and died in the same year.
Jahangir Mandir palace at Orchha in Madhya Pradesh,
The Jahangir Mahal was built by Bir Singh Deo. William Prinsep, an employee of the Calcutta firm Palmer & Co., came from a family who served in India for several generations. After the collapse of the company he worked as an indigo broker, was on the board of the Assam Company, and was credited with the establishment of the Indian Tea industry as well as establishing the Bengal Coal Company and inheriting the Bengal Salt Company on the death of his brother George.
Taken by Lala Deen Dayal in the 1880s, from the Curzon Collection: 'Views of places proposed to be visited by Their Excellencies Lord & Lady Curzon during Autumn Tour 1902'. Orchha was founded in 1501 by the Bundela Rajput Raja Rudra Pratap (r.1501-1531) on an island of rock beside the Betwa River, approached by a bridge. The city reached the height of its political power with its greatest architectural achievements during the reign of Raja Bir Singh Deo (r.1605-1627). Its fortunes later declined and it was eventually abandoned in 1783. The Jahangir Mandir was built in c.1605 by Bir Singh Deo and named after his imperial patron, the Mughal emperor Jahangir (r.1628-58).
Orchha is unusual among Rajput capitals because there are three separate garh palaces rather than one gradually-extended palace. This is a general view of the last to be built and most sophisticated, the Jahangir Mandir, built in c.1605 by Bir Singh Deo and named after his imperial patron. It has a square symmetrical plan and elevation around an inner courtyard and is crowned by eight large domes. The photograph is from an album containing architectural and landscape studies of various sites in Central India. The majority of the photographs were taken by Deen Dayal while on tour with Sir Lepel Griffin (1838-1908), who served as Resident at Indore and Agent to the Governor-General of Central India between 1881 and 1888. Many are reproduced in autotype in his ‘Famous Monuments of Central India’ (London, 1886). The album was formerly in the collection of Sir William Lee-Warner (1846-1912), who served in the Indian Civil Service and was a Member of the Council of India between 1902 and 1912.
Photograph of the Fort and Raj Mandir Palace at Orchha in Madhya Pradesh, taken by Lala Deen Dayal in 1882. It was built beside the Betwa River, with a fortified palace complex on an island in the river, approached by a causeway over a bridge
Orcha citadel
Royal Palace Orcha
Phool Bagh Orcha
General view from the south-west of the Raj Mandir and Jahangir Mandir Palaces, Orchha, a photo by Edmund William Smith, 1880'
William Prinsep (1794-1874), of the town of Orchha in Madhya Pradesh, beneath its massive rock, with the fort and a mosque in the foreground, dated 1818. The image is inscribed below: 'The Fort and Town of Oochar. No. 1.' The area is famous for its pinkish-grey granite outcrops of rock. Orchha, meaning 'hidden place', is situated near the Betwa river. Orchha's Fort complex contains the Raj Mahal , the Rai Praveen Mahal and the Jahangir Mahal. The Raj Mahal is a medieval granite bridge built by Rudra Pratap and completed by Madhukar Shah. The Rai Praveen Mahal was built in the mid-1670's by Raja Indramani for his concubine.
The Raj Mandir was built by Madhukar Shah during his reign, 1554 to 1591
.
This view shows one of the rocks with two soldiers on the top and in the foreground a mounted trooper of the Dromedary Corps. Orchha, meaning 'hidden place', is situated near the Betwa river and the area is famous for its pinkish-grey granite outcrops of rock.
Photograph of the Jahangir Mandir and Raj Mandir in Orchha, from the Archaeological Survey of India Collections, taken by Edmund William Smith in the 1880s.
Orchha was founded in 1501 by the Bundela Rajput Raja Rudra Pratap (r.1501-1531) on an island of rock beside the Betwa River that is approached by a bridge. The city reached the height of its political power with its greatest architectural achievements during the reign of Raja Bir Singh Deo (r.1605-1627). Its fortunes later declined and it was eventually abandoned in 1783. The Jahangir Mandir was built in c.1605 by Bir Singh Deo and named after his imperial patron, the Mughal emperor Jahangir (r.1628-58). The palace is one of the finest examples of mediaeval fortification in India from the period of the Bundela Rajputs. The building is square and is crowned by domes with rounded angle bastions capped by open pavilions. There are eight domes and a number of small chattris. The Raj Mandir was built by Madhukar Shah between 1554 and 1591. The palace is square with a central open courtyard. The centre of each side is projected outwards. The roof is flat but on the top of the outer wall there is a line of small chattris
Orcha (1818) (The actual city of Orcha had declined and been abandoned. This was just a village/small town near it's ruins)
The southern part
Bir SingDeo Chatri
Mausoleum at Orcha
General View
Orcha Courtyard Temple RamRaja ji
Orcha Fort
Sawan Bhadon Towers
The photograph is from an album containing architectural and landscape studies of various sites in Central India. The majority were taken by Deen Dayal while on tour with Sir Lepel Griffin (1838-1908), who served as Resident at Indore and Agent to the Governor-General of Central India between 1881 and 1888. Many are reproduced in autotype in his ‘Famous Monuments of Central India’ (London, 1886). This photograph is similar to plate 74, 'Oorcha Fort'. The album was formerly in the collection of Sir William Lee-Warner (1846-1912), who served in the Indian Civil Service and was a Member of the Council of India between 1902 and 1912.
The Sawan Bhadon towers, which one can see here are actually air shafts, which captured the prevailing wind and circulating cool air to the underground halls that served as pleasure retreats for the royals during summer months. There is an resourceful system of water ventilation connecting the underground palace with Chandan Katora. These cooling towers, came to Orchha from their origin in Yazd in Iran.
हिंदुस्तान का दिल.... बुंदेलखंड
हिंदुस्तान का दिल.... बुंदेलखंड
As understood by the state governments of Uttar Pradesh (UP) and Madhya Pradesh (MP),
'Bundelkhand' comprises seven districts of southern UP and six districts of northern MP MP
- Jhansi, Lalitpur, Jalaun, Hamirpur, Mahoba, Banda, Chitrakoot districts (all in UP), and
- Datia, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Sagar and Damoh districts (all in MP).
The above delineation is different from boundaries suggested by proponents of a 'greater' or
'cultural' Bundelkhand,
who include many more districts of MP.
However, the definition used by the UP and MP governments is the most useful from a practical
viewpoint.
This definition is also generally used by the media and civil society organisations when they refer
to Bundelkhand.
(The listing of UP Bundelkhand districts is derived from the scope of the 'Bundelkhand Vikas Nidhi'
set up by the
UP government In 1990-91. The listing of MP Bundelkhand districts is derived from the scope of the
The boundaries of the Bundelkhand region so defined are:
- in the north, the Yamuna and the Ganga plain
- in the east, the Vindhyan hills and Panna-Ajaigarh ranges
- in the west, the Sindh and Chambal rivers, and the Malwa and Udaipur-Gwalior regions
- in the south, the Narmada and tributaries of the Ken and Betwa
- in the south and east, the Vindyachal and Bagelkhand regions
The Bundelkhand region within these boundaries has an area of around 70,000 sq km with a
population of 15.5 million (Census 2001).
By way of rough comparison, Bundelkhand is one and one-third the size of Punjab, but with less
than two-thirds the population of that state.
Location of Bundelkhand
Bundelkhand is spread over southern Uttar Pradesh (UP) and northern Madhya Pradesh (MP), between 23°10' and 26°30' north latitude and 78°20' and 81°40' east longitude. The region covers a geographical area of around 70,000 sq km and includes seven districts of UP and six districts of MP.
Districts of Bundelkhand
Bundelkhand comprises 13 districts: Jhansi, Lalitpur, Jalaun, Hamirpur, Mahoba, Banda and Chitrakoot (all in UP), and Datia, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Sagar and Damoh (all in MP)
Sub-regions of Bundelkhand
Bundelkhand can be broadly divided into four sub-regions: Bundelkhand Plain in the north, Bundelkhand Upland in the centre and south, and Sagar and Damoh (Vindhyanchal) plateaus in the deep south. As a geographical region, the Sagar plateau is part of Malwa and Damoh plateau is part of Vindhyanchal.
Major Towns and Roads of Bundelkhand
The northern part of Bundelkhand (Bundelkhand Plain) shows higher urbanisation than the central and southern part of the region, and enjoys good connectivity to Kanpur, Allahabad, etc. The two largest towns of the region are Jhansi and Sagar.
बुंदेलखंड का दिल ...झाँसी - Gateway to Bundelkhand.
बुंदेलखंड का दिल ...झाँसी - Gateway to Bundelkhand.
Heart of Bundelkhand - Jhansi
The ancient name of this historical city was Balwantnagar. From 1817 to 1854 Jhansi was the capital of the princely state of Jhansi which was ruled by Maratha Rajas.
Pahuj Dam ( Image courtesy : Atul Gaur )
Maharaja Chhatrasal, the Bundela ruler of Panna was beset by incursions into the Bundela country by the Muslim governors of theMughal Empire. In 1729 Mohammed Khan Bangash attacked Chattrasal so later in 1732 Chhatrasal called in the aid of the Marathas to fight Mughals. The Peshwa, Baji Rao I helped Maharaja Chattrasal and they jointly defeated the Mughal army.
The town of Jhansi and surroundings were the stronghold of the Chandela rulers. Balwant Nagar was the name of this place; however in 11th century Jhansi lost its importance. In 17th century under Raja Bir Singh Deo I (r. 1605–1627) of Orchha rose to prominence again. Raja Bir Singh Deo had good relations with the Mughal emperor Jehangir. In five year construction period (1613–1618) Raja Bir Singh Deo got constructed the Jhansi fort and around it got established a Balwant Nagar, which later on came to be known as Jhansi.
According to a legend the Raja of Orchha was sitting on the roof of his palace with his friend, the Raja of Jaitpur, and asked the latter whether he could discern this new fort that he had built on Bangara hill, and he replied that he could see it 'jhainsi' (meaning rather indistinct). This name 'Jhainsi' in course of time became corrupted to 'Jhansi'. It was one of the most strategically situated forts of central India being built on an elevated rock rising out of the plain and commanding the city and the surrounding country.
Peshwa Baji Rao I was rewarded by the bequest of one-third of the Maharaja's dominions upon his death two years later and Jhansi was included in this part, thus Jhansi became a Maratha territory.[2]
The Maratha general developed the city of Jhansi, and peopled it with inhabitants from Orchha state. In 1742 Naroshanker was made thesubedar of Jhansi.[3] During his tenure of 15 years he not only extended the Jhansi fort which was of strategic importance but also constructed some other buildings. The extended part of the fort is called Shankergarh. In 1757 Naroshanker was called back by the Peshwa; his successor was Madhav Govind Kakirde who was himself succeeded by Babulal Kanahai, who governed the area from 1757-66. Next in the line of subedars was Vishwas Rao Laxman (1766-1769) who was followed by Raghunath Rao II Newalkar. He was a very able administrator and succeeded in increasing the revenue of the state. The Maha Lakshmi Temple and the Raghunath Temple were built by him.
About A.D. 8oo the Parihar dynasty, are said to have been ousted by the Chandels, and Dangha Varma, a chief of the Chandel Rajputs, appears to have established the earliest paramount power in Bundelkhand, trying to unite most of the local chieftains, towards the close of the 10th century A.D. Under his dynasty the area attained its greatest splendour in the early part of the 11th century, when its raja, whose dominions extended from the River Jumna to the Narbadda river, marched at the head of 36,000 horse and 45,000 foot, with 640 elephants, to oppose the invasion of Mahmud of Ghazni.
Although the early Bundelas appeared in 13th century AD, we don't know much about them till the middle of the 16th century when a Bundela chief called Rudra Pratap established base on the banks of the Betwa in Orchha (literally 'hidden place'), near Jhansi, at a time when the Mughals were yet to establish their supremacy over North India.
Rudra Pratap and his immediate descendants built many magnificent structures including the Jhansi fort; the enormous Orchha fort that encloses most of the village even today; and a soaring Ram Raja temple, the only place in India where Ram is worshipped as a king even today with martial honours.
The Bundela rulers of Orchha continued the Chandela tradition of building tanks.
Mughal rule in India was firmly established in the reign of Akbar. At this time, Orchha was ruled Rudra Pratap's grandson, Madhukar Sah, who increased the kingdom's territories and challenged the emperor's authority
When Akbar's son, Salim (later known as Jehangir) rebelled, a son of Madhukar Sah, Bir Singh, sided with Salim and arranged to kill Abul Fazl, a high ranking advisor of Akbar.
 |
| HH Saramad-i-Rajha-i-Bundelkhand Maharaja Mahendra Sawai Shri Sir VIR SINGH Ju Deo Bahadur |
When Salim alias Jahangir ascended the Delhi throne, he rewarded Bir Singh by granting him Orchha and a high rank in the Mughal court.
In his later years, Bir Singh quarelled with his Mughal patron and there were feuds within the family itself, leading eventually to the creation of another Bundela state, Datia. Another state, Chanderi, had been formed even earlier.
These states were eventually recognised by Mughal rulers, in return for armed support supplied by Bundela in wars fought by the Mughal rulers in other parts of India, notably the Deccan.
While the Bundela states occupied parts of Chhatarpur, Lalitpur, Jhansi and Datia districts, much of the rest of Bundelkhand was under Mughal rule, under the subahs or provinces of Agra, Malwa and Allahabad.
Akbar's favourite minister, Birbal, held Kalinjar as his jagir. Islamic religious and cultural centres came up at Kalpi (Hamirpur), Banda and Mahoba.
 |
| Maharaj Chhatrasal, |
In the late 17th century, when Mughal power began to wane, arose one of Bundelkhand's great historical figures: Maharaj Chhatrasal, founder of an independent kingdom and a second line of Bundela rulers.In his early life Chhatrasal did military service for the Mughals in the Deccan and during this time he is believed to have met Chattrapati Shivaji, who inspired him to found an independent kingdom.
Another influence on his life is believed to be a charismatic religious leader called Prannath, who founded the Pranami sect, which rejects caste barriers and reveres both Hindu and Muslim religious texts.The weak Moghul emperors who followed Aurangazeb recognised Chhattrasal's rule.
However, as he expanded his territory into the district of Jhansi, the Mughal governor of Allahabad, Muhammed Khan Bangash, counterattacked with great force, compelling Chhatrasal to seek help from the other great power of the time, the Marathas, led by Peshwa Baji Rao in Pune.
Maratha armies helped the Bundelas deliver a humbling defeat to Bangash in 1729 and before he died two years later, Chhatrasal conferred a third of his kingdom to the Peshwa.
Orcha ... The Kingdom
- Raja Pancham Singh 1048/1071
- Raja Virbhadra Singh 1071/1087, married and had issue.
- Raja Karanpal Singh (qv)
- Kunwar Randhir Singh
- Kunwar Hirashah
- Kunwar Hansraj
- Kunwar Kalyanshah
- Raja Karanpal Singh 1087/1112, married and had issue.
- Raja Kinnar Shah (qv)
- Raja Shaukan Dev (qv)
- Raja Nanak Dev (qv)
- Kunwar Vir Singh, married and had issue.
- Raja Mohanpal Singh (qv)
- Raja Abhaybhupati Singh (qv)
- Raja Kinnar Shah 1112/1130
- Raja Shaukan Dev 1130/1152
- Raja Nanak Dev 1152/1159
- Raja Mohanpal Singh 1159/1197
- Raja Abhaybhupati Singh 1197/1215
- Raja Arjunpal Singh 1215/1231, married and had issue.
- Raja Virpal (qv)
- Raja Sohanpal (qv)
- Kunwar Dayapal
- Raja Virpal 1231/1251
- Raja Sohanpal 1251/1259, married and had issue.
- Raja Sahjendra Singh (qv)
- Kunwar Ram Singh
- Kunwar Indrajit Singh, ancestor of the later Rajas of Bihat.
- Raja Sahjendra Singh 1259/1283
- Raja Nanak Dev II 1283/1307, married and had issue.
- Raja Prithviraj Singh (qv)
- Kunwar Indraraj
- Raja Prithviraj Singh 1307/1339
- Raja Ram Singh 1339/1375, married and had issue.
- Raja Ramchandra Singh (qv)
- Raja Mednepal Singh (qv)
- Raja Ramchandra Singh 1375/1384
- Raja Mednepal Singh 1384/1437
- Raja Arjun Dev 1437/1468
- Raja Malkhan Singh 1468/1501, married and had issue.
- Kunwar Kharag Singh
- Kunwar Jagjit Singh
- Rauja RUDRA PRATAP (qv)
- Kunwar Jait Singh
- Kunwar Shah Diwan
- Kunwar Devi Singh
- Raja RUDRA PRATAP 1501/1531, he managed to increase his lands considerably during the confusion caused by Padshah Baber's invasion; married and had issue. He died 1531.
- Kunwar Kirat Shah
- Kunwar Bhupat Shah
- Raja BHARTI CHAND (qv)
- Raja MADHUKAR SHAH (qv)
- Kunwar Anand Das
- Kunwar Chandan Das
- Kunwar Durga Das
- Kunwar Ghanshyam Das
- Kunwar Prayag Das
- Kunwar Bhairon Das
- Kunwar Khande Rai
- Kunwar Udyajit Singh of Mahewa, married and had issue.
- Kunwar Ragho Das
- Kunwar Kosi Das
- Kunwar Ganga Das
- Kunwar Hridaya Narayan
- Kunwar Bharti Chandra
- Kunwar Prem Chandra, married and had issue.
- Kunwar Bhagwan Das, married and had issue.
- Kunwar Bhagwan Das, married and had issue.
- Kunwar Chandju
- Kunwar Kharag Rai
- Kunwar Champat Rai, married and had issue. He died after 1649.
- Kunwar Gopal Rai
- Kunwar Sarvahan
- Kunwar Anand Rai
- Maharajadhiraja Chhatrasal, born 1649, married and had issue. He died 1731.
- Kunwar Rajaraj
- Kunwar Jagatraj [Raja JAGATRAJ SINGH of Jaitpur]
- Kunwar Hirde Shah [Raja HIRDE SHAH of Panna]
- Kunwar Unoop Singh
- Kunwar Bharti Chand [Dewan BHARTI CHAND of Jaso]
- Kunwar Padam Rao [Rao PADAM RAO of Jigni]
- Kunwar Govind Das
- Kunwar Umrood Singh
- Kunwar Sher Singh
- Kunwar Man Singh
- Kunwar Mohan Singh
- Kunwar Dalpat Singh
- Kunwar Ratan Shah
- Kunwar Sujan Rai
- Kunwar Kunwar Sen
- Kunwar Man Shah, ancestor of the Garrauli Royal Family.
- Raja BHARTI CHAND 1531/1554, he unsuccessfully tried to oppose Sher Shah on his march to Kalinjar in 1545. He died 1554
- Raja MADHUKAR SHAH 1554/1592, a religious recluse who allowed the fortunes of the state to decline from this time; the Mughal forces invaded Orchha for the first time in 1577 when Sadik Khan managed to take Orchha after a severe fight; in 1591 the Raja seized some parganas near Gwalior and was attacked and defeated by the Imperial troops forcing him to flee to the jungles, where he died soon afterwards of a natural death; married and had issue. He died 1592.
- Kunwar Horal Deo, died 1577.
- Raja RAM SHAH (qv)
- Raja BIR SINGH DEO [Virsingh Dev] (qv)
- Kunwar Indrajit Singh
- Kunwar Pratap Singh
- Kunwar Har Singh Deo, ancestor of the Bhasnai branch, to which belonged HH Maharaja Lokendra Sir BHAWANI SINGH Bahadur ofDatia.
- Raja RAM SHAH, Raja of Orchha 1592/1605 (deposed), and Raja of Chanderi 1608/1612, sued for pardon and was allowed to succeed, but he was a weak ruler and was unable to keep his brothers in check; Padshah Akbar deposed the Raja and placed his brother on the gadi; he was imprisoned in Delhi for a short time, but was eventually released and granted the fiefs of Chanderi and Banpur in 1608; married and had issue.
- Kunwar (name unknown) Singh, married and had issue.
- Raja Bharat Shah of Chanderi 1612/1646, married and had issue.
- Raja Devi Singh of Chanderi 1646/1717, married and had issue.
- Raja Duraj Singh of Chanderi 1717/1733, married and had issue.
- Raja Durjan Singh of Chanderi 1733/-, married and had issue.
- Raja Man Singh of Chanderi -/1760, married and had issue.
- Raja Anirudh Singh of Chanderi 1760/1774, married and had issue.
- Raja Ram Chand of Chanderi 1778/1802, married and had issue.
- Raja Parjapal of Chanderi 1802
- Raja Mur Pahlad of Chanderi 1802/1842, married and had issue.
- Raja Mardan Singh of Chanderi 1842/1858, the state lapsed with his death and was annexed by the ruler of Gwalior.
- Raja Hati Singh of Chanderi 1774/1778
- Raja BIR SINGH DEO 1605/1627, a ruler of strong principles and no scruples, he amassed great wealth and property; he was not only a great warrior but an enthusiastic builder, leaving many monuments, forts and temples; married and had issue. He died 1627.
- Kunwar Chandrabhan
- Kunwar Narhari Das
- Raja JHUJHAR SINGH (qv)
- Kunwar Tulsi Das
- Kunwar Beni Das
- Raja BHAGWAN RAO of Datia.
- Kunwar Kishan Singh
- Kunwar Hardaul of Baragaon, married and had issue.
- Kunwar Bejani Shah of Baragaon, married and had issue.
- Kunwar Pratap Singh of Baragaon, married and had issue.
- Kunwar Diwanrai Singh of Baragaon, married and had issue.
- Kunwar Umaid Singh, ancestor of the Banka Pahari Royal Family.
- Kunwar Hindu Singh, ancestor of the Tori Fatehpur Royal Family.
- Kunwar Samant Singh, received Bijna around 1690 and was the ancestor of the Bijna Royal Family.
- Kunwar Mokham Singh, ancestor of the Chirgaon Royal Family.
- Kunwar Aman Singh, ancestor of the Durwai Royal Family.
- Raja JHUJHAR SINGH 1627/1635, a weak and turbulent ruler, he soon plunged his state into difficulties; after serving the Mughal Emperor in the Deccan, he returned home and suspected his brother of adultery with his wife, he forced his brother to drink poison whose name became exalted into a local deity; he went into open rebellion against the Mughal forces in 1634-1635, but was pursued and driven into the jungles where he was killed; married and had issue. He died 1635.
- Raja PAHAR SINGH (qv)
- Raja DEVI SINGH 1635/1641
- Raja PAHAR SINGH 1641/1653, of Kaniyadana, married and had issue.
- Raja SUJAN SINGH I (qv)
- Raja INDRAMANI SINGH (qv)
- Raja SUJAN SINGH I 1653/1672
- Raja INDRAMANI SINGH 1672/1675, married and had issue.
- Raja JASHWANT SINGH (qv)
- Raja JASHWANT SINGH 1675/1684, married and had issue.
- Raja BHAGWAT SINGH (qv)
- Raja BHAGWAT SINGH 1684/1689, married and had issue.
- Raja UDWAT SINGH (qv)
- Raja UDWAT SINGH 1689/1735, married and had issue.
- Raja PRITHVI SINGH (qv)
- Raja AMAR SINGH of Khaniadhana.
- Raja PRITHVI SINGH 1735/1752, during his rule, more of his territories were lost to the Marathas.
- Raja Mahendra SANWANT SINGH 1752/1765, he was granted the title of Mahendra by Padshah Alamgir.
- Raja Mahendra HATI SINGH 1765/1768
- Raja Mahendra MAN SINGH 1768/1775
- Raja Mahendra BHARTI CHAND 1775/1776, adopted from Bijna State.
- Raja Mahendra VIKRAMAJIT 1776/1817 (abdicated) and in 1834, adopted from Bijna State, he entered into relations with the British authorities in 1812, abdicated in favour of his son, but resumed power on his death. He died 1834.
- Raja Mahendra DHARAM PAL 1817/1834, died 1834.
- Raja Mahendra TEJ SINGH 1834/1842, adopted from Bijna State, died 1842.
- Raja Mahendra SUJAN SINGH II 1842/1848, adopted from Bijna State, died 1854
- HH MaharajaMahendra HAMIR SINGH 1848/1874, Maharaja [cr.1865], he received a sanad of adoption in 1862. He died 15th March 1874.
Maharaja Pratap Singh of Orchha
- HH Saramad-i-Rajha-i-Bundelkhand Maharaja Mahendra Sawai Shri Sir PRATAP SINGH Bahadur Ju Deo 1874/1930, born 1854, K.C.S.I. [cr.1900], G.C.S.I. [cr.1906], K.C.B.(mil)[cr.1901], G.C.I.E. [cr.1900], K.C.I.E [cr.1894], Hon. ADC to HM, Saramad-i-Rajha-i-Bundelkhand [cr.1882], granted a personal salute of 17 guns; married and had issue. He died 3rd March 1930.
- Raja Bahadur Bhagwant Singh, Yuvaraj Saheb of Orchha; married, as his third wife, the third daughter of Rana PADAM CHAND of Jubbal, and had issue, four sons. He died vp.
- HH Saramad-i-Rajha-i-Bundelkhand Maharaja Mahendra Sawai Shri Sir VIR SINGH Ju Deo Bahadur (qv)
- Rao Raja Karan Singh Ju Deo, married and had issue.
- Rajkumari Jayanti Devi [Rani Jayanti Devi of Koti], married Rana DEVESH CHAND of Koti in Himachal Pradesh, and had issue. She died 10th March 2010.
- Rao Raja Narendra Singh Ju Dev, married and has issue, one daughter and two sons.
- Rajkumari Gita Rathod
- Rajkumar Dhruv Singh Dev
- Rajkumar Rudra Singh Dev, born 1957, married 14th December 1987, Rajkumari Manjari Kumari, daughter of Raja VISHWARAJ PRATAP SINGH of Kawardha, and his wife, Rani Shashi Prabha Devi (now the Rajmata Sahiba of Kawardha).
- Rao Raja Gayanendra Singh Ju Dev, married and has issue, three daughters and one son.
- Rajkumari Gauri Parikh
- Rajkumari Hema Chand
- Rajkumari Maya Rana
- Rajkumar Vishwajeet Singh Dev
- Rao Raja Jayanendra Singh Ju Deo, married and had issue.
- Rao Raja Praduman Singh Ju Dev, married and has issue, three sons.
- Rajkumar Brijraj Singh Dev
- Rajkumar Mrigendra Singh Dev
- Rajkumar Shivraj Singh Dev
- Rajkumari Usha Kumari
- Rao Raja Mahendra Singh Ju Deo, married and had issue, three daughters and one son.
- Rajkumari Ila Raghuvanshi
- Rao Raja Dinesh Singh Ju Dev, married and has issue, one daughter and two sons.
- Rajkumari Abha Singh
- Lt.-Col. Rajkumar Abhay Singh Dev
- Rajkumar Ajay Singh Dev
- Rajkumari Gayatri Kumari
- Rajkumari Kumud Singh
- Kunwar Sawant Singh, second son, adopted into Bijawar in 1898, as HH Bharat Dharmendra Maharaja Sawai Sir SAWANT SINGH Bahadur of Bijawar.
- Maharajkumari (name unknown) [HH Maharani Sahiba of Chhatarpur], married 1884 (as his first wife), HH Maharaja Sir VISHWANATH SINGH Bahadur of Chhatarpur. She died sp 1920.
Bundelkhand Maharaja Mahendra Sawai Shri Sir VIR SINGH Ju Deo Bahadur
- HH Saramad-i-Rajha-i-Bundelkhand Maharaja Mahendra Sawai Shri Sir VIR SINGH Ju Deo Bahadur 1930/1956, born 14th April 1899, K.C.S.I., married and had issue. He died 1956.
- HH Saramad-i-Rajha-i-Bundelkhand Maharaja Mahendra Sawai Shri DEVENDRA SINGH Ju Deo Bahadur (qv)
- Maharajkumari Sudha Kumari, born 22nd November 1930, married into Dhami, and had issue. She died 25th February 1978.
- HH Saramad-i-Rajha-i-Bundelkhand Maharaja Mahendra Sawai Shri DEVENDRA SINGH Ju Deo Bahadur 1956/-
- HH Saramad-i-Rajha-i-Bundelkhand Maharaja Mahendra Sawai Shri MADHUKAR SHAH Ju Deo Bahadur (see above)
OTHER MEMBERS:
- Rani Mahendra Kumari, married (as his first wife), Raja SURENDRA BIKRAM SINGH of Itaunja.
Ref : http://dsal.uchicago.edu/reference/gazetteer/pager.html?objectid=DS405.1.I34_V19_253.gif
VEER CHHATRASAL , THE WARRIOR FROM BUNDELKHAND
( Portrait of Mastani )
( Chhatrasal on his horse )
( Statue of Chhatrasal )
( Chhatrasal on horse )
( Chhatrasal meeting Shivaji )
VEER CHHATRASAL , THE WARRIOR FROM BUNDELKHAND WHO FOUGHT THE MUGHALS ALL ALONG HIS LIFE
"Bundele harbolon ke munh hum ne suni kahaani thi
Khoob Ladi mardaani woh tau jhansi vaali Rani thi."
These are lines from the most popular poem written by Subhadra Kumari Chauhan on Rani Lakshmibai of Jhansi , the warrior queen from Bundelkhand . Bundelkhand is known for its colourful culture, rich history, beautiful landscapes and breathtaking architecture. This area is enriched by various Bundela and Chandela period attractions like the temples of Khajuraho, the fort and temples of Orchha, Panna National Park , etc.
It is pertinent to mention that before Bundela Rajputs, Chandelas ruled much of the Bundelkhand region of Central India for approximately 500 years between the 9th and the 13th centuries AD. The capital city of Chandelas was Khajuraho which was later changed to Mahoba. Kalinjar was their important fort.The Chandellas built the most famous Kandariya Mahadeva Temple in 1050 AD. and a number of beautiful temples at Khajuraho.The Chandel dynasty is famous in Indian history for Maharaja Rao Vidyadhara, who repulsed the attacks of Mahmud of Ghazni.Paramardi the last independent Chandella ruler was defeated by Qutb-ud-din Aibak in 1203 A.D.
The Bundela dynasty emerged from the 11th century Kshatriya Rajput King Pancham, who laid the foundation of the Bundela Kingdom. Being ruled by the Bundela kings, this land came to be known as ‘Bundelkhand’ , a vast area surrounded by rivers like Yamuna, Betwa, Chambal, Tons, Ken, Kilkila, Dhasan, Sone Kunwari, Pahuj, and Narmada.Before the advent of British colonial rule in India, the region of Bundelkhand also included several princely states . Veer Chhatrasal belonged to Bundela clan of Kshatriya Rajputs .
Veer Chhatrasal was born at Kachar Kachnai in Tikamgarh in a Rajput family on 4 May 1649, to Champat Rai and Sarandha. He was a descendant of Rudra Pratap Singh of Orchha.Rudra Pratap Singh Bundela ( r 1501-1531 ) was the founder and first Raja of the kingdom that became the princely state of Orchha, India, during the Lodhi dynasty . He built the fort at what is now the town of Orchha on the banks of the river Betwa .
Veer Chhatrasal's father was a Bundela chieftain who rebelled against Aurangzeb, who had him executed in 1661CE.Young Veer Chhatrasal requested the legendary guerrilla warrior Shivaji to employ him, but was advised to return to his homeland and fight for its independence from Mughals. Chhatrasal listened to Chhatrapati Shivaji’s advice and returned to Bundelkhand. There, he set up a camp in the jungles of Panna and raised a small army with which he launched an attack on Mughal forts in the region. His bravery made him famous — at the age of 22, once he defeated an entire troop of Mughal soldiers with a team of just five horsemen and 25 infantry soldiers. Soon his kingdom extended from Panna in the east and Gwalior on the west.In the years that followed, Chhatrasal never stopped fighting against the presence of Mughals in Bundelkhand.In 1700, Aurangzeb made a series of attempts to subdue Veer Chhatrasal known as Maharaja Chhatrasal by that time but was defeated every time.
In fact, in 1730, the Mughals sent their famous Pathan warrior Muhammad Khan Bangash to Bundelkhand. Though Chhatrasal was aged now, he won a final victory over the Mughals with help from Peshwa Baji Rao I.As a sign of appreciation and respect for the Peshwa, Chhatrasal gave his beautiful daughter Mastani as bride to Baji Rao I.
Maharaja Chhatrasal is the only king in the history of the world who, even after sitting in power, wrote poetry to boost public awareness and morale of the Hindu kings to uproot the invaders .In Bundelkhand, he is well-known as the ”master of sword and pen" (Kalam aur Talwaar ke Dhani) . Maharaja Chhatrasal is considered synonymous with Bundelkhand as the leader of the culture and prosperity of the region. Many villages, towns, cities, and places are still glorifying the great character of Maharaja Chhatrasal within and even outside the Bundelkhand. Today, his bravery is remembered in the names of several roads, colleges and even a prominent stadium known for wrestling, Chhatrasal Stadium in North Delhi.The Bundeli people still remember him in folk songs:-
" Maharaja adhipati bhaye, maharaja chhatrasal ..
Rajan mein raja bhaye, asuran kere kaal."
The great Temple of Keshava Rai ( also known as Sri Krishna Janam Bhoomi Temple ) at Mathura was rebuilt by Bir Singh Deo Bundela during Jahangir’s time at a cost of thirty-three lakhs of rupees after being repeatedly plundered and destroyed by invaders . It was one of the most magnificent temples ever built in India and enjoyed veneration of the Hindus throughout the land. Prince Dara Shikoh, who was looked upon by the masses as the future Emperor, had presented a carved stone railing to the temple which was installed in front of the deity at some distance; the devotees stood outside this railing to have ‘darshan’ of Keshava Rai. The railing was removed on Auranzeb’s orders in October 1666.The temple of Keshava Rai was demolished in the month of Ramzan, 1080 A.H. (13th January – 11th February 1670) by Aurangzeb’s order.He built a mosque over the existing temple's plinth .
Mastani and Maharaja Chhatrasal Bundela were followers of the Pranami Sampradaya , a Hindu sect based on the Bhakti /worship of Sri Krishna. Her mother was a Shia Muslim from Iran , a follower of Islam. Mastani died in 1740, shortly after Bajirao's death. Her cause of death is unknown. According to some, she died of a shock after knowing about her husband's death. But, many believe that she committed suicide after she heard of Bajirao's death . Mastani was buried in the village of Pabal. Her grave is called both Mastani's Samadhi and Mastani's Mazaar.
Despite being a lifetime freedom warrior, Chhatrasal was a greatly respected leader, a protector of art, culture, and religion, and an inspirational poet. Chhatrasal is the only known Hindu Maharaja who demonstrated love for the entire humanity through his actions. He proved himself to be a unique humanitarian Hindu Maharaja of medieval India.A patron of art and literature, his court had several noted poets like Kavi Bhushan, Lal Kavi, Bakhshi Hansaraj, etc.
Dr Shashi Shekhar Toshakhani informs this:-
" It is said that when Shivaji’s famous court poet Bhushan went to Orchha, capital of Chhatrasal’s kingdom, Chhatrasal himself came out to receive him and offered to carry his litter (पालकी) on his own shoulders. Feeling that this was the height of courtesy, Bhushan jumped out of the litter and uttered : “Shivaa ko saraahaun ki saraahaun Chhatrasal ko!” (शिवा को सराहौं कि सराहौं छत्रसाल को”)— Shall I admire Shivaji or shall I admire Chhatrasal ?"
Prominent people from Bundelkhand include Acharya Rajneesh, Maharishi Mahesh Yogi, Tantiya Tope, Vrindavan Lal Verma,Dhyan hand ( hockey wizard) ,Indeevar ( film lyricist), Maithili Sharan Gupt( national poet) ,Phoolan Devi ( bandit queen) , Uma Bharati( politician), Subodh Khandekar( Olympic hockey player),Pankaj Mishra ( novelist ) ,Harishankar Parsai( writer) ,Joy Mukherjee ( actor) ,Shashadhar Mukherjee( film producer ),Raja Bundela( actor politician) ,Dr Hari Singh Gaur( member constitution drafting committee) and many more.
Alas! Chhatrasal finds little space in our history books.
( Avtar Mota )
Exploring the many splendors of Bundelkhand
This post is an introduction to the Bundelkhand region. I hope that it will contribute to raising awareness about this region and discover some of its hidden treasures.
Geography of Bundelkhand
The northern part of this region lies in the state of Uttar Pradesh (purple in the map below) while its southern part lies in the state of Madhya Pradesh (green in the map).
It is a Hindi speaking area. The Bundeli language is the most common of the Hindi dialects spoken in the area. It in turn consists of several sub-dialects.
A Brief History of Bundelkhand
Oral histories and legends of the region describe it as the ancient reign of king Luv, the son of Lord Rama. In the Pre-Buddhist period, this area came under the kingdom of Ujjain.
In the Buddhist period (around 500 BCE), this area was known as Chedi Janapada (literally "Ruled by the people") as shown in Thomas Lessman map of 500 BCE.
Chandelas arrived here in the 9th century as the feudal lords of the Pratihara, however soon they became independent. They ruled Bundelkhand for around 300 years. Initially they ruled from Khajuraho and then shifted to Mahoba. They built the famous Khajuraho temples in the 10th century, and the fort and a few artificial lakes in Mahoba in the 11th-12th centuries. In late 12th century, as their power weakened, a part of Bundelkhand came under the Khangar dynasty, who took over the Jingarh fortress of the Chandelas and renamed it Garh Kundhar.
In early 13th century the Chandelas were defeated by the sultan of Delhi, Qutubuddin Aibek, who was of Turkish origins. After almost two centuries, in the 16th century, for a short period the Chandela dynasty rose again, but it could not last and during the reign of Akbar, the region passed under the Mughal empire.
As part of the empire, Bundelkhand was ruled by Rajput kings, who recognized the Mughal sovereignty. (Below, Thomas Lessman map from 1500 CE showing the Rajput states). These kings are known as Bundela kings and this was the period, when the region got its name Bundelkhand. Bundela kingdoms started in Orchha, moved to Chattarpur and then to Jhansi.
Temples, Shrines and Dargahs of Bundelkhand
The region is predominantly Hindu. Earlier temples attest to the strong presence of Shaivism in the region with a number of Shiva temples. The image below shows an old Shiva temple in the lower parts of the Jhansi fort.
Bundelkhand region is full of ruins of magnificent fortresses and temples, many of which are known only to local persons and to academics.
For example, according to Dr Ramsajivan who wrote a PhD thesis on this theme in 2006, there are 41 important fortresses in Bundelkhand - Kalinjar, Ajaygarh, Rasin, Madfa, Sherpur Sevda, Rangarh, Tarhua, Bhuragarh, Mahoba, Sirsagarh, Jaitpur, Mangalgarh, Maniyagarh, Baruasagar, Orchha, Jhansi, Garh Kundhar, Chirgaon, Airch, Urai, Kalpi, Datiya, Badhoni, Gwalior, Chanderi, Chhattarpur, Panna, Singhorgarh, Rajnagar, Batiyagarh, Bajawaor (Jatashanker), Beergarh, Dhamoni, Patharigarh (Patharkachhar), Barigarh, Gaurhar, Kulpahar, Talbehat and Devgarh.
Building of the forts followed guidelines given in India's ancient architecture texts of Vaastu Shastra. These forts had thick high walls and were surrounded by moats or natural barriers such as rivers. The image below shows a branch of Betwa river that separates the Orchha fort from the town.
Bundelkhand is not an easy region to visit. Being at the border of two states, many towns of the region are not well connected. It is a drought prone area and one of the poorest parts of India. Except for Gwalior, Jhansi, Orchha and Khajuraho, most of its rich history and monuments are ignored and neglected.
I hope that this post will stimulate some of you to visit and document some of its lesser known places and monuments.
http://kyabaat.blogspot.com/2017/09/exploring-many-splendors-of-bundelkhand.html
















































































































































































































































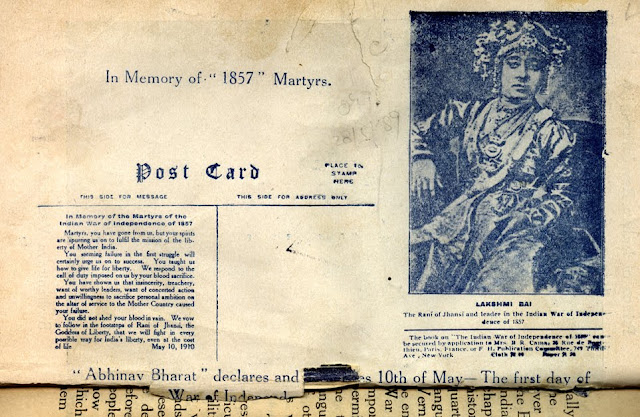










































































































































































































.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)