कंडोलिया मंदिर, उत्तराखंड
मंदिर के बारे में दो कथाएँ सुनने को मिलीं. पहली यह कि कुमाऊँ क्षेत्र से कोई दुल्हन पौड़ी आई तो अपने साथ अपने इष्ट देवता को कंडी ( छोटी टोकरी ) में रख कर ले आई. जिसे बाद में ऊँचे स्थान पर स्थापित किया गया. स्थान और मंदिर का नाम कंडोलिया मंदिर पड़ गया. दूसरी कथा ये है कि डूंगरियाल नेगी समाज ने अपने इष्ट गोरिल देवता को पौड़ी में बसने का अनुरोध किया था. पहले स्थापना नीचे चौक में की गई परन्तु देवता ने स्वयं को शिखर पर स्थापित करने को कहा. उन्हें कंडी में ले जा कर पहाड़ी के ऊपर स्थापित किया गया इसलिए स्थान और मंदिर कंडोलिया कहलाए. हर जून में यहाँ तीन दिन का भंडारा और मेला लगता है.
पौड़ी बस अड्डे से मंदिर के लिए आसानी से सवारी मिल जाती है. समुद्र तल से पौड़ी की ऊँचाई 1815 मीटर है. नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोटद्वार है जो 108 किमी दूर है और एअरपोर्ट देहरादून में है जो 155 किमी दूर है. मंदिर के पास सुंदर पार्क, बच्चों के झूले और कार पार्किंग है. लगभग दो किमी आगे क्यूंकालेश्वर मंदिर और रांसी स्टेडियम भी देखा जा सकता है. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
 |
| कंडोलिया देवता का निवास |
 |
| प्रवेश द्वार |
 |
| मंदिर की सीढ़ियाँ |
 |
| ठा. गुलाब सिंह गौरी सिंह नेगी मु. पौड़ी अपनी तरफ से कन्डोलिया देवता का मकान व आँगन बनाया है 15-07-1989 |
 |
| मनौतियाँ पूरा होने की प्रतीक घंटियां |
 |
| धनुष बाण |
 |
| मंदिर के बारे में प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया नोटिस बोर्ड |
 |
| घंटी बजाओ सब कुछ पाओ |
 |
| आसपास का सुंदर दृश्य |
 |
| ठंडा और शांत जंगल |
 |
| बच्चों के लिए पार्क |
क्यूंकालेश्वर मंदिर, उत्तराखंड
ऋषिकेश से मंदिर की दूरी लगभग 115 किमी है. मंदिर गर्मियों में 5.30 बजे खुलता है और सर्दी में 6 बजे और शाम 6 बजे तक खुला रहता है. पार्किंग है. खाने पीने का इन्तेजाम कर के चलें.
मंदिर में लगे एक बोर्ड के अनुसार इसका निर्माण और शिव स्थापना गंगा दशहरे के दिन जून 1833 में श्री मुनि मित्र शर्मा द्वारा हुई. बोर्ड के लेख के अनुसार मंदिर 'इन्द्रकील पर्वत के दक्षिण में और बहिनकील पर्वत के पश्चिम में' है. पौड़ी बस अड्डे से अगर मंदिर की ओर जाएं तो पहले कंडोलिया देवता मंदिर है, उससे और ऊपर एक किमी चलें तो आप क्यूंकालेश्वर मंदिर पहुँच सकते हैं. रास्ता घने और सुंदर जंगल में से है पर सड़क अच्छी है इसलिए हमने तो अपनी गाड़ी दौड़ा दी.
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो :
 |
| घने जंगल के बीच क्यूंकालेश्वर मंदिर. ये फोटो पहले Instagram में भी डाली थी |
 |
| मंदिर का एक और दृश्य |
 |
| मंदिर में शिव- पार्वती, गणेश और राम-सीता की भी मूर्तियाँ हैं |
 |
| पूजा स्थल |
 |
| कुंड |
 |
| घने जंगल से गुज़रती सड़क |
 |
| मंदिर की ओर जाती सीढ़ियों पर श्रीमति स्नेहा बगवाड़ी भट्ट - हमारी Friend, Philospher and Guide |
 |
| आशीर्वाद के साथ स्वागतम |
 |
| मुख्य द्वार के पास दीवार पर बना सुंदर चित्र |
 |
| मुख्य द्वार |
 |
| मुख्य द्वार के दोनों स्तंभों पर चार चार मूर्तियों की नक्काशी की हुई है पर सभी आठों मूर्तियों के सर पर अंग्रेजी स्टाइल के मुकुट हैं |
 |
| शांत और हरे भरे जंगल में मन रमता है. पर अफ़सोस गाड़ी दिल्ली के शोर शराबे और ट्रैफिक में वापिस ले जाएगी |
 |
| यज्ञ शाला |
 |
| महंत जी का निवास |
गुप्तकाशी
दिल्ली > ऋषिकेश > देवप्रयाग > श्रीनगर > रुद्रप्रयाग > अगस्त्यमुनि > गुप्तकाशी.
गुप्तकाशी की ऊँचाई 1320 मीटर है और ये शहर केदार खण्ड में है और केदारनाथ से 50-55 किमी पहले है. यहाँ से केदारनाथ पैदल जाना बहुत मुश्किल काम है. पर पास ही हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है जिसमें 12-15 मिनट में केदारनाथ पहुंचा जा सकता है.
गुप्तकाशी की लोक कथा है कि पांडव महाभारत के युद्ध के बाद पश्चाताप करने और भगवान शिव का दर्शन करने यहाँ आए. परन्तु भगवान शिव मिलना नहीं चाहते थे इसलिए नंदी के रूप में यहाँ गुप्त हो गए. इसलिए स्थान का नाम गुप्तकाशी पड़ गया. नकुल और सहदेव ने नंदी को पहचान कर भीम की सहायता से नंदी को पकड़ने की कोशिश की पर वो एक बर्फीली गुफा में गायब हो गए. बाद में भगवान् शिव पांच अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुए - कूबड़ केदारनाथ में, रौद्र मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, पेट इत्यादि मध्यमहेश्वर में, और लटाएं कल्पेश्वर में. रुद्रनाथ और कल्पेश्वर चमोली गढ़वाल जिले में है. इन सभी स्थानों पर मंदिर हैं और ये सभी स्थान भी सुंदर हैं. गुप्तकाशी से केदारनाथ, उखीमठ, चोपटा और देवरिया ताल भी घूमने जा सकते हैं.
गुप्तकाशी और आसपास के कुछ फोटो:
 |
| 1. गुप्तकाशी की सुबह. जिस दिन आसमान साफ़ हो तो बर्फीली चोटियों का सुंदर दृश्य नज़र आता है |
 |
| 2. लगता है इनके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है. मन्दिर से धार्मिक पुस्तकें और सामग्री सादर घर ले जाई जा रही हैं |
 |
| 4. मानसून के समय इस तरह के दृश्य अक्सर देखने को मिलते हैं. नीचे घाटी गरम है इसलिए भाप ऊपर उठती है. ऊपर ठंडक पा कर बादल बनते हैं. पल पल बादलों की शक्ल सूरत बदलती रहती हैं |
 |
| 5. गुप्तकाशी का नवोदय विद्यालय. दोबारा अगर स्कूल में पढ़ने जाना हो तो ये जगह बेहतरीन है |
 |
| 6. गुप्तकाशी की मुख्य रोड जो केदारनाथ की तरफ जाती है |
 |
| 7. गुप्तकाशी का बाज़ार अभी खुला नहीं है इसलिए सड़क पर शान्ति है |
 |
| 9. देवर चौरा गाँव की महिलाएं पशुओं के लिए चारा और चूल्हे के लिए लकड़ी लाती हुई. बूंदा बांदी और 10-15 किलो के वजन के बावजूद चहरे पर मुस्कराहट है. यहाँ 'बेटी बचाओ' जैसे नारे की ज़रुरत नहीं है |
 |
| 10. केदारनाथ को जाने वाली सड़क को चौड़ा किया जा रहा है. इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा क्यूंकि ज्यादातर पहाड़ भुरभुरे से लगते हैं और भूस्खलन की आशंका बनी रहती है |
 |
| 11. गुप्तकाशी के द विलेज रिट्रीट रिसोर्ट में. ये सुंदर रिसोर्ट यहाँ की एक महिला उद्यमी श्रीमति स्नेहा बगवाड़ी भट्ट चलाती हैं |
 |
| 12. सड़कें बन रही हैं तो मलबा ढुलाई के लिए खच्चर भी काफी संख्या में दिखते हैं |
 |
| 14. लहराती चलती मस्त नदी मधु जो मध्यमहेश्वर से निकल कर मन्दाकिनी में मिल जाती है |
 |
| 15. सुप्रभात |
राफ्टिंग के झटके
- देखो भई ना तो मुझे तैरना ही आता है और ना ही चप्पू चलाना. हम तो बोटिंग कर लेंगे.
कई एक साथ बोल पड़े,
- चलो अंकल चलो !
- आप ने कुछ नहीं करना !
- चप्पू नहीं चलाना बस आप बोट के बीच में बैठ जाना !
तो साब हम भी चल पड़े अब जो होगा देखा जाएगा. राम झूला पहुँच कर राम भरोसे बोलेरो में बैठे और सभी आठों दिलेर बन्दे 20 किमी दूर शिवपुरी पहुँच गए. बोलेरो की छत से रबड़ की बोट उतार कर नीचे ले जाई गई और गंगा किनारे रेत पर रख दी गई. इस बोट को बोट कहने के बजाए राफ्ट या रैफ्ट कहना बेहतर है. इसी की सवारी करनी थी. आसमान पर बादल छाए थे और बूंदाबांदी हो रही थी. तेज़ और ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे. गंगा के हरियल पानी के दोनों तरफ ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ थी. गाइड नेगी ने नमस्ते करके भाषण देना शुरू कर दिया:
- सभी हेलमेट पहन लें. राफ्ट से कभी कोई गिर जाए और किसी चट्टान से टकरा जाए तो चोट ना लगे इसलिए ये पहनना बहुत ज़रूरी है.
- ( सुबह सुबह गंगा किनारे यही बताना था क्या? ).
- लाइफ-जैकेट कसकर बाँध लें. पानी में गिरने के बाद जैकेट ऊपर की ओर उठाती है और ढीली हो सकती है. अगर ढीली हो जाए तो बेल्ट खींच कर कस लें.
- ( ये लो सुबह सुबह ठन्डे पानी में गिरा रहा है! कैसा आदमी है ये? ).
- जूते चप्पलें उतार दें, मोबाइल और पर्स इस वाटरप्रूफ थैले में डाल दें, चप्पू को ऐसे पकड़ना है, ऐसे फॉरवर्ड चलाना है, ऐसे बैकवर्ड चलाना है, इस थैली में लम्बी रस्सी है अगर कोई बोट से गिरा तो जल्दी से रस्सी निकाल कर उसकी तरफ फेंकनी है ( मरवा देगा आज क्या? ), टीम की तरह काम करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है और टीम को बोट सुरक्षा के साथ आगे ले जानी है, चलिए बैठिये, सबसे आगे कौन बैठेगा?
 |
| Ready to Raft. From left to right - 1. Selfie Master Ankit Taneja, 2. Cliff Jumper Dhruv Gera, 3. Lightweight Sippy Taneja Wardhan, 4. Ustad Mukul Wardhan, 5. White Beard Harsh Wardhan, 6. Expert Commentator Swati Singh Taneja, 7. Expert Rafter Divya Gera and 8. Fearless Swimmer Garima Gera |
राफ्टिंग क्या है?
ये राफ्टिंग एक खेल समझ लीजिये जिसमें जोश है, मनोरंजन है, एडवेंचर है और ख़तरा भी है. टीम के हर सदस्य का एक दूसरे का ख़याल रखना और सहयोग करना भी सिखाता है. यह खेल नदियों के ढलान पर ही खेला जाता है. ऐसे में पानी का बहाव तेज़ होता है जिसकी वजह से रबड़ का हवा भरा हुआ राफ्ट खुद ही तेज़ी से आगे भागता है. कुछ कुछ दूरी पर पानी झरने की तरह नीचे पत्थरों या चट्टानों पर गिरता है. कहीं कहीं भंवर बनते हैं कहीं बीच में चट्टान खड़ी मिलती है तो कहीं किनारे पर रेतीला बीच - river beech मिलता है. हलके चप्पुओं द्वारा अपने राफ्ट को पत्थरों, चट्टानों और भंवरों से बचा कर निकालना होता है. और of course खुद को भी गिरने से बचाना होता है.
1970 से यह खेल अमरीका में शुरू हुआ और फिर पूरे विश्व में फ़ैल गया. इस खेल के तमाम पहलुओं पर नज़र रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राफ्टिंग संघ भी बन गया है. इस खतरे वाले खेल के खतरों को एक से दस तक के स्केल पर इस तरह से क्लास में बाँट दिया गया है:
क्लास 1 - पानी का बहाव धीमा और उबड़ खाबड़ पथरीला इलाका कम जिसे नौसिखिये भी पार कर सकें.
क्लास 2 - पानी थोड़ा ज्यादा और बहाव भी. बड़ा पथरीला इलाका और थोड़ा सा ख़तरा.
क्लास 3 - सफ़ेद झागदार पानी ( white water ) और हलकी ऊँची नीची लहरें भी.
क्लास 4 - सफ़ेद झागदार तेज़ पानी, मध्यम ऊँचाई वाली लहरें और चट्टानें. ताकत और कौशल की जरूरत.
क्लास 5 - सफ़ेद झागदार तेज़ धारा ऊँची तरंगें और बड़ा एरिया. ज्यादा ताकत और कुशलता की जरूरत और
क्लास 6 - सफ़ेद झागदार ऊँची ऊँची लहरें, बड़े बड़े पत्थर, तेज़ बहाव और बड़ी चट्टानें याने खतरनाक राफ्टिंग.
इस खेल में राफ्ट बाई या दाईं ओर उलट सकता है, किसी चट्टान से टकरा कर अगला हिस्सा ऊपर उठ कर पीछे की और पलटी खा सकता है. ऐसा भी हो सकता है की ढलान पर जब राफ्ट की नाक पानी में जाए तो राफ्ट उठ ही ना पाए. उस स्थिति में पिछला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा और शायद सभी सवारियों को गिरा देगा. राफ्ट किसी नुकीले पत्थर से टकरा कर कट फट जाने का भी ख़तरा हो सकता है हालांकि ये राफ्ट गाड़ियों के टायर जैसे सख्त रबड़ के बने होते हैं.
भारत में ये खेल बहुत पुराना नहीं है शायद 15 से 20 साल पुराना होगा. यहाँ कई जगह पर राफ्टिंग का मज़ा लिया जा सकता है. इनमें से कुछ हैं -
- सिक्किम में तीस्ता नदी पर भी राफ्टिंग के कई स्थान हैं .
- अरुणाचल में सुबनसरी नदी में टूटिंग - पासी घाट तक क्लास 4 या ऊपर के खतरे वाली राफ्टिंग की जा सकती है.
- हिमाचल में कुल्लू मनाली में भी राफ्टिंग हो सकती है पर ख़तरा ज्यादा है.
- कोलाड, महाराष्ट्र में कुंडलिका नदी की 15 किमी की लम्बाई में राफ्टिंग की जा सकती है.
- बारापोल नदी कुर्ग, कर्णाटक में भी राफ्टिंग की जा सकती है.
 |
| चार दाएं बैठो |
 |
| और चार बाएँ बैठो |
लो राफ्ट चली!
अब गाइड ने हमें बैठाना शुरू कर दिया. चार बाएँ बैठेंगे, चार दाएँ और पीछे गाइड नेगी जी पधारेंगे. सबको एक एक चप्पू दे दिया गया. एक हाथ चप्पू के हैंडल के टॉप पर रखना है और दूसरा पीले ब्लेड से चार छे इंच ऊपर. बैठ तो गए पर बैठ कर पकड़ें किसको? दोनों हाथ में तो पैडल पकड़ना था. बोट के अंदर चार गोल तकिये से लगे हुए थे. अपने अगले पैर के पंजे को फर्श और गोल तकिये के बीच फसाना है और पिछले पैर के पंजे को गोल मुंडेरी और फर्श के बीच फ़साना है. फर्श में छेद थे जिसमें से ठंडा पानी आ रहा था. बोट के चारों तरफ एक रस्सी थी उसे इमरजेंसी में पकड़ा जा सकता था.
- बाप रे बाप! नेगी जी ये क्या करवा रहे हो? गिर जाएंगे यार.
पर नेगी जी कहाँ सुन रहे थे. उन्होंने तो जोर से नारा लगा दिया 'हर हर गंगे' और अपने चप्पू को पत्थर से लगाकर जोर मारा और राफ्ट को धारा में धकेल दिया! सबने जवाब दिया 'हर हर गंगे'.
राफ्ट ठन्डे पानी में हिचकोले खाता हुआ स्पीड पकड़ने लगा. कुछ राफ्ट के फर्श से और कुछ चप्पुओं के छपाक छपाक करने से तुरंत सब गीले हो गए. नेगी जी जोश दिलवा रहे थे,
- पैडल फा-र-वा-र्ड! पै-ड-ल फा-र-वा-र्ड! जोर लगा के! लेफ्ट साइड में पहला नंबर ठीक से चप्पू चलाओ!
इशारा मेरी तरफ था. पीछे बैठी गरिमा चिल्लाई,
- अंकल आपको ही कह रहा है!
- अरे तू छोड़ उसको. यहाँ समझ नहीं आ रहा की चप्पू पकडूँ, रस्सी पकड़ूं या पैर फसा कर रखूं ? सब कुछ तो हिचकोले खा रहा है और ठण्ड अलग रही है. चलने से पहले अखबार में अपना होरोस्कोप भी नहीं देखा !
धारा के बीच में आकर राफ्ट की रफ़्तार और तेज़ हो गई, हिचकोले तेज़ हो गए और राफ्ट आड़ी तिरछी आगे भागने लगी. ऊपर-नीचे, दाएं-बाएँ फिर भी आगे और आगे.
- 'पै-ड-ल -- फा-र-वा-र्ड'! तैयार हो जाओ रैपिड आने वाला है ! स्टॉप पैडल---स्टॉप पैडल !
अभी सम्भल भी ना पाए थे कि बोट ने डाईव मार दी. बर्फीले पानी की लहर छपाक से सिर पर आकर गिरी. पता नहीं कितनी बार ऊपर नीचे और दाएं बाएँ हुए. चश्मे पर पानी पड़ा और दिखना बंद हो गया. याद आया कि अभी तक कमबख्त वसीयत भी नहीं लिखी थी ! अब वापिस जा कर सबसे पहले यही काम करना है. तब तक नेगी जी की जोरदार आवाज़ आई,
- पै-ड-ल फा-र-वा-र्ड ---- पै-ड-ल - फा-र-व-र्ड. रैपिड निकल गया बहुत अच्छे !
बोट थोड़ा संभल गई और समतल पानी में बढ़ने लगी. यहाँ गंगा का पाट चौड़ा था. आसपास नज़र डाली तो तीन बोट आगे भी भागी जा रही थीं. उनमें बैठे छोरे छोरियां जोश में चिल्ला रहे थे और सभी मजे ले रहे थे. नेगी जी बिना रुके बोले जा रहे थे,
- बहुत अच्छे बहुत अच्छे. रोलर कोस्टर आने वाला है. शाबाश शाबाश. चप्पू तैयार है? टी-म फा-र-व-र्ड!
पांच सौ मीटर सामने लहरों का मेला नज़र आ रहा था. अंदाज़न तीन फीट ऊँची होंगी. और सौ मीटर आगे जाने पर नज़र आया की इन लहरों के बाच दो से चार फुट तक के गैप भी हैं और इसका मतलब है की बोट खूब उछ्लेगी और सीधी नहीं रह पाएगी. रौंगटे खड़े हो गए और सारे शरीर में सिहरन दौड़ गई. रस्सी और पैडल को उँगलियों और अंगूठे में कस लिया. दोनों पैर फिर से अच्छी तरह फंसा लिए. बुरे फंसे आज तो. गौतम बुद्ध का डायलॉग याद आ गया - वर्तमान पर ध्यान दो भूत या भविष्य पर नहीं ! सही बिलकुल सही केवल लहरों को ही देखना है स्वर्ग की तरफ नहीं. तो फिर लहरों पर नज़र गड़ा दी ready, steady & go!
राफ्ट तेजी से नीचे गई और एक ऊँची लहर सबके ऊपर गिरी. फिर राफ्ट ऊपर उठी सबने चीख मार दी. बौछार चश्में पर पड़ी और दिखना बंद हो गया और दो, तीन या शायद चार मिनट कुछ नहीं पता चला क्या हुआ. बर्फीले पानी की भारी बौछार, लहरों का शोर, राफ्ट के हिचकोले, सबकी चिल्लाहट और गाइड की आवाज़ सब कुछ एक साथ हो रहा था.
फिर से राफ्ट सीधी हो गयी, सबने एक दूसरे को देखा और गाइड की आवाज़ भी कान में पड़ने लगी - 'शाबाश शाबाश'. अब तो सारे हंस रहे थे. सांस में सांस आ गई. अगले तीन चार किमी गंगा शांत नज़र आ रही थी. नेगी जी ने कहा जिसने पानी में उतरना है वो उतर सकता है और राफ्ट की रस्सी पकड़ कर साथ साथ तैर सकता है. बारी बारी से सब ने मज़ा लिया पर भई अपने बस की बात नहीं थी. 67 के ना हो कर 27 या 37 के होते तो शायद हम भी करतब दिखाते. ध्रुव और गरिमा ने बहादुरी दिखाई और रस्सी छोड़ कर बोट से आगे निकल गए और तैर कर फिर नजदीक आ गए तो गाइड ने उन्हें जैकेट से पकड़ कर ऊपर उठा लिया.
और आगे चले तो Cliff Jumping Point आ गया. वहां धीरे से लहरों को काटते हुए राफ्ट को किनारे लगा दिया गया. किनारे पर उबड़ खाबड़ पत्थरों पर चाय और मैगी के खोखे थे. लगभग 50 - 60 नंगे पैर राफ्टर वहां जमा थे. गरमा गरम चाय पीकर जान आ गई हालांकि सर्दी की वजह से कंपकपी जारी थी. तब तक ध्रुव Cliff पर चढ़ गया और ऊपर से जम्प लगा दी शायद 20 - 25 फुट की ऊँचाई रही होगी.
Tea break के बाद एक बार फिर से राफ्ट पर सभी सवार हो गए. ब्रेक से पहले मेरी सीट बाएँ तरफ से पहली थी अब दाएं साइड में चौथी हो गयी. गाइड ने बताया कि मुश्किल वाले रैपिड खत्म हो गए और आगे पानी सीधा सीधा सा ही है. धीरे धीरे राफ्ट को आगे ले जा कर फिर से दाहिने किनारे पर ले गए. लगभग 12- 13 किमी लम्बी यात्रा समाप्त हुई जो हमेशा के लिए याद रहेगी.
मेरे कंधे अभी भी दुःख रहे हैं. मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किसने कहा था कि बस अंकल आपने बीच में बैठे रहना है और आपने कुछ नहीं करना है! 😠😜
 |
| Team of Eight Greats |
हरिद्वार पर फोटो-ब्लॉग - 1/3
गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से शुरू होती है और लगभग 250 किमी की पहाड़ी यात्रा करके हरिद्वार पहुँचती है. यहाँ से गंगा की मैदानी यात्रा शुरू हो जाती है. इसीलिए हरिद्वार का एक और नाम है गंगाद्वार. प्राचीन काल में यहाँ कपिल ऋषि ने तपस्या की थी इसलिए हरिद्वार को कपिलस्थान भी कहा गया है. एक और नाम मायापुरी भी पुराने समय में प्रचलित रहा है.
हरिद्वार के नाम की एक और रोचक जानकारी मिली कि हर हर महादेव याने शिव भक्त इसे हरद्वार कहते हैं. जबकि हरि याने विष्णु भक्त इस स्थान को हरिद्वार कहते हैं.
उत्तराखंड के चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का द्वार हरिद्वार ही है. हरिद्वार का सबसे पवित्र और प्रसिद्द घाट है हर की पौड़ी( या हर की पैड़ी ). कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तहरी ने यहाँ गंगा तट पर तपस्या की थी. राजा विक्रमादित्य ने उनकी याद में ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ये घाट बनवाया था जो कालान्तर में हर की पौड़ी कहलाया.
हर की पौड़ी की शाम की आरती बड़ी आकर्षक लगती है. साथ ही घाट पर 24 घंटे का मेला ही लगा रहता है. मुंडन भी यहीं है, पूजा पाठ भी और अस्थि प्रवाह भी. गंगा सब कुछ समेट लेती है. दिल्ली, बिहार, राजस्थान, गुजरात, बंगाल और यहाँ तक की दक्षिण भारत से भी भक्तगण आते रहते हैं. बच्चे, बूढ़े और जवान, पण्डे, साधू संत, बहरुपिए, जेबकतरे, मांगने वाले, बेचने वाले, तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के चेहरे याने पूरी मानवता का दर्शन हर की पौड़ी पर हो जाता है.
इस बार सुबह के चार घंटे घाट पर मेला देखते देखते हुए ही गुज़ार दिए. बहुत से फोटो लिए जिन्हें तीन भागों में प्रस्तुत किया है और यह पाहला भाग है:
 |
| 1. हर की पौड़ी. ये घंटाघर 1938 में बना था और तब से अब तक इसने करोड़ों लिटर पानी बहते देखा होगा. करोड़ों लोगों ने डुबकी मार ली होगी. 'धर्म किये धन ना घटे नदी ना घट्टे नीर, अपनी आंखन देखि ले यों कथि कहिहें कबीर' |
 |
| 2. हर की पौड़ी से आगे बढ़ता शहर. साफ़ सफाई बढ़िया होती और रख रखाव अच्छा होता तो और भी सुंदर हो सकता है |
 |
| 3. गंगा से निकली एक धार हर की पौड़ी से गुज़रती है और आगे अपर गंग नहर के रूप में मोदी नगर होते हुए एटा की ओर चली जाती है. हजारों साल से निरंतर फल, फूल, खेती और मानव सेवा में लगी हुई है गंगा चाहे मानव उसका कम ही ध्यान रखता है |
 |
| 4. गुड़िया रानी सामान की पहरेदारी करते करते थक गई लगती है |
 |
| 5. श्रद्धांजलि के फूल प्रवाहित करने की तैयारी |
 |
| 6. चदरिया झीनी रे झीनी |
 |
| 7. हर की पौड़ी पर कई तरह के विधि विधान हर समय चलते रहते हैं. 'कहना था सो कह दिया अब कुछ कहा ना जाय, एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाय' - कबीर |
 |
| 8. नियम तो हर की पौड़ी में भी वही है - महिलाऐं शौपिंग करेंगी और पुरुष जेब ढीली करेंगे |
 |
| 9. जल पुलिस और थल जेबकतरे - हम आस पास हैं! |
 |
| 10. गंगा स्नान हो गया है और मोबाइल पर सूचना दी जा रही है तब तक पतिदेव कपड़े सुखा लेंगे |
 |
| 11. भांत भांत के रंग भांत भांत के चोले |
 |
| 12. कोऊ काहे में मगन कोऊ काहे में - चिलम का सुट्टा, स्नान के बाद कान की सफाई या फिर यूँ ही विश्राम. 'माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मनका डार दे मन का मनका फेर' -कबीर |
 |
| 13. तीन सौ साल पुराना बरगद और श्री महंत केदार पुरी जी का धूना याने 24 घंटे लकड़ी जलती रहती है, धुआं उठता रहता है और बाबा जी भस्म लगाते रहते हैं. 'चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जा को कुछ ना चाहिए वा ही शहनशाह' - कबीर |
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. आरती का समय हरिद्वार पर फोटो-ब्लॉग - 2/3
समुद्र मंथन के बाद अमृत का घड़ा लेकर गरुड़ ने देवलोक की ओर उड़ान भरी तो
अमृत की कुछ बूँदें छलक कर हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग और नासिक में गिरीं.
इससे हरिद्वार की मान्यता जानी जा सकती है. शिवालिक पहाड़ियों और गंगा तट के
बीच बसा तीर्थ हरिद्वार, दिल्ली से 225 किमी दूर है. समुद्र तल से इसकी
ऊँचाई लगभग 250 मीटर है. यहाँ का तापमान मौसम के अनुसार 5 से 40 डिग्री तक
जा सकता है. सितम्बर से अप्रैल तक घूमने के लिए अच्छा मौसम है. हर तरह की
धर्मशालाएं और होटल यहाँ उपलब्ध हैं. तीर्थ होने के कारण बारहों महीनें
यात्रियों का आना जाना लगा रहता है. गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से शुरू होती है और लगभग 250 किमी की पहाड़ी यात्रा करके हरिद्वार पहुँचती है. यहाँ से गंगा की मैदानी यात्रा शुरू हो जाती है. इसीलिए हरिद्वार का एक और नाम है गंगाद्वार. पुराने समय में यहाँ कपिल ऋषि ने तपस्या की थी इसलिए हरिद्वार को कपिलस्थान भी कहा गया है. एक और नाम मायापुरी भी पुराने समय में प्रचलित रहा है. हरिद्वार के नाम की एक और रोचक जानकारी मिली कि हर हर महादेव याने शिव भक्त इसे हरद्वार कहते हैं. जबकि हरि याने विष्णु भक्त इस स्थान को हरिद्वार कहते हैं. उत्तराखंड के चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का द्वार हरिद्वार ही है. हरिद्वार का सबसे पवित्र और प्रसिद्द घाट है हर की पौड़ी( या हर की पैड़ी ). कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तहरी ने यहाँ गंगा तट पर तपस्या की थी. राजा विक्रमादित्य ने उनकी याद में ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ये घाट बनवाया था जो कालान्तर में हर की पौड़ी कहलाया. हर की पौड़ी पर 24 घंटे मेला ही लगा रहता है. मुंडन भी यहीं है, पूजा पाठ भी और अस्थि विसर्जन भी और गंगा सब कुछ समेट लेती है. कुछ के लिए यह तीर्थ है और कुछ के लिए जीविका का स्थान. पण्डे, बहरूपिये, भीख मांगने वाले वगैरा वगैरा यात्रियों पर ही निर्भर हैं. बहुत से फोटो लिए जिन्हें तीन भागों में प्रकाशित किया जाएगा. तीन में से दूसरा भाग प्रस्तुत हैं. पहला भाग इस लिंक पर उपलब्ध है : http://jogharshwardhan.blogspot.com/2017/05/13.html
|
गेलुग बौद्ध विहार, देहरादून
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
गुरूद्वारा पांवटा साहिब - ਪਾਂਉਟਾ ਸਾਹਿਬ
ऐतिहासिक पांवटा साहिब गुरुद्वारा यमुना
नदी के किनारे जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है. देहरादून से
पांवटा साहिब 45 किमी की दूरी पर है और चंडीगढ़ से करीब 130 किमी. जाने के
लिए बसें और टैक्सी दोनों ओर से उपलब्ध हैं. देहरादून से जाने वाली सड़क
अच्छी है पर सिंगल हैं और ट्रैफिक ज्यादा है. दून
घाटी के अंतिम छोर पर पांवटा साहिब है. दून घाटी में बहती यमुना नदी
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच की सीमा रेखा है. गुरुद्वारा साहिब के
साथ बहती यमुना नदी और आस पास पहाड़ियाँ सुंदर लगती है. पर नदी का पूरा पाट
पथरीला होने के कारण दोपहर में तेज़ गर्मी होती है. सुबह पहुंचना आरामदेह
रहेगा.
यह
शहर दसवें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ( जन्म 22 दिसम्बर 1666 -
निर्वाण 07 अक्टूबर 1708) का बसाया हुआ है. गुरु महाराज अप्रैल 1685 में
यहाँ पधारे थे. कहते हैं की घोड़े से उतर कर उन्होंने अपने पांव यहाँ टिका
दिए और इसलिए जगह का नाम पांवटा साहिब पड़ गया. एक दूसरी कहावत के अनुसार
उनके पांव में एक जेवर था पांवटा जो यमुना में नहाते हुए खो गया इसलिए इस
जगह का नाम पांवटा पड़ गया.
गुरु
महाराज यहाँ चार साल से ज्यादा रहे और यहीं पर उन्होंने कई भजन कीर्तन और
'दसम ग्रन्थ' की शुरुआत की जिसे आनंदपुर साहिब में पूरा किया. यहीं उनके
पुत्र साहिबज़ादा बाबा अजित सिंह जी का जन्म हुआ था. यहाँ गुरु महाराज ने
घुड़सवारी, तैराकी और हथियारों के इस्तेमाल में दक्षता हासिल की और इस तरह
से जीवन भर 'संत-सिपाही' रहे.
गुरुद्वारा
साहिब परिसर तीन एकड़ में फैला हुआ है. परिसर में दस्तार अस्थान है जिसमें
पगड़ी बाँधने का कम्पटीशन कराया जाता था. इसके पास ही कवि दरबार अस्थान है
जहाँ शबद कीर्तन और कवि गोष्ठियां होती थीं. और तालाब अस्थान है जहां गुरु
महाराज वेतन बांटते थे. एक छोटा म्यूजियम भी है जहाँ गुरु महाराज के हथियार
और कलम रखे हुए हैं. यहाँ लगभग 2000 से ज्यादा लोग रोज़ आते हैं. साथ ही एक
हॉल में लंगर की सुंदर व्यवस्था है. जब भी जाएं प्रसाद स्वरुप भोजन का
आनंद जरूर लें.
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
यह शहर दसवें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ( जन्म 22 दिसम्बर 1666 - निर्वाण 07 अक्टूबर 1708) का बसाया हुआ है. गुरु महाराज अप्रैल 1685 में यहाँ पधारे थे. कहते हैं की घोड़े से उतर कर उन्होंने अपने पांव यहाँ टिका दिए और इसलिए जगह का नाम पांवटा साहिब पड़ गया. एक दूसरी कहावत के अनुसार उनके पांव में एक जेवर था पांवटा जो यमुना में नहाते हुए खो गया इसलिए इस जगह का नाम पांवटा पड़ गया.
गुरु महाराज यहाँ चार साल से ज्यादा रहे और यहीं पर उन्होंने कई भजन कीर्तन और 'दसम ग्रन्थ' की शुरुआत की जिसे आनंदपुर साहिब में पूरा किया. यहीं उनके पुत्र साहिबज़ादा बाबा अजित सिंह जी का जन्म हुआ था. यहाँ गुरु महाराज ने घुड़सवारी, तैराकी और हथियारों के इस्तेमाल में दक्षता हासिल की और इस तरह से जीवन भर 'संत-सिपाही' रहे.
गुरुद्वारा साहिब परिसर तीन एकड़ में फैला हुआ है. परिसर में दस्तार अस्थान है जिसमें पगड़ी बाँधने का कम्पटीशन कराया जाता था. इसके पास ही कवि दरबार अस्थान है जहाँ शबद कीर्तन और कवि गोष्ठियां होती थीं. और तालाब अस्थान है जहां गुरु महाराज वेतन बांटते थे. एक छोटा म्यूजियम भी है जहाँ गुरु महाराज के हथियार और कलम रखे हुए हैं. यहाँ लगभग 2000 से ज्यादा लोग रोज़ आते हैं. साथ ही एक हॉल में लंगर की सुंदर व्यवस्था है. जब भी जाएं प्रसाद स्वरुप भोजन का आनंद जरूर लें.
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
टेहरी गढ़वाल
टेहरी का पुराना नाम त्रिहरि बताया जाता है और उससे भी पुराना नाम गणेश प्रयाग. यहाँ भागीरथी और भिलांगना मिलती हैं और ऋषिकेश की ओर चल पड़ती हैं.
सन् 888 तक गढ़वाल में छोटे छोटे 52 गढ़ हुआ करते थे जो सभी स्वतंत्र राज्य थे. इनके मुखिया ठाकुर या राणा या राय कहलाते थे. एक बार मालवा के राजा कनक पाल सिंह बद्रीनाथ दर्शन के लिए आये. एक गढ़ के राजा भानु प्रताप ने अपनी इकलौती बेटी की शादी कनक पाल सिंह से कर दी. इसके बाद कनक पाल सिंह और उनके उत्तराधिकारियों ने धीरे धीरे सारे गढ़ जीत कर एक गढ़वाल राज्य बना लिया. 1803 से 1815 तक गढ़वाल में नेपाली राज रहा. ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय छोटे राजाओं ने एंग्लो-नेपाल युद्ध में नेपाली शासन को हरा दिया और टेहरी रियासत राजा सुदर्शन शाह को दे दी गयी.
सुदर्शन शाह और उनके वंशजों ने रियासत का भारत में विलय होने तक राज किया. इनमें से प्रमुख थे प्रताप शाह जिसने प्रताप नगर बसाया, कीर्ति शाह जिसने कीर्ति नगर बसाया और नरेंद्र शाह जिसने नरेंद्र नगर बसाया. ऋषिकेश से टेहरी जाते हुए नरेंद्र नगर रास्ते में देखा जा सकता है.
टेहरी का नाम टेहरी बाँध से जुड़ा हुआ है. इस बाँध की परिकल्पना पहले पहल 1961 में की गई. बहुत सी सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बाधाओं को पार करने के बाद 2006 में परियोजना चालू हुई. भारत का सबसे ऊँचा और विश्व में पांचवे नंबर का ऊँचा बाँध है जो 2400 मेगावाट बिजली, 102 करोड़ लिटर पीने का पानी और 2,70,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की क्षमता रखता है. सुरक्षा कारणों से अंदर जाना मना है और अगर किसी उच्च अधिकारी की सिफारिश पर पहुंच भी गए तो फोटो खींचना मना है.
बाँध से दूर झील में बोटिंग, स्कीइंग वगैरा की जा सकती है. झील के बीच में नाव की सवारी रोमांचक है. पर जब नाविक ने बताया की कहीं कहीं पानी की गहराई 800 मीटर तक भी है तो एक बार तो नौका सवारी भयभीत और रौंगटे खड़े करने वाली लगती है. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
 |
| नया बसा न्यू टेहरी शहर, पहाड़, घाटियाँ, बादल, कोहरा और सुनहरी धूप |
 |
| टेहरी की घाटियों बारिश के बाद घाटी से उठता कोहरा |
 |
| नई टेहरी का एक दृश्य |
 |
| टेहरी से 12 किमी पहले है चंबा |
 |
| सुबह सुबह का दृश्य |
 |
| बारिश के बाद कोहरा |
 |
| भागीरथी. बारिशों में पानी का तल ऊपर सीमा रेखा तक चला जाता है |
 |
| भागीरथी के साथ साथ |
 |
| टेहरी झील का बोट क्लब |
 |
| हाँ तैयार हूँ जनाब ! |
 |
| स्पीड बोट, चेयर बोट, स्कीइंग और वाटर स्कूटर उपलब्ध हैं |
 |
| मानसून के बाद पानी छोटी पहाड़ियों को डुबो देता है |
 |
| झील अलग से ना बना कर पानी घाटियों में ही इकठ्ठा कर लिया जाता है |
 |
| पानी घटने पर पुराने टेहरी की झलक नज़र आती है |
 |
| टेहरी शहर का 1992 का फोटो - सिंह राशि, नाम त्रिहरी ( टेहरी ). जन्म 28 दिसम्बर 1815, जलमग्न 29 जुलाई 2005 शाम 5.34 बजे |
 |
| पहाड़ों पर चढ़ना उतरना आसान नहीं है और ना ही गाड़ी चलाना. पर फिर मज़ा भी तो है ! एक स्थानीय कहावत है की "जवानि मा नि देखि देस बुढेन्दा खाबेस". याने आप जल्द से जल्द बस्ता बाँध लो पहाड़ों की सैर के लिए |
ऋषिकेश के रंग
ऊँचे पहाड़ों और गहरी घाटियों में से उछलती कूदती गंगा शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे ऋषिकेश तक आ पहुंचती है. ऋषिकेश से आगे गंगा की चाल धीमी पड़ जाती है. पर गंगा नदी आगे के मैदानों में खेती, जंगल, पशु-पक्षी और मनुष्यों की सेवा में जुट जाती है हालांकि मनुष्यों ने इसे दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. गंगा के बहाव के दाहिनी ओर ऋषिकेश बसा हुआ है और बाएँ तट पर जंगल हैं. इन जंगलों में अब कई आश्रम बन गए हैं. गंगा के दाहिने ओर से बाएँ तट पर जाने के लिए दो पुल हैं - लक्ष्मण झूला और राम झूला. ये पुल ऋषिकेश की ख़ास निशानियाँ हैं और तेज़ हवा हो तो दोनों पुल झूलते रहते हैं. इसी कारण पुल या सेतु के बजाए झूला कहा जाता है.
ऋषिकेश में मंदिर, आश्रम, घाट, धर्मशालाएं, योग संस्थान और आयुर्वेद उपचार के बहुत से संस्थान हैं. पर्यटकों के लिए बोटिंग और राफ्टिंग भी उपलब्ध है. जहाँ मन लगे वहां पैसा खर्चें और आनंद लें. प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
 |
| गंगा के बाएँ किनारे पर परमार्थ आश्रम में शाम की आरती का एक दृश्य |
 |
| राम झूला से नज़र आती रबड़ की नाव |
 |
| राम झूला. लोहे की रस्सी से बना ये पुल 750 फीट लम्बा है और जिसे 1986 में बनाया गया था |
 |
| गंगा के बाएँ तट से नज़र आता लक्ष्मण झूला |
 |
| चना मुरमुरा का आनंद लें |
 |
| सफ़ेद रेत और गंगा का हरा पानी |
 |
| लक्ष्मण झूला. कहा जाता है कि लक्ष्मण ने जूट की रस्सी के सहारे यहाँ गंगा पार की थी. लोहे की रस्सी से 1889 में पुल बनाया गया. 1930 में फिर से नया पुल बनाया गया. यह पुल 450 फीट लम्बा है और पानी से लगभग 60 फीट ऊँचा है. पैदल तो इसपर चलते ही हैं दुपहिया भी चलते हैं |
 |
| राफ्टिंग के लिए रबर बोट पर ॐ का सुरक्षा कवच |
 |
| लक्ष्मण झूले के पास एक मंदिर - ऊपर और ऊपर |
 |
| विदेशी लड़कियां गंगा में दिया बहाने की तैयारी में |
 |
| साधू के फोटो के बिना तो ऋषिकेश का ब्लॉग अधूरा ही रह जाएगा ! देखने में तो 30 के आस पास लग रहा था. दस का नोट लेने के बाद कहने लगा की चार धाम की यात्रा पर निकले हैं, नंगे पाँव हैं चप्पल के लिए पैसे दे दें |
 |
| गंगा के बाएं तट पर बहुत से आश्रम हैं जैसे - स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन, गीता भवन और 84 कुटिया. अपनी गाड़ी से जाने के लिए इस नहर के साथ साथ जाना होगा. सड़क ज्यादा अच्छी नहीं है पर सीनरी बहुत सुंदर है |
 |
| इसी नहर किनारे चीला में एक छोटा पन-बिजली घर भी नज़र आ जाता है |
 |
| आरती का समय |
Rajaji Tiger Reserve, Chilla, Uttarakhand
This Reserve is spread over an area of 820 sq km in Haridwar, Dehradun & Pauri Garhwal districts of Uttarakhand. Chilla is in Pauri district though it is nearer to Rishikesh / Haridwar. This is second tiger reserve in Uttarakhand first being Jim Corbett National Park.
As the Ganga flows, Rishikesh town is on right bank & forests are on left bank. For crossing over on foot or on a two wheeler there is Laxman Jhoola or Ram Jhoola. There is no bridge in Rishikesh town for cars. For cars there is a barrage for going to the left bank or a bridge on Haridwar-Kotdwar road can be used. Nearest railway station is Haridwar & airport Dehrdun.
As for stay, there are forest rest houses and a small hotel run by Garhwal Mandal Vikas Nigam. Tariff for GMVN are 2.5k to 6k. Location & service of this hotel is good. Please book online as nearest alternate is either in Haridwar or Rishikesh.
Forest has deer, sambhar, wild boars, elephants, tiger & leopards. But in 3 hr safari we could not spot any tiger or leopard. Lots of colourful birds are there. Better have a binocular handy.
Gypsies are available @ 1500 per trip, guide costs 300 & entry ticket 150 ( seniors 50% ), foreigners 600 per person. Timings are 6 to 9 in the morning and 3 to 6 in the evening. Full day safari is also available. Reserve remains closed in July & August due to rains. Some photos:
 |
| Welcome to Rajaji Tiger Reserve Chilla, Pauri Garhwal |
 |
| Meet Juhi two month old baby elephant. She was found by a forest guard crying in a ditch with her mother nowhere in sight. At that time she was one month old. Forest guard has named the baby elephant 'Juhi' |
 |
| Juhi lives in this room & wants to get in. She is being fed with liquid diet made of baby food, milk & water. She consumes 26 litres of it per day |
 |
| Deer, spotted deer, wild boar, elephants & Sambhar can be seen. There are 14 tigers & many leopards also but they did not oblige us |
 |
| jumbo safari is also available |
 |
| Group of elephants. Binoculars are useful item in jungle |
 |
| We decided to take on 36 km long jungle road on our EcoSport. It took almost three hours of tough gruelling ride. Sighting of tiger or leopard would have given some satisfaction! |
 |
| View from the Machan in Hotel - in the background is a small hydro-elec plant and Shivalik Hills |
दुगड्डा, उत्तराखंड
1953 में कोटद्वार रेलवे स्टेशन बनने के बाद दुगड्डा का व्यापारिक महत्व घट गया क्यूंकि कोटद्वार व्यापर का केंद्र बन गया. मोटर मार्ग बनने से पहले उपरी क्षेत्र के लोग खोह नदी के किनारे-किनारे नीचे आया करते थे ओर रसद खच्चरों की सहायता से ऊपर पहुँचाया जाता था.
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो :
मिन्द्रोल्लिंग बौद्ध विहार, देहरादून
तिब्बती भाषा में मिन्द्रोल्लिंग - mindrolling- शब्द का अर्थ है place of perfect emancipation याने पूर्ण मुक्ति का स्थान. पहला मिन्द्रोल्लिंग मठ 1676 में तिब्बत में स्थापित किया गया था. देहरादून में छठा मिन्द्रोल्लिंग मठ है जिसकी शुरुआत 1965 में की गई थी. इससे पहले 1959 में चीन तिब्बत में घुसपैठ कर गया था और मठ के लोगों को वहां से भागना पड़ा था. मिन्द्रोल्लिंग मठ बौध दर्शन के वज्रयान या तांत्रिक बौध धर्म का पालन करता है.
प्रस्तुत हैं कुछ फोटो:
गुप्तकाशी
गुप्तकाशी का समबन्ध पांडवों से जुड़ा हुआ है। और इस के नाम पर एक कहानी भी प्रचलित है की महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण ने पांडवों से कहा कि वे युद्ध में उनके द्वारा मारे गए परिजनों और ब्राह्मणों की हत्या से मुक्त होने के लिए शिव का ध्यान करें। परन्तु शिव युद्ध मे हुई कई घटनाओं से नाराज़ थे और पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे। शिव ने नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों की ओर प्रस्थान कर गए। पर पांडव पीछा करते रहे। एक दिन गुप्तकाशी में भीम ने नंदी को पिछले पैरों और पूँछ से पकड़ लिया। लेकिन नंदी तुरंत अंतरध्यान या गुप्त हो गए। इसी कारण इस जगह को गुप्तकाशी कहा जाता है।
 |
| बर्फ़ से ढका चौखम्बा पर्वत जो की गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर स्थित है |
 |
| नीचे घाटी में बहती मंदाकिनी |
 |
| चौखम्बा - इसके चार कोनों की ऊँचाई इस तरह से है: 7138, 7070, 6995 और 6854 मीटर |
 |
| गुप्तकाशी का एक मनोरम दृश्य |
 |
| गुप्तकाशी का एक और दृश्य - बढ़ती आबादी और बेतहाशा निर्माण |
 |
| घाटी के दूसरी ओर देखिए मूसलाधार बारिश के बाद हुए भूस्खलन के निशान |
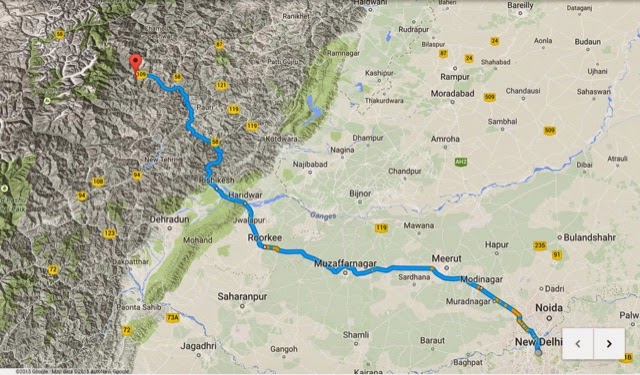 |
| नई दिल्ली से हरिद्वार होते हुए गुप्तकाशी का रास्ता 417 किमी |
पौड़ी गढ़वाल के कुछ चित्र
 |
| सुबह के उजाले में चमकता पौड़ी शहर का एक भाग |
 |
| ढलती शाम, गरमा-गरम पकोड़े और साथ में चाय का आनंद |
 |
| घुमावदार पर सुंदर रास्ते |
 |
| सीढ़ीनुमा खेत बारिश की इंतज़ार में |
http://yogi-saraswat.blogspot.com/2021/12/kakbhushundi-trek-uttarakhand-blog.html
Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog
काकभुशुण्डि ट्रैक ! दो रास्तों से किया जा सकता है -पहला रास्ता गोविंदघाट से भ्यूंडार होते हुए काकभुशुण्डि ताल तक जा सकते हैं और दूसरा रास्ता : विष्णुप्रयाग के पास स्थित पैंका गाँव से काकभुशुण्डि ताल तक जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पूरा ही सर्किट करना था इसलिए हमने भ्यूंडार के रास्ते से जाकर पैंका गाँव उतरने का निर्णय लिया। हम 4 सितम्बर की गोविंदघाट की ठंडी रात को रजाई में दुबके ....आने वाले कुछ दिनों के ख्वाब मन में बसाये सो गए ! हम यानि कुल 15 लोग !!
कल की बात कल करेंगे .....
Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 1 From Bhyundar to Kaagi
Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 2 From Kaagi to Raj Kharak
कागी बड़ी प्यारी जगह है। खूब बड़ा मैदान है जहाँ बड़ी-बड़ी घास उगी हुई थी और नदी है, नदी के किनारे खूब सारे पेड़ दिख रहे हैं। कल हम कुल 16 किलोमीटर चले होंगे जिसमे से 3 किलोमीटर गोविंदघाट से पुलना तक जीप से आये थे और बाकी दूरी ट्रैकिंग की थी।
अभी चार बजे हैं और हम जहाँ हैं वहां सफ़ेद रंग के फूलों का एक बहुत शानदार मैदान है। अनुपम छटा है इन फूलों की और सच कह रहा हूँ - मन प्रफुल्लित हो गया है इन्हें देखकर। बहुत प्यारा गार्डन है। नदी के पाट पर चलते हुए अब हमें एक जगह से ऊपर चढ़ना है। हमारे कुछ मित्र हमें दूर आगे की पहाड़ी पर बैठे हुए कुछ इशारा कर रहे हैं और जोर-जोर से चिल्ला के कुछ कहना चाहते हैं। बराबर में जो नदी बह रही है उसका किनारा अब खत्म हो गया है .... यानी किनारे-किनारे नहीं जा सकते ! और दूसरी तरफ इस नदी को पार कर के जाना मतलब नदी के वेग के साथ बह जाना होगा। मैं , डॉ अजय त्यागी , सुशील कुमार जी , कुलवंत सिंह जी और त्रिपाठी जी इधर हैं बाकी लोग आगे की पहाड़ी से उतर गए हैं।
Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 3 From Raj Kharak to Machhli Tal
अभी किचन टैण्ट तैयार हो रहा था , पंकज भाई इधर -उधर Explore कर रहे थे और मैं जूते निकाल रहा था। चप्पल पहने ही थे कि पंकज भाई थोड़ा ऊपर से आवाज लगाने लगे -योगी भाई ! आओ , आपको ब्रह्मकमल दिखाता हूँ! मैंने अभी तक किसी ट्रेक में ब्रह्मकमल नहीं देखे , या आप कह सकते हैं मुझे देखने को नहीं मिले ! मैं एक तरह से दौड़ लिया ब्रह्मकमल देखने को ! पहली बार देखने को और फिर तो उसे छूकर देखा , इधर से देखा , उधर से देखा , नीचे से देखा , ऊपर से देखा ! एंगल बदल -बदल के देखा !
Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 4 From Machhali Tal to Shila Samudra
अगर इस ट्रैक ब्लॉग को आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिये
Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 5 From Shila Samudra to Kagbhushundi to Bramghat
अगर इस ट्रैक ब्लॉग को आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिये !

 |
| कांकुल पास (Kankul Pass) |
Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 6 From Brahma ghat to Farswan Top
Kakbhushundi Trek Uttarakhand Blog : Day 7 From Farswan Top to Painka village
अगर इस ट्रैक ब्लॉग को आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिये !
रात जरुर बहुत मुश्किल थी लेकिन सुबह उतनी ही ठण्डी और सुहावनी थी मगर चाय के लिए न दूध बचा था न नीबू था इसलिए चाय बस ... चाय पत्ती और चीनी मिला हुआ गरम पानी ही था। हाँ ! मैग्गी जरूर मिल गई और गर्मागर्म मैग्गी खाकर शरीर में जान भी आ गई और .....गर्मी भी।
इस भयंकर ट्रैक का ये आखिरी दिन था हमारा। भयंकर दोनों तरह से -खूबसूरत भी भयंकर और रिस्क भी भयंकर ! फर्स्वाण टॉप पर थे हम 4166 मीटर की ऊंचाई पर टंगे थे और यहाँ से जोशीमठ के साथ -साथ औली और उर्गम घाटी का जबरदस्त नजारा दिखाई दे रहा था। जोशीमठ और औली एकदम किसी हरेभरे कटोरे जैसे दिखाई दे रहे थे फर्स्वाण टॉप से। खूब फोटोग्राफी की क्योंकि जो दृश्य इस वक्त दिखाई दे रहा था उसे जीवन भर देखने और उसे महसूस करने के लिए ये फोटो और वीडियो ही एकमात्र माध्यम रहेंगे हमारे लिए।
फर्स्वाण टॉप से उतरते हुए एकदम लगातार उतराई ही उतराई है और ऐसी उतराई है कि आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि अब गिरे कि तब गिरे ! लगभग 500 मीटर चलने के बाद slope थोड़ा कम होता है लेकिन उतराई बनी रहती है और जब आप करीब एक किलोमीटर उतरने के बाद एक ऐसे पत्थर के नीचे पहुँचते हैं जहाँ वो पहाड़ से आगे निकला हुआ है , वहां तक आप 500-600 मीटर की ऊंचाई कम कर चुके होते हैं। यानी इस एक किलोमीटर की दूरी में आप 4166 मीटर की ऊंचाई से 3500 -3600 मीटर की ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते ही आपको Treeline देखने को मिलने लगती है। यहाँ आपको पगडण्डी देखने को मिल जाती है क्यूंकि पैंका गाँव के लोग फर्स्वाण टॉप तक अपनी भेड़ बकरियों और गायों को चराने के लिए लाते रहते हैं।
ये जो पगडण्डी है उस पर चलते हुए पहाड़ के दूसरी तरफ देखने पर आपको लगातार हिमालय के सुन्दर दृश्य दिखाई देते रहते हैं। मौसम साफ़ हो तो आपको हिमालय की अद्भुत खूबसूरत और बर्फ से लकदक चोटियां एकदम साफ़ दिखाई देती हैं। हलकी उतराई -चढ़ाई करते हुए आप एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ बैठने के लिए भी खूब जगह है और जहाँ से पैंका गाँव पहली बार दिखाई देता है। यहाँ से आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। हालाँकि मोबाइल सिग्नल आपको फर्स्वाण टॉप पर भी मिल जाएंगे लेकिन वहां नेटवर्क ढूंढना पड़ता है जबकि यहाँ एकदम बढ़िया नेटवर्क मिल जाता है और लगभग हर कंपनी के नेटवर्क मिल जाते हैं।
इस जगह के बारे में गाइड ने एक डरावनी बात बताई थी ! सच है या नहीं , मैं नहीं जानता ! गाइड के शब्दों को ही ज्यों का त्यों लिख रहा हूँ यहाँ : एक गाँव (पैंका नहीं ) की लड़की को दूसरे गाँव के लड़के से प्यार हो गया था , ये करीब 20 वर्ष पुरानी बात है ! उस लड़की के परिवार वालों को ये बात नागवार गुजर रही थी और अंततः उस लड़की के घरवालों ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसे यहाँ ले आए। यहाँ उन लोगों ने उस लड़के की हत्या कर दी और कई महीनों के बाद पुलिस उस लड़के के खून से सने कपडे ढूंढ पाई और आख़िरकार उन लोगों को सजा मिली।
आज हमें फर्स्वाण टॉप से पैंका गाँव तक की करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और सिर्फ तय ही नहीं करनी थी बल्कि समय से तय करनी थी जिससे हम आगे जोशीमठ तक जा सकें और अगली सुबह अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकें। हम उसी खुली सी ऊँची जगह पर बहुत देर तक बैठे रहे जबकि कुछ मित्र आगे जा चुके थे। यहाँ से पैंका गाँव दिखाई तो दे रहा था लेकिन अभी बहुत दूर था। लगातार नीचे उतरते रहे और अब रास्ता खो गया। बहुत बड़ी बड़ी घास में से निकल रहे थे और इसका नुकसान ये हुआ कि घास में छुपे पत्थरों से टकरा -टकराकर मेरे सहित कई मित्र गिरे और पटियाला से आये सुशील भाई तो बहुत बुरी तरह गिरे। वो एक छोटे पत्थर से टकराकर बड़े पत्थर पर जाकर गिरे जिससे उनके सीने में बहुत चोट लग गई। डॉक्टर अजय त्यागी जी साथ थे मगर हमें डर सताता रहा की कहीं कोई पसली में चोट न लग गई हो ! फिर बहुत मुश्किल हो जाता ! तो .... ऐसे होते हैं ट्रैक और ऐसी होती है ट्रैकिंग !
बहुत देर तक सुशील भाई के सीने पर Iodex की मालिश करते रहे लेकिन दर्द तो था ही और वो दर्द उन्हें ही झेलना था , हम केवल उनकी मदद कर सकते थे उनका दर्द नहीं ले सकते थे। काश! हम सब उनका दर्द भी थोड़ा -थोड़ा बाँट सकते तो उनका दर्द कुछ कम होता।
हम पांच लोग साथ थे उस वक्त तक। मैं , डॉक्टर अजय त्यागी जी , सुशील भाई , कुलवंत जी और त्रिपाठी जी। डॉक्टर साब आगे चल रहे थे मगर घास के खत्म होते होते एकदम घना जंगल शुरू हो गया। डॉक्टर साब एक जगह मुझे अकेले बैठे मिले तो मैंने हँसते हुए पूछ लिया -डॉक्टर साब डर लग रहा है क्या ? अरे नहीं योगी जी ! थक सा गया हूँ ! उन्हें पता नहीं डर रहा था या नहीं लेकिन मुझे तो लग रहा था लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम सभी के फ़ोन चल रहे थे और गाइड / पॉर्टर हमें लगातार रास्ता बताये जा रहे थे। कहीं -कहीं पगडण्डी भी दिख जाती थी।
मैं अकेला ही चला जा रहा था , डॉक्टर त्यागी आगे निकलकर आँखों से ओझल हो चुके थे पीछे वाले तीनों लोग ज्यादा ही दूर रह गए थे। एक जगह कई सारे लंगूर दिखाई दे गए और वो सब के सब ऐसे रास्ता रोके बैठे थे कि -बेटा पहले यहाँ की चुंगी चुका के जा तब आगे जाने देंगे तुझे ! मैं 10 -15 मिनट तक हुर्र हुर्र कर के उन्हें भगाता रहा।
एक जगह दूर कहीं जली हुई सी लकड़ी पड़ी थी लेकिन एकदम से जब उस पर मेरी नजर पड़ी तो मैं पसीना -पसीना हो गया ! मुझे लगा ये कोई भालू है जो इस वक्त सोया पड़ा है। मैं एक पेड़ के पीछे जाकर उसका movement देखने लगा लेकिन जब कुछ देर तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो हिम्मत कर के पेड़ के पीछे से निकलकर आया और उसे गौर से देखा फिर अपनी ही मूर्खता पर हंसने लगा। ये शायद मूर्खता से ज्यादा तेज नजर थी क्यूंकि बहुत ही घना जंगल था / है वो।
सैकड़ों तरह के वृक्ष और खाली जगहों में खिलखिलाते फूल जैसे मेरे साथ इस ट्रैक के पूरा होने का जश्न मना रहे थे। मैं फूल नहीं पहचानता , शायद कोई वनस्पति विज्ञानं का जानकार ही इतने फूलों को पहचान सकेगा लेकिन एक कुकुरमुत्ता (Mushroom ) बड़ा सुन्दर लगा। उसकी फोटो लगाऊंगा।
एक जगह थोड़ा फंस गया मैं। आगे एक जगह वॉटरफॉल जैसा दिख रहा था लेकिन ये Natural waterfall नहीं था बल्कि पत्थरों को जोड़ जोड़कर पानी को रोका गया था जिससे ये जगह वॉटरफॉल जैसी बन गई थी लेकिन इसे पार करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। आसपास दूसरा रास्ता देखने को नजर दौड़ाई तो रास्ता तो नहीं दिखा , दूर झाड़ियों में से झांकता एक छोटा मगर खूबसूरत वॉटरफॉल जरूर नजर आया। आख़िरकार जूते उतारे और लोअर ऊपर चढ़ाया , लेके राम जी का नाम ... उस वॉटरफॉल को भी पार कर आया !
गाइड और पॉर्टर फ़ोन पर बार -बार ये पूछते रहे -सर ग्रीन हट तक पहुँच गए क्या ? ग्रीन हट तक पहुँच गए क्या ? ये ग्रीन हट असल में वन विभाग की बनाई हुई है जहाँ शायद आपकी परमिशन चेक होती होगी ! ये बिलकुल जंगल के बीच में है और यहाँ मुझे कुछ जली हुई लकड़ियां , पानी का एक घड़ा और थोड़े मिटटी के बर्तन दिखाई दिए। शायद रात में रुकने का कुछ इंतेज़ाम भी रहता हो लेकिन इसमें जो दरवाजा लगा था उसमे टाला बंद था तो अंदर नहीं देख पाया। अगर कैसे भी हमें यहाँ कोई परमिशन चेक करने वाला मिल जाता तो हम तो पकड़े जाते :) हमारे पास परमिशन थी ही नहीं और परमिशन न ले पाने का जिक्र मैं इस ट्रेक की पहली ही पोस्ट में कर चूका हूँ जब हम गोविंदघाट से निकले थे ! खैर अगर कोई मिलता भी तो देखा जाता !
शाम के लगभग चार बजने को थे जब पहली बार पैंका गाँव के बाहर स्थित गाँव के मंदिर के ऊपर लगा झंडा दिखा देने लगा था। मंदिर के पीछे की एक पहाड़ी पर बहुत ऊंचाई से गिरता झरना शानदार समापन कर रहा था हमारी इस जबरदस्त यात्रा का। मंदिर के आगे शीश झुका कर भगवान को सुरक्षित इस ट्रैक से वापस लाने के लिए उनका धन्यवाद किया। मंदिर बंद था लेकिन उसके आगे बैठकर अपने आप को खोजता रहा कुछ देर तक ! क्या मैं इस लायक था ? क्या एक भयंकर रूप से अस्थमा से पीड़ित रहा यहाँ इस ट्रैक पर आने लायक था ? लेकिन जिस के सर पर भगवान शिव का हाथ होता है वो सब कर लेता है !
जैसे ही पैंका गाँव में प्रवेश किया , हरजिंदर भाई और हनुमान गौतम जी चटाई पर थकान उतारते हुए दिखे एक घर के बाहर। वो दोनों बहुत पहले ही यहाँ आ चुके थे और स्नान करने के बाद लस्सी भी खेंच चुके थे , शायद खाना भी खा चुके थे :) मुझे और डॉक्टर साब को भी चाय मिल गई :) वैसे भी आज सुबह चाय नहीं मिल पाई थी ! बहुत देर तक उनके यहाँ बैठे रहे ! सुन्दर और संपन्न गाँव है पैंका। पॉर्टर ने सरकारी स्कूल में खाना बना रखा था और ये आज का , इस ट्रैक का हमारा अंतिम भोजन था।
गाँव से उतर के नीचे विष्णुप्रयाग तक पहुंचे जहाँ से कुछ लोगों को वापस गोविंदघाट जाना था और मुझे गाइड / पोर्टरों के साथ जोशीमठ पहुंचना था। रात करीब 8 -8 :30 बजे मैं , हनुमान जी , त्रिपाठी जी और सभी पोर्टरों के साथ भरी बारिश में जोशीमठ एक होटल में पहुंचा और सुबह 5 बजे की पहली बस लेकर हरिद्वार और फिर गाजियाबाद !!
जय हो कागभसुण्डी महाराज की !!
काशी विश्वनाथ मंदिर-उत्तरकाशी
इस यात्रा को आरंभ से पढ़ने के लिए क्लिक करें..
31 मई 2019
 |
| kashi viswanath temple, uttarkashi |
सुबह जल्दी ही उठ गए हैं और फ्रेश होने के पश्चात लगभग 6 बजे हम यहां से उत्तरकाशी की तरफ निकल चलें। कुछ किलोमीटर चलने पर भटवारी आया अभी दुकाने बंद थी इसलिए हम लगभग 30 km आगे चलकर उत्तरकाशी के बस स्टैंड पहुँचे। बस स्टैंड से काशी विश्वनाथ मंदिर मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही। हम जल्द ही मंदिर के सामने थे। मंदिर के बाहर बैठे एक प्रसाद बेचने वाले से गंगा घाट के लिए रास्ता पूछा तो उसने रास्ता समझाते हुए बताया कि केदार घाट पर चले जाना, वह बहुत बढ़िया बना है। हमने पहले ही तय कर लिया था कि पहले गंगा घाट पर स्नान करेंगे फिर बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन। मंदिर से लगभग 500 मीटर चलने पर ही केदार घाट पहुँच गए। यह घाट काफी साफ सुथरा दिख रहा था। सुबह-सुबह अभी कुछ औरतें व एक दो आदमी ही स्नान कर रहे थे। महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की के लिए एक दो चेंजिंग रूम भी बने हैं। यह घाट कुछ कुछ हरिद्वार की हर की पौड़ी की याद दिलाता है लेकिन यह उससे काफी छोटा है। हरिद्वार में गंगा स्नान करना भी मुझे बड़ा ही आनंद प्रदान करता है।
 |
| उत्तरकाशी शहर व केदार घाट |
काशी विश्वनाथ मंदिर
घाट से चलकर हम थोड़ी ही देर में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए। मंदिर के बाहर दीवारों पर स्थानीय लोगों ने या फिर प्रशासन की तरफ से पेंटिंग की हुई है जो बहुत अच्छी दिख रही थी। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमने प्रसाद भी लिया और बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश किया। मंदिर परिसर में कई मंदिर बने है। सबसे पहले हम विश्वनाथ मंदिर में गए। सबसे पहले नंदी जी के दर्शन होते है फिर हम मुख्य कक्ष में प्रवेश करते है यहाँ भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान है, यह शिवलिंग दक्षिण दिशा की तरफ झुका है जिसे साफ देखा जा सकता है। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि यह मंदिर भगवान परशुराम जी ने बनाया था लेकिन यह शिवलिंग स्वयंभू है अर्थात किसी ने इसे यहां पर स्थापित नही किया है यह स्वयं प्रकट हुआ है और इसका दक्षिण की तरफ झुका होना ही इसका सबूत है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इस शिवलिंग को स्थापित करता तो सीधा ही करता। उन्होंने बताया कि बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर की एक ही मान्यता है। उन्होंने यह भी बताया कि पुराणों में भी उत्तरकाशी का वर्णन है और पहले इस नगरी का नाम बाड़ाहाट था। भगवान शिव को जो हम सब के आराध्य हैं, हमने उनको नमस्कार किया साथ में जल व प्रसाद भी चढ़ाया और बाहर आ गए। बाहर अन्य काफी भक्त मौजूद थे फिर हम सब ने मिलकर भगवान शिव की आरती भी की। सचमुच यह पल मुझे हमेशा याद रहेंगे।
 |
| काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर |
 |
| मंदिर के बाहर दीवारों को कुछ ऐसे सजाया गया है |
 |
| मैं सचिन त्यागी अपने परिवार के साथ विश्वनाथ मंदिर पर |
 |
| मंदिर का पिछला हिस्सा |
 |
| अन्दर जो जल चढाया जाता है वो इधर से बाहर गिरता है |
शक्ति मंदिर
विश्वनाथ मंदिर के सामने ही एक मंदिर बना जिसे शक्ति मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण यहां पर स्थापित एक बहुत बड़ा त्रिशूल है। इस त्रिशूल की ऊंचाई लगभग 26 फ़ीट है और यह काफी चौड़ा भी है। इस विशाल त्रिशूल को देखते ही ऐसा लगता है जैसे यह साक्षात शिव जी का त्रिशूल हो, लेकिन वहां पर बैठे पंडित जी ने बताया कि यह बहुत प्राचीन है, माना जाता है कि यह 1500 वर्ष से भी पुराना है। उन्होंने बताया कि यह बहुत भारी है जिसे एक व्यक्ति का उठा पाना भी सम्भव नही है जबकि यह एक उंगली मात्र लगने से ही कंपन(हल्का सा हिलने) करने लगता है। इस त्रिशूल को माता पार्वती (मां दुर्गा) के त्रिशूल रूप में पूजा जाता है। मंदिर परिसर में और अन्य मंदिर भी बने हैं इनको भी देखा गया और हम मंदिर परिसर से बाहर आ गए।
 |
| शक्ति मंदिर |
 |
| शक्ति मंदिर के अन्दर का दर्शय |
 |
| वह प्राचीन व विशाल त्रिशूल |
 |
| शक्ति मंदिर व पीछे वाला विश्वनाथ मंदिर ,उत्तरकाशी |
उत्तरकाशी में देखने को और बहुत से मंदिर है। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) भी जहां पर पर्वतारोहण का कोर्स किया जाता है। व कई प्रमुख ट्रेक भी आस पास है जैसे दायरा बुग्याल, डोडिताल ट्रेक, नचिकेता ताल ट्रेक आदि। उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक जिला है जिसमे यमनोत्री गंगोत्री धाम भी स्तिथ है।
अब हम वापिस चलने को तैयार थे। समय देखा तो सुबह के 9:30 हो रहे थे। आज मैंने ऋषिकेश रुकना तय किया जो उत्तरकाशी से लगभग 175 km की दूरी पर है और लगभग सात घंटे का सफर है। मैंने गूगल से चम्बा तक का रास्ता जाना तो गूगल मैप ने मुझे दो रास्ते सुझाये। पहला उत्तरकाशी से धरासू बैंड होते हुए चिन्यालीसौड़ और फिर चम्बा जो लगभग 106 किलोमीटर का था और दूसरा उत्तरकाशी से चौरंगिखाल होते है नई टिहरी। यह रास्ता थोड़ा बड़ा था यह लगभग 144 km का था। चौरंगिखाल से तीन किलोमीटर का एक छोटा ट्रेक करके नचिकेता ताल तक पहुँचा जाता है। फिलहाल मुझे यह ट्रेक तो करना नही था इसलिए चिन्यालीसौड़ वाला रास्ते से जाना तय किया। लगभग 10 बजे हम उत्तरकाशी शहर से बाहर आ गए। एक दुकान देखकर चाय और ब्रेड का नाश्ता भी कर लिया। धरासू बैंड पहुँचे यही से एक रास्ता यमनोत्री के लिए अलग हो जाता है। हमे चिन्यालीसौड़ की तरफ जाना था इसलिए हम धरासू बैंड से बाँये तरफ हो गए। रास्ते मे हमे कई जगह जंगल जलते हुए मिले एक जगह तो आग रास्ते के इतने करीब भी आ गया थी कि हमारे चहरों ने भी उसकी तपन को महसूस किया। आग की वजह से हर तरफ धुंआ ही धुंआ फैला हुआ था। पहाड़ो पर गाड़ी चलाने का जो एक आनंद होता है वह आज मुझे बिल्कुल भी नही आ रहा था। रास्ते मे एक होटल पर रुके, खाने का मन नही हुआ इसलिए निम्बू पानी और ताज़े खीरे खाये गए। यहाँ पर एक व्यक्ति से पूछा कि हर जगह इतनी आग क्यो लगी है और कोई इसको बुझाता भी क्यो नही तो उस व्यक्ति ने बताया कि कुछ आग तो गांव वाले लगा देते है जिससे बारिश के बाद नई घास बढ़िया आती है जिससे पशुओं के लिए चारे की कमी नही होती है। क्योंकि चीड़ की पत्तियों घास को उगने ही नही देती है। और कुछ जगह आग चीड़ के पिरुल की वजह से भी लग जाती है। पिरुल जल्दी तप जाता है और आग पकड़ लेता है जिसकी वजह से भी आग लग जाती है। अब हम आगे चल पड़े और लगभग दोपहर के तीन बजे चम्बा पहुँच गए। चम्बा से नई टिहरी, टिहरी झील व कानाताल जगह बेहद नजदीक है। चम्बा पहुँचे ही थे कि मेरा बेटा देवांग कुछ अस्वस्थ नज़र आया इसलिए आज की रात हम ने चम्बा में ही रुकने का निर्णय किया।
 |
| एक जगह दूर आग जलती दिख रही थी |
 |
| हमने देखा की अब वह आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी |
 |
| आग सड़क तक आ गयी थी और इसकी तपन को हम गाड़ी में ही महसूस कर रहे थे |
 |
| जंगल के जंगल जल रहे थे जिसकी वजह से हर जगह धुआं फैला हुआ था |
 |
| रात को चंबा में ही रुके |
बद्रीनाथ यात्रा : गाजियाबाद से ऋषिकेश
दिल्ली- सहारनपुर पैसेंजर का गाज़ियाबाद स्टेशन पर निर्धारित समय 2 बजकर 15 मिनट का है लेकिन कभी भी ढाई बजे से पहले अपना मुंह नही दिखाती। उस दिन भी अपने रुतबे में ही रही और 2 बजकर 35 मिनट पर पहुंची। जगह मिलने का कोई मतलब ही नही था और जगह चाहिए भी नही थी क्योंकि फिर फोटो नही ले पाता। मेरठ सिटी स्टेशन पर जाकर जगह मिल गयी और अपनी पसंद वाली खिड़की वाली सीट कब्ज़ा ली। अब तक गाज़ियाबाद , नया गाज़ियाबाद , गुलधर , दुहाई हॉल्ट , मुरादनगर , मोदी नगर , मोहिउद्दीनपुर, परतापुर स्टेशन निकल चुके थे। अगला स्टेशन आया मेरठ सिटी और फिर मेरठ छावनी , ट्रेन आधी से ज्यादा खाली हो गयी। यहां एक कप चाय भी पी। अँधेरा शुरू हो गया था और छोटे छोटे स्टेशन एक एक कर निकल रहे थे -पाबली ख़ास , दौराला , सकौती टांडा , खतौली , मंसूरपुर। मंसूरपुर में चीनी मिल है और मोदी नगर और मोहिउद्दीनपुर में भी चीनी मिल है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत ही उपजाऊ और धनी इलाका है लेकिन कुछ वर्षों से इधर आपसी वैमनस्य बहुत बढ़ गया है। ये पूरा इलाका गन्ने की खेती के लिए बहुत प्रसिद्द है इसीलिए यहां बहुत सी चीनी मिल हैं। निजी क्षेत्र की भी और सरकारी क्षेत्र की भी। मंसूरपुर से आगे का स्टेशन जरौदा नारा आता है और फिर मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पहुँचते पहुँचते ट्रेन पूरा एक घण्टा देरी से चल रही थी लेकिन हमें क्या लेना ? हमें तो बस कैसे भी अभी सहारनपुर तक पहुंचना है और फिर ऋषिकेश। बामनहेड़ी , रोहना कलां , देवबंद , तल्हेरी , नांगल और टपरी जंक्शन होते हुए , रोते हुए आखिर लगभग रात को 9 बजे सहारनपुर पहुँच पाई ये दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर। लेकिन जैसे ही प्लेटफार्म पर उतरा और बाहर निकलने लगा तो देखा, पता नही कहाँ से भयंकर रैला चला आ रहा है लोगों का। किसी से पूछा आज कोई रैली थी क्या इधर ? नही भाई ! फिर ये भीड़ ? कल मावस ( अमावस ) है सब नहान के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। ओह , इसका मतलब भीड़ से सामना होने वाला है हरिद्वार तक। सहारनपुर से हरिद्वार 80 किलोमीटर है। और सहारनपुर से ऋषिकेश के लिए पैसेंजर गाडी है रात को ग्यारह बजे। वो ही जो दिल्ली से आती है और गाजियाबाद पर शाम को छह बजे आती है। मैंने सोचा अगर ढाई बजे चलकर पैसेंजर ट्रेन रात को 9 बजे पहुँच रही है यानि साढ़े छह घंटे लगा रही है तब ये दूसरी वाली क्या उड़ के आ जाएगी ? खैर जब आएगी तब आ जाएगी अभी तो घर से लाया हुआ खाना खाते हैं और एक कप चाय पीते हैं। बैठने की थोड़ी जगह मिली तो खाना खोल लिया।
वापस स्टेशन लौटा तो पता चला दिल्ली से चलकर हरिद्वार के रस्ते ऋषिकेश को जाने वाली सवारी गाडी अपने निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से चल रही है। एक घंटा देरी से मतलब ये हुआ कि इसका निर्धारित समय है रात को 10 बजकर 50 मिनट और एक घंटा और मतलब 11 बजकर 50 मिनट। कोई मतलब ही नहीं कि साढ़े बारह से पहले पहुँच जाए। थोड़ा सा लेट मार लेता हूँ। थोड़ी देर बाद एक और घोषणा हुई , फलां फलां यानि यही वाली ट्रेन प्लेटफार्म संख्या 3 पर पहुँच रही है। प्लेटफार्म की घडी की तरफ देखा तो अभी तो 11 बजकर 55 मिनट हुए थे और गाडी समय पर आ पहुंची भले निर्धारित समय पर नही हो। अब यही ट्रेन सहारनपुर से ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए जायेगी। भीड़ का रेला अपने पूरे जोश में था और इतना जोश में था कि लोगों को उतरने तक का मौका नही देना चाहता था। मैंने खिड़की से अपना छोटा सा बैग एक सिंगल सीट पर डाल दिया लेकिन इसका भी कोई ज्यादा फायदा नही हुआ और हरिद्वार तक एक आदमी के बैठने की सीट पर तीन आदमी बैठकर गए। सहारनपुर से निकलने के बाद बलिआखेड़ी , चुड़ियाला , इकबालपुर , रूड़की , ढंढेरा , लण्ढौरा , दौसनी और लस्कर जंक्शन निकल गए। इसमें रूड़की वो जगह है जहां आई आई टी है और जहाँ का सिविल इंजीनियरिंग का स्कूल कभी एशिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था , अब क्या स्थिति है मुझे नही मालुम। लस्कर के बाद ऐथल , पथरी , इक्कर, ज्वालापुर और फिर हरिद्वार। हरिद्वार पर गाडी बिलकुल खाली हो गयी। और इतनी खाली हो गयी कि ऋषिकेश जाने वाले कुल तीन लोग थे डिब्बे में। उनमें से भी एक रायवाला उतर गया। आखिर मोतीचूर , रायवाला , वीरभद्र को पार करते हुए साढ़े पांच बजे ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिससे मौसम सुहावना हो रहा था और ऐसे में जब आप आदमियों के समुद्र में से निकलकर आ रहे हों तब ऐसा मौसमऔर भी खुशगवार लगता है।
आज इतना ही , अगली पोस्ट में ऋषिकेश के कुछ चुनिंदा दर्शनीय स्थल देखेंगे !!
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| धन्यवाद सहित ये फोटो ब्लॉगर मित्र AJ जी की है !! |
 |
| धन्यवाद सहित ये फोटो जाने माने ब्लॉगर मित्र नीरज जाट की खींची हुई है !! |
 |
|
धन्यवाद सहित ये फोटो ब्लॉगर मित्र पवन गुप्ता जी की है !!
|
 |
 | ||||||
नीलकण्ठ महादेव मंदिर :ऋषिकेश
वहां गाड़ियों की इतनी भीड़ हो जाती है कि अगर आप थोड़ी देर से जा रहे हैं यानि 10 बजे के बाद तो आपको आपकी गाडी बहुत दूर पीछे ही रोक देनी पड़ेगी। पैदल चलते चलते पसीने आ गए। हाथ -मुंह धोकर मंदिर में प्रवेश कर रहा था कि उधर से एक जाना पहिचाना चेहरा दिखाई पड़ा ! ये वरिष्ठ पत्रकार एन.के सिंह जी थे ! आप जानते हैं उन्हें ? वो मुझे नही जानते लेकिन मैंने उन्हें कई बार टेलीविज़न पर होने वाली बहस में देखा है इसलिए पहिचानता हूँ ! मैंने तुरंत पूछा -आप एन.के सिंह जी ? थोड़ी सी बात चीत हुई ! उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी साथ में थे ! सेल्फ़ी लेना भूल गया !!
अब ज़रा नीलकण्ठ महादेव के बारे में बात कर लेते हैं ! लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया गया था। विषपान के बाद विष के प्रभाव के से उनका गला नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया था। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्थान करते हैं।
तो आइये फोटो देखते हैं !
 |
| त्रिवेणी घाट ऋषिकेश |
 |
| त्रिवेणी घाट ऋषिकेश |
 |
| जय गंगा मैया |
 |
| जय गंगा मैया |
 |
| राम झूला |
 |
| राम झूला |
 |
| जय नीलकण्ठ महादेव |
 |
| जय नीलकण्ठ महादेव |
 |
 |
 |
| ये किसानों की आजीविका |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ऋषिकेश से जोशीमठ : बद्रीनाथ यात्रा
रुद्रप्रयाग पञ्च प्रयागों में से एक है ! प्रयाग गढ़वाल क्षेत्र में स्थित नदियों के मिलन को को कहते हैं ! ये पांच प्रयाग हैं : देवप्रयाग , रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग , कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग !
देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है जो आगे गंगा बन जाता है ! रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मन्दाकिनी का मिलन होता है ! रुद्रप्रयाग शिव को समर्पित जगह है ! ऐसा माना जाता है कि रुद्रप्रयाग में नारद मुनि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और भगवान शिव यहां रूद्र अवतार में प्रकट हुए ! नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम स्थल है। अलकनंदा बद्रीनाथ से आगे सतोपंथ से आती है और नंदाकिनी नंदा देवी चोटी से निकलती है। नंदप्रयाग में ऐसा माना जाता है कि यहां राजा नन्द ने पत्थरों पर यज्ञ किया था और उन्हीं पत्थरों को यहां के मंदिर में प्रयोग किया गया है ! समुद्र तल से लगभग 870 मीटर की ऊंचाई पर बसा नंदप्रयाग कर्णप्रयग से 20 किलोमीटर की दूरी पर है !
कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदिया अपना संगम बनाती हैं ! और इस जगह को कर्णप्रयाग का नाम महाभारत के कर्ण की वजह से मिला जिन्होंने यहां भगवान सूर्य की उपासना की थी और सुरक्षा कवच प्राप्त किया था । और सबसे आखिर में बद्रीनाथ के पास विष्णुप्रयाग है जो अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम स्थल है। यहां नारद मुनि ने भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या की थी !
रुद्रप्रयाग में सोने से पहले वहां के एक आदमी को बोल दिया था कि भाई मुझे सात बजे जगा देना लेकिन हुआ इसका उल्टा - कभी भी सात बजे से पहले न जगने वाला प्राणी आज छह बजे ही जाग गया था और जब वो आदमी जगाने आया तब तक तो नहा भी चुका था ! आठ बजे नाश्ता लेकर कर्णप्रयाग की बस ले ली और वहां उमा देवी मंदिर के दर्शन करने के पश्चात पिंडर और अलकनंदा के संगम के दर्शन किये। यहां पिंडर बिलकुल साफ़ सुथरी है और उसका पानी दूर से देखने पर हरीतिमा लिए हुए लगता है जबकि अलकनंदा बहुत मैली , कीचड से भरी हुई सी !
कर्णप्रयाग से बहुत देर हो गयी। जोशीमठ तक जाने के लिए कुछ भी नही मिल रहा था ! जो बस या गाड़ियां ऋषिकेश -हरिद्वार की तरफ से आ रही थीं वो सब पहले से बुक थीं और कोई रोक ही नही रहा था ! आखिर चमोली तक की बस में ही बैठना पड़ा ! और फिर चमोली से एक सूमो में जोशीमठ पहुँच गए ! अब जोशीमठ पहुँच गए तो उसने इधर ही उतार दिया ! मुझे आगे आज तपोवन जाना था ! किसी से पूछा तपोवन के लिए गाडी कहाँ से मिलेगी ? करीब एक किलोमीटर आगे जाना पड़ा ! उसी स्टैंड से बद्रीनाथ , गोविंदघाट ( हेमकुंड साहिब ) और तपोवन के लिए सूमो गाड़ियां मिलती हैं ! तो अब तपोवन चलेंगे ! लेकिन तपोवन की बात आपको अगली पोस्ट में सुनाएंगे ! तब तक इंतज़ार करिये ! इंतज़ार का फल मीठा होता है !
 |
| देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम |
 |
| नन्द प्रयाग से दूरियां |
 |
| नन्द प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम |
 |
 |
 |
 |
| रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मन्दाकिनी का मिलन होता है |
 |
| रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मन्दाकिनी का मिलन होता है |
 |
| रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मन्दाकिनी का मिलन होता है |
 |
 |
| उमा मंदिर कर्णप्रयाग |
 |
| उमा मंदिर कर्णप्रयाग |
 |
| उमा मंदिर कर्णप्रयाग |
 |
| उमा मंदिर कर्णप्रयाग |
 |
 |
| कर्णप्रयाग से दूरियां बताता साइन बोर्ड |
 |
| कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदिया अपना संगम बनाती हैं |
 |
| कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदिया अपना संगम बनाती हैं |
 |
| कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदिया अपना संगम बनाती हैं |
 | |
| कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदिया अपना संगम बनाती हैं |
 |
| चमोली से दूरियां |
 |
| जोशीमठ से दूरियां |
 |
| और ये विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम |
जोशीमठ से तपोवन
तपोवन जोशीमठ से कोई 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा लेकिन कुल मिलाकर एक घण्टा लग जाता है । सवारियां चढाने उतारने और कभी कभी दूर से आती दिखती सवारी का इंतज़ार करने में बहुत समय खा जाते हैं ये गाडी वाले । लेकिन यहाँ ये भी बात ध्यान देने की है कि ये सिर्फ हमारे लिए ही नही हैं । जिस स्थान पर तपोवन में जीप ने उतारा वहां पहले से ही तीन जीप और खड़ी थीं । उनसे जाने का समय पता कर लिया और ये भी कि मैं वापस जरूर आऊंगा और एक दूसरे का नंबर भी आदान प्रदान कर लिया । स्टैंड से 15-20 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है तपोवन का मन्दिर । छोटा सा क़स्बा है तपोवन । अपनी गाडी से जा रहे हैं तो पैदल चलने की नौबत नही आती । मंदिर तक गाडी पहुँच जाती है लेकिन जीप वाले आगे नही जाते । रास्ते में एक दुकान दिखी "चख लो जी" । यहां और सब खाने की चीजों के अलावा दो अलग तरह के नाम दिखे । अरज्या और थोकपा । कैसे होते हैं ? मैंने कभी खाये नही । आज खा के देखूंगा ।खाने की तो बात अलग मैंने इनके नाम भी कभी नही सुने मैंने । आपने सुने हैं क्या ? पहले मंदिर के दर्शन कर लें फिर खाएंगे ये दोनों चीज । देखते हैं कैसे होते हैं । पहले भगवान के दर्शन कर लिए जाएँ । चलता रहा । शिव भगवान् के दूत सांप ने स्वागत किया । एकांत लगता है । वीरान सा मंदिर है । बस दो तीन लोग नहाने वाले कुण्ड में खड़े कपडे धो रहे थे । मैंने इधर उधर पूरा घूम लिया । न कोई पुजारी न कोई पंडित । बैग वहीँ मंदिर के बरामदे में छोड़कर फ़ोटो लेने के लिए चला गया और जब लौटकर आया तो वहां एक पुजारी एक परिवार को इस मंदिर की कहानी सुना रहा था । वो शायद अभी मंदिर में अंदर दर्शन करके नही आये । किसी के माथे पर तिलक नही था । मैं सही सोच रहा था । मैं उनके पीछे ही हो लिया । परिवार में एक युवा जोड़ा और उनकी दो छोटी छोटी बच्चियां । बहुत खूबसूरत । महिला गज़ब की सुन्दर थी । अगर कुछ और न सोचें तो कहूँगा कि मैंने जिंदगी में फिल्मों के अलावा इतना खूबसूरत चेहरा कभी नही देखा । खूबसूरत लेकिन साथ में बहुत संस्कारित भी । उन्होंने मंदिर में भगवान् को 100 रूपये का चढ़ावा चढ़ाया । शर्मवश मुझे भी 10 रूपये चढाने पड़े । प्रसाद मिला उन्हें भी और मुझे भी । प्रसाद ग्रहण कर उस खूबसूरत चेहरे ने पुजारी के पाँव छुए और उनकी बच्चियों ने भी । इसीलिए मैंने लिखा संस्कारित । पुजारी ने मुझे एक आँख भी नही देखा । जरूरत भी नही थी । खूबसूरत चेहरा जब सामने हो तो मुझे कौन देखता ।
अब बैग उठाकर चलने का समय था । लौटते हुए "चख लो जी" में अरज्या और थोकपा चख लिया जाए । अभी आखिरी गाडी निकलने में समय है । उस दुकान में पहुंचा तो इधर उधर दीवारों पर लगे चित्र देखकर अंदेशा हुआ कि ये डिश कहीं माषाहार में तो नही ? पूछा तो समझ गया ! ये माषाहारी डिश है ! बच गया ! मैं माषाहार नही करता इसलिए नहीं कि ब्राह्मण हूँ बल्कि इसलिए कि मुझे पसंद नही है !
तपोवन कई मामलों में पहिचान पाये हुए है । यहां आपको गरम पानी का स्रोत मिलेगा । और ऐसा माना जाता है कि इस गरम पानी से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं । लेकिन ट्रैकर्स के लिए ये कुवारी पास जाने और चित्रकांठा जाने के लिए बेस के रूप में काम करता है ।
जोशीमठ से बद्रीनाथ जी
लौटने पर तपोवन स्टैंड पर दो सूमो गाड़ियां खड़ी थीं । पहले वाली से पूछा कितनी देर में चलोगे ?10 मिनट में ही चल पड़ेंगे । मैंने बैग पिछली सीट पर फैंक दिया । बीच की सीट पर चार लोग पहले से ही जमे पड़े थे । भूख और गर्मी दोनों परेशान कर रहे थे । सामने की ही दुकान से कोल्ड ड्रिंक और दो समोसे खेंच लिए । 10 मिनट तो हो गए । दुकान वाले ने बता दिया ये अभी कम से कम 15 मिनट नही जाने वाला । आराम से खा लो । मेरे बाद भी कोई सवारी नही आई तो आखिर उसे चलना ही पड़ा । लगभग पौने चार बज रहे होंगे । साढ़े चार बजे वापस जोशीमठ के उसी स्टैंड पर थे जहाँ से अभी दो घंटे पहले तपोवन गए थे लेकिन अब ये हमारे लिए तपोवन स्टैंड न होकर बद्रीनाथ स्टैंड हो गया था । ऊपर चढ़कर तपोवन स्टैंड है और सीधे रास्ते पर नीचे की तरफ बद्रीनाथ स्टैंड । सूमो और कमांडर गाड़ियों की लाइन लगी रहती है । लाइन अब भी थी लेकिन दो ही गाडी वाले सवारी ढूंढ रहे थे । एक बद्रीनाथ के लिए और दूसरा पांडुकेश्वर और गोविंदघाट तक के लिए । पांडुकेश्वर और गोविंदघाट बद्रीनाथ से लगभग 20 किलोमीटर पहले रह जाते हैं । एक गाडी वाला कम से कम 10 सवारी लेकर जाता है । बद्रीनाथ वाली गाडी में छह सवारी हम से पहले थी और मेरे जाने से हो गयी सात । थोड़ी देर बाद कोई एक भाईसाब और आ गए । सवारी हो गयी आठ । अब भी दो सवारी चाहिए थीं उस गाडी वाले को । इतनी देर में एक कप चाय पी ली जाए । सामने ही दुकान है । वो भाईसाब भी उधर ही आ गए चाय पीने । परिचय हुआ बात चली । वो भी गाजियाबाद से ही आये थे । दैनिक जागरण के संपादक महोदय प्रदीप वशिष्ठ जी । नॉएडा कार्यालय में कार्यरत हैं । इस यात्रा में पत्रकारों से ही मिलने का योग है क्या ? पहले नीलकंठ महादेव में एन.के. सिंह जी से मुलाकात हुई थी और आज प्रदीप जी से । अच्छा है । इतनी देर में दो पति पत्नी और आ गए । चंडीगढ़ से थे । मामला फंस गया । गाडी वाला किराया मांग रहा था 100 रूपये प्रति सवारी और वो 60 से ज्यादा देने को तैयार नही थे । महिला को कोई फर्क नही पड़ रहा था लेकिन पुरुष 60 से आगे ही नही बढ़ रहा था । होता ज्यादातर इसका उल्टा है । महिला मोलभाव करती हैं और पुरुष जल्दी मान जाते हैं । खैर जब उन्हें पता चल गया कि अब बस भी नही मिलेगी यहाँ से और कोई गाडी वाला भी नही जाएगा इसके बाद । वो तैयार हो गए । गाडी चल पड़ी । और साढ़े सात बजे बद्रीनाथ के स्टैंड में गाडी प्रवेश कर गई । उससे पहले एक एंट्री पॉइंट पर चारधाम यात्रा के परमिशन लैटर लेने होते हैं ।मेरे पास पहले से ही था । ऋषिकेश से बनवा लिया था । बस स्टैंड पर ही इसके लिए काउंटर बनाये हुए हैं । ऑनलाइन भी बनवाया जा सकता है ।
बद्रीनाथ के बस स्टैंड पर ही आपको कई सारे लड़के मिल जायंगे , होटल चाहिए ? कमरा चाहिए ? गर्म पानी मिलेगा !! तवे की रोटी मिलेगी। …… !! ऐसे ऐसे ! मेरा पहले से तय था कि वहीं रुकना है जहां 2007 में रुका था ! इसलिए कोई झंझट नही , सीधा वहीँ चलते हैं !! आज थकान बहुत हो गयी , नहायेंगे , खाएंगे और बस सोयेंगे !! लेकिन प्रदीप वशिष्ठ जी को भूल गए ? हालाँकि वो जोशीमठ से ही कहते आ रहे थे , मेरी वहां जान पहिचान है ! देहरादून से फ़ोन करा दूंगा ! अपने आप ही कोई लेने आ जाएगा और बढ़िया होटल में रुकेंगे ! जाने कहाँ कहाँ फ़ोन मिला दिए उन्होंने !! कोई नही आया ! आखिर उन्हें मेरे साथ आना पड़ा ! फिर भी उन्हें चैन नही मिला। बोले - कितने रूपये का पड़ेगा ये कमरा !! मैंने बताया अभी मुफ्त का ! ये अभी आपसे कोई पैसा नही लेंगे ! ये लोग नवम्बर में गाजियाबाद आएंगे तब आपकी जो श्रद्धा हो उस हिसाब से दे देना ! नही तो मत देना ! वो तैयार हो गए रुकने के लिए ! मेरा मन नही था आज दर्शन करने का लेकिन उन्होंने जिद की तो नहा धोकर भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन को निकल लिए ! लौटकर फिर उनकी वो ही रामलीला शुरू हो गयी ! और आखिर में साढ़े दस बजे वो किसी दूसरे होटल में चले गए ! अब सोऊंगा !! दो दो रजाई लेकर ! ठण्ड है अच्छी खासी !
 |
 |
 |
 |
| ऐसे भी रास्ते हैं |
 |
| प्रथम दर्शन |
 |
 |
 |
| जे फोटो इंटरनेट ते लई है मैंने |
 |
| ये पांडुकेश्वर मंदिर |
 |
| ये पांडुकेश्वर मंदिर |
 |
| ये पांडुकेश्वर मंदिर |
 |
 |
| जय श्री बद्रीनाथ जी |
 |
| जय श्री बद्रीनाथ जी |
 |
| ये वहां रखी हुण्डी |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ये प्रदीप वशिष्ठ जी ! |
 |
| ये प्रदीप वशिष्ठ जी ! बैग वाली महिला मत पूछिए कौन हैं ? |
 |
| ये मैं |
 |
 |
 |
 |
| ये छोटा सा कमरा |
बद्रीनाथ जी मंदिर
 |
| बद्रीनाथ जी की शानदार सुबह |
 |
| जय बद्री विशाल !! |
 |
| अलकनंदा अठखेलियां कर रही है !! |
 |
| जय बद्री विशाल !! एक सेल्फ़ी |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| क्या शानदार और सुन्दर बनावट है |
 |
| क्या शानदार और सुन्दर बनावट है |
 |
| इस कुण्ड में भगवान के दर्शन करने से पहले एक "डिप " लेने की परंपरा है |
 |
| बद्रीनाथ में मुण्डन और पूर्वजों का तर्पण भी होता है |
 |
 |
 |
| बद्रीनाथ में मुण्डन और पूर्वजों का तर्पण भी होता है |
 |
 |
| नहा लिया |
 |
 |
| ये वो गर्म कुण्ड |
 |
 |
 |
 |
 |
| नारद कुण्ड ! ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्मवलम्बियों ने भगवान बद्रीनाथ जी
की मूर्ति इस कुण्ड दी थी जिसे आदि शंकराचार्य जी ने वापस निकला और पुनः
स्थापित किया |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ये अलकनंदा नदी के बीच में स्थित चट्टान ! इसे पीछे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कुत्ते का मुंह हो |
 |
 | ||||||||
माणा : भारत का आखिरी गांव
 |
| बद्रीविशाल की जय ! |
 |
 |
| नर नारायण पर्वतों का शानदार दृश्य |
 |
 |
| नर नारायण पर्वतों का शानदार दृश्य |
 |
| एक पहाड़ पर indian army ऐसे लिखा है |
 |
| माणा पहुँचने वाले हैं |
 |
| गाज़ियाबाद यहां से 527 किलोमीटर है !! |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ये माणा की चौपाल है जहां एक दिन पहले ही कोई राज्यस्तरीय कार्यक्रम हुआ था |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| मुझे भी अपने जूते उतारने पड़े |
 |
 |
| ये माणा में अंदर |
 |
| गणेश गुफा!! वास्तव में गुफा तो नही लगी |
 |
 |
| व्यास गुफा |
 |
| व्यास गुफा |
 |
| व्यास गुफा |
 |
| व्यास गुफा |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| इसने कहा कि मेरा भी एक फोटो खींच दो |
 |
| ये मैं |
 |
| मौसम एकदम से ख़राब होने लगा |
 |
 |
 |
 |
| कुछ मस्ती हो जाए |
 |
| ये बाबा बिल्कुल सरस्वती के किनारे अपनी धूनी जमाये बैठे हैं |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| सरस्वती की तेज धारा |
 |
 |
 |
 |
| ये भीम शिला |
 |
 |
 |
| सरस्वती की तेज धारा |
 |
 |
 |
 |
 |
सरस्वती यहां अलकनंदा में विलीन हो जाती है !! |
 |
| अब किसको आखिरी दुकान कहियेगा ? |
माणा से वसुधारा फॉल की ओर
हालाँकि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी इतना आभास हो रहा था कि धूप की किरणें बर्फ से टकराकर रिफ्लेक्ट हो रही हैं ! इसी के कारण स्किन जलने लगी थी ! हालाँकि आँखों पर चश्मा चढ़ा रखा था और मुंह पर गमछा लपेटा हुआ था लेकिन फिर भी नाक खुली रह गयी और घर लौटकर मालुम हुआ कि नाक पर एक पपड़ी जम गयी है ! ओह ! चार पांच दिन लग गए सही होने में ! बड़ा अजीब सा मौसम होता है ! सुबह सर्दी थी और जैकेट पहननी पड़ी थी और अब इतनी गर्मी है कि जैकेट उतार के कंधे पर लटकानी पड़ी और कुछ कदम चलते ही पानी की जरुरत पड़ने लगी ! मेरे पास बस पानी की एक ही बोतल थी और उसमें से भी एक बार दो लोगों को जो अलग से जा रहे थे उन्हें पिला चुका था ! पानी की कमी होने लगी थी ! किसी से पूछा पानी कहाँ मिल जाएगा ? बोले वसुधारा फॉल पर एक बाबा का आश्रम है वहीँ पानी मिल पायेगा ! एक एक घूंट पानी बचाने लगे ! सब के पास लगभग खतम होने को था !
 |
| बर्फ तो है लेकिन मैली हो चुकी है |
 |
| भाईसाब योगी सारस्वत |
 |
 |
 |
 |
 |
| ये SLET के छात्रों की मंडली |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| इस बर्फ से धीरे धीरे कर के नीचे पानी बह रहा था उसी से अपनी बोतल भर ली |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ये दूसरी तरफ की पहाड़ियां जिन पर बर्फ का नामोनिशान भी नहीं ! कोई प्लीज बताइये ऐसे क्यों होता है की पहाड़ पर एक तरफ तो इतनी बर्फ और दूसरी तरफ बिलकुल भी नही ? |
 |
 |
 |
 | |
 |
 |
| ये ग्लेशियर जिसे पास करने में बड़ी दिक्कत हुई |
 |
| सरदार जी सबसे बाद में आये |
 |
 |
| ऐसा रास्ता है ! पथरीला ! कुछ दूर चलने के बाद ये भी गायब हो जाता है |
 |
 |
 |
| इसमें एक गुफा सी थी , इस पत्थर के नीचे ! थोड़ी देर वहां बैठे रहे |
 |
 |
| ये आईटीबीपी की कोई बटालियन है ! नीचे वापस आते हुए दिखे |
 |
 |
 |
 |
 |
वसुधारा फॉल :माणा
वहीँ एक और बाबा मिले जिन्हे मैंने चलते फिरते बाबा लिखा है ! ये असल में तीन चार दिन से यहां थे और दो दिन से भूखे थे ! किसी ने इन्हे चार पराठे खिला दिए और इनका मन तृप्त हो गया ! फोटो में दिखेंगे आपको ! बाबा से फुर्सत पाकर अब इधर उधर के फोटो लेने शुरू किये और धीरे धीरे उन लोगों के पास पहुँच गया जो इधर बहुत देर से आराम फरमा रहे थे और अपने कैमरे को ट्राइपॉड पर रखकर बस बैठे बैठे ही फोटो खींचे जा रहे थे ! ओह , ग्लव्स भी हैं ! पूरी तैयारी के साथ आये हैं लेकिन वसुधारा फॉल के पास तक नही जा रहे ? हिम्मत नही हो रही !! वसुधारा फॉल को कोई कोई वसुंधरा फॉल भी कहते हैं ! हालाँकि मैं सिर्फ वसुधारा फॉल तक ही गया लेकिन इसके लगभग पांच किलोमीटर आगे अलकापुरी है जो धन के देवता कुबेर का निवास स्थान माना जाता है ! यहां से सतोपंथ और बलाकुन चोटियां स्पष्ट दिखाई देती हैं ! सतोपंथ वो जगह है जहां पांडवों ने मोक्ष प्राप्त किया था ! पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग के लिए गए थे और उनके प्रस्थान के रास्ते को स्वर्गरोहिणी कहा जाता है !
वसुधारा फॉल पर उस महिला की मौत की खबर ने सबको सतर्क कर दिया था या ये कहूँ कि सबको डरा दिया था। इसलिए कच्ची बर्फ पर चलकर फॉल तक जाने की कोई हिम्मत नही दिखा पा रहा था ! SLET के छात्र भी एक साथ बैठे जाने क्या रणनीति बना रहे थे और इतने में मैंने अपने आपको वहां जाने के लिए प्रोत्साहित कर लिया ! भगवान का नाम लिया और पहला कदम बढ़ा दिया ! 445 फुट यानि लगभग 145 मीटर ऊँचे फॉल को देखने का लोभ छोड़ ही नही पा रहा था ! वहां जो रास्ता था वो ये बता रहा था कि लोग मुझसे पहले वहाँ गए हैं लेकिन वो शायद सुबह गए होंगे और दोपहर बाद बर्फ और भी कमजोर हो जाती है इसलिए खतरा और भी ज्यादा था ! बीच रास्ते में पता नही कैसे बर्फ मेरे जूतों में घुस गयी ! लेकिन अगर यहाँ जूता खोलूंगा तो संतुलन गड़बड़ा जाएगा , पांच मिनट में ही पैर एक तरह से गल सा गया ! उधर जाकर ही बर्फ निकाली ! बर्फ कहाँ वो तो अब पानी बन चुकी थी ! फॉल के बिलकुल जड़ में खड़े होकर फोटो लेने का मजा ही कुछ अलग था लेकिन यहां तक पहुँचने के लिए कितनी बार भगवान को याद कर लिया होगा ! एक जगह बिलकुल खाली खाली जगह सी दिखी ! दूर से हाथ मारा -बर्फ पूरी टूट गयी ! बच गया ! कहीं पैर पड़ जाता तो लेने के देने पड़ जाते ! ज्यादा हिम्मत वाले लोग उस फॉल के नीचे नहाकर भी आते हैं लेकिन मैं इतना हिम्मत वाला नही था या फिर फैमिली की फ़िक्र !! पीछे मुड़कर देखा -SLET के छात्र अलविदा कहने को हाथ उठा रहे थे और मैं अभी उनसे बहुत दूर था ! उन्होंने वहां तक आने की हिम्मत नही दिखाई ! सही किया !!
उधर एक वीडियो बनाया ! कई सारे फोटो खींचे और चल दिया ! मैं अभी वापिस पहुंचा था कि उन चार में से एक मेरे पास आया ? डर नही लगा आपको ? मैं कैसे कहता कि नही लगा ? बहुत डर लगा था लेकिन हिम्मत से और भगवान की कृपा से संभव हो पाया ! वो केरल के रहने वाले थे ! धीरे धीरे करके एक ने हिम्मत दिखाई और जब वो उस पार पहुँच गया तब दूसरा स्टार्ट हुआ ! मैं उन्हें देखते हुए वापिस आकर एक जगह बैठ गया ! भगवान को धन्यवाद दिया और अपने खींचे हुए फोटो देखने लगा !!
 |
| 145 फुट की ऊंचाई से गिरता वसुधारा फॉल |
 |
 |
 |
 |
 |
वसुधारा से लौटते हुए !!
अगर हम ऐसे मान के चलें कि ऋषिकेश 100 लोग गए हैं तो 20 लोग बद्रीनाथ पहुँचते हैं और उन 20 में से मुश्किल से चार लोग माणा तक जाते हैं और उन चार में से मुश्किल से आधा आदमी वसुधारा तक पहुँचता है !! मैं थोड़ा भाग्यशाली कहूँगा अपने आपको कि मैं वहां तक अपने आपको ले जा सका ! जय बद्रीविशाल की !
बद्रीनाथ लौटने की कोई जल्दी नही थी इसलिए वहीँ माणा में जिस दुकान पर चाउमिन खाई थी , पैर थोड़े से फैला लिए घंटे आराम ले लिया ! लौटते हुए बद्रीनाथ के बाहर की ओर लाल रंग की जर्सी पहने बहुत सारे लोग अलग अलग बैठे थे और शायद कुछ लिख रहे थे ! वहां आर्मी के जैसे टेंट भी लगे थे ! वहीँ एक जगह चार पांच लोग खड़े थे , मैं भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया ! असल में वो एक पेपर चल रहा था ! स्काईंग एण्ड माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट , औली के जो नए रेक्रुइट्स थे , उनकी ट्रैनिंग के बाद का पेपर चल रहा था ! यहां ये उनकी आखिरी ट्रैनिंग थी और उनका पेपर चल रहा था ! इतना में कोई एक सैनिक बड़े से कटोरे में हलवा लेकर आया ! मुझे भी दिया। हलवा सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना था और इसकी तारीफ मैंने उनके सामने ही कर दी ! इसका फायदा भी हुआ -बोले आपको अच्छा लगा तो आप और ले लो ! और इस बार बाकायदा प्लेट भरकर मिला ! इस दरम्यान आपस की बातचीत भी चलती रही और मास्टर होने की इज्जत मिलने लगी और बैठने के लिए कुर्सी दे दी गयी ! धन्यवाद मित्रो !
मस्ती मारते हुए आराम आराम से वापस अपने घोसले ( होटल ) की तरफ लौट रहा था जैसे शाम को चिड़िया अपने बच्चों के पास लौट आती है ! थकान के मारे बुरा हाल हुआ पड़ा था ! बस लगभग होटल के गेट पर ही था कि एक वृद्ध आदमी ने रोक लिया -अरे बेटा ! मैं अपना होटल भूल गया हूँ , मुझे पहुंचा दोगे क्या ? मैंने पूछा -कौन से होटल में हैं आप ? उन्हें होटल का नाम भी याद नही था बस इतना याद था कि 500 बीएड वाले होटल के पास है ! असल में वहां 500 बिस्तरों वाला गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक होटल है जो खासा प्रसिद्द है ! वो वृद्ध व्यक्ति हरियाणा के रोहतक से आये हुए थे अपने परिवार के साथ ! लेकिन उनका परिवार माणा चला गया था और वो यहां अकेले रह गए थे और अकेले ही धीरे धीरे घूमने निकल गए और अपना रास्ता भटक गए ! मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था और उनके साथ बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा था ! ऐसे चलने में और भी ज्यादा थकान हो जाती है ! लेकिन मैं कैसे एक वृद्ध व्यक्ति को ऐसे अकेला छोड़ देता ? मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा था कि आपके पास फ़ोन है ? उन्होंने तुरंत मना कर दिया ! नही है ! मैंने पूछा - कोई नंबर याद हो जिससे बात कर सकूँ ? लेकिन जब कहीं कोई बात नही बनी और चलते चलते दो घण्टे हो गए तब हम दोनों एक जगह बैठ गए तब महोदय ने अपना फ़ोन निकाला और बोले इसमें से विकास का नंबर लगाओ ! विकास उनका छोटा बेटा था जो माणा गया हुआ था ! नंबर नही मिला तब दुसरे बेटे को फ़ोन किया और तब कहीं जाकर पता चला कि वो लोग बद्रीनाथ मंदिर के बिलकुल पास किसी बंगाली गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं ! अब फिर उतना ही पैदल चलना पड़ेगा ! मुझे गुस्सा तो बहुत आया ! ये फ़ोन दो घंटे पहले भी तो निकाला जा सकता था ? लेकिन मन को शांत किया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें उसी बंगाली गेस्ट लेकर गया और अंदर पहुंचा कर आया ! हालत खराब हो गयी और इस चक्कर में रात के साढ़े आठ बज गए ! जाते ही पहले चाय पी और फिर नहाया !
आज का कार्यक्रम बहुत व्यस्त और बहुत थकान वाला रहा लेकिन कल से यही सफर बेहतरीन याद बन जाएगा ! थकान स्वतः ही खत्म हो जायेगी लेकिन यादें जरूर बनी रहेंगी और ये यादें ही आगे ऊर्जा का संचरण करती रहेंगी ! अब आगे पुनः जोशीमठ चलेंगे ! आते हुए जोशीमठ होकर आया जरूर था लेकिन वहां कुछ देखा नही था इसलिए फिर से उधर चलेंगे और ज्योतिर्मठ यानि जोशीमठ की यात्रा करेंगे !!
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| बर्फ भी कहाँ कहाँ जम जाती है !! |
 |
 |
 |
| वसुधारा फॉल पर आश्रम |
 |
| एक छोटा सा मंदिर भी है लेकिन इसका ताला लगा था ! |
 |
| एक छोटा सा मंदिर भी है लेकिन इसका ताला लगा था ! खिड़की में से फोटो खींचना पड़ा |
 |
 |
 |
| शानदार पहाड़ ! मेरे लिए तो ये ही माउंट एवेरेस्ट है !! |
 |
 |
 |
| इस बैड पर आधा घण्टा नींद निकाली |
 |
| आते जाते लोगों के जूते चप्पल भी टूट जाते हैं !! |
 |
| ऐसे निशाँ बना रखे हैं नंबर लिखकर ! 1 /1 से शुरू होकर 7 /40 तक जाते हैं |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| स्काइंग एण्ड मॉउंटेनीरिंग इंस्टिट्यूट औली के नए रिक्रूट लिखित परीक्षा दे रहे हैं |
 |
| वापस बद्रीनाथ में |
 |
 |
 |
| एक बार और दर्शन करता चलूँ |
 |
| जय बद्री विशाल की !! |
जोशीमठ : बद्रीनाथ यात्रा
जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहते हैं बल्कि इसे उल्टा कहा जाए , ज्योतिर्मठ को जोशीमठ भी कहते हैं ! क्योंकि इसकी जो पहिचान है वो मठ की वजह से ही है। 6150 फुट की ऊंचाई पर बसा जोशीमठ हिमालय क्षेत्र की बड़ी बड़ी वादियों का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है ! ये भगवान आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित चार मठों में से एक है जो उत्तर दिशा में स्थित है ! बाकी के तीन मठ - श्रंगेरी , पुरी और द्वारका हैं। और आजकल जोशीमठ , औली के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। वो ही औली जहां जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेम्स होते हैं ! उन्हें क्या कहते हैं , नाम नही मालूम !! आइये थोड़ा सा घूमते चलते हैं यहां भी , नही तो जोशीमठ और जोशीमठ के लोग कहेंगे कि यहां से निकला था और हमें मिलकर भी नही गया ! जोशीमठ के बच्चे बिलकुल अलग हैं , यहां उन्हें जून के महीने में स्कूल जाना होता है जब सब जगह छुट्टियां होती हैं और इन्हें दिसंबर में छुट्टियां मिलती हैं !
अगर जोशीमठ के इतिहास की बात करें तो ये बहुत पुराना स्थान है। आज के जोशीमठ का पुराना नाम भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर कार्तिकेयपुरा हुआ करता था फिर ज्योतिर्मठ और फिर जोशीमठ। यहां आपको 8 वीं सदी में भगवान आदि शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिष्ठापित भारत का पुराना वृक्ष देखने को मिलता है जिसे कल्पवृक्ष कहते हैं।
 |
| ये पाषाण जब विभक्त हो जाएगा तब भगवान शिव अपने नए "आवास " पर शिफ्ट होंगे जिसे भविष्य केदार कहा जाएगा |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ये वो 2300 वर्ष पुराना कल्पवृक्ष |
 |
 |
 |
 |
 |
| ये वो 2300 वर्ष पुराना कल्पवृक्ष |
 |
| यहां लोगों ने भगवान आदि शंकराचार्य जी को मंदिर के नीचे एक गुफा में बंद किया हुआ है ! यहीं भगवान शंकराचार्य जी ने तपस्या करी थी !! |
 |
| भगवान शंकराचार्य जी |
जोशीमठ से गाजियाबाद
जोशीमठ भले एक छोटा सा क़स्बा हो लेकिन महवपूर्ण जगह मानी जाती है ! विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें भगवान शंकराचार्य जी और हिन्दू धर्म के प्रति गहरी आस्था और गहन अध्ययन करने की लगन है ! जैसा मैंने पहले भाग में लिखा कि जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहते हैं ! भगवान आदि शंकराचार्य जी द्धारा 8 वीं सदी में स्थापित इस मठ को चलाने के लिए नियुक्त किये गए शंकराचार्य स्वामी रामकृष्ण तीर्थ के पश्चात करीब 1941 तक ये मठ 165 साल तक बिना शंकराचार्य के ही रहा।
भगवान शंकराचार्य की गुफा और उनका मंदिर देखने के बाद सामने ही एक प्राचीन मंदिर की तरफ चला गया। हालाँकि मंदिर तो बन्द था लेकिन बाहर से देखने में बहुत सुन्दर लग रहा था। उसके कुछ फोटो खींचने के बाद और आगे बढ़ा तो महाभारत से प्रसिद्द भीष्म पितामह की विशाल मूर्ति लेटी हुई अवस्था में दिखाई देती है ! जीवन में पहली बार भीष्म पितामह की मूर्ति देखि है और वो भी इतनी विशाल ! चलते रहने के लिए सुन्दर और साफ़ सुथरा रास्ता बना हुआ है जिसके दोनों तरफ हरियाली है ! बीच में एक हरा भरा पार्क भी है जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है ! भीष्म पितामह की मूर्ति के बिल्कुल विपरीत दिशा में संकट मोचक हनुमान जी का मंदिर है जो बहुत विशिष्ट नही लगा ! इससे आगे हाथी की एक मूर्ति है फिर सामने मुख्य मंदिर दिखाई देता है जहां लगभग 20 फुट ऊँची भगवान शिव की प्रतिमा लगी हुई है। जब वहां पहुंचा तब मुझे एक भी श्रद्धालु नही दिखा बस तीन चार लड़के दिखे जो मंदिर के ही कर्मचारी थे। इधर -उधर देखते हुए जब बिल्कुल मंदिर के पास पहुँचा तो उस दो मंजिल के मंदिर की ऊपरी मंजिल पर एक संत जैसे सज्जन सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दिए ! मैंने उनसे ऊपर आने की अनुमति मांगी तो उन्होंने इशारे से ऊपर का रास्ता बता दिया ! 10 -15 मिनट उनके पास बैठा और उनसे ज्ञान प्राप्त किया और ज्योतिर्मठ के विषय में और भी जानकारी प्राप्त की ! स्फटिक शिवलिंक के प्रथम बार दर्शन किये और उन्हें दक्षिणा दी ! हालाँकि मैं आसानी से किसी को भी दक्षिणा नही देता क्योंकि मैं स्वयं दक्षिणा लेने वालों में से हूँ , यानि विप्र हूँ लेकिन उन्हें दक्षिणा देने में अच्छा लगा !
बद्रीनाथ यात्रा का समापन !!
पांडुकेश्वर मंदिर जोशीमठ. PanduKeshwar Temple
हेलो दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। इसलिए के माध्यम से हम आप लोगों के साथ उत्तराखंड का प्रसिद्ध पांडुकेश्वर मंदिर के बारे में ( PanduKeshwar Temple) जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देवभूमि प्राचीन काल से ही अपने पवित्र एवं देवतुल्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां के कण कण में देवी देवताओं का वास है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी पहचाना जाता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है पांडुकेश्वर मंदिर, इसके बारे में आज हम आप लोगों के साथ जानकारी साझा करने वाले हैं। दोस्तों आशा है की आपको पंडोकेश्वर मंदिर के बारे में ( PanduKeshwar Temple ) जानकर अच्छा लगेगा इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ना।
उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित पांडुकेश्वर मंदिर ( PanduKeshwar Temple) अलकनंदा नदी के तट पर बना एक खूबसूरत सा मंदिर है जोकि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ पारंपरिक शैली में निर्मित किया गया है। हिंदी में प्रवेश करने पर आप देख पाएंगे कि मंदिर का निर्माण उत्कृष्ट शैली के अंतर्गत किया गया है। मंदिर के अंदर जटिल नक्काशी दार मूर्तियां स्थापित की गई है मंदिर की शोभा को बढ़ाते हैं।
भगवान शिव जी को समर्पित पांडुकेश्वर मंदिर के दर्शन करने पर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संतुष्ट के साथ-साथ मन की शांति और खुशी प्राप्त होती है। अपने खूबसूरत आवरण में स्थित होने के कारण पांडुकेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं का एक आकर्षित स्थल बना हुआ है। मंदिर में मुख्य रूप से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गतिविधियों के अलावा इसकी प्राकृतिक सौंदर्य मन को तरोताजा कर देती है।
पांडुकेश्वर मंदिर स्थापत्य शैली. PanduKeshwar Temple Sheli
दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पांडे कैसे मंदिर का निर्माण उत्कृष्ट तरीके से बड़ी ही खूबसूरत शैली में निर्माण किया गया है। एक हिंदू मंदिर होने के कारण पांडेश्वर मंदिर का निर्माण नागरा शैली में किया गया है । इस शैली में निर्मित मंदिरों की मुख्य विशेषता है कि मंदिर का ऊपरी हिस्सा आकाश की ओर लंबे और घुमावदार होते हैं। मंदिर के अंदर बने मोतियों को भी विशेष शैली के अंतर्गत निर्मित किया गया है।
पांडुकेश्वर मंदिर की कहानी. PanduKeshwar Temple Kahani
प्यारें पाठकों जिस तरह से हर किसी मंदिर के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक कहानी छुपी होती है ठीक उसी तरह से पांडे क्वेश्चन मंदिर के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है जो कि इस मंदिर को बहुत खास बनाती है चलिए उसे कहानी के बारे में जानते हैं।
पौराणिक कहानियों के आधार पर किवदंति है कि हिंदू के महाकाव्य महाभारत में पांडवों के पिता पांडु ने इस क्षेत्र में गहन तपस्या की थी जहां पर आज के समय में यह प्रसिद्ध पांडुकेश्वर मंदिर स्थापित है। उनकी गहन तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद और दिव्य शक्तियां प्रदान की।
ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी के प्रति पांडू की गहन भक्ति के सम्मान में पांडुकेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। और यह वही जगह है जहां पर पांडु ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की थी। इसलिए यह पार्टकेश्वर मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जो लोग जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए इस मंदिर का विशेष महत्व है।
ऐसा भी माना जाता है कि भगवान आदि शंकराचार्य और हिंदू महाकाव्य महाभारत लिखने वाले ऋषि व्यास भी इस मंदिर में आए थे।
पांडुकेश्वर मंदिर कैसे पहुंचे, PanduKeshwar Temple Kese Pahuchen
दोस्तों यदि आप भी जोशीमठ में स्थित पांडुकेश्वर मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो बताना चाहेंगे कि पांडुकेश्वर मंदिर उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित है जहां सड़क मार्ग और वायु मार्ग के अलावा रेल मार्ग के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है।
सड़क मार्ग द्वारा पांडुकेश्वर मंदिर( PanduKeshwar Temple) पहुंचने के लिए आप अपने नजदीकी शहर या गांव से आराम से जोशीमठ तक पहुंच सकते हैं। के अलावा पंडोकेश्वर मंदिर का नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है जहां से आप फाउंडेशन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।
रेल मार्ग के द्वारा पांडेश्वर मंदिर पहुंचना काफी आसान है मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है जो जोशीमठ से लगभग 265 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
दोस्तों वैसे सड़क मार्ग के माध्यम से ही पांडुकेश्वर मंदिर के दर्शन करना उचित रहेगा।
पांडुकेश्वर मंदिर Q&A
Q – पांडुकेश्वर मंदिर कहां स्थित है ?
Ans – पांडवकेश्वर मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ में स्थित एक हिंदू धार्मिक स्थल है जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है।
Q – पांडुकेश्वर मंदिर का इतिहास ?
Ans – पांडुकेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में किवदंती है कि पांडवों के पिता पांडु ने इस क्षेत्र में कहां गहन तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान की।
Q – पांडुकेश्वर मंदिर की वास्तुकला कैसी है ?
Ans – पांडुकेश्वर मंदिर की वास्तुकला नागरा शैली है। मंदिर को जटिल नक्काशी और मूर्तियों के द्वारा सुसज्जित तरह से सजाया गया है।
हेलो दोस्तों उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज के इस लेकर माध्यम से हम आप लोगों के साथ बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास (History of Badrinath Temple) एवं बद्रीनाथ मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही दिव्य आत्माओं का निवास स्थान रही है और प्राचीन काल से ही उत्तराखंड को देवों की भूमि के नाम से पहचाना जाता है। उन्हें पवित्र स्थलों में से एक है उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर जो कि अपने उत्कृष्ट वास्तु कला एवं बद्रीनाथ का इतिहास के लिए भी ( History of Badrinath Temple ) पहचानी जाती है। आज के इसलिए के माध्यम से हम आपको बद्रीनाथ मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले थे आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आएगा इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ना।
उत्तराखंड के चार धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। अलकनंदा नदी के बाएं तट पर और नारायण नामक दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थिति बद्रीनाथ मंदिर पंच बद्री समूह में से। उत्तराखंड के इतिहास में पंच केदार एवं पंच प्रयाग मंदिरों का समूह बड़ा ही पवित्र एवं धार्मिक स्थल माने जाते हैं।
ऋषिकेश से 214 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है बद्रीनाथ मंदिर पूरी वर्ष भर में लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। प्राचीन शैली में बना हुआ विशाल और आकर्षक है। समुद्र तल से बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई ( Badrinath temple height) करीब 15 मीटर मापी गई है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार किवदंती है कि भगवान शिव जी ने बद्रीनारायण की छवि शालिग्राम के एक काले पत्थर पर खोजी थीं।

बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण। who built badrinath temple
बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमारे पाठकों के माध्यम से बार-बार टिप्पणियां की जा रही थी। उसी का उत्तर देने के लिए आज हमने यह लेख लिखा है आपके लिए। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया और कब किया यह एक ऐतिहासिक और रहस्य में घटना बनी हुई है लेकिन इतिहास के कुछ पहलुओं के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कहा जाता है की गढ़वाल के राजा ने 16वीं शताब्दी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। जिसमें उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति स्थापित की थी।
जबकि इतिहास की दूसरी घटनाओं के आधार पर यह भी किवदंति है की बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने आठवीं सदी में की थी। आदि गुरु शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार मंदिर के पुजारी भारत के केरल राज्य से होते थे।
उत्कृष्ट वास्तु कला से निर्मित बद्रीनाथ मंदिर तीन भागों में विभाजित है जो कि गर्भ ग्रह, दर्शन मंडप और सभा मंडप है। प्रदेश के दौरान आप देख पाएंगे कि मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित है साथ ही मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की एक ऊंची काले पत्थर के प्रतिमा विद्यमान है।
धरती का बैकुंठ के नाम से पहचाने जाने वाली बद्रीनाथ मंदिर में वन तुलसी की माला , चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं।

बद्रीनाथ धाम मंदिर की स्थापना का जिक्र पौराणिक लोक कथाओं में भी देखने को मिलता है पहले इस मंदिर में भगवान शिव का वास हुआ करता था एक बार भगवान विष्णु ध्यान मग्न होने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे इस दौरान भगवान नारायण इस केदार भूमि में आए और उन्हें यह जगह पसंद आने लगी.
लोक कथाओं के अनुसार किंवदंती है कि जब भगवान विष्णु वहां आए तो उन्होंने अलकनंदा नदी के पास पहुंचकर एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और तेजी से रोने लगे । जिसे सुनकर भगवान शिव जी और माता पार्वती उनके पास आए और उनसे रोने का कारण पूछने पर भगवान विष्णु जी ने बताया कि उन्हें ध्यान योग के लिए यही जगह चाहिए इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने उन्हें ध्यान करने के लिए यह जगह दे दी। वह वही जगह है जहां पर आज के समय में पवित्र बद्रीनाथ मंदिर स्थापित है। इस तरह से बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास ( History of Badrinath Temple ) अपने आप में पौराणिक होने के साथ-साथ ऐतिहासिक भी माना जाता है।
बद्रीनाथ मंदिर का रहस्य क्या है. History of Badrinath Temple
दोस्तों क्या आप जानते हैं की बद्रीनाथ मंदिर का रहस्य क्या है आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर में शंकर नहीं बजाया जाता। जानते हैं कुछ ऐसे अनसुनी रहस्यमई बातें जो की बद्रीनाथ मंदिर का रहस्य उजागर करते हैं।
लोक कथाओं के अनुसार यह हम कह सकते हैं कि लोगों के अनुसार केवदंती है की मां लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी रूप में ध्यान कर रही थी तब वह ध्यान मांगने थी इस समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए आज के समय में भी बद्रीनाथ मंदिर में शंकर नहीं बजाया जाता है।

बद्रीनाथ मंदिर की मान्यता, Belief of Badrinath Temple.
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जीव जानती है कि जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हो रही थी तो गंगा नदी 12 धाराओं में बट गई थी इसलिए इस जगह पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस जगह को भगवान विष्णु ने अपना निवास स्थान बनाया जिसके कारण यह जगह बद्रीनाथ के नाम से विख्यात हुई।
बद्रीनाथ मंदिर की मान्यता यह भी बताई जाती है कि प्राचीन काल में यह स्थान खूबसूरत पेड़ों के पेड़ों से भरा हुआ रहता था इसलिए इस जगह का नाम बद्री वन पड़ गया।
बद्रीनाथ मंदिर की मान्यता यह भी बताई जाती है कि इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ को ब्राह्मण हत्या से मुक्ति मिली थी जिस घटना को ब्राहकपाल के नाम से भी जाना जाता है।
केदारनाथ मंदिर का इतिहास. Kedarnath Temple History
हेलो दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज के इस लेकर माध्यम से हम आप लोगों को उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर एवं केदारनाथ धाम का इतिहास ( Kedarnath Temple History) के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही दिव्य आत्माओं का निवास रही है उन्हें पवित्र एवं धार्मिक स्थलों में से एक है केदारनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड के अलावा पूरे देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है आज के इस लेख में हम आपको केदारनाथ मंदिर का इतिहास के बारे में जानकारी देंगे तो इसलिए को अंत तक जरूर पढ़ना।
हिमालय पर्वत की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार के समूह का एक मंदिर माना जाता है। कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर में से एक है। 80वी शताब्दी में निर्मित केदारनाथ मंदिर 6 फुट पहुंचे चबूतरे पर बना हुआ है।
तीनों दिशाओं से सुंदर से पहाड़ों से गिरा हुआ केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 22000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तीन पहाड़ों एवं पांच नदियों के संगम पर स्थित केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के सबसे पवित्र स्थान में से एक माना जाता है आस्था और भक्ति का प्रतीक है मंदिर हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है।
केदारनाथ मंदिर का निर्माण एवं वास्तुकला. Architecture of Kedarnath Temple
केदारनाथ मंदिर जितना आकर्षित लगता है उतनी ही सुंदर एवं प्राचीन इसकी वास्तुकला है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप जिसे गर्भ ग्रह कहा जाता है बना हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में नंदी बैल विराजमान है एवं मंदिर के मध्य भाग में श्री केदार स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। श्री ज्योतिर्लिंग के चारों दिशाओं में चार बड़े-बड़े स्तंभ विद्यमान है और यह स्तंभ चारों वेदों के आधार माने जाते हैं। जिसके अग्रभाग पर भगवान गणेश जी और मां पार्वती के यंत्र का चित्रण किया गया है।
वास्तु कला से निर्मित चार विशाल का स्तंभों पर मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी भाग में एक अखंड दीपक विद्यमान है जो की हजारों सालों से मंदिर को प्रकाशित कर रहा है। मान्यता है कि इस अखंड ज्योति का रखरखाव पुरोहितों द्वारा सदियों से किया जा रहा है ताकि यह अखंड ज्योति सदैव मंदिर के भाग में जलता रहे।

आपको जानकर हैरानी होगी कि 400 साल बर्फ के अंदर दबा हुआ था केदारनाथ मंदिर जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वादियां इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ मंदिर ने न केवल सन 2013 की बाढ़ की आपदा का सामना किया बल्कि केदारनाथ धाम लगभग 400 वर्षों तक बर्फ के बीच दबा हुआ रहा। इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार मान्यता है मंदिर की दीवारों पर पीली रेखाएं अंकित है जो की लगातार ग्लेशियर के पिघलने से मानी जाती है। 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच हिम युग की शुरुआत हुई थी 13वी भी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच तक केदारनाथ मंदिर बर्फ के भीतर दबा हुआ था।
केदारनाथ मंदिर का इतिहास एवं मान्यताएं. Kedarnath Temple History
केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। भगवान शंकर का निवास स्थान केदारनाथ मंदिर हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास पौराणिक कहानियों ( Kedarnath Temple History) के आधार पर मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार और महान तपस्वी ऋषि नर और नारायण केदार पर्वत पर भगवान शंकर की तपस्या किया करते थे। उनके कठिन तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। स्थान पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए उसे स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनाया गया जिसे आज के समय में केदारनाथ मंदिर के रूप में पहचाना जाता है।
केदारनाथ मंदिर का इतिहास ( Kedarnath Temple History ) से संबंधित दूसरी कथा यह भी है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद पांडव भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहां आए थे। कुरुक्षेत्र में पांडवों के द्वारा अपने भाइयों और रिश्तेदारों को मारने का अपराध बोध लग गया। इसके निवारण के लिए पांडव को भगवान शिव जी के दर्शन करना जरूरी था। भगवान भोलेनाथ जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे इसलिए वह उनसे छुपकर विभिन्न जगहों में छुपने लगे।
दोस्तों इस तरह से केदारनाथ मंदिर का इतिहास ( History of Kedarnath Temple) से संबंधित कई प्रकार की कहानी उजागर होकर सामने आती है। आधार पर हम कह सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन और रहस्यों से सम्मिलित है।

6 महीने तक नहीं बुझता है केदारनाथ मंदिर का दीपक। Kedarnath Temple beliefs.
भारी भरकम एवं हिमपाल की वजह से जब 6 महीने के लिए मंदिर के पट बंद किए जाते हैं तो मंदिर के पुजारी द्वारा केदार बाबा की मूर्ति को उसकी पेमेंट में स्थानांतरित किया जाता है। पवित्र मंदिर के कपाट बंद किए जाने के समय मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि यह दीपक 6 महीने तक जलता रहता है। और आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर का दीपक 6 महीने तक जलती रहने के साथ-साथ मंदिर की साफ सफाई भी ठीक उसी क्रम में हुई ही रहती है जैसे की मंदिर में पूजा के दौरान रहती है।
दोस्तों यह थी कहानी केदारनाथ मंदिर का इतिहास ( Kedarnath Temple History) के बारे में। है कि आपको केदारनाथ मंदिर का इतिहास के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो अपने परिवार हो दोस्तों के साथ जरूर साझा करें । उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही लेख पढ़ने के लिए आप देवभूम में उत्तराखंड को जरूर फॉलो करें अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं।
द्रोणागिरी पर्वत उत्तराखंड. Dronagiri Parwat Uttarakhand
हेलो दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज के इस लेख के माध्यम से हम आप लोगों के साथ द्रोणागिरी पर्वत के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड को प्राचीन काल से ही पवित्र एवं दिव्य आत्माओं का निवास स्थान माना जाता है। इन पवित्र स्थानों में उलझे आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं । जिनके बारे में जानने के लिए पूरी देश और दुनिया के लोग बेताब है। उन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है द्रोणागिरी पर्वत। देवभूमि उत्तराखंड के आज के इस लेख में हम आपको द्रोणागिरी पर्वत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा। इसलिए इसलिए कि को अंत तक जरूर पढ़ना।
द्रोणागिरी पर्वत कहां स्थित है. Dronagiri Parwat Kaha Isthit Hai
भारत के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के जोशीमठ के पास स्थित द्रोणागिरी पर्वत एक ऐतिहासिक स्थल है जोकि पूरे वर्ष भर में हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। अक्सर हमारे पाठकों द्वारा यह भी पूछा गया है कि द्रोणागिरी पर्वत कहां स्थित है। आशा करते हैं कि उन्हें जानकारी प्राप्त हो गई होगी।
द्रोणागिरी पर्वत और द्रोणागिरी गांव उत्तराखंड के इतिहास में राजस्थान रखते हैं। द्रोणागिरी गांव लगभग समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। द्रोणागिरी पर्वत का रहस्य रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन दोनों स्थानों को उत्तराखंड के लोगों द्वारा खास महत्व दिया जाता है।
द्रोणागिरी पर्वत के बारे में. Dronagiri Parwat Ke Baren Me
प्यारे पाठको द्रोणागिरी पर्वत उत्तराखंड के उन पर्वतों में से एक हैं जिसमें हजारों प्रकार के तमाम जड़ी बूटियों पाई जाती है जिनका उल्लेख रामायण में भी देखने को मिलता है।
द्रोणागिरी पर्वत द्रोणागिरी गांव वालों का पवित्र स्थल माना जाता था वह लोग द्रोणागिरी पर्वत आस्था और भक्ति भावना के साथ पूजा किया करते थे। क्योंकि द्रोणागिरी पर्वत ने गांव वालों को हजारों प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां प्रदान की थी जोकि वे इलाज बीमारियों की दवाई का काम करते थे।
रामायण में जब भगवान लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में होते हैं तो भगवान राम के द्वारा भगवान हनुमान जी को उनके उपचार के लिए जड़ी-बूटी के लिए भेजा जाता है। भगवान लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में थे तो उनका ठीक हो ना केवल संजीवनी बूटी के द्वारा ही था इसलिए भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी की तलाश करते करते हैं द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। जहां उन्हें संजीवनी बूटी मिल जाती है लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं होती है इसलिए वह संजीवनी बूटी को ले जाने के बजाय पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही उठाकर ले जाते हैं।
इसलिए रामायण में उल्लेखित द्रोणागिरी पर्वत को विशेष महत्व दिया गया है। और उत्तराखंड के इतिहास में द्रोणागिरी पर्वत का विशेष स्थान है। आज के समय में भी यहां के द्रोणागिरी पर्वत को विशेष स्थान देते हैं।
द्रोणागिरी गांव में आज भी नहीं होती है हनुमान जी की पूजा
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत के समीप स्थित द्रोणागिरी गांव में क्यों हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी की तलाश करते करते द्रोणागिरी पर्वत में पहुंचते हैं और संजीवनी बूटी की पहचान ना होने के कारण वह पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही भगवान राम जी के पास ले जाते हैं।
लेकिन द्रोणागिरी गांव के लोग द्रोणागिरी पर्वत को पवित्र मानते थे और वह उसकी पूजा किया करते थे। इसलिए जब हनुमान जी ने यह पर्वत उठाया तो गांव वाले काफी नाराज हो गए और उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि आज के समय में भी उत्तराखंड के द्रोणागिरी गांव में के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। शायद यह उन लोगों का द्रोणागिरी पर्वत के प्रति लगाव और भक्ति का प्रतीक हो।
प्यारे दोस्तों आशा करते हैं कि आपको द्रोणागिरी पर्वत के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह नहीं पसंद आया होगा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।
उत्तराखंड से जोड़ी ऐसी ही मूलभूत जानकारियों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज देवभूमि उत्तराखंड और यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड को जरूर फॉलो करें।
द्रोणागिरी पर्वत F&Q
Q – हनुमान जी संजीवनी बूटी कहां से लाए।
Ans – भगवान लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में थे तो भगवान हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी किस तरह की गई। और आखिरकार उन्हें संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर मिली। लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी। इसलिए वह संजीवनी बूटी के साथ पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही अपने साथ ले गए।
Q – संजीवनी बूटी पार्वत कहां पर है।
Ans – दोस्तों वैसे तो संजीवनी बूटी पर्वत कहीं भी हो सकता है। यदि संजीवनी बूटी की तरह की जाती है तो यह किसी भी पर्वत पर मिल सकती है। लेकिन रामायण में उल्लेखित संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर स्थित थी। द्रोणागिरी पर्वत में कई प्रकार की जड़ी बूटियां मौजूद थे। जिनमें से एक संजीवनी बूटी थी इसके लिए हनुमान जी के द्वारा पूरे पर्वत को ही उठाया गया।
Q – संजीवनी बूटी पार्वत कहां पर है।
Ans – दोस्तों वैसे तो संजीवनी बूटी पर्वत कहीं भी हो सकता है। यदि संजीवनी बूटी की तरह की जाती है तो यह किसी भी पर्वत पर मिल सकती है। लेकिन रामायण में उल्लेखित संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर स्थित थी। द्रोणागिरी पर्वत में कई प्रकार की जड़ी बूटियां मौजूद थे। जिनमें से एक संजीवनी बूटी थी इसके लिए हनुमान जी के द्वारा पूरे पर्वत को ही उठाया गया।
Q – द्रोणागिरी पर्वत कहां स्थित है
Ans – द्रोणागिरी पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य में जोशीमठ के पास स्थित है। द्रोणागिरी पर्वत द्रोणागिरी गांव का पवित्र स्थल माना जाता था। लेकिन संजीवनी बूटी की तरह करते जब हनुमान जी इस पर्वत पर पहुंचे तो वह इस पूरे पर्वत को ही उठाकर ले गए। तब से यहां के लोग भगवान हनुमान जी से काफी नाराज है। इसलिए द्रोणागिरी गांव में हनुमान जी का नाम लेना भी मना है।
Q – रात में चमकने वाली जड़ी बूटी
Ans – संजीवनी बूटी रात में चमकने वाली जड़ी बूटियों में से एक है। इसका औषधीय गुण मूर्छित अवस्था के उपचार में भी किया जाता है। रामायण में जब भगवान लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो भगवान हनुमान जी द्वारा द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी को ही उपचार के लिए ले जाया गया था।
Q – द्रोणागिरी पर्वत किस राज्य में है।
Ans – द्रोणागिरी पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ में स्थित है। यह पर्वत समुद्र तल से 12000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके समीप द्रोणागिरी गांव स्थित है। प्राचीन काल में द्रोणागिरी पर्वत द्रोणागिरी गांव का पवित्र स्थल था। द्रोणागिरी गांव के लोगों द्वारा द्रोणागिरी पर्वत की पूजा की जाती थी।
Q – द्रोणागिरी पर्वत का रहस्य
Ans – द्रोणागिरी पर्वत का रहस्य अपने आप में खास स्थान रखता है। रामायण में उल्लेखित द्रोणागिरी पर्वत के बारे में जानकारी मिलती है कि भगवान हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी की तलाश करते हुए वह द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। और जब उन्हें द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी मिली तो है पूरे पर्वत को ही उठाकर भगवान राम जी के पास ले गए।
नरसिंह देवता उत्तराखंड. Narsingh Devta Uttarakhand
नमस्ते दोस्तों जय देव भूमि उत्तराखंड कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग क के आज के नए लेख में। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड के लोक देवता नरसिंह देवता के बारे में जानकारी (Narsingh Devta Uttarakhand) देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड देव भूमि के नाम से भी जानी जाती है और प्राचीन काल से ही यहां पवित्र आत्माओं का निवास रहा है उन्हीं पवित्र आत्माओं में से एक है उत्तराखंड के लोक देवता नरसिंह देवता। आज के इस लेख में हम आपको नरसिंह देवता उत्तराखंड के बारे में जानकारी देना चाहते हैं।
नरसिंह देवता उत्तराखंड. Narsingh Devta Uttarakhand
देवों की जन्मभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही पवित्र एवं दिव्य आत्माओं का निवास स्थान रही है। जिनका उल्लेख पौराणिक बताओ मैं भी सुनने को मिल जाती है। उन्हीं पवित्र एवं दिव्य आत्माओं में से एक हैं नरसिंह देवता उत्तराखंड (Narsingh Devta Uttarakhand )जिन्हें उत्तराखंड के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार नरसिंह देवता भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार थे। जिनकी शारीरिक रचना मुंहा सिंह का और धड़ मनुष्य का था। इसलिए वह नरसिंह देवता के नाम से जाने गए। लेकिन ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि उत्तराखंड में नरसिंह देवता को भगवान विष्णु के चौथे अवतार के रूप में नहीं पूजा जाता है। किंतु उत्तराखंड में वह सिद्ध योगी नरसिंह देवता के रूप में पूजे जाते हैं।
उत्तराखंड में भगवान विष्णु के चौथे रूम नरसिंह देव की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। और ना ही किसी भी नरसिंह देवता के जागर में भगवान विष्णु के चौथे अवतार का वर्णन मिलता है। नरसिंह देव की पूजा करने के लिए जागरण एवं घंडियाल लगाई जाती है जिसमें उनके बावन वीरो एवं नौ रूपों का वर्णन मिलता है। ग्रंथों में भी वर्णित है कि नरसिंह देवता एक जोगी के रूप में पूजे जाते हैं। जो कि एक प्रिय झोला, चिमटा और तीमर का डंडा साथ में लिए रहते हैं।
उत्तराखंड में नरसिंह देवता नौ रूपों में पूजे जाते हैं। Narsingh Devta Ke Roop
- इंगला बीर
- पिंगला वीर
- जतीबीर
- थती बीर
- घोर- अघोर बीर
- चंड बीर
- प्रचंड बीर
- दूधिया नरसिंह
- डौंडिया नरसिंह
उत्तराखंड के गढ़वाल एवं कुमाऊं में नरसिंह देवता कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दोनों मंडलों में इनकी पूजा का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। लेकिन इनका मुख्य मंदिर उत्तराखंड के जोशीमठ के पास स्थित है। बद्रीनाथ का मामा भी कहा जाता है। नरसिंह के जागर गीतों में इन्हें काली के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। जोशीमठ में स्थित नरसिंह देवता के मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यह लगभग 12000 साल पुराना है। जिसकी स्थापना किसी और ने नहीं बल्कि आदिगुरु श्री शंकराचार्य जी ने की थी। प्राचीन काल में यह जगह कार्तिकेय पुर के नाम से जानी जाती थी
नरसिंह देवता की उत्पत्ति. Narsingh Devta ki Kahani
नरसिंह देवता की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में कोई सटीक एवं सच्ची जानकारी तो नहीं है लेकिन जितनी भी कहानियां हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि।
नरसिंह देव की उत्पत्ति केसर के पेड़ से हुई थी। नरसिंह देव की जागर से जानकारी मिली है कि उनके जागर में केसर का पेड़ का जिक्र किया गया है। किवदंती है कि केसर का पेड़ हिला और भगवान शिव जी ने केसर के बीज बोए और उनकी दूध से सिंचाई की। उस डाली पर 9 फल लगे और वह 9 फल अलग-अलग स्थानों पर जा गिरे । तब जाकर वाहनों अलग-अलग भाई पैदा हुए। पहला फल केदारघाटी में जा गिरा जहां केदारी नरसिंह पैदा हो गए। दूसरा फाइल बद्री खंड में गिरा जहां बद्री नरसिंह पैदा हुए। ऐसे ही जहां जहां पर वह फल गिरते गए वहां वहां पर नरसिंह देवता उत्पन्न होते गए। जहां जहां पर भी वह दूसरे गए उनके अलग-अलग नाम उत्पन्न होते गए। लेकिन जब नरसिंह देवता की पूजा की जाती है तो इन नौ रूपों का जिक्र जरूर किया जाता है। कोयला और राख की सहायता से इनकी धून भी रमाई जाती हैं। जिस आदमी पर नरसिंह देव अवतरण लेते हैं उन्हीं गढ़वाल में डांगर कहा जाता है। जब उन पर नरसिंह देवता आते हैं तो उनके मुंह से वाणी आदेश के रूप में सुनाई देती हैं। वह आदेश नरसिंह देव के सभी नौ रूपों का होता है।
दोस्तों यह था हमारा आज का लेख , जिसमें हमने आपको नरसिंह देवता के बारें में जानकारी दी आशा करते है की आपको यह लेख पसंद आया होगा, आपको यह लेख केसा लगा हमें टिप्पणी के माध्यम से व्यक्त करें। यदि आप भी ऐसा ही जानकारीयुक्त लेख हम तक पहुंचना चाहते है तो आप हमें ईमेल के माध्यम से भी लिख सकते है।
उत्तराखंड के प्रमुख बोलियां. Uttarakhand ki Boliya
नमस्ते दोस्तों जय देव भूमि उत्तराखंड। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग के आज के नए लेख में। आज हम आपको उत्तराखंड की प्रमुख भाषाएं एवं बोलियों के बारे में जानकारी देने वाले है । जैसा कि आप सभी लोग जानते है कि उत्तराखंड राज्य भाषाई तौर पर काफी समृद्ध है। यहां पर विभिन्न प्रकार की बोलिय बोली जाती है। जो कि उत्तराखंड राज्य को एक पहचान दिलाने में मदद करते हैं। उत्तराखंड की बोलियां राज्य की पहचान है बोलियों के माध्यम से राज्य की संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत रखा गया है।
उत्तराखंड के प्रमुख बोलियां. Uttarakhand ki Boliya
देवभूमि उत्तराखंड में मुख्य रूप से हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा वार्तालाप के लिए अपनी हर क्षेत्र के अलग-अलग बोलियां बनाई गई हैं। इन बोलियों को मुख्य रूप से गढ़वाली एवं कुमाऊनी क्षेत्र के रूप में बांटा गया है। कुमाऊंनी एवं गढ़वाली बोलियों को अलग-अलग भागों में अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से बांटा गया है। चलिए एक नजर राज्य के प्रमुख बोलियों की ओर डालते हैं।
कुमाऊनी बोली. Uttarakhand ki Boliya
कुमाऊनी बोली कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरी तथा दक्षिणी सीमांत को छोड़कर बाकी के संपूर्ण भाग में कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। इस भाषा के मूल रूप के संबंधों में कुमाऊनी का विकास , दरद, खस, एवं प्राकृत से माना जाता है। हिंदी भाषा की ही भांति कुमाऊनी भाषा का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आज के कुमाऊनी भाषा में तद्भव तत्सम एवं स्थानीय शब्दों के अतिरिक्त आर्ययोत्तर भाषा के शब्द मिले-जुले होते हैं। कुमाऊनी भाषा हिंदी की खड़ी बोली से सर्वाधिक प्रभावित है। कई विद्वानों द्वारा इसे पहाड़ी हिंदी का नाम भी देने लगे।
कुमाऊनी उत्तराखंड की प्रमुख लोक भाषाओं में से एक है जिसकी प्रमुखता एवं प्रसिद्धि का मुख्य कारण है कि इस बोली का शब्द संपदा एवं साहित्य अभिव्यक्ति में संपूर्ण उपयोग किया गया। कुमाऊनी बोलियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा गया है।
पूर्वी कुमाऊनी बोलियां. Uttarakhand ki Boliya
कुम्मयां – मुख्य रूप से यह बोली नैनीताल से लगे हुए काली कमाई क्षेत्र में बोली जाती है।
असकोटी – यह असकोटी क्षेत्र की बोली है इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव पड़ा हुआ है।
शौर्याली – यह बेली जोहार और पूर्वी गंगोली क्षेत्र में बोली जाती है
सिराली – सिराली कुमाऊनी बोली मुख्य रूप से अस्कोट क्षेत्र के सीरा में बोली जाती हैं।
पश्चिमी कुमाऊनी बोलियां. Uttarakhand ki Boliya
पछाई – यह अल्मोड़ा जिले के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। यहां तक कि गढ़वाल के कुछ क्षेत्र में भी यह बोली बोली जाती है।
दनपुरिया – यह बोले मुख्य रूप से दानापुर किए उत्तरी भाग में बोली जाती है।
खस पराजिया – यह बोली दानपुर क्षेत्र के आसपास अधिक संख्या में वार्तालाप में लाई जाती हैं।
फल्दा कोटी – अल्मोड़ा एवं नैनीताल के कुछ क्षेत्रों में बोले जाने वाली यह भाषा पाली पछाऊ के क्षेत्र में अधिक बोली जाती है।
चोगखिरिया – इस बोली का उपयोग चौगखर में अधिक बोली जाती है।
गंगोई – यह बोली दानापुर और गंगोली के क्षेत्र में वार्तालाप में लाई जाती है।
उत्तरी कुमाऊनी बोलियां. Uttarakhand ki Bhasayen
जौहरी – जौहरी बोली उत्तराखंड के जौहर व कुमाऊं के उत्तर स्मृति क्षेत्रों में बोली जाती है।
दक्षिणी कुमाऊनी बोलियां. Kumauni Boliya
रचभेसी – रचभेसी नैनीताल के रौ एवं चौमांसी पट्टियों, भीमताल, काठगोदाम आदि क्षेत्रों में अधिक बोली जाती हैं।
गढ़वाली बोली. Uttarakhand ki Bhasayen
उत्तराखंड की प्रमुख भाषा में कुमाऊनी भाषा की तरह गढ़वाली बोली का भी प्रमुख योगदान है। गढ़वाली बोली के पीछे एवं स्थापना के पीछे दरद या खस से मानते है। गढ़वाली साहित्य के प्रमुख कवि हरिराम धस्माना ने वेद महिला पुस्तक में गढ़वाली और वैदिक संस्कृत शब्दों की सूची तैयार की । जिसके आधार पर माना जाता है कि गढ़वाली में कई शब्दों का प्रयोग भौतिक रूप में किया गया है।
बोली की दृष्टि से गढ़वाली बोली को 8 भागों में बांटा गया है जिसका श्रेया डॉक्टर ग्रियर्सन को जाता है। यह 8 भाग मुख्य रूप से इस प्रकार से हैं श्री नगरी, नागपुरिया, दासौल्य, बधाणी, मांझ, कुमोऊं, राठी, सालानी एवं टिहरयाली।
जौनसारी – गढ़वाल क्षेत्र के जौनसार एवं बाबर क्षेत्र में इस बोली का उपयोग अधिक किया जाता है।
भोटिया – यह बोले मुख्य रूप से चमोली एल्बम पिथौरागढ़ के दूरदराज इलाकों में बोली जाती है।
खड़ी हिंदी – खड़ी हिंदी भाषा उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून एवं रुड़की के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है।
निष्कर्ष – दोस्तों आज के लेख में हमने आपको उत्तराखंड के लिए भाषाएं एवं गोली के बारे में जानकारी दी। जिसके अंतर्गत हमने जाना कि उत्तराखंड में गढ़वाली एवं कुमाऊंनी बोली मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती है।
आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया होगा यही आपको यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ जरूर साझा करें। उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक एवं इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।
उत्तराखंड राज्य परिचय. Uattarakhand Parichay
हेलो दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज हम आप लोगों के साथ उत्तराखंड का संपूर्ण परिचय से संबंधित जानकारियां साझा करने वाले हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देव भूमि उत्तराखंड अपने सांस्कृतिक कला एवं परंपराओं के लिए पूरे देश विदेशों में मशहूर है ठीक उसी प्रकार से इसे ऐतिहासिक तौर पर भी देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इस लेख के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड का संपूर्ण परिचय देना चाहते हैं।
उत्तराखंड के बारे में. Uttarakhand Ke baren Me
प्रसिद्ध राज्य उत्तराखंड भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। जो कि अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के तौर पर एक नई पहचान बनाया हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को स्थापना की गई। इससे पहले उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। लोगों की एक अलग मांग के कारण उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग किया गया और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के रूप में एक नई राज्य की नींव रखी गई। जबकि 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड में परिवर्तित हो गया। पहले इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था।
उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल एवं पश्चिम में हिमाचल और उत्तर में तिब्बत राज्य स्थित है। भारत का 26 वा राज्य के रूप में सामने आया जबकि हिमालय क्षेत्र का यह दसवां राज्य है। प्राचीन काल से ही उत्तराखंड दिव्य आत्माओं का निवास स्थान रही है इसलिए इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य को दो भागों में बांटा गया है गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल। हिंदू शास्त्रों के अनुसार उत्तराखंड के कुमाऊं को मानस खंड एवं गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि की संज्ञा दी गई है।
उत्तराखंड राज्य में हिंदू धर्म की पवित्र एवं भारत की सबसे बड़ी नदियां गंगा और यमुना का उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री से माना जाता है। इन नदियों के तट पर बसे वैदिक संस्कृति के पवित्र तीर्थ स्थान भी शामिल हैं। जिन्हें भारत के तीर्थ स्थलों के रूप में भी जाना जाता है। बताना चाहेंगे कि भारत के चार छोटे धाम यमुनोत्री, गंगोत्री एवं केदारनाथ, बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में ही शामिल है।
उत्तराखंड राज्य भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है जहां पर पर्यटन एवं राज्य की संस्कृति को मुख्य स्रोत माना जाता है। बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण उत्तराखंड भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। जहां पर हर साल लाखों की संख्या में देश विदेशों से पर्यटक आया करते हैं। चार छोटे धामों का घर होने के कारण इस राज्य का विशेष महत्व है। ठीक उसी तरह से राज्य की संस्कृति भी राज्य की प्रसिद्धि का एक कारण है।
राज्य की संस्कृति एवं परंपराएं वहां के लोगों के रहन-सहन से झलकती है। उत्तराखंड के पारंपरिक पोशाक इस राज्य को विशेष स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। राज्य के पारंपरिक पोशाक मुख्य रूप से गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में अलग-अलग तरीके से पहने जाते हैं। उत्तराखंड को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। उत्तराखंड संस्कृति को जीवंत रखने के लिए उत्तराखंड के लोगों द्वारा आज के समय में भी विभिन्न प्रकार के त्यौहार एवं लोक पर्व बनाए जाते हैं। यह मेले मुख्य रूप से राज्य के लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जो कि उनकी संस्कृति एवं कलाओं को प्रदर्शित करती है।
उत्तराखंड के भौगोलिक संरचना. Geographical Structure of Uttarakhand In Hindi
उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का 18 वां राज्य है। एक पर्वतीय राज्य होने के कारण राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय है। उत्तराखंड राज्य का 86% भाग पर्वतीय है इसमें से 65% भाग जंगलों से ढका हुआ है। उत्तराखंड राज्य भारत का 26 वां राज्य है जो 28°43′ से 31° 27′ उत्तरी अक्षांशों तथा 77° 34′ से 81°02′ पूर्वी देशांतर तक है। उत्तराखंड राज्य भारत का दसवां हिमालय राज्य के रूप में जाना जाता है।
उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर है जो कि भारत देश की संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 1.69 प्रतिशत है। प्रसिद्ध राज्य उत्तराखंड में 13 जिले स्थित है जबकि देहरादून राज्य की राजधानी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बताना चाहेंगे कि असम राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण मानी जाती है।
सन 2022- 23 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 17 लाख 99 आगे गई है। जिसमें से पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 5960315 मानी गई है। जबकि महिलाओं की जनसंख्या लगभग 5739784 आंकी गई है। जो कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 0.85 प्रतिशत हैं।
सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 1,00,86,349 थी जो कि 2022 में बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख 99 हो गई है।

उत्तराखंड राज्य का इतिहास. History of Uttarakhand State In Hindi
उत्तराखंड का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में विभिन्न राजाओं का शासन माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कुर्मांचल क्षेत्र को मानस खंड के नाम से जाना जाता था। मानस खंड का कुर्मांचल व कुमाऊं नाम चंद राजाओं के शासन काल से प्रचलित हुआ। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मान्यता है कि चंद राजाओं का शासन कत्युरियों के बाद माना जाता है। 1790 से 1815 ईस्वी तक कुमाऊं पर गौरखाओ का शासन रहा। उत्तराखंड राज्य का इतिहास में गोरखाओ के शासन के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के अधिकांश भागों पर गौरखाओ का शासन रहा। अंग्रेजों ने उत्तराखंड में राज करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारतीयों को उसमें रोजगार देने का कार्य शुरू किया जिससे कि धीरे-धीरे भारतीय मूल के लोग अंग्रेजों के गुलाम बनते गए।
इतिहास के पन्नों से ज्ञात होता है कि केदारखंड कई गढ़ों में विभक्त था। और इन प्रमुख गढ़ों पर विभिन्न राजाओं का राज हुआ करता था। इतिहासकारों के अनुसार पंवार वंश के राजा ने इन सभी गढ़ों को अपने अधीन करके गढ़वाल राज्य की स्थापना की और उसकी राजधानी प्राय श्रीनगर में स्थापित कि ।
1949 में पहरी राज्य का विलय संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के 1 जिले के रूप में किया गया। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध वह मध्य नजर रखते हुए उत्तराखंड वासियों द्वारा नए राज्य की मांग की गई जिसके फलस्वरूप 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के रूप में एक नया राज्य बनाया गया है। नए राज्य के मांग की मुख्य कारण उत्तराखंड मूल के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से माना जाता है।
उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था. Economy of Uttarakhand State In Hindi
उत्तराखंड राज्य भारत का एक पर्वतीय राज्य है। इसलिए राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि कार्यों पर निर्भर रहती है। आज के समय में भी उत्तराखंड की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों के माध्यम से ही अपना पालन पोषण किया करती है। जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का हिस्सा भी सर्वोत्तम माना जाता है जिसका मूल कारण है उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य। उत्तराखंड में कृषि मुख्य रूप से मौसम पर निर्भर है क्योंकि पहाड़ के अधिकांश भागों में सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने के कारण किसानों को मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है जबकि मैदानी क्षेत्र जैसे कि देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार आदि जगह में सिंचाई के पर्याप्त साधन होने से कृषि उत्पादों के उत्पादन में बढ़ोतरी देखी जा सकती हैं। लेकिन राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय है जिसके कारण पहाड़ में बसे लोग परंपरागत कृषि के तौर तरीकों से अपनी आजीविका उत्पन्न किया करते हैं।
राज्य के प्रमुख उत्पादों में गेहूं, चावल के अलावा गन्ना एवं सरसों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में आधुनिक कृषि के यंत्रों का उपयोग करके उत्पादन की मात्रा में बढ़ोतरी की जाती है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी दालें एवं गेहूं, तिलहन के साथ धान एवं मडुवे का उत्पादन किया जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में सीडी नुमा खेत पाए जाते हैं।
सन 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2,76,677 करो रुपए होने का अनुमान है। जिसमें बीते वर्ष के अनुसार 9% की वृद्धि हुई है। जीडीपी के अनुसार उत्तराखंड का स्थान भारत में 20वें स्थान पर आता है।
उत्तराखंड राज्य की संस्कृति. Culture of Uttarakhand State In Hindi
उत्तराखंड की संस्कृति राज्य को एक विशेष पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका निभाती है। आज के समय में उत्तराखंड की संस्कृति इतनी मशहूर है कि इसे हर कोई अपनाना चाहता है। यही कारण है कि देश विदेशों में भी उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखी जा सकती हैं। उत्तराखंड की संस्कृति के मुख्य तत्व राज्य के पारंपरिक भोजन के पकवान एवं उत्तराखंड राज्य के पारंपरिक पोशाक शामिल है । इनके अलावा भी राज्य की वस्तु एवं शिल्प कला उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में मदद करते हैं। इन सभी तत्वों के बिना उत्तराखंड की संस्कृति अधूरी मानी जाती है।
माना जाता है कि किसी भी राज्य की संस्कृति वहां के लोगों के रहन-सहन के माध्यम से प्रस्तुत होती है ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य की संस्कृति उत्तराखंड राज्य के लोगों के पारंपरिक पोशाक एवं उनके दैनिक जीवन में बनाए गए पारंपरिक खानपान से प्रस्तुत होती है। चलिए एक नजर उत्तराखंड की संस्कृति के प्रमुख तत्वों की ओर डालते हैं।
उत्तराखंड के पारंपरिक पोशाक. Traditional dress of uttarakhand
उत्तराखंड भारत के उन राज्यों में से एक है जहां की संस्कृति की झलक वहां के पारंपरिक पोशाक से प्रदर्शित होती हैं । वाकई में उत्तराखंड संस्कृति की झलक वहां के लोगों के रहन सहन के साथ उनके पारंपरिक पोशाक से झलकती है। सामान्यतः यहां के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सामान्य कपड़े पहनते हैं लेकिन किसी खास त्यौहार एवं पर्व के समय हैं यहां के लोग अपने पारंपरिक पोशाक में उतरते हैं। और उसके बाद जो उनकी खूबसूरती होती है वह वाकई में चार चांद लगने जैसी होती है।

गढ़वाली पुरुषों के पोशाक – कुर्ता, मिरजाई, सफेद टोपी, पगड़ी, बास्कट, धोती, पायजामा,
गढ़वाली स्त्रियों के पोशाक – पिछोड़ा, धोती, गाती, आगड़ी, आदि।
गढ़वाली बच्चों के कपड़े – झगली, घाघरा, कोट, संतराथ, चूड़ीदार पाजामा, आदि
कुमाऊनी महिलाओं के कपड़े – घागरी, आगड़ा, खानू आगड़ी, धोती, पिछोड़, आदि
कुमाऊनी पुरुषों के परिधान – पैजामा, धोती, सुराव, कोट, कुर्ता, कमीज, टांक, टोपी, भोटू।
कुमाऊनी बच्चों के कपड़े – संतराथ, झगुल, कोट, लम्बी फ्रॉक।
उत्तराखंड राज्य का खान पान. Food of uttarakhand state In Hindi
उत्तराखंड राज्य के भोजन के व्यंजन राज्य की संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग है। उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन के व्यंजन लोगों के रहन-सहन एवं वहां की संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वाकई में उत्तराखंड के भोजन के लिए उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने का कार्य करते हैं । पोषक तत्वों से भरपूर यहां के पारंपरिक भोजन शुद्ध होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक होते हैं। उत्तराखंड के बारे में एक तथ्य यह भी है कि यदि आप उत्तराखंड जाओ तो आपको वहां का पारंपरिक भोजन जरूर खाना चाहिए। क्योंकि इस पारंपरिक भोजन में कहीं ना कहीं लोगों का प्यारा एवं अपनेपन का अहसास छुपा होता है। शायद इसीलिए पर्यटकों की जुबान से यहां के भोजन के व्यंजनों के बारे में हमेशा अच्छा ही सुना जाता है। उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन के व्यंजन कुछ इस प्रकार से है ।
- मडुवे की रोटी
- चोंसू
- जोली भात
- कपिलु
- कंडेली की भुज्जी
- सिसौन का साग
- गहत की दाल
- फानू
- बाड़ी
- मक्के की रोटी
उत्तराखंड राज्य के प्रमुख त्यौहार. Major festivals of Uttarakhand state In Hindi
जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उत्तराखंड को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर त्योहार सबसे ज्यादा मनाए जाते हैं और बताना चाहेंगे कि इन सभी त्योहारों को मनाने के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व जरूर होता है। ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर यह भी माना जाता है कि उत्तराखंड के लोक पर्व एवं त्यौहार लोगों के द्वारा ही बनाएं जाते हैं इन सभी पर्वों को मनाने के पीछे प्रकृति के नए रूप से लेकर किसी विशेष स्थान एवं व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं।
दीपावली – दीपावली उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो कि हर वर्ष बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। शुभ अवसर पर घर के आंगन के लिपाई पुताई की जाती है एवं ऐपन कला के माध्यम से आंगन को सजाया जाता है।
रक्षाबंधन – श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व उत्तराखंड में भी बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ आयोजित किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड में अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा रक्षा देते है। इसी दिन बहन द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा भी पूर्ण की जाती है।
मकर संक्रांति – जनवरी के शुरुआत में मनाया जाने वाला यह पारंपरिक त्यौहार माघ माह की एक गति को ऐतिहासिक महत्व के साथ मनाया जाता है। इस दिन उत्तराखंड के सभी घरों में घुघुतिया बनाए जाते हैं। छोटे बच्चों द्वारा उन्हें कौवों खिलाया जाता है। इस तरह से उत्तराखंड वासी अपने परंपराओं को संजोते है।

घी सक्रांति – घी सक्रांति हर वर्ष सितंबर माह के मध्य में मनाई जाती है। घी संक्रांति मनाने के पीछे प्रकृति के नए रूप एवं किसानों के उपज की उगने की खुशी में घी संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। घी संक्रांति के दिन घी का सेवन करने का विशेष महत्व माना जाता है।
फूल संक्रांत – सावन माह की शुरुआत में उत्तराखंड का पारंपरिक त्योहार फूल देई आयोजित की जाती है। इस दिन सभी बच्चों द्वारा गांव के सभी घरों के देहलियों में फूल फेंके जाते है और घर की महिलाओं द्वारा उन्हें अनाज एवं अन्य चीज़ें दी जाती है।
पंचमी – पंचमी जिसे उत्तराखंड में उत्तरेनी के नाम से भी जाना जाता है। इस लोक पर्व के दिन जौ के पत्तों की पूजा करके उन्हें मंदिर में चढ़ाया जाता है।
गंगा दशहरा – गंगा दशहरा उत्तराखंड के लोगों में से एक है यह हर वर्ष जेष्ठ दशमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को दशहरा पत्र देते हैं। जिसे घर की देहलियोँ पर लगाने का रिवाज है।
कलाई – कलाई उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लोगों का प्रमुख त्योहार है। कुमाऊं के लोगों द्वारा फसल काटने के उपलक्ष में कलाई त्यौहार मनाया जाता है।
जांगड़ा – जांगड़ा त्योहार महासू देवता का त्यौहार है। जोकि भाद्र मास में हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बिहार में महासू देवता को स्नान कराया जाता है।
उत्तराखंड राज्य के प्रमुख मेले एवं पर्व . Major Fairs and Festivals of Uttarakhand State
जिस तरह से उत्तराखंड में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं ठीक उसी तरह से उत्तराखंड राज्य में मेलों का आयोजन भी बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है। आमतौर पर यह मिले किसी व्यक्ति विशेष एवं स्थान से जुड़े हुए होते हैं जिसके इतिहास एवं महत्व को संजोने के लिए उत्तराखंड के लोग मेलों का आयोजन किया करते हैं। इन मेलों के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति एवं परंपराओं की झलक प्रस्तुत होने के साथ-साथ स्थानीय विक्रेताओं को व्यापार का एक मंच प्राप्त होता है।
नंदा देवी मेला – प्रसिद्ध नंदा देवी मेला हिमालय की पुत्री बिंदा देवी की पूजा अर्चना के लिए प्रत्येक वर्ष भादर शुक्ल पक्ष की पंचमी को हर्ष और उल्लास के साथ आयोजित की जाती है। प्रसिद्ध नंदा देवी का मेला गढ़वाल एवं कुमाऊँ दोनों मंडलों में आयोजित किया जाता है।
सोमनाथ मेला – सोमनाथ मेला उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा राम गंगा के तट पर वैशाख महीने के अंतिम रविवार को सोमनाथ का मेला आयोजित किया जाता है।
स्याल्दे बिखौती मेला – अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट में प्रत्येक वर्ष बेशाख माह के पहले दिन स्याल्दे बिखौती मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला कस्तूरी शासनकाल से मनाया जाता है।
श्री पूर्णागिरी मेला – उत्तराखंड राज्य के चंपावत टनकपुर के पास अन्नापूर्ण शिखर स्थित श्री पूर्णागिरी मंदिर में है प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में पूर्णागिरि का मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला 30 से 40 दिनों तक चलता है।
जौलजीबी मेला – उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में प्रति वर्ष 14 से 19 नवंबर तक जौलजीबी मेला लगता है। इस मेले में जोहार, दारमा, व्यास आदि जनजाति के लोग बहुत संख्या में शामिल होते हैं।

माघ मेला – उत्तराखंड के उत्तरकाशी नगर में प्रति वर्ष 14 जनवरी को माघ मेला आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध माघ मेला 8 दिनों तक चलने वाला मेला है जिसमें खंडार देवता की डोली वह हरि महाराज के ढोल के साथ शुभारंभ किया जाता है।
श्रावणी मेला – श्रावणी मेला उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के जोगेश्वर धाम में प्रतिवर्ष सावन माह में आयोजित किया जाता है यह मेला 1 महीने तक चलता है। जोगेश्वर मंदिर में आयोजित होने वाले इस मेले के बारे में बताया जाता है कि महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दिया हाथ में लेकर पूजा अर्चना करती है।
गौचर मेला – गौचर मेला उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेले में से एक है जो कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में आयोजित किया जाता है। यह मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मेलों में से एक है। मेले में उत्तराखंड की संस्कृति एवं परंपराओं की झलक प्रदर्शित की जाती है।
उत्तरायणी का मेला – हर वर्ष मकर सक्रांति के शुभ अवसर पर गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र के लोगों द्वारा उत्तरायणी मेला आयोजित किया जाता। गोमती एवं सरयू नदी के संगम पर यह मेला कई दिनों तक आयोजित किया जाता है।
उत्तराखंड के प्रमुख चित्रकला शैली. Major painting styles of Uttarakhand
उत्तराखंड की चित्रकला शैली उत्तराखंड की संस्कृति का एक अंग है जोकि यहां की संस्कृति को प्रदर्शित करती है। उत्तराखंड चित्रकारिता का इतिहास प्राचीन हैं। लेकिन आज भी बहुत से जगह पर यह चित्र कलाएं देखने को मिल जाती है। चित्रकला की विभिन्न सी शैलियां मौजूद है जो की निम्न प्रकार से हैं।
ऐपण चित्र शैली – ऐपण चित्र शैली का उपयोग मुख्य रूप से चौकी एवं दहलीज को सौंदर्य प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। खास तौर पर
ऐपण चित्र शैली का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं मांगलिक कार्यों के शुभ अवसर पर किया जाता है।
बसोली चित्र शैली – इस चित्र शैली में मुख्य रूप से प्राकृतिक सुंदरता का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। लगभग सन 1950 में बसोली चित्रकला शैली सामने आए। इस शैली के चित्रों में मुगल कला का संबंध देखने को मिलता है।
पोथी चित्रण – पोथी चित्रण शैली का उपयोग पुरोहितों द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। इतिहास से ज्ञात होता है कि इस विशिष्ट शैली का उपयोग जन्म कुंडली एवं पंचायत बनाने के लिए किया जाता था।
गुलेर चित्र शैली – गुलेर चित्र शैली उत्तराखंड की प्राचीनतम चित्रकला शैलियों में से एक है। कांगड़ा कलम चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली के चित्रकार राजा हरिश्चंद्र के कार्य अवधि के माने जाते हैं।
ज्यूंति मातृका चित्र – एक शैली के चित्रों में मुख्य रूप से देवी देवताओं एवं भगवान के रूपों का चित्रण किया जाता था। चित्रकारा द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगों से लकड़ी एवं कपड़ों पर यह शैली प्रदर्शित की जाती थी।
उत्तराखंड के चार छोटे धाम. The four small dhams of Uttarakhand
जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है न केवल यह प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है अभी तो भारत के चार छोटे धामों का घर भी उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड के चार प्रमुख स्थानों में बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं यमुनोत्री, गंगोत्री शामिल। भारतीय इतिहास एवं पौराणिक कथाओं में मैं चार धाम यात्रा का बड़ा महत्व माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इन छोटे चार धामों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। देवों की निवास स्थली होने के कारण उत्तराखंड को देवभूमि की संज्ञा भी दी जाती है।
केदारनाथ धाम. Kedarnath Dham
भारत के चार छोटे धामों में से एक केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है। यहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है बताना चाहेंगे कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11746 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जोकि अपने विशाल शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली के अंतर्गत कटमा पत्थरों के विशाल शिलाखंड को जोड़कर किया गया है।

बद्रीनाथ धाम. Badrinath Dham
बद्रीनाथ धाम भारत के चार छोटे दामों में से एक है जो कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में एवं नारायण पर्वत के मध्य स्थित है। भगवान श्री विष्णु के अवतार बद्रीनारायण को समर्पित यह मंदिर 108 दिव्या देशमों में से एक हैं। समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम मंदिर वैदिक काल का एक प्राचीन अविष्कार माना जाता है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की बद्रीनारायण के रूप में पूजा की जाती है यह बद्री में से एक मंदिर है।

गंगोत्री धाम. Gangotri Dham
गंगा नदी के उद्गम स्थल को गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है यह भारत के चार छोटे दामों में से एक है जो कि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। चार छोटे धामों की यात्रा में इसका ब पड़ाव दूसरे नंबर पर आता है। हिंदू धर्म में गंगोत्री को मोक्षदायिनी माना जाता है। किवदंती है कि यहां की यात्रा करके मनुष्य के इस जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं। प्रसिद्ध में गंगोत्री धाम मंदिर समुद्र तल से 980 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री धाम मंदिर के निर्माण विषय के बारे में बताया जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिर का निर्माण कराया गया था।

यमुनोत्री धाम मंदिर., Yamnotri Dham
यमुनोत्री धाम मंदिर चार छोटे धामों में से एक है। चार धाम यात्रा का यह पहला पड़ाव रहता है जो कि देवी यमुना को समर्पित है। समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम मंदिर काली पर्वत की चोटी पर बनी हुई है। मंदिर के निर्माण के बारे में बताया जाता है कि 1919 में टिहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने यमुनोत्री धाम मंदिर की स्थापना की। यमुना नदी में स्नान मोक्ष प्राप्ति के समान माना गया है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहां पर स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।

उत्तराखंड की प्रमुख भाषाएं. Major languages of Uttarakhand
उत्तराखंड की संस्कृति में वहां की भाषाओं का योगदान विशेष स्थान पर आता है। दरअसल राज्य के लोग वार्तालाप में अपनी बोली का उपयोग किया करते हैं। जिससे उत्तराखंड की संस्कृति एवं उत्तराखंड राज्य को एक उससे महत्व मिलता है तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड में कौन-कौन सी प्रमुख भाषाएं बोली जाती है।
उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से गढ़वाली एवं कुमाऊनी भाषा का उपयोग वार्तालाप के रूप में किया जाता है। दरअसल स्थानीय लोगों द्वारा जिस भाषा में वार्तालाप किया जाता है उन्हें स्थानीय बोली के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाली एवं कुमाऊनी बोली को भी मुख्य रूप से स्थानीय लोगों द्वारा अलग-अलग भागों में बांटा गया है।
पूर्वी कुमाऊनी बोलियां. Eastern Kumaoni Dialects
कुम्मयां – मुख्य रूप से यह बोली नैनीताल से लगे हुए काली कमाई क्षेत्र में बोली जाती है।
असकोटी – यह असकोटी क्षेत्र की बोली है इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव पड़ा हुआ है।
शौर्याली – यह बेली जोहार और पूर्वी गंगोली क्षेत्र में बोली जाती है
पश्चिमी कुमाऊनी बोलियां. Western Kumaoni Dialects
पछाई – यह अल्मोड़ा जिले के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। यहां तक कि गढ़वाल के कुछ क्षेत्र में भी यह बोली बोली जाती है।
दनपुरिया – यह बोले मुख्य रूप से दानापुर किए उत्तरी भाग में बोली जाती है।
जौहरी – जौहरी बोली उत्तराखंड के जौहर व कुमाऊं के उत्तर स्मृति क्षेत्रों में बोली जाती है।
कुमाऊं के प्रमुख साहित्यकार. Prominent writers of Kumaon
- गुमानी पंत
- कृष्ण पांडे
- चिंतामणि जोशी
- लीलाधर जोशी
- शिवदत्त सती
- गंगाधर उपरेती
गढ़वाली बोली. Garhwali dialect
जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती है और यह बोलियां स्थानीय लोगों के वार्तालाप से समाज में आएं। बोली की दृष्टि से ही गढ़वाली को डॉक्टर ग्रियर्सन ने 8 भागों में विभाजित किया है। श्रीनगर, नागपुरिया, सैलानी, की हरियाली आदि प्रमुख हैं।
गढ़वाल के प्रमुख साहित्यकार. Prominent writers of Garhwal
- चंद्रमोहन रतूड़ी
- सत्यनारायण रतूड़ी
- आत्माराम गोरोला
- सत्य शरण
उत्तराखंड राज्य के प्रमुख व्यक्ति. Prominent person of Uttarakhand state
जिस तरह से उत्तराखंड को एक पहचान दिलाने में हर एक चीज का अपना अपना योगदान है ठीक उसी तरह से उत्तराखंड में कुछ ऐसे भी दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया जिनकी बदौलत से आज उत्तराखंड देश विदेशों में भी मशहूर है। और न केवल मशहूर है बल्कि आज अपनी संस्कृति एवं परंपराओं को संजोया हुआ भी है।
बद्री दत्त पांडे
बद्री दत्त पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार में हुआ। इन्होंने अंग्रेजी शासन के प्रति देखें और व्यंग्यात्मक लिखो से प्रहार किया। जिनके कारण कारण यह उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध हुए।
हेमवती नंदन बहुगुणा
धरतीपुत्र के नाम से विख्यात हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी के बुधारी गांव में हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचारों को कम करने एवं आवाज उठाने के लिए हेमंती नंदन बहुगुणा का योगदान विशेष स्थान पर आता है।
जिया रानी
जिया रानी घुमाओ की लक्ष्मी बाई के नाम से भी जानी जाती है। कुमाऊं पर रोहिल्ला और तुर्कों के आक्रमण के दौरान रानी बाग युद्ध में उनका डटकर मुकाबला किया था। कुमाऊं के इतिहास में इन्हें न्याय की देवी भी माना जाता है।
रानी कर्णावती
1531 के अल्मोड़ा युद्ध में महिपति का देहावसान हो जाने के पश्चात उनकी पत्नी कर्णावती ने अपने पुत्र युवराज के वयस्क होने तक राज्य का शासन संभाला। उत्तराखंड के इतिहास में इन्हें नाक काटने वाली रानी के नाम से भी जाना जाता है।
डाट काली मंदिर देहरादून. Daat Kali Mandir Dehradun
नमस्ते दोस्तों जय देव भूमि उत्तराखंड स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग के आज के इस लेख में। आज हम आपको उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर डाट काली मंदिर के बारे में (Daat Kali Mandir Dehradun)जानकारी देने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड संपूर्ण आकर्षक का केंद्र है यहां पर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ धार्मिक स्थलों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के प्राचीन मंदिर है जो कि अपनी दिव्य शक्तियों एवं पौराणिक महत्व के लिए पूरे देश भर में मशहूर है। उन्हीं प्रमुख मंदिरों में डाट काली मंदिर जोकि उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। चलिए आज इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानते हैं।
डाट काली मंदिर देहरादून. Daat Kali Mandir Dehradun
डाट काली मंदिर भारत के प्राचीन एवं प्रमुख मंदिरों में से एक है जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। प्रमुख हिंदुओं का एक मंदिर है जोकि अपने पौराणिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व को संजोया हुआ है। देहरादून नगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह है पवित्र मंदिर मां काली को समर्पित है। समानता है इस मंदिर को मां काली का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के बारे में एक प्रसिद्ध तथ्य यह है कि यह मुख्य सिद्ध पीठों में से एक है।
डाट काली मंदिर का निर्माण लगभग 13 जून 1804 का माना जाता है। मां डाट काली को देवी सती का अंश माना जाता है जो कि भगवान शिव जी की पत्नी थी। मंदिर के निर्माण विषय में कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तब मां काली अभियंता के सपनों में आए थे और उन्होंने दिव्य मंदिर की स्थापना के लिए कहां और महंत सुखबीर गुसेन को माता की मूर्ति प्रदान की।
किवदंती यह भी है कि अंग्रेजों द्वारा दून की घाटी में प्रवेश के लिए
सुरंग बनाने का काम शुरू किया गया। तमाम कोशिशों के चलते हुए भी वह काम
अपने चरम अवस्था पर नहीं पहुंच पाया। क्योंकि यह पवित्र स्थान मां काली (Daat Kali Mandir Dehradun)को समर्पित था। मां डाट काली मंदिर के समीप भद्रकाली मंदिर स्थित है। जहां पर दर्शनार्थी दर्शन के लिए आया करते हैं।
स्थानीय
लोगों की मान्यता है कि मां डाट काली का शेर जिनके पैर में सोने का कड़ा
होता है। मैं आज भी शिवालिक पर्वत श्रेणी में घूमते हैं।
मां डाट काली मंदिर से जुड़े प्रमुख तथ्य. Daat Kali Mandir Dehradun
पवित्र मंदिर मां डाट काली के बारे में बताया जाता है कि मंदिर में एक दिव्य ज्योति है जो कि 1921 से लगाकर जल्दी आ रही है।
स्थानीय मान्यता है कि जब भी कोई नए वाहन खरीदते हैं तो वहां मां डाट काली के मंदिर में जरूर पूजा करते हैं।
मंदिर के बारे में एक प्रमुख विशेषता यह भी मानी जाती है कि जो भी वक्त यहां पर सच्चे मन से कामना करते हैं मां काली उनकी मनोकामना जरूर करती है।
वैसे तो इस मंदिर में श्रद्धालु आते रहते हैं लेकिन खासतौर पर नवरात्रि के समय दिव्य मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों का आवागमन लगा रहता है।
मान्यता है कि मंगलवार से 11 दिन तक किया गया डाट चालीसा पाठ बड़े-बड़े कष्टों को भी हार लेता है
मां डाट काली मंदिर खुलने का समय. Daat Kali Mandir Dehradun Khulne Ka Samay
प्रसिद्ध मां डाट काली का यह पवित्र मंदिर दर्शनार्थियों के लिए सुबह 5:00 बजे से लेकर 9:00 बजे तक खुला रहता है। इसी बीच सभी दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं और पूजा पाठ करके मां डाट काली से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बताना चाहेंगे कि इस मंदिर में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। इसलिए यदि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ तो फोटोग्राफी जैसी गतिविधियों से दूर रहें।
मां डाट काली मंदिर कैसे पहुंचे. Daat Kali Mandir Dehradun kese pahuchen
मां डाट काली मंदिर देहरादून से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोकि NH-72A के अंतर्गत आता है। देहरादून से मंदिर तक आने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी एवं बस के माध्यम से भी आ सकते हैं।
देहरादून तक आप सड़क मार्ग के साथ-साथ रेल मार्ग एवं वायु मार्ग के द्वारा भी पहुंच सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 250 किलोमीटर है। दिल्ली के साथ-साथ अन्य प्रसिद्ध शहरों से देहरादून के लिए बस सेवा नियमित रूप से चलती रहती है।
मां डाट काली का नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून है जो कि यहां से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप चाहे तो देहरादून रेलवे स्टेशन से ऑटो एवं प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से भी आ सकते हैं। जबकि मां डाट काली मंदिर का नजदीकी एयरपोर्ट जौलीग्रांट है जहां से मंदिर की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आप बस एवं स्थानीय पक्षियों के माध्यम से भी आ सकते हैं ।
दोस्तों यह तो हमारा आजकल एक जिसमें हमने आपको मां डाट काली के पवित्र मंदिर के बारे में जानकारी दी। आशा करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड का आपको यह लेख पसंद आया होगा। यदि आपको यह नहीं पसंद आया है तो अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।
मुक्तेश्वर मंदिर उत्तराखंड. Mukteswar Mandir
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के आज की नई लेख में। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर के बारे में (Mukteswar Mandir )जानकारी देने वाले हैं। मंदिर के बारे में एवं उसकी पौराणिक इतिहास के बारे में जाने के लिए इसलिए को अंत तक जरूर पढ़ना। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा।
मुक्तेश्वर मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जोकि सुंदर से पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। आस्था एवं भक्ति भावना से ओतप्रोत यह मंदिर ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व को संजोया हुआ है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहां पर सच्चे दिल से कामना करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है।
मुक्तेश्वर मंदिर सुंदर से पहाड़ों के बीच में स्थित समुद्र तल से 2315 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य एवं नंदा देवी पर्वत के खूबसूरत मनमोहक हास्य यहां से देखे जा सकते हैं। जोकि भक्तों के आगमन का मुख्य कारण है। प्रसिद्धमुक्तेश्वर मंदिर मुक्तेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है।
यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव जी के प्रसिद्ध देवालय में से एक है । पुराणों में इस मंदिर के बारे में बताया गया है कि यहां शालीनता के रूप में भगवान शिव के 18 मंदिरों में से एक है। जोकि नैनीताल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का इतिहास एवं पौराणिक मान्यता वास्तव में इस मंदिर को बहुत खास बनाती है ।
जैसे ही आप लोग सड़क से मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो मंदिर में प्रवेश के लिए 100 से भी अधिक सीढ़ियां चढ़ने पड़ती है फिर चढ़ने के बाद जब प्रांगण दिखाई देता है। मंदिर में प्रवेश करते ही हम देख पाएंगे कि भगवान शिव जी की एक अनुपम प्रतिमा के साथ भगवान विष्णु एवं मां पार्वती के साथ हनुमान जी की प्रतिमाएं भी विद्यमान है। मंदिर के आसपास विभिन्न प्रकार के सदाबहार पेड़ पौधे हैं जिनकी छाया में श्रद्धालु विश्राम किया करते हैं।
मुक्तेश्वर मंदिर का इतिहास.Mukteswar Mandir ka itihas
मुक्तेश्वर धाम मंदिर का इतिहास प्राचीन है। मंदिर के निर्माण विषय में आज भी किवदंती है कि लगभग मंदिर का निर्माण 350 वर्ष पहले हुआ था। वास्तव में इस मंदिर की निर्माण कला एवं निर्माण शैली से ज्ञात होता है कि यह मंदिर कई युगों पुरानी है। मुक्तेश्वर मंदिर की इतिहास के बारे में (Mukteswar Mandir ka itihas)किंवदंती है कि भगवान शिव जी इस स्थान पर तपस्या में लीन रहा करते थे। मंदिर निकट स्थित चौली की जाली के बारे में बताया जाता है कि शिवरात्रि के दिन संतान सुख की कामना के साथ कोई भी महिला पत्थर पर बने उस छेद को पार कर दी है तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। मंदिर की मान्यता एवं आस्था की सत्यता के बारे में लोगों का कहना है कि वाकई में भगवान शिव जी भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। शायद इसीलिए यहां पर शिवरात्रि के दिन हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित होती है।
मुक्तेश्वर मंदिर कैसे पहुंचे. Mukteswar mandir Kese Pahuchen
मुक्तेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग के साथ-साथ रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विकल्प भी उपलब्ध है आप चाहे तो किसी भी माध्यम से मुक्तेश्वर धाम मंदिर तक पहुंच सकते हैं।
सड़क मार्ग से मुक्तेश्वर मंदिर – मुक्तेश्वर मंदिर सड़क मार्ग से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है । जिसके कारण सभी लोग यहां आराम से पहुंच सकते हैं। यह दिल्ली से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश की राजधानी देहरादून से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आप बस के माध्यम से आराम से यहां तक पहुंच सकते हैं।
रेल मार्ग से मुक्तेश्वर मंदिर – मुक्तेश्वर का नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम हैं। काठगोदाम से मुक्तेश्वर की दूरी मात्र 70 से 75 किलोमीटर है। जहां के लिए आप किराए की टैक्सी यहां बस के माध्यम से भी आ सकते हैं।
मुक्तेश्वर मंदिर हवाई मार्ग द्वारा- मुक्तेश्वर हवाई मार्ग द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। मुकेश का नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर है। जहां से मुक्तेश्वर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। यहां से मुक्तेश्वर के लिए गाड़ियां चलती रहती है। आप चाहे तो बस एवं किराए की टैक्सी लेकर भी मुक्तेश्वर धाम मंदिर में पहुंच सकते हैं।
शीतला माता मंदिर उत्तराखंड. Sheetla Mata Mandir Uttarakhand
नमस्ते दोस्तों जय देव भूमि उत्तराखंड स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग के आज के नए लेख में आज की इस ले के माध्यम से हम आपको शीतला देवी मंदिर उत्तराखंड (Sheetla Mata Mandir Uttarakhand) के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही देवों की भूमि रही है और इन्हीं देवों की भूमि में आज भी ऐसे पवित्र स्थल है जो अपने ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के लिए पहचाने जाते हैं। उन्हीं पवित्र मंदिरों में से एक है शीतला देवी मंदिर जोकि उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित है। आज हम आप लोगों के साथ शीतला माता मंदिर का इतिहास (Sheetla Mata Mandir History) एवं शीतला माता मंदिर क्यों प्रसिद्ध है (Sheetla Mata Mandir Manyta ) आदि के बारे में जानकारी देने वाले आशा करते हैं कि आपको यह लेख जरूर पसंद आएगा।
प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित है जो कि नैनीताल रोड पर 7 किलोमीटर की दूरी पर काठगोदाम नामक जगह पर पहाड़ी चोटी पर स्थित है। आसपास के जगहों का यह एक प्रसिद्ध मंदिर शीतला माता मंदिर है जो कि बहुत ही मान्यताओं के साथ यहां पर पहचानी जाती है। प्रकृति के विहंगम वादियों के बीच में स्थित शीतला माता मंदिर आस्था एवं भर्ती का प्रसिद्ध केंद्र बना हुआ है। सालाना हजारों की संख्या में दर्शनार्थी जहां पर दर्शन के लिए आया करते हैं। आसपास प्राकृतिक सुंदरता एवं शुद्ध वातावरण होने के कारण यह जगह लोगों को बहुत लुभाती है। मंदिर प्रांगण की बात की जाए तो विशिष्ट शैली से निर्मित शीतला माता मंदिर आकर्षक डिजाइन से तैयार किया गया है। मंदिर में माता शीतला देवी के अलावा अन्य स्थानीय देवी देवताओं की प्रतिमा भी है जो की मंदिर की हास्य को और ज्यादा आकर्षक एवं मनमोहन बनाते हैं।
ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर माना जाता है कि इस मंदिर के पीछे चंद राजाओं के समय में हाट बाजार लगाया जाता था। जिसमें दूर-दूर से लोगों की भीड़ एकत्रित होती थी और वह यहीं से सामान खरीदा करते थे।
शीतला माता मंदिर का इतिहास. Sheetla Mata Mandir History
शीतला माता मंदिर अपने अद्भुत इतिहास के लिए पहचाने जाती है। किवदंती है कि भीमताल की पंडित बनारस में जाकर शीतला माता मंदिर की मूर्ति को वहां से लाए थे। जब वह माता के इस पवित्र प्रतिमा को ला रहे थे तो उन्हें रास्ते में रात हो गई एवं पहाड़ी रास्ते खराब होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाए। उस रात उन्होंने रानी बाग के गुलाम घाटी में विश्राम करना निश्चित किया। मध्य रात्रि में उन्हीं व्यक्तियों में से एक ही सपने में माता शीतला देवी ने दर्शन दिए और उन्होंने बंदे को यहीं स्थापित करने के लिए आज्ञा दी। उसके बाद सभी लोगों ने यहां पर मंदिर बनाने का विचार किया और माता शीतला देवी का एक सुंदर सा मंदिर निर्माण की आज ओके आज के समय में एक ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहां पर सच्चे दिल से कामना करते हैं मां शीतला देवी उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है।
मां शीतला देवी मंदिर मान्यता. Sheetla Mata Mandir Manyta
माता शीतला देवी के मंदिर की एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि बताया जाता है कि जब छोटे बच्चों को कोई भी छोटी मोटी बीमारी आती है तब बच्चों को माता शीतला देवी के मंदिर में लाया जाता है। माता की कृपा से वह बच्चे खुद ही ठीक होने लगते हैं। माता शीतला उन्हें शीतलता प्रदान करती है। मां शीतला देवी की मंदिर की मैंने तो हमें यह भी कहा जाता है कि मंदिर के समीप ही एक बड़ा सा बांस का वृक्ष है जिसके नीचे मां भगवती उमा देवी ने विश्राम किया था।
माता शीतला देवी मंदिर कैसे पहुंचे. Sheetla Mata Mandir Kese Jayen
दोस्तों यदि आप भी माता शीतला देवी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं और माता शीतला देवी मंदिर कैसे पहुंचे के बारे में सोच रहे हैं तो (sheetla Mata Mandir Kese Jayen ) हम आपको बताना चाहेंगे कि मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग सबसे अच्छा माध्यम है क्योंकि माता शीतला देवी मंदिर सड़क मार्ग से कुछ ही दूरी पर स्थित है।
रेल मार्ग द्वारा
यदि रेल मार्ग द्वारा माता शीतला देवी मंदिर पहुंचने के बारे में बात करें तो बताना चाहेंगे कि माता शीतला देवी मंदिर हल्द्वानी से (sheetla Mata Mandir from haldwani )लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम में स्थित है जो कि जोकि मंदिर से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप आराम से किराया की टैक्सी की माध्यम से यहां तक पहुंच सकते हैं।
वायु मार्ग द्वारा
माता शीतला देवी का नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है जहां से मंदिर की दूरी मुश्किल से 30-35 किलोमीटर है आप पंतनगर से टैक्सी एवं बस के माध्यम से भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं।
मुक्तेश्वर में घूमने की जगह. Mukteswar Ghumne Ki Jagah
हेलो दोस्तों नमस्ते कैसे हैं आप सभी लोग आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। देवभूमि उत्तराखंड के आज के ब्लॉग इस लेख में हम आपको मुक्तेश्वर घूमने की जगह के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप भी अपने परिवार के साथ यात्रा करने का विचार बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी यात्रा उत्तराखंड में करें। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता के साथ करें तो आज हम उन्हें खूबसूरत जगह में से एक मुक्तेश्वर में घूमने की जगह के बारे में जानकारी देने वाले हैं आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा।
लेकिन यात्रा करने से पहले एवं यात्रा की जानकारी देने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी मुकेश्वर के बारे में देना चाहिए़ ताकि आप अच्छे से अपनी यात्रा की योजना बना पाए। और आप अपने परिवार के साथ यात्रा करने के लिए तैयार हो सके।
मुक्तेश्वर के बारे में. Mukteswar ke Bare Main
मुक्तेश्वर भारत के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का एक खूबसूरत सा पर्यटन स्थल है जो की समुद्र तल से 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह जगह खूबसूरत पहाड़ों के मध्य में स्थित है। यह स्थल मुख्य रूप से नैनीताल से 50 किलोमीटर की दूरी पर एवं हल्द्वानी से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस खूबसूरत यात्रा योजना में पहाड़ के खूबसूरत वादियों के साथ-साथ क्लाइंबिंग एवं रोपलिंग आनंद भी ले सकते हैं।
मुक्तेश्वर का मौसम. Mukteswar Ka Mosam
शहर की तपतपाती गर्मी से मुक्तेश्वर आपको कहीं ना कहीं निजाता दिलाने वाला है। प्रकृति की सुरम्य घाटियों के बीच में स्थित मुक्तेश्वर अपनी खूबसूरत मौसम के लिए पूरे वर्ष भर प्रसिद्ध रहता है। गर्मी के समय में यहां का मौसम पर्यटकों को शहर की गर्म आवोहवा से ठंडक प्रदान करता है। गर्मियों के समय में यहां का तापमान सामान्य 15 डिग्री के आसपास बना रहता है जिसके कारण यह जगह हमेशा ठंडी बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार से सर्दियों के समय में मुक्तेश्वर का तापमान 5 डिग्री के आसपास बना रहता है। जबकि कभी-कभी बारिश होने के कारण यहां का तापमान माइनस में भी चला जाता है। उस समय यहां पर प्रकृति के खूबसूरत वादियां बर्फ से ढकी हुई दिखाई देती है।
वैसे तो मुक्तेश्वर में घूमने की जगह बहुत सी है(Mukteswar Ghumne Ki Jagah) लेकिन आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी जनों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। यह सभी जगह मुक्तेश्वर की आस पास की होने वाली है और इन सभी जगहों के दर्शन आप अपने परिवार के साथ कह सकते हैं। मक्केश्वर यात्रा योजना की जानकारी केवल आप ही लोगों के लिए बनाई गई है। आप अपनी यात्रा के दौरान इन सभी जगहों के दर्शन आराम से कर सकते हैं।
मुक्तेश्वर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह भालू गाड़ झरना.
मुक्तेश्वर में घूमने की जगह किस श्रेणी में सबसे पहले हम आपको लेकर
चलने वाले हैं भालू गाड़ झरना में। प्रकृति की बहुत करीब यह जगह अपने
खूबसूरत वातावरण के साथ एक सुंदर से बहते हुए झरने के लिए प्रसिद्ध है।
झरना मुक्तेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । जहां के लिए आप
किराए की गाड़ी भी ले सकते हैं।
यहां पर आपको लगभग 60 फीट ऊंचा झरना
मिलने वाला है इस जलने के बारे में बताया जाता है कि इसका पानी का प्रभाव
पूरे वर्ष भर बना रहता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह है खूबसूरत
होने के साथ-साथ उन्हें आनंदित ली करने वाली है।

लेकिन यात्रा करने से पहले हम आपको बता दें कि भालू गाड़ झरना मै यात्रा करने के लिए स्थानीय पंचायत द्वारा ₹20 प्रवेश शुल्क के रूप में लिया जाता है। यदि आपको नहीं पता कि आप किस तरीके से इस खूबसूरत सी झील का आनंद ले सकते हैं। तो स्थानीय पंचायत द्वारा ₹200 का ट्रैवल गाइड शुल्क लिया जाता है जिसमें वह आपको यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
मुक्तेश्वर में घूमने के लिए जगह मुक्तेश्वर महादेव मंदिर.
मुक्तेश्वर के धार्मिक स्थलों में (Mukteswar ke mandir ) सबसे प्रमुख स्थान पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का नाम आता है । समुद्र तल से 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर पहाड़ी चोटी पर बनी हुई है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है लेकिन जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको मंदिर में भगवान शिव जी की प्रतिमा के साथ भगवान विष्णु, पार्वती एवं हनुमान जी की प्रतिमा के साथ अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं भी दिखाई देती है । मंदिर के प्रांगण एवं मंदिर तक पहुंचने के लिए 100 सीढ़ियां चढ़ने पड़ती है। आस्था एवं भक्ति का प्रतीक इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जो भी वक्त यहां पर सच्चे मन से कामना करते हैं भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। हर वर्ष हजारों की संख्या में भक्तों का आना जाना यहां पर लगा रहता है। प्राकृतिक सुंदरता एवं आसपास का वातावरण काफी खूबसूरत होने के कारण यह पर्यटकों के मन को खूब लुभाती है इस जगह से नंदा देवी एवं त्रिशूल आदि हिमालय पर्वतों के दर्शन भी हो जाते हैं।

मुक्तेश्वर के पर्यटन स्थल धानाचुली.
देवभूमि उत्तराखंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य इसकी मुख्य पहचान है। और उन्हीं खूबसूरत जगह में से एक है धानाचुली जो कि नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर क्षेत्र में स्थित हैं। खूबसूरत पहाड़ियां एवं समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह एक छोटा सा गांव है। जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं संस्कृति के लिए भी मशहूर है। परिवार के साथ यात्रा करने के लिए गई है एक अच्छी जगह है।
मुक्तेश्वर की सबसे खूबसूरत जगह शीतला गांव
मुक्तेश्वर के सबसे हसीन वादियों के बीच में स्थित शीतला गांव समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित। हिमालय के साथ-साथ नंदा देवी एवं त्रिशूल जैसे हिमपात पर्वत यहां से देखे जा सकते हैं। जो कि हजारों पाठकों को अपनी मनमोहक दृश्यों से लुभाती है। इसी जगह के सामने अपी और नहापा पर्वत है जो नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं। यदि आपको बर्फ देखने का शौक है तो आप अपने परिवार के साथ इस खूबसूरत सी जगह के दर्शन कर सकते हैं यहां से आपको हिमपात एवं बर्फीली चोटियां दिखाई देंगी। जो कि आपकी यात्रा को और अधिक हसीन बनाने वाले।

मुक्तेश्वर की खूबसूरत जगह चौली की जाली
मानो यह जगह प्राकृतिक सौंदर्य को अपने आगोश में लिए बैठे हो। मुक्तेश्वर मंदिर के पीछे यानी कि थोड़ी सी दूरी पर स्थित चौली की जाली मुक्तेश्वर में घूमने के लिए एक अच्छी जगह है जो कि अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको इस खूबसूरती जगह के दर्शन जरूर करना चाहिए। एचडी के दर्शन करने के दौरान आप अपने परिवार के साथ फोटोग्राफी एवं रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग का आनंद भी ले सकते हैं। यह जगह मुक्तेश्वर बाजार से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मुक्तेश्वर मंदिर से ढाई सौ मीटर की दूरी पर स्थित है आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं।
मुक्तेश्वर के पर्यटन स्थल नंदा देवी शिखर
मुक्तेश्वर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ऊंची ऊंची खूबसूरत पहाड़ों के लिए पहचानी जाती हैं। इस जगह आप नंदा देवी पर्वत के मनमोहक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। यह भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 7816 मीटर है। यहां इस चोटी से आप संपूर्ण मुक्तेश्वर के साथ-साथ कई अन्य जगहों के शानदार हास्य देख सकते हैं। नंदा देवी पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य में पूर्व में गोरी गंगा तथा पश्चिमी क्षेत्र में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। यदि आप अपने दोस्तों के साथ मुक्तेश्वर यात्रा के लिए आते हैं तो आप यहां ट्रैकिंग का आनंद भी ले सकते हैं।

मुक्तेश्वर में घूमने के लिए जगह ब्रह्मेश्वर मंदिर
ब्रह्मेश्वर मंदिर मुक्तेश्वर के धार्मिक स्थलों (Mukteswar ke mandir ) में से एक है जो कि चोली की जाली नामक चट्टान के समीप स्थित है। भगवान शिव जी को समर्पित यह मंदिर आस्था एवं भक्ति का प्रमुख केंद्र है जहां पर हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए करते हैं। यह प्रसिद्ध मंदिर सड़क मार्ग से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के निर्माण विषय में क्यों बनती है कि मंदिर का निर्माण 1050 में हुआ था। आज के समय में यह मंदिर देवी-देवताओं की प्रतिमाओं के साथ सुसज्जित हैं।
मुक्तेश्वर का पर्यटन स्थल किल्मोरा शॉप
किल्मोरा मुक्तेश्वर की उन प्रमुख दुकानों में से एक है जहां पर जायका का एक आदर्श स्वाद लिया जा सकता। अपनी स्थानीय उत्पादों के साथ दुकान अपने प्रसिद्धि पर हैं जहां पर आप सर्दियों के वस्त्र एवं स्थानीय उत्पाद अनाज, जड़ी-बूटी आदि विशेष प्रकार की वस्तुएं प्रदान की जाती है। इस दुकान के सामानों की मुख्य विशेषता यह है कि यह समान शुद्ध एवं ऑर्गेनिक तरीके से उगाया एवं बनाया जाता है।
मुक्तेश्वर कैसे पहुंचे. Mukteswar Kese Pahuchen
मुक्तेश्वर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग के साथ-साथ रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विकल्प भी उपलब्ध है आप चाहे तो किसी भी माध्यम से यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
सड़क मार्ग से मुक्तेश्वर – मुक्तेश्वर सड़क मार्ग से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है । जिसके कारण सभी लोग यहां आराम से पहुंच सकते हैं। यह दिल्ली से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश की राजधानी देहरादून से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आप बस के माध्यम से आराम से यहां तक पहुंच सकते हैं।
रेल मार्ग से मुक्तेश्वर – मुक्तेश्वर का नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम हैं। काठगोदाम से मुक्तेश्वर की दूरी मात्र 70 से 75 किलोमीटर है। जहां के लिए आप किराए की टैक्सी यहां बस के माध्यम से भी आ सकते हैं।
मुक्तेश्वर हवाई मार्ग द्वारा- मुक्तेश्वर हवाई मार्ग द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। मुकेश का नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर है। जहां से मुक्तेश्वर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। यहां से मुक्तेश्वर के लिए गाड़ियां चलती रहती है। आप चाहे तो बस एवं किराए की टैक्सी लेकर भी यहां तक पहुंच सकते हैं।
दोस्तों यह था हमारा आज का लेख , जिसमें हमने आपको मुक्तेश्वर में घूमने के लिए जगह के बारें में जानकारी दी आशा करते है की आपको यह लेख पसंद आया होगा, आपको यह लेख केसा लगा हमें टिप्पणी के माध्यम से व्यक्त करें। यदि आप भी ऐसा ही जानकारीयुक्त लेख हम तक पहुंचना चाहते है तो आप हमें ईमेल के माध्यम से भी लिख सकते है।
गौचर मेला उत्तराखंड.Gochar Mela Uttarakhand
मेले उत्तराखंड की शान है देवभूमि की पहचान है मेलों के माध्यम से ही राज्य की संस्कृति को अनोखी एवं अलौकिक छवि प्राप्त होती है। नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग के नए लेख में। आज हम आप लोगों के साथ उत्तराखंड का प्रसिद्ध मेला गौचर मेला के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा।
जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेरे उत्तराखंड की शान है उत्तराखंड की पहचान है। मेलें त्यौहार एवं लोक पर्व के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति एवं परंपराओं को एक अलग पहचान मिलती है। वरन यह मेले अपने पौराणिक इतिहास के साथ उस जगह के महत्व एवं उससे जुड़े लोगों के इतिहास के बारे में महत्व को जागृत करती है। उन्हीं प्रसिद्ध मेला में से एक हैं गोचर मेला जोकि उत्तराखंड के चमोली जिले में हर वर्ष बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। दरअसल यह मेला न केवल लोगों की भीड़ भाड़ एकत्रित करती है बल्कि लोगों की कौशल स्थानीय उत्पाद एवं उत्तराखंड की संस्कृति को भी जीवंत रखती है।
प्रसिद्ध बाजार मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर हर दिन 14 नवंबर को आयोजित किया जाता है। 1 सप्ताह तक चलने वाला यह मेला हजारों लोगों को आकर्षित करता है। मेले के कुछ दिन पहले से ही स्थानीय लोगों एवं समिति द्वारा तैयारियां शुरू की जाती हैं
गौचर मेले का इतिहास. Gochar mele ka itihas
उत्तराखंड में मेले किसी खास महत्व एवं किसी खास समय पर ही आयोजित किए जाते हैं। यह वह समय होता है जब इन पर्वों से जुड़े लोगों की कुछ खास तिथियां होती है जिनमें वह स्मरण के तौर पर मेले के रूप में आयोजित करते हैं। उसी तरह से गाजर मेले के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि 1943 में अंग्रेज कमिश्नर मिस्टर बनोर्डी ने मेले की शुरुआत की थी। मेला शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत और तिब्बत के व्यापार को बढ़ावा देना था। जिसके लिए हर वर्ष 14 नवंबर को बड़ी ही धूमधाम के साथ गोचर मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला 1 सप्ताह तक आयोजित किया जाता है जिसमें स्थानीय व्यापारी अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचाते हैं।
सांस्कृतिक प्रदर्शन है गौचर मेला. Gochar mela uttarakhand
गोचर मेला आज के समय में न केवल एक मेले की तरह आयोजित होता है। बल्कि लोगों के कौशल को परखने एवं स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यह एक आधुनिक माध्यम बना हुआ है। जहां एक तरफ यह मेले उत्तराखंड की सांस्कृतिक छटा को प्रदर्शित करते हैं ठीक उसी प्रकार से यहां स्थानीय उत्पाद को भी बढ़ावा देते हैं । गोचर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जिनके माध्यम से उत्तराखंड संस्कृति प्रदर्शन को एक मंच मिल जाता है। मेले के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले सभी लोग उत्तराखंड के पारंपरिक पोशाक में नजर आते हैं जो कि इस मेले के सौंदर्य को और ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। स्थानीय लोगों की कौशल से बने उत्पाद जैसे कि ऊनी वस्त्र, खिलौने, औजार, एवं स्थानीय उत्पाद जैसे कि शहद, जलेबी, संतरे, स्थानीय दालें प्रमुख है। व्यापारी इन सभी उत्पादों का व्यापार किया करते हैं जो कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड संस्कृति के अंग है और उन के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को एक अलग पहचान मिलती है।
गौचर मेले से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q- गोचर मेला क्या है?
Ans – गोचर उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मेला है जोकि उत्तराखंड के चमोली जिले में हर वर्ष 14 नवंबर को बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। जिसमें हजारों की संख्या में लोग पधार कर मेले के आकर्षक का आनंद लेते हैं।
Q – गोचर मेला कब है 2023 ?
Ans – गोचर मेला 2023 में 14 नवंबर को है। यह मेला हर वर्ष बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। जिसमें यहां के लोग स्थानीय उत्पाद के साथ अपने कौशल को प्रदर्शित करते हैं।
Q – गोचर मेला कब से प्रारंभ हुआ।
Ans – प्रसिद्ध गोचर मेले की शुरुआत सन 1943 से प्रारंभ हुआ। जिसे अंग्रेज कमिश्नर मिस्टर बनोर्डी द्वारा आयोजित किया गया था। मेले का मुख्य मकसद भारत और तिब्बत के व्यापार को बढ़ावा देना था।
Q- गोचर मेला क्यों आयोजित किया जाता है।
Ans – जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मेरे उत्तराखंड की शान होते हैं उत्तराखंड की संस्कृति का अंग होता है इसलिए मेलों का आयोजन पूरी धूमधाम के साथ किया जाता। हालांकि यह मेलें ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व से जुड़े होते हैं।
मां कोकिला देवी मंदिर उत्तराखंड. Kokila Devi Temple Uttarakhand
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज के इस लेख के माध्यम से हम आप लोगों के साथ उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर मां कोकिला देवी मंदिर के बारे में जानकारी (Kokila Devi Temple Uttarakhand) देने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में मां कोकिला के कई पावन धाम है । अपने पौराणिक इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के लिए पहचाने जाते हैं। आस्था और भक्ति के प्रतीक इस मंदिर के प्रति आज भी लोगों का अटूट विश्वास देखने को मिलता है। इस लेख में हम मां कोकिला देवी मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आएगा। इसलिए इसे अंत तक जरूर पढ़ना।
मां कोकिला जो देवी भगवती के नाम से भी जानी जाती है। उत्तराखंड की कुलदेवी मानी जाती है। मां कोकिला देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में कोटा गाड़ी नामक एक गांव में स्थित है। प्रसिद्ध मां कोकिला देवी मंदिर अपनी धार्मिक मान्यता और इतिहास के लिए जानी जाती है।
मंदिर की स्थापना के पीछे बताया जाता है कि स्थानीय व्यक्ति को सपने में देवी के द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के अनुसार मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर में मां कोकिला देवी की प्रतिमा को ढक कर रखा जाता है। मंदिर के नीचे भूगर्भ से जल निकलता है और इस जल को गंगाजल के स्वरूप पवित्र माना गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा इस पवित्र धारा से निकलता हुआ जल को घरों में ले जाया जाता है। मान्यता यह भी है कि इस जल स्रोत का पानी कभी नहीं घटता।
मां भगवती उत्तराखंड की न्याय की देवी (Kokila Devi Temple Uttarakhand)के रूप में भी पूजी जाती है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार जब भी गांव के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं तो वह मां कोकिला मंदिर की मंदिर में न्याय के लिए आया करते हैं।
मां कोकिला मंदिर का रहस्य. Kokila Devi Mandir Rahasay
प्यारी पाठक हो हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा होता है ठीक उसी प्रकार से मां कोकिला देवी मंदिर के पीछे भी रहस्य (Kokila Devi Mandir Rahasay) छुपा हुआ है। कोकिला को न्याय की देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब लोगों सब जगह से निराश होते हैं तो उसके बाद है मां के इस पावन धाम में आते हैं और मां से न्याय की गुहार लगाते हैं। और मां को केला देवी उन्हें न्याय जरूर दिलाती है। मंदिर का एक रहस्य (Kokila Devi Mandir Rahasay) यह भी है कि यहां पर लोग चिट्ठियों में अपने मन्नते मांग कर न्यायिक की गुहार लगाते हैं।
मंदिर के स्थानीय गांव के लोगों द्वारा माता कोकिला के नाम पर जंगलों को दिया गया है। जिस का सदुपयोग यहां के लोगों द्वारा पर्यावरण और जंगल को बचाने के लिए किया जाता है।
मां कोकिला देवी मंदिर पौराणिक मान्यता. Kokila Devi Mandir Manyta
प्यारे पाठको को केला देवी उत्तराखंड की न्याय की देवी के रूप में भी पूजी जाती है। देवी अपने भक्तों को न्याय जरूर दिलाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम ढलने के बाद कोटा गढ़ी गांव के पास स्थित पहाड़ियां फन उठाए खड़े होते हैं। जो कि ठीक नागों की तरह प्रतीत होते हैं मान्यता है कि प्राचीन काल में यह नागों की भूमि हुआ करती थी। इस मंदिर की चोटी से कभी भी गारूड आर पार नहीं जा सकते।
कोकिला देवी मंदिर की पौराणिक मान्यता के अनुसार (Kokila Devi Mandir Manyta) यह भी माना जाता है कि। इस मंदिर की शक्ति पर किसी शस्त्र के बाहर का गहरा निशान दिखाई देता है। इस शक्ति लिंग पर एक गाय आकर स्वयं दूध चढ़ा कर चली जाती है। जब गाय की मालकिन गाय के दूध न देने से परेशान होती है तो एक दिन वह गाय के पीछे यहां पहुंच जाती है और गाय को दुहाते देख लेती हैं।
उसने एक हथियार से उस शक्ति पर वार कर डाला इससे पृथ्वी की ओर खून की धाराएं बहने लगी। आज के समय में भी पृथ्वी पर खून की धारा स्वरूप प्रतीक होता है। मान्यता के अनुसार (Kokila Devi Mandir Manyta)आज के समय में भी इस शक्ति लिंग पर गांव के लोग दूध चढ़ाया करते हैं।
मां कोकिला देवी मंदिर कैसे पहुंचे. Kokila Devi Temple Kese Pahuchen
यदि हम भी मां कोकिला देवी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो बताना चाहेंगे कि। मंदिर के दर्शन करने के लिए सड़क मार्ग सबसे अच्छा विकल्प है। सड़क मार्ग के माध्यम से कोटगाड़ी मंदिर पहुंचा काफी आसान है।
मां कोकिला देवी मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है यहां से लगभग 205 किलोमीटर की दूरी पर मां का पावन धाम स्थित है। यहां से आप प्राइवेट टैक्सी और बस के माध्यम से भी मां के दर्शन कर सकते हैं। कि बंदे का नजदीकी एयरपोर्ट नैनी सैनी हवाई अड्डा है यहां से मन्दिर 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
दोस्तों यह तो हमारा आज का लेख जिसमें हमने आपको मां कोकिला देवी मंदिर के बारे में जानकारी दी। यदि आपको यह नहीं पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।
हनुमान गढ़ी मंदिर नैनीताल. Hanumaan Gari Mandir Nainitaal
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको हनुमान गढ़ी मंदिर नैनीताल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भगवान हनुमान को समर्पित विभिन्न पावन धाम है जिनमें से नैनीताल के माल रोड पर स्थित हनुमान गढ़ी मंदिर अपनी आस्था और भक्ति के लिए पूरे देश परदेश में प्रसिद्ध है। आज के इस लेख में हम हनुमान गढ़ी मंदिर नैनीताल के इतिहास और हनुमान गढ़ी मंदिर नैनीताल (Hanumaan Gari Mandir Nainitaal) के मान्यताओं के बारे में जानकारी साझा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा।
हनुमान गढ़ी मंदिर नैनीताल. Hanumaan Gari Mandir Nainitaal
भगवान हनुमान जी के प्रसिद्ध पावन धामों में से एक हनुमान गढ़ी मंदिर उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पूरे वर्ष भर में हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। नैनीताल के माल रोड के पास स्थित यह हनुमानगढ़ी मंदिर की स्थापना बाबा नीम करोली महाराज द्वारा की गई थी।
समुद्र तल से 6401 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह खूबसूरत सा हनुमान गढ़ी मंदिर भगवान हनुमान ( Hanumaan Gari Mandir Nainitaal) के प्रबल भक्तों के लिए एक मशहूर जगह है। खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ सूर्यास्त सूर्य उदय की मनमोहक प्रस्तुत करता है।
हनुमानगढ़ी मंदिर की वास्तुकला. Hanumaan Gari Mandir Wastukala
भगवान हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी मंदिर की वास्तुकला अपने आप में एक खास महत्व रखती है। मंदिर एक अद्भुत वास्तु कला से निर्मित है। प्रवेश करने पर आप देख पाएंगे कि मंदिर परिसर में मौजूद मंदिरों पर भगवा , सफेद और लाल रंग दिखाई देंगे।
भगवान हनुमान जी की एक सुंदर सी जी गगनचुंबी मूर्ति। मंदिर की सबसे प्रमुख और आकर्षक भाग में से एक है। यहां पर भगवान हनुमान जी एक हाथ में गदा और सिर के ऊपर एक स्वर्ण छत्र स्थापित है।
हनुमानगढ़ी मंदिर नैनीताल का इतिहास. Hanumaan Gari Mandir Nainital Ka Itihas
ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर किंवदंती है कि कलयुग में हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना गया है। इसलिए भगवान हनुमान जी के पावन धाम पूरे देश में विद्यमान है।
बाबा नीम करौली द्वारा यह पवित्र मंदिर 1950 में निर्मित किया गया। मंदिर परिसर में पहुंचने के लिए 70 चरणों की चढ़ाई चढ़ने पड़ती है। हनुमानगढ़ी मंदिर नैनीताल के पास ही शीतला माता मंदिर और लीलाशाह बापू का आश्रम भी है। नैनीताल के तल्लीताल में स्थित यह पावन धाम हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।
हनुमानगढ़ी मंदिर नैनीताल की मान्यताएं. Hanumaan Gari Mandir Nainitaal Manyataye
हनुमान गढ़ी मंदिर नैनीताल कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं जिनके आधार पर इस मंदिर को विशेष स्थानों में से एक माना जाता है। भगवान हनुमान जी के पावन चरणों में से एक हनुमान गढ़ी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त यहां पर सच्चे मन से कामना करते हैं भगवान हनुमान जी उनकी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं।
पौराणिक मान्यता है कि मंदिर निर्माण से पहले बाबा नीम करोली इस जगह पर आया करते थे और एक मिट्टी के टीला के पास बैठकर राम नाम जपा करते थे। उस समय यहां पर घना जंगल था। और मान्यता है कि यह सब देख कर वहां मौजूद पेड़ पौधे भी भगवान राम का नाम जपने लगे।
यह दृश्य देख बाबा नीम करोली जी बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने कीर्तन कराने का फैसला किया। कीर्तन करने के बाद उन्होंने सभी लोगों के लिए प्रसाद भंडारा किया । बताया जाता है कि प्रसाद बनाते समय घी कम पड़ जाता है। जिसे देख बाबा नीम करोली एक पानी का कनस्तर कढ़ाई में डाल देते हैं। और एक रहस्यमई बात यह है कि वह पानी का कनस्तर की के रूप में तब्दील हो जाता है। यहां से देख वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस तरह से कुछ हनुमानगढ़ी मंदिर नैनीताल की ऐतिहासिक मान्यताएं प्रसिद्ध है।
हनुमान गढ़ी मंदिर नैनीताल का प्रवेश समय. Hanumaan Gari Mandir Nainitaal Timing
प्यारे पाठको भगवान हनुमान गढ़ी मंदिर नैनीताल का प्रवेश समय सुबह 5:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और शाम के 4:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक रहता है। भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का क्षेत्र देने की जरूरत नहीं है। यहां पर प्रवेश निशुल्क है।
हनुमानगढ़ी मंदिर नैनीताल कैसे पहुंचे. Hanumaan Gari Mandir Nainitaal Kese Pachuchen
दोस्तों यदि आप भी हनुमानगढ़ी मंदिर नैनीताल के दर्शन करना चाहते हैं तो बताना चाहते हैं कि हनुमान गढ़ी मंदिर तल्लीताल माल रोड से लगभग साडे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग की अच्छी संपर्कता होने के कारण आप सड़क मार्ग को प्राथमिकता दे सकते हैं।
सड़क मार्ग द्वारा
सड़क मार्ग द्वारा हनुमानगढ़ी मंदिर नैनीताल पहुंचना काफी आसान है क्योंकि यह मंदिर सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग की अच्छी संपर्कता होने के कारण आप देश के किसी भी कोने से हनुमानगढ़ी मंदिर नैनीताल के दर्शन कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से यहां मंदिर लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
रेल मार्ग द्वारा
यदि रेल मार्ग द्वारा हनुमानगढ़ी मंदिर नैनीताल पहुंचना चाहते हैं तो मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जहां से मंदिर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आप बस और टैक्सी के माध्यम से भी आ सकते हैं।
वायु मार्ग द्वारा
हनुमानगढ़ी मंदिर नैनीताल का नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है यहां से प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां से सड़क मार्ग द्वारा बस और टैक्सी के माध्यम से भी नैनीताल पहुंच सकते हैं।
दोस्तों यह तो हमारा आज का लेख जिसमें हमने आपको हनुमान गढ़ी मंदिर नैनीताल ( Hanumaan Gari Mandir Nainitaal)के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।
नैना देवी मंदिर नैनीताल. Naina Devi Temple Nainital
हेलो दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज के इस लेख के माध्यम से हम आप लोगों के साथ नैना देवी मंदिर नैनीताल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही दिव्य आत्माओं का निवास स्थान है। उन्हीं दिव्या एवं पवित्र स्थलों में से एक हैं नैना देवी मंदिर नैनीताल जोकि अपने इतिहास और पौराणिक कहानी के लिए पहचानी जाती है। देवभूमि उत्तराखंड के आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको नैना देवी मंदिर नैनीताल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आशा करते हैं दोस्तों की आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा।
नैना देवी मंदिर उत्तराखंड के पवित्र धामों में से एक हैं जोकि राज्य के पर्यटन स्थल नैनीताल स्थित है। नैना देवी मंदिर नैनीताल धर्मों की पीठ पवित्र स्थल है। नैनीताल के नैनी झील के किनारे पर स्थित मल्लीताल में मां नैना देवी का पवित्र धाम है।
मां नैना देवी मंदिर नैनीताल की स्थापना 1842 में मोतीराम शाह द्वारा की गई। जबकि ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर किंवदंती है कि मां नैना देवी का मंदिर सन 1880 में भूस्खलन से नष्ट हो गया था। जिसे बाद में दोबारा बनाया गया।
मां नैना देवी मंदिर नैनीताल में मां नैना देवी की पूजा की जाती है। मां नैना देवी मंदिर की मुख्य खासियत यह है कि यहां पर मां के संपूर्ण प्रतिमा नहीं है बल्कि केवल मां नैना देवी के दो नयन विराजमान है। इन्हीं दो नयनों कि यहां पर पूजा की जाती है।
नैना देवी मंदिर का रहस्य. Naina Devi Mandir Rahasay
मां नैना देवी मंदिर का रहस्य अपने आप में खास महत्व रखता है। यहां आए श्रद्धालुओं को मां नैना देवी मंदिर के रहस्य के बारे में जरूर जाना चाहिए। मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो देखने को मिलता है कि मंदिर में केवल मा नैना देवी के दो नयन विराजमान हैं जिनके प्रति स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है। शायद यही कारण है कि पूरे वर्ष भर में मां नैना देवी मंदिर नैनीताल में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आया करते हैं।
मां नैना देवी मंदिर का रहस्य अद्भुत है किंवदंतियों के आधार पर यह भी माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री उमा का विवाह भगवान शिवजी से हुआ था। जिसका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में भी देखने को मिलता है।
मां नैना देवी मंदिर नैनीताल जब आप प्रवेश करोगे तो आप देख पाओगे कि यहां पर मां नैना देवी का मंदिर मंदिर स्थित है इसी के साथ में मंदिर के प्रांगण में एक विशाल पीपल का पेड़ है जो कि यहां आए भक्तों को आराम प्रदान करता है। मां नैना देवी मंदिर का मुख्य मंदिर दो शेरों की मूर्तियों से गिरा हुआ है। वाकई में मां नैना देवी मंदिर का रहस्य अपने आप में खास स्थान रखता है।
नैना देवी का इतिहास. Naina Devi Mandir Itihas
मां नैना देवी का इतिहास पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार किवदंती है कि दक्ष की पुत्री उमा का विवाह भगवान शिव जी से हुआ था। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे किंतु दक्ष प्रजापति देवताओं के अनुरोध को मना नहीं कर सकते थे इसलिए मां नैना देवी का इतिहास हमें यह बताता है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान शिव जी से किया था।
पौराणिक कहानी के आधार पर माना जाता है कि एक बार दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करवाते हैं। जिसमें वह सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं लेकिन अपनी बेटी उमा और दामाद शिवजी को नहीं बुलाते हैं। लेकिन की बेटी उमा जैसे तैसे करके यज्ञ में पहुंच जाती है। दक्ष प्रजापति द्वारा उनका अपमान किया जाता है जोकि उमा से बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सका।
वह दुखी हो उठती है और हवन कुंड में यह कहते हुए कूद पढ़ती है कि मैं अगले जन्म में सिर्फ सिर्फ को ही अपना पति बनाऊंगी। आपने मेरे पति और मेरा जो अपमान किया है उसके फल स्वरुप यज्ञ की हवन कुंड में स्वयं जाकर आपके यज्ञ को असफल करती हूं।

दोस्तों इस तरह से मां नैना देवी मंदिर का इतिहास पौराणिक कहानियों के आधार पर जानने को मिलता है। इसके बाद जब यह दृश्य देख भगवान शिव जी अत्यंत क्रोधित होते हैं तो वह तांडव करना शुरू कर देते हैं। सभी देवी देवताओं का एहसास होता है कि कहीं भगवान शिवजी सृष्टि पर पलने ना कर दे इसलिए वह दक्ष प्रजापति के साथ सभी लोग माफी मांगते हैं।
जब भगवान शिव जी उमा के जले हुए शरीर को कंधे में लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे तो जिस स्थान पर उमा के अंग गिरे उस स्थान पर शक्तिपीठ हो गाएं। और जिस स्थान पर उमा के नयन गिरे वह स्थान नैना देवी के रूप में प्रसिद्ध हुआ।
प्यारे पाठको वाकई में मां नैना देवी का इतिहास अपने आप में एक खास महत्व रखता है। और देवभूमि उत्तराखंड को एक खास स्थान प्राप्त करता है कि यहां पर आज के समय में भी दिव्य आत्माओं का निवास स्थान है।
मां नैना देवी मंदिर कैसे जाएं. Naina Devi Mandir Kese Pahuchen
प्यारे दोस्तों यदि आप भी मां नैना देवी मंदिर कैसे जाएं प्रसन्न से परेशान हैं तो हम आपको एक ऐसा माध्यम बताने वाले हैं किसके द्वारा आप मां नैना देवी मंदिर नैनीताल के दर्शन आराम से कर सकते हैं।
मां नैना देवी मंदिर नैनीताल पहुंचने का सबसे बढ़िया साधन सड़क मार्ग है सड़क मार्ग के द्वारा मां नैना देवी मंदिर के दर्शन आराम से किए जा सकते हैं। मां नैना देवी का मंदिर नैनीताल में स्थित है जो कि देश के प्रसिद्ध शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
इसके अलावा मां नैना देवी मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून है और मां नैना देवी मंदिर नैनीताल का नजदीकी हवाई अड्डा जौलीग्रांट है यहां से नैनीताल की दूरी मात्र 40- 50 किलोमीटर है । यहां से आप बस एवं टैक्सी के माध्यम से भी अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं।
दोस्तों यह तो हमारा आज का लेख मां नैना देवी मंदिर नैनीताल के बारे में जिसमें हमने आपको मां नैना देवी का इतिहास और मां नैना देवी का रहस्य के बारे में जानकारी दें। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया होगा। यदि आपको यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हमें टिप्पणी के माध्यम से बताएं कि आपको मां नैना देवी मंदिर नैनीताल के बारे में जानकर कैसा लगा।
त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड. Trishul Parwat Uttarakhand
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज के इस लेख के माध्यम से हम आप लोगों के साथ उत्तराखंड का त्रिशूल पर्वत के बारे में (Trishul Parwat Uttarakhand)जानकारी साझा करने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार के धार्मिक और पवित्र स्थल है जो कि अपने इतिहास और पौराणिक कहानियों को अपने में समेटे हुए हैं। इन पर्वतों का उत्तराखंड के इतिहास और उत्तराखंड के जनजीवन में काफी महत्व माना जाता है। उन्हीं स्थानों में से एक है त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड जोकि उत्तराखंड के पवित्र स्थलों में से एक है। आज हम आप लोगों के साथ उत्तराखंड का त्रिशूल पर्वत के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ना।
त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड.Trishul Parwat Uttarakhand
भारत के उत्तराखंड राज्य में समुद्र तल से 23490 फीट की ऊंचाई पर स्थित त्रिशूल पर्वत हिमालय की तीन चोटियों का एक समूह है। तीन शिखरों का समूह होने के कारण है इस पर्वत का नाम त्रिशूल पर्वत रखा गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी के अस्त्र त्रिशूल के नाम से ही इस पर्वत का नाम त्रिशूल पर्वत रखा गया।
त्रिशूल पर्वत के 3 शिखरों में से सबसे पहला शिखर 7120 मीटर जबकि दूसरा शिखर है 6690 और तीसरा शिखर 6007 मीटर ऊंचा है। यह पर्वत पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है इसलिए यह पवित्र होने के साथ-साथ यात्रा का एक वैकल्पिक स्थल भी है।
त्रिशूल पर्वत का फतह सबसे पहले 1960 में ब्रिटिश पर्वतारोही ने किया था। इससे पहले भी कई लोगों ने त्रिशूल पर्वत में करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहे। किवदंती है कि कोई भी पर्वत रोही इस पर्वत के शिखर पर नहीं चढ़ता क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है।
त्रिशूल पर्वत के नीचे एक बेहद खूबसूरत रहस्यमई झील स्थित है जिसका नाम रूपकुंड हैं। रूपकुंड झील मनुष्य और घोड़ों के 600 से अधिक कंकाल पाए जाने के कारण प्रसिद्ध हुआ। इसके निकटवर्ती पर्यटन स्थलों में कौसानी और बेदनी बुग्याल भी स्थित है।
त्रिशूल पर्वत कैसे पहुंचे. Trishul Parwat Kese Pahuche
प्यारे पाठको हो यदि आप भी घूमने के शौकीन हैं और त्रिशूल पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं तो त्रिशूल पर्वत पहुंचने के लिए सड़क मार्ग सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन त्रिशूल पर्वत की चढ़ाई चढ़ने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। ट्रेकिंग के माध्यम से ही आप अपने इस खूबसूरत से सफर को हसीन बना सकते हैं।
त्रिशूल पर्वत का नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार एवं ऋषिकेश हैं इसके अलावा यदि बात की जाए नजदीकी हवाई अड्डे की तो देहरादून त्रिशूल पर्वत का नजदीकी हवाई अड्डा है। इन स्थानों से आप त्रिशूल पर्वत के दर्शन ट्रेकिंग के माध्यम से और अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं।
दोस्तों यह तो हमारा आज का लेख जिसमें हमने आपको त्रिशूल पर्वत के बारे में जानकारी दें। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया होगा यदि आपको यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भी भेज सकते हैं।
त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड F&Q
Q – त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई
Ans – भारत के उत्तराखंड राज्य में समुद्र तल से 23490 फीट की ऊंचाई पर स्थित त्रिशूल पर्वत हिमालय की तीन चोटियों का एक समूह है। त्रिशूल पर्वत को कौसानी और बेदनी बुग्याल से भी देखा जा सकता है।
Q – त्रिशूल पर्वत कहां है
Ans – त्रिशूल पर्वत भारत के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। आस्था और धार्मिक महत्व होने के कारण यह पर्वत पवित्र माना जाता है। तीन शिखरों का समूह होने के कारण इसका नाम त्रिशूल पर्वत रखा गया।
उत्तराखंड की कोसी नदी. Kosi Nadi Uttarakhand
नमस्ते दोस्तों देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में आपका स्वागत है। आज के इस लेख में हम आपको उत्तराखंड की प्रसिद्ध नदी कोसी नदी के बारे में जानकारी ( Kosi Nadi Uttarakhand )देने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड पवित्र धामों का घर है यहां पर मंदिर एवं धार्मिक स्थल के अलावा नदियों का भी अपने आप में पौराणिक एवं ऐतिहासिक मान्यता है। जिसके आधार पर इन्हें पवित्र और कितनी शक्तियों का निवास माना जाता है। आज के इस लेख में हम आपको उत्तराखंड की कोसी नदी के बारे में ( Kosi Nadi Uttarakhand ) एवं कोशी नदी की पौराणिक कहानी के बारे में जानकारी देंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा।
उत्तराखंड की कोसी नदी. Kosi Nadi Uttarakhand
प्यारे पाठको यह लेख उत्तराखंड की कोसी नदी के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कोसी नदी देश के अन्य राज्यों बिहार और नेपाल देश में भी निकलती है लेकिन पहले केवल उत्तराखंड की कोसी नदी को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
कोसी नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। कोसी नदी को पवित्र नदियों में से एक माना जाता है यह उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में बहती है रामगंगा इसकी सहायक नदी के रूप में जाने जाते हैं। बात करें यदि कोसी नदी के उद्गम स्थल की तो कौसानी के पास धारापानी नामक स्थान से कोसी नदी उत्पन्न होती है। यहां से उद्गम होने के बाद यह पवित्र नदी सोमेश्वर से अल्मोड़ा की कोसी घाटी, हवालबाग, गरम पानी कैची, मोहान तक बहती है। इसके बाद यह नदी शहर की ओर प्रवेश करती है।
इस तरह से कोसी नदी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में बहती है और यह कुल मिलाकर 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
कोसी नदी की लोककथा. Kosi Nadi Lokkatha
उत्तराखंड के हर पवित्र धाम एवं स्थान का किसी ना किसी लोककथा से नाता जरूर जुड़ा होता है। ठीक उसी तरह से पवित्र नदी कोसी का भी अपने आप में एक प्रचलित लोक कथा है जो कि इसके इतिहास को और ज्यादा महत्व प्रदान करती है। उत्तराखंड की लोक कथाओं के अनुसार कोसी नदी को (Kosi Nadi Uttarakhand ) शापित नदी बताया गया है।
किवदंती है कि कोशी रामगंगा भागीरथी काली गंगा आदि कुल सात बहने थी। लोककथा के आधार पर प्रचलित है कि एक बार यह सातों पहने हैं साथ चलने की बात करते हैं। मगर उनमें से 6 बहनें समय पर नहीं आती। जिससे कोसी नदी को गुस्सा आ जाता है और वह अकेले चलने लगती है। जब बाकी छह बहने आई तो उन्हें किस बारे में पता चला कि कोसी जा चुकी है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन छह बहनों ने गुस्से में आकर कोसी को श्राप दिया कि वह हमेशा अलग बहती रहे और उसे कभी भी पवित्र नदी नहीं माना जाएगा। इस तरह से दोस्तों उत्तराखंड के लोक कथाओं में कोसी नदी की कहानी सुनने को मिलती है।

कोसी नदी की पौराणिक कहानी. Kosi Nadi Uttarakhand Poranaki kahani
कोसी नदी की पौराणिक कहानी का ऐतिहासिक स्रोत उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार बद्री दत्त पांडे जी की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास से लिया गया है।
बद्री दत्त पांडे के अनुसार ऋषि कौशिकी के द्वारा कौशिकी का अवतरण “धरती पर कराया गया था। बताया गया है कि ऋषि कौशिकी भटकोट शिखर पर बैठ कर तपस्या करते थे। एक समय की बात है उन्होंने स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर मां गंगा की स्तुति की। जिससे मां गंगा की एक जलधार उनके हाथ में प्रकट हुई। उन्होंने इस धारा का उपयोग जनकल्याण ही तो भटकोट बूढ़ा पिननाथ शिखर महादेव, बाधादित्य, में चली जाती है।
इस तरह से कुमाऊं के इतिहास नामक पुस्तक से कोशी नदी की पौराणिक कहानी जानने को मिलती है। उत्तराखंड में कोसी नदी पवित्र मानी जाती है।
कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियां. Kosi Nadi Ki Sahayak Nadi
उत्तराखंड से उत्पन्न होने वाली कोसी नदी की 118 सहायक नदियां है। सहायक नदियों से तात्पर्य छोटी-छोटी नदियों एवं स्थानीय भाषा में गधेरे से है
- देवगाड़
- मिनोलगाड़
- सुमालीगाड़
कोशी नदी F&Q
Q -कोसी नदी का मुहाना
Ans – उत्तराखंड की पवित्र नदियों में से एक कोसी नदी का मुहाना रामगंगा से माना जाता है। उत्तराखंड के इतिहास में कोसी नदी का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है।
Q – कोसी नदी की लंबाई
Ans – कोसी नदी की लंबाई उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल और उत्तर प्रदेश में बहने की दूरी इस नदी की मात्र 225 किलोमीटर है।
उत्तराखंड के भोजन के व्यंजन. Uttarakhand ke Bhojan Ke Byanjan
नमस्ते दोस्तों देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में आपका स्वागत है। आज के लेख के माध्यम से हम आप लोगों के साथ उत्तराखंड के लिए भोजन के व्यंजन उत्तराखंड का खानपान और उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन के व्यंजन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपने पारंपरिक भोजन ( Uttarakhand ke Bhojan Ke Byanjan)के लिए देश विदेशों में मशहूर है यहां के भोजन के व्यंजन संस्कृति के अंग है जिनके माध्यम से राज्य की संस्कृति बेखुदी से झलकती है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा।
उत्तराखंड का खानपान. Uttarakhand Ka Khaanpaan
प्यारे पाठको उत्तराखंड का खानपान उत्तराखंड की संस्कृति का एक अंग है खानपान के माध्यम से भी राज्य की संस्कृति को विशेष स्थान प्राप्त है। उत्तराखंड का पारंपरिक भोजन का स्वाद हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि यहां के भोजन के व्यंजन शुद्ध एवं पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। और उत्तराखंड का खानपान ( Uttarakhand Ka Khaanpaan )का सबसे अच्छी खासियत यह है कि इस भोजन को तैयार करने के लिए स्थानीय उत्पादों एवं लोगों के कौशल का उपयोग किया जाता है।
किंतु स्थानीय मसाले उत्तराखंड के भोजन को स्वाद के शिखर तक पहुंचाते हैं। ठीक उसी तरह से पहाड़ी खेतों से उगा हुआ फसल और खाद्य उत्पाद शुद्ध ऑर्गेनिक होता है इसीलिए पहाड़ी खानपान का स्वाद सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार के भोजन के व्यंजन बनाए जाते हैं जोकि स्थानीय लोगों के माध्यम से वहां के स्थानीय उत्पाद से तैयार किए जाते हैं। यदि आप उत्तराखंड के भोजन के व्यंजन ( Uttarakhand ke Bhojan Ke Byanjan) का स्वाद गहराई से अनुभव करना चाहते हैं तो आपको एक बार उत्तराखंड जरूर जाना चाहिए। उत्तराखंड के प्रमुख भोजन के व्यंजन निम्न प्रकार से है
- कंडेली का साग
- मंडवे की रोटी
- गहत की दाल
- फानु
- बाड़ी
- झंगोरा की खीर
- भांग की चटनी
कंडेली का साग. Kandeli Ka Saag Uttarakhand
उत्तराखंड के खानपान में कंडेली का साग का नाम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लिया जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में परोसा जाता है। पोस्टिक तत्व से भरपूर कंडेली का साग हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पोस्टिक तत्व पाए जाते हैं जो विभिन्न बीमारियों के उपचार में भी उपयोग में लाया जाता है। पालक की सब्जी की तरह दिखने वाला यह भोजन का व्यंजन उत्तराखंड में सर्दियों के समय में उपयोग किया जाता है।
सामान्यतः कंडेली का साग कंडेली के पत्तों की सहायता से तैयार की जाती है। उत्तराखंड में इसे बिच्छू घास के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सब्जी और आयुर्वेद में इसका विभिन्न रोगों के उपचार में उपयोग किया जाता है।
मंडवे की रोटी. Mandwe Ki Roti Uttarakhand
मडुवे की रोटी उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन में से एक है। इसे मंडुवे के आटे के माध्यम से तैयार किया जाता है। देखने में इसका रंग हल्का सा काला होता है लेकिन पौष्टिक तत्वों से भरपूर इस की रोटी काफी स्वादिष्ट होती है। मंडवें की रोटी और कंडेली का साग का उपयोग एक साथ किया जाता है। माना जाता है कि जब इन दोनों व्यंजनों का एक साथ सेवन किया जाता है तो इनके स्वाद का अनुमान लगाना काफी मुश्किल होता है। दोनों का स्वाद काफी स्वादिष्ट और मजेदार होता है।
गहत की दाल. Gahat Ki Daal Uttarakhand
गहत की दाल उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन की बिंजिन में से एक है यह नन्हें से हरे पीले दिखने वाले छोटे-छोटे दाल के दानों से तैयार किया जाता है। गहत की दाल पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है लेकिन स्थानीय मसालों के माध्यम से इसे और स्वादिष्ट और मजेदार बनाया जाता है। पहाड़ी खानपान के शौकीन लोग हफ्ते में एक दिन अपने घर में गहत की दाल और झंगोरें का भात का सेवन जरूर किया करते हैं। गहत की दाल और झंगोरे का भात स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है।
फानु. Faanu Uttarakhand
फाणु उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन के व्यंजन में से एक है जिसे पहाड़ के
मिक्स दालों के माध्यम से तैयार किया जाता है। इसमें गहत उड़द और विभिन्न
प्रकार की अन्य दालें शामिल होती है।
पौष्टिक तत्वों से भरपूर फाणू दिन
के भोजन के साथ उपयोग में किया जाता है। वैसे तो इसे भात के साथ खाया जाता
है लेकिन इसे रात्रि के भोजन में रोटी के साथ भी सेवन किया जाता है।
उत्तराखंड के घरों में यह पारंपरिक व्यंजन हफ्ते में एक दिन जरूर बनाया
जाता है।
बाड़ी. Baadi Khaanpaan Uttarakhand
मंडवे के माध्यम से तैयार होने वाली बाड़ी उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन के व्यंजनों में से एक है। सामान्यतः बाड़ी का उपयोग फानू के साथ करना उचित माना जाता है। क्योंकि इन दोनों का स्वाद आपस में मिलकर काफी बेहतरीन स्वाद को तैयार करता है।
वैसे तो बाड़ी व्यंजन का उपयोग सभी लोग करते हैं लेकिन खासतौर पर उत्तराखंड के बुजुर्ग लोग इसके काफी शौकीन हैं। जिस घर में बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी रसोई मैं हफ्ते में एक दिन बाड़ी व्यंजन जरूर बनाया जाता है।
झंगोरा की खीर. jangoren Ki khir Uttarakhand
झंगोरा और दूध की सहायता से तैयार किया जाने वाला यह स्वादिष्ट भोजन का व्यंजन तीर की तरह दिखाई देता है लेकिन इसमें चावल की जगह झंगोरा का उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन के व्यंजन में शामिल झंगोरा का खीर पहाड़ी स्वाद की शौकीन लोगों के लिए एक दिलचस्प भोजन का व्यंजन होने वाला है। मुख्य रूप से झंगोरा हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है इसमें तमाम प्रकार के पोस्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में सही माना जाता है। इसलिए उत्तराखंड का खानपान स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है।
भांग की चटनी. Bhang Ki Chatni Uttarakhand
उत्तराखंड में भांग की चटनी स्वादिष्ट चटनीयों में से एक है। भांग की सहायता से तैयार किया जाने वाला यह चटनी दिखने में तो नॉर्मल चटनी की तरह दिखती है लेकिन इसका स्वाद बेहद स्वादिष्ट होता है। इसमें स्थानीय मसालों के साथ पुदीना और धनिया का उपयोग किया जाता है जो की इसके स्वाद को शिखर तक पहुंचाता है। यदि आप भी भांग की चटनी का स्वाद लेना चाहते हैं उत्तराखंड में आपको एक बार जरूर जाना चाहिए और वहां के पारंपरिक भोजन के व्यंजनों का लुफ्त उठाना चाहिए।
प्यारे पाठको यह थे उत्तराखंड के भोजन के व्यंजन जिसमें हमने जाना कि उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन का स्वाद किस तरीके से लिया जा सकता है और कौन-कौन से भोजन के व्यंजनों का उपयोग किस समय पर किया जाता है। यदि आपको देवभूमि उत्तराखंड का यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।
उत्तराखंड के जिले. Uttarakhand Ke Jille
नमस्ते दोस्तों देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में आपका स्वागत है। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड के जिलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड भारत का एक पर्वतीय राज्य है जोकि अपने इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं के अलावा यहां के पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में कितने जिले हैं यह प्रश्न हमेशा हमारे पाठकों को चिंतित करता है। इसलिए आज हम आपको उत्तराखंड के जिलों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा इसलिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ना।
उत्तराखंड के जिले. Uttarakhand Ke Jille
प्यारे पाठको देवभूमि उत्तराखंड भारत का एक प्रसिद्ध राज्य है जो कि अपनी सांस्कृतिक छवि के लिए पूरे देश विदेश में मशहूर है। देश विदेश का हर एक नागरिक उत्तराखंड की संस्कृति और कला को जानने के लिए उत्सुक है। जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के जिलों के बारे में जानना भी उनके लिए अनिवार्य है।
उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक करके एक अलग राज्य बनाया गया 9 नवंबर सन 2000 को यह एक पृथक राज्य उत्तराखंड के रूप में सामने आया। लेकिन 2007 से पहले इसका नाम उत्तरांचल था जिसे बदलकर उत्तराखंड किया गया।
उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं और इन 13 जिलों के मुख्यालय भी बनाए गए हैं। जिनका कार्य राज्य के सर्वांगीण विकास में सहयोग करना है। उत्तराखंड के अधिकांश जिले पर्वतीय है जबकि राज्य के विकासशील जिले शहरी क्षेत्र में है।
उत्तराखंड के 13 जिलों के नाम. Uttarakhand Ke Jille Ke Naam
उत्तराखंड के 13 जिलों के नाम कुछ इस प्रकार से है
- नैनीताल
- पौड़ी गढ़वाल
- टिहरी गढ़वाल
- उत्तरकाशी
- पिथौरागढ़
- रुद्रप्रयाग
- उधम सिंह नगर
- अल्मोड़ा
- बागेश्वर
- चमोली
- चम्पावत
- देहरादून
- हरिद्वार
उत्तराखंड के मंडल. Uttarakhand Ke Mnadal
प्यारे पाठको उत्तराखंड राज्य को तीन मंडलों में विभाजित किया गया है। जिसके आधार पर इसके जिलों को तीन भागों में बांटा गया है ।
- कुमाऊं मंडल
- गढ़वाल मंडल
- गैरसैन मंडल
कुमाऊं मण्डल. Kumaoun Mandal
दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुकी है कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले भी राज्य में 2 मंडल गढ़वाल और कुमाऊं मंडल शामिल थे उन्हीं में से एक है कुमाऊं मंडल। कुमाऊँ मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी। स्थापना के समय कुमाऊं मंडल में 6 जिले शामिल थे लेकिन गैरसैण तीसरा मंडल बनने के बाद इसमें कुल 4 जिले आते हैं।
कुमाऊं मंडल के जिले. Kumaun Mandal Ke Jille
- नैनीताल
- पिथौरागढ़
- चंपावत
- उधम सिंह नगर।
गढ़वाल मंडल. Garhwal Mandal
गढ़वाल मंडल की स्थापना सन 1969 को हुई थी। गढ़वाल मंडल की स्थापना के समय इस में कुल 7 जिले शामिल थे। लेकिन जब गैरसैण उत्तराखंड का तीसरा मंडल के रूप में सामने आया तो गढ़वाल मंडल में कुल 5 जिले शामिल है ।
गढ़वाल मंडल के जिले. Garhwal Mandal Ke Jille
- उत्तरकाशी
- देहरादून
- पौड़ी गढ़वाल
- टेहरी गढ़वाल
- हरिद्वार।
गैरसैण मंडल. Gairsen Mandal
सन 2021 में जब गैरसैण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए बात सामने आई तो इसके नजदीकी जिले के लोगों द्वारा इसे उत्तराखंड का तीसरा मंडल बनाने के लिए मांग की गई। जिसके फल स्वरुप है यह 2021 में उत्तराखंड का तीसरा मंडल गैरसैंण के रूप में सामने आया। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से अलग किए गए जिलों को गैरसैण मंडल में शामिल किया गया। वर्तमान समय में गैरसैण मंडल में 4 जिले शामिल है।
गैरसैण मंडल के जिले. Gairsen Mandal Ke Jille
- रुद्रप्रयाग
- चमोली
- अल्मोड़ा
- बागेश्वर
उत्तराखंड के जिले F&Q
Q – क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड के बड़े जिले
Ans – 1 – उत्तरकाशी – 8016 वर्ग किलोमीटर
2 -चमोली – 7692 वर्ग किलोमीटर
3 – पिथौरागढ़ – 7110 वर्ग किलोमीटर
4 – पौड़ी गढ़वाल – 5438 वर्ग किलोमीटर
5 -टिहरी गढ़वाल – 4085 वर्ग किलोमीटर
Q – जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड के बड़े जिले
Ans – 1- हरिद्वार – 1,927,029
2 – देहरादून – 1,695,860
3 – उधम सिंह नगर – 1,648,367
4 – नैनीताल – 955,128
5 – पौड़ी गढ़वाल – 686,572
Q – उत्तराखंड के जिलों की स्थापना
Ans – अल्मोड़ा – गठन – 1891
चमोली – गठन – 1960
चम्पावत – गठन – 1997
देहरादून – गठन – 1817
हरिद्वार – गठन – 1988
Q – उत्तराखंड में कितने गांव हैं
Ans – उत्तराखंड में कुल 16999 गांव है।
Q – उत्तराखंड में कितने तहसील हैं
Ans – राज्य में तहसीलों की कुल संख्या 78 है। 78 तहसीलों के अलावा राज्य के अलग-अलग जिलों में कुल छह उप तहसीलें भी अस्तित्व में हैं।
Q – उत्तराखंड में नए जिले
Ans – उत्तराखंड में प्रस्तावित चार नए जिले डीडीहाट, कोटद्वार, रानीखेत और यमुनोत्री हैं।
उत्तराखंड की राजधानी कहां है. Uttarakhand Ki Raajdhani
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज हम आप लोगों के साथ उत्तराखंड की राजधानी कहां है एवं उत्तराखंड की राजधानी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी देने वाले हैं आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ना।
देवभूमि उत्तराखंड भारत के पर्वतीय राज्य के रूप में भी मशहूर है जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को भारत के 26 वें राज्य के रूप में हुई थी। अपनी अद्भुत वास्तु एवं शिल्प कला के साथ-साथ यह अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के लिए भी पहचानी जाती है।
देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी मुख्य रूप से राज्य का शहरी क्षेत्र देहरादून है। मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है लेकिन ग्रीष्म काल में उत्तराखंड की राजधानी गैरसैन के रूप में विख्यात है।
देहरादून – दून घाटी के बीच में स्थित देहरादून उत्तराखंड राज्य की शीतकालीन राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। जिले का मुख्यालय होने के साथ-साथ यह राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में से एक है जो कि समुद्र तल से 1400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से या उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है। आधुनिक संसाधनों से उपयुक्त यह शहर राज्य के प्रमुख शिक्षा केंद्र एवं चिकित्सा केंद्र का भी घर है।
देहरादून मुख्य रूप से उत्तराखंड का एक पर्यटन स्थल भी है जो कि नैनीताल एवं मसूरी जैसे हिल स्टेशनों का खूबसूरत दृश्य प्रदान करता है। यहां से प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल मसूरी 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है साथी नैनीताल की दूरी यहां से मात्र 40 किलोमीटर के आसपास है।
गैरसैण –
गैरसैण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए जानी जाती है। गर्मियों के समय में देहरादून जैसे महानगर में गर्मियां अधिक होती है इसलिए गैरसैण एक हिल स्टेशन होने के साथ-साथ ग्रीष्म काल में उत्तराखंड की राजधानी भी हुआ करती है। गैरसैण उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी. Uttarakhand ki Grishmkalin Raajdhani Kab Bani
गैरसैण उत्तराखंड का एक पर्यटन स्थल होने के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है इसलिए इसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में दर्जा मिला हुआ है। 8 जून 2020 को गैरसैण उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया गया। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कदम को स्वीकृति प्रदान की।
उत्तराखंड की दो राजधानी क्यों है. Uattarakhand ki 2 Rajdhani Kon Si Hai
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड दो राजधानी तो बनाई गई लेकिन क्या थी इसकी वजह इसके कारण देहरादून एवं गैरसैण उत्तराखंड की राजधानी के लिए चुना गया।
दरअसल गैरसैण गैरसैण प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक ऐसी जगह है जहां पर हर एक व्यक्ति यात्रा के लिए आना चाहता है। सड़क मार्ग वायु मार्ग एवं रेल मार्ग की अच्छी संपर्क का होने के कारण यहां पर सभी लोग आराम से पहुंच सकते हैं इसलिए उत्तराखंड की राजधानी ग्रीष्म काल में गैरसैण स्थापित की जाती है। उत्तराखंड राज्य का कोर्ट नैनीताल जिले में स्थित है।
गैरसैण गढ़वाल एवं कुमाऊँ मंडल के दूरवर्ती गांव का एक निकटतम स्थल है जहां पर दोनों मंडल के निवासी राजधानी से संबंधित कार्य कर सकते हैं। इसलिए गैरसैण को उत्तराखंड की द्वितीय राजधानी के लिए चुना गया।
उत्तराखंड 2023 की राजधानी क्या है. Uttarakhand Ki Rajdhani 2023 Kya hai
उत्तराखंड राज्य की मुख्य रूप से दो राजधानियां बनाई गई है शीतकाल एवं ग्रीष्म काल। शीतकाल में उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में स्थापित की जाती है राजधानी से सभी संबंधित कार्य देहरादून में किए जाते हैं जबकि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम होने के कारण लोग पहाड़ों की ओर जाना पसंद करते हैं इसलिए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में स्थित है।
दोस्तों यह तो हमारा आजकल है कि इसमें हमने आपको उत्तराखंड राज्य की राजधानी से संबंधित मुख्य बातों के बारे में जानकारी प्रदान की। आज के लेख में हमने जाना कि उत्तराखंड राज्य में दो राजधानियां शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन समय के आधार पर बनाई गई है। जो कि स्थाई होने के साथ-साथ सभी कार्यों को इन स्थलों के माध्यम से करते हैं।
उत्तराखंड का पारंपरिक फल से शहतूत. Sahtut Fal Uttarakhand
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आजकल इसलिए के माध्यम से हम आप लोगों के साथ उत्तराखंड का पारंपरिक फल शहतूत के बारे में बात करने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों प्रकार के फल फ्रूट एवं जड़ी बूटियां विद्यमान है जो कि अपने स्वादिष्ट स्वाद के साथ-साथ अपने औषधीय गुणों के लिए भी पहचानी जाती है। उन्हीं औषधीय फलों में से एक है शहतूत फल ( Sahtut Fal Uttarakhand ) जोकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह लेख उत्तराखंड का पारंपरिक फल शहतूत के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ साझा किया जा रहा है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लोग जरूर पसंद आएगा इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ना।
उत्तराखंड का पारंपरिक फल से शहतूत. Sahtut Fal Uttarakhand
शहतूत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक स्वादिष्ट फल है जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है। उत्तराखंड में शहतूत फल को किम फल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि शहतूत को अंग्रेजी में शहतूत in English Mulberries के नाम से पहचाना जाता है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम Morus Alba है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और कश्मीर के अलावा हिमालय क्षेत्र में अधिक पाया जाता है।
शहतूत के फल कंगनी अनाज के बाली की तरह लाल रंग के होते हैं। जिसमें तमाम प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका पौधा 20 से 30 फीट ऊंचा होता है। शहतूत के फल ग्रीष्म ऋतु में मई जून के महीने से पटना से हो जाते हैं । शहतूत फल का स्वाद खाने में मीठा होने के साथ-साथ हल्का तीखा होता है।
उत्तराखंड और पहाड़ी फल शहतूत. Sahtut Fal Uttarakhand
शहतूत फल का नाता उत्तराखंड के साथ बड़ा ही दिलचस्प और यादगार रहता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मियों के समय में पकने वाला यह फल पहाड़ी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूरवर्ती पहाड़ों में यह फल अपने स्वाद के लिए पहचाना जाता है। उत्तराखंड के लोगों द्वारा गर्मियों के समय में जंगल में घास काटते समय एवं ग्वालों को चराते समय बड़े ही स्वाद के साथ शहतूत फल को खाया जाता है।
गर्मियों के समय शहतूत फल जहां अपने पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है वही यह गर्मियों में धूप की किरणों से तपते किसानों को गर्मी से राहत दिलाने में मदद करती है। इसके औषधीय चमत्कारी गुण शरीर को ठंडक पहुंचाने में सहायता करते हैं।
शहतूत में पाए जाने वाले पोषक तत्व. Sahtut Fal Ke Poshak Tatwa
शहतूत पौष्टिक एवं विटामिन तत्वों से भरपूर एक प्राकृतिक फल है जोकि मनुष्य की सेहत के लिए बेहद खास माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले तमाम प्रकार के पोषक तत्व मनुष्य के शरीर के लिए औषधि के कार्य करते हैं।
- शहतूत में भरपूर मात्रा में विटामिन के और विटामिन सी पाया जाता है। जोकि मनुष्य के शरीर को ऊर्जावान बनाने में सहायता करता है
- शहतूत फल में कार्बोहाइड्रेट होता है जो शर्करा को ग्लूकोस में बदलने की ताकत रखता है । शहतूत के लगातार सेवन से शरीर में मौजूद है आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है।
- एकदम कच्चे शहतूत में 60 कैलोरी होती है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं।
पारंपरिक फल शहतूत खाने के फायदे. Sahtut Fal Ke Fayede
प्यारे दोस्तों शहतूत हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाला है यह फल औषधीय तत्वों से भरपूर होता है जिसके सेवन से मनुष्य को कई प्रकार के फायदे होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं।
- शहतूत के सेवन करने से लिवर से जुड़ी बीमारियों में राहत मिलती है। शहतूत का सेवन करना है किडनी के लिए लाभदायक माना जाता है।
- शहतूत के सेवन से जुड़ी से जुड़ी कई प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है।
- पाचन शक्ति को अच्छा रखता है शहतूत का फल। ग्रीष्म ऋतु में शरीर को ठंडक पहुंचाने में यह फल बेहद मदद करता है।
- सर्दी, खांसी और जुकाम में शहतूत का सेवन करना लाभदायक माना जाता है।
दोस्तों यह था हमारा है आजकल एक जिसमें हमने आपको उत्तराखंड का पारंपरिक फल शहतूत के बारे में ( Sahtut Fal Uttarakhand ) जानकारी साझा की। आशा करते हैं कि आपको पहाड़ी फल mountain fruit शहतूत के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। देवभूमि उत्तराखंड का यह लेख आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।
अस्वीकरण
प्यारे पाठको यह लेख केवल जानकारी एवं शैक्षणिक जानकारी के लिए साझा किया गया है। शहतूत का उपयोग किसी भी प्रकार के उपचार में करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। देवभूमि उत्तराखंड आपको कभी भी किसी भी प्रकार की औषधि को अपनाने की सलाह नहीं देता है।
उत्तराखंड की राजधानी कहां है. Uttarakhand Ki Raajdhani
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज हम आप लोगों के साथ उत्तराखंड की राजधानी कहां है एवं उत्तराखंड की राजधानी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी देने वाले हैं आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ना।
देवभूमि उत्तराखंड भारत के पर्वतीय राज्य के रूप में भी मशहूर है जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को भारत के 26 वें राज्य के रूप में हुई थी। अपनी अद्भुत वास्तु एवं शिल्प कला के साथ-साथ यह अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के लिए भी पहचानी जाती है।
देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी मुख्य रूप से राज्य का शहरी क्षेत्र देहरादून है। मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है लेकिन ग्रीष्म काल में उत्तराखंड की राजधानी गैरसैन के रूप में विख्यात है।
देहरादून – दून घाटी के बीच में स्थित देहरादून उत्तराखंड राज्य की शीतकालीन राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। जिले का मुख्यालय होने के साथ-साथ यह राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में से एक है जो कि समुद्र तल से 1400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से या उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है। आधुनिक संसाधनों से उपयुक्त यह शहर राज्य के प्रमुख शिक्षा केंद्र एवं चिकित्सा केंद्र का भी घर है।
देहरादून मुख्य रूप से उत्तराखंड का एक पर्यटन स्थल भी है जो कि नैनीताल एवं मसूरी जैसे हिल स्टेशनों का खूबसूरत दृश्य प्रदान करता है। यहां से प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल मसूरी 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है साथी नैनीताल की दूरी यहां से मात्र 40 किलोमीटर के आसपास है।
गैरसैण –
गैरसैण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए जानी जाती है। गर्मियों के समय में देहरादून जैसे महानगर में गर्मियां अधिक होती है इसलिए गैरसैण एक हिल स्टेशन होने के साथ-साथ ग्रीष्म काल में उत्तराखंड की राजधानी भी हुआ करती है। गैरसैण उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी. Uttarakhand ki Grishmkalin Raajdhani Kab Bani
गैरसैण उत्तराखंड का एक पर्यटन स्थल होने के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है इसलिए इसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में दर्जा मिला हुआ है। 8 जून 2020 को गैरसैण उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया गया। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कदम को स्वीकृति प्रदान की।
उत्तराखंड की दो राजधानी क्यों है. Uattarakhand ki 2 Rajdhani Kon Si Hai
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड दो राजधानी तो बनाई गई लेकिन क्या थी इसकी वजह इसके कारण देहरादून एवं गैरसैण उत्तराखंड की राजधानी के लिए चुना गया।
दरअसल गैरसैण गैरसैण प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक ऐसी जगह है जहां पर हर एक व्यक्ति यात्रा के लिए आना चाहता है। सड़क मार्ग वायु मार्ग एवं रेल मार्ग की अच्छी संपर्क का होने के कारण यहां पर सभी लोग आराम से पहुंच सकते हैं इसलिए उत्तराखंड की राजधानी ग्रीष्म काल में गैरसैण स्थापित की जाती है। उत्तराखंड राज्य का कोर्ट नैनीताल जिले में स्थित है।
गैरसैण गढ़वाल एवं कुमाऊँ मंडल के दूरवर्ती गांव का एक निकटतम स्थल है जहां पर दोनों मंडल के निवासी राजधानी से संबंधित कार्य कर सकते हैं। इसलिए गैरसैण को उत्तराखंड की द्वितीय राजधानी के लिए चुना गया।
उत्तराखंड 2023 की राजधानी क्या है. Uttarakhand Ki Rajdhani 2023 Kya hai
उत्तराखंड राज्य की मुख्य रूप से दो राजधानियां बनाई गई है शीतकाल एवं ग्रीष्म काल। शीतकाल में उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में स्थापित की जाती है राजधानी से सभी संबंधित कार्य देहरादून में किए जाते हैं जबकि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम होने के कारण लोग पहाड़ों की ओर जाना पसंद करते हैं इसलिए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में स्थित है।
दोस्तों यह तो हमारा आजकल है कि इसमें हमने आपको उत्तराखंड राज्य की राजधानी से संबंधित मुख्य बातों के बारे में जानकारी प्रदान की। आज के लेख में हमने जाना कि उत्तराखंड राज्य में दो राजधानियां शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन समय के आधार पर बनाई गई है। जो कि स्थाई होने के साथ-साथ सभी कार्यों को इन स्थलों के माध्यम से करते हैं।
बागेश्वर धाम उत्तराखंड. Bageshwar Dham Uttarakhand
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज के इस लेख के माध्यम से हम आप लोगों के साथ उत्तराखंड के बागेश्वर धाम के बारे में (Bageshwar Dham Uttarakhand) जानकारी देने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों धार्मिक एवं पवित्र स्थल है जो कि अपने इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हुए हैं। उन्हीं स्थानों में से एक हैं उत्तराखंड का बागेश्वर धाम जोकि उत्तराखंड के पवित्र स्थलों में से एक हैं। आज हम आप लोगों के साथ बागेश्वर धाम के बारे में जानकारी (Bageshwar Dham Uttarakhand) साझा करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ना।
बागेश्वर धाम उत्तराखंड. Bageshwar Dham Uttarakhand
सरयू नदी के संगम पर स्थित बागेश्वर धाम उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में अवस्थित है। भगवान शिव जी को समर्पित यह धाम उत्तराखंड के पवित्र धामों में से एक है जो कि अपने इतिहास और पौराणिक महत्व के लिए पहचाना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में भगवान शिव जी के अनेकों तीर्थ स्थल है जिनमें से एक बागेश्वर धाम है। इसमें शिव शक्ति की जल लहरीपुरा दिशा को है। प्रसिद्ध बागेश्वर धाम मंदिर में भगवान शिव जी स्वयं मां पार्वती के साथ जल लहरी के मध्य विराजमान हैं। इस मंदिर के समीप ही बानेस्वर मंदिर भी स्थित है।
बागेश्वर धाम मंदिर का पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि हुआ करती थी। भगवान शिव जी यहां बाग रूप में निवास करते हैं। मान्यता है कि पहले इस जगह को व्यागेश्वर नाम से जाना जाता था। जिसे 1602 में चंद्रवंशी राजा लक्ष्मीचंद ने बनवाया था।
बागेश्वर धाम मंदिर की पौराणिक कथा. Bageshwar Dham Uttarakhand Kahani
बागेश्वर धाम मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार शिव पुराण के मानस खंड में
बागेश्वर को सेवर के गण जगदीश ने बसाया था। इस समय मंदिर काफी छोटा था
जिसके बाद चंद्रवंशी राजा लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में भव्य रुप से बनाया।
मान्यता
है कि अनादि काल में मुनि वशिष्ठ अपने कठोर बल से ब्रह्मा के कमंडल से
निकली मां सरयू को ला रहे थे। परंतु जब वह इस जगह की नजदीक पहुंचे तो
ब्रह्मा का पाली के पास मार्कंडेय ऋषि तपस्या में लीन थे। जिसे देख वशिष्ट
जी को उनकी तपस्या भंग होने का खतरा सताने लगा।
पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि महादेव ब्रह्मा कपाली के पास एक गाय पर झपटने का प्रयास किया। गांव के रंभाने की आवाज से मार्कंडेय ऋषि की आंखें खुल गई। जिसके बाद ऋषि बाग को गाय से बचाने के लिए भागे तो गाय ने मां सीता का रूप ले लिया। इसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती ने मार्कंडेय ऋषि को दर्शन देकर उन्हें इच्छा अनुसार वरदान दिया जिसके बाद सरयू नदी आगे बढ़ सकी।
एक तरह से बागेश्वर धाम मंदिर की पौराणिक कहानी (Bageshwar Dham Uttarakhand) कथाओं में देखने को मिलती है। दोस्तों ऐसा करते हैं कि आपको बागेश्वर धाम के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और आपको यह लेख कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।
आप भी अपना किमती लेख हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो गेस्ट पोस्ट के माध्यम से आप अपनी वाणी को हम तक पहुंचा सकते हैं।
ओम पर्वत का रहस्य. Om Parwat Ka Rahasya
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज के इस लेख के माध्यम से हम आप सभी लोगों के साथ उत्तराखंड का ओम पर्वत का रहस्य के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे अनेकों स्थान है जो कि अपने रहस्य और पौराणिक इतिहास के लिए पहचाने जाते हैं। उन्हीं स्थानों में से एक है उत्तराखंड का ओम पर्वत जोकि अपने रहस्य के लिए पहचाना जाता है। आज के इस लेख में हम आपको ओम पर्वत का रहस्य (Om Parwat Ka Rahasya)एवं ओम पर्वत के बारे ( Om Parwat Ke Baren Me)में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ना।
ओम पर्वत उत्तराखंड. Om Parwat Ka Rahasya
ओम पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों में से एक है। ओम पर्वत समुद्र तल से 6191 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रसिद्ध ओम पर्वत अपने रहस्य ( Om Parwat Ka Rahasya ) में के लिए पहचाना जाता है। इस पहाड़ पर बर्फ के बीच में ओम शब्द का आकार दिखाई देता है शायद इसीलिए इस पर्वत को ओम पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह चोटी न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी को पर्वत का विशेष महत्व माना गया है। नाबीडांग यह पर्वत आसानी से देखा जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय पर कुल आठ प्रकार की प्राकृतिक आकृतियां बनी हुई है। इनमें से केवल ओम पर्वत के बारे में अभी तक जानकारी हासिल हो पाई है।
ओम पर्वत से आदि कैलाश की दूरी लगभग 26 किलोमीटर है इसलिए यहां से आदि कैलाश की यात्रा सरल मानी जाती है। यदि आप भी ओम पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान यात्री लिपुलेख के शिविर से ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं।
रहस्यमई ओम गुफा में भगवान शिव जी का वास माना जाता है। इसलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा और कैलाश पर्वत की यात्रा ( Kailash Parwat Ki Yatra ) के साथ-साथ ओम पर्वत की यात्रा भी बड़ी ही शुभ मानी जाती है। कई पर्वतारोहियों के माध्यम से इस पर्वत पर पहुंचने का प्रयास किया गया है ।
कैलाश मानसरोवर का महत्व. Kailash Maansarovar Ka Mahatwa
ओम पर्वत के साथ कैलाश मानसरोवर का बड़ा महत्व माना जाता है हिंदू
मान्यताओं के अनुसार कैलाश मानसरोवर को शिव पार्वती का घर माना जाता है ।
पौराणिक कहानियों एवं इतिहास के अनुसार कई देवता दानव , ऋषि मुनि सदियों से
यहां तपस्या करते हैं।
किवदंती है कि जो भी मनुष्य मानसरोवर की धरती को छू लेता है वह ब्रह्मा के बनाए स्वर्ग के दर्शन करता है।
ओम पर्वत का रहस्य. Om Parwat Ka Rahasya
हिंदू पौराणिक कहानियों में ओम पर्वत का वर्णन बेखुदी से देखने को मिलता है लेकिन ओम पर्वत का रहस्य ( Om Parwat Ka Rahasya) को लेकर आज भी लोग चिंतित और जानने को बेताब रहते हैं। इतिहास के अनुसार हिमालय पर्वत पर आठ प्रकार की प्राकृतिक आकृतियां विद्यमान हैं जिनमें से केवल ओम की आकृति वाले पर्वत को ही पहचाना गया है। बाकी सात प्रकार की आकृति वाले पर्वत आज भी अपने रहस्य को संजोए हुए हैं। हिंदू मान्यताओं में ओम पर्वत को बड़ा ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओम पर्वत को भगवान शिव जी और मां पार्वती के निवास स्थान माना गया है।
दोस्तों यह तो हमारा आजकल एक जिसमें हमने आपको ओम पर्वत का रहस्य के बारे में (Om Parwat Ka Rahasya) जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको ओम पर्वत के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।
ओम पर्वत का रहस्य F&Q
Q – ओम पर्वत किस जिले में स्थित है
Ans – ओम पर्वत भारत और नेपाल के बीच हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। जो कि पश्चिमी नेपाल के दारचूला जिले में स्थित है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत के दर्शन लिपुलेख दर्रा के सामने से किए जा सकते हैं।
Q – ओम पर्वत कहां स्थित है
Ans – ओम पर्वत भारत और नेपाल की सीमा के बीच स्थित है। ओम पर्वत को आदि कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। बर्फ से बने ओम की आकृति के कारण इस पर्वत का नाम ओम पर्वत रखा गया। इस पर्वत के आसपास बसे शिखर आज भी अपने रहस्य को संजोए हुए हैं।
Q – ओम पर्वत की खोज किसने की
Ans – ओम पर्वत की खोज का श्रेया टीआरसी प्रबंधक विपिन पांडे को जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान टीआरसी प्रबंधक विपिन पांडे ने 1981 में ओम पर्वत की खोज की थी।
Q – ओम पर्वत की ऊंचाई कितनी है
Ans – यदि बात की जाए ओम पर्वत की ऊंचाई की तो बताना चाहेंगे कि वह पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 6191 मीटर है। यह पर्वत दिव्य आत्माओं का निवास माना जाता है।
Q – ओम पर्वत उत्तराखंड
Ans – समुद्र तल से 6191 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ओम पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य की पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ओम पर्वत आदि कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में ओम पर्वत का रहस्य बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है।
बाबा बर्फानी उत्तराखंड. Barfani Baba Uttarakhand
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको बाबा बर्फानी उत्तराखंड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। प्यारे दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही दिव्य आत्माओं का निवास। पौराणिक आज है यहां पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि अपने इतिहास और चमत्कारों के लिए पहचानी जाती हैं उन्हीं जगहों में से एक है बाबा बर्फानी जो कि अपने इतिहास और पौराणिक कहानी के लिए पहचाने जाते हैं। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको बाबा बर्फानी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आशा करते हैं दोस्तों की आपको देव भूमि उत्तराखंड का यह लेख जरूर पसंद आएगा।
प्रसिद्ध बाबा बर्फानी जी की गुफा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नीति गांव के पास बसी यह ऐतिहासिक गुफा भगवान शिव जी की एक गुफा है। किवदंती है कि सर्दियों के समय में चमोली की सिमर सेंड महादेव के इस आध्यात्मिक गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। जैसे स्थानीय लोग बाबूक उडियार कहते है।
प्रसिद्ध बाबा बर्फानी गुफा में पूरे वर्ष भर में हजारों की संख्या में पर्यटक आए करते हैं हालांकि सर्दियों के समय में बर्फ भरे रास्ते होने से उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा बाबा बर्फानी गुफा की यात्रा बंद की जाती है। इसके बाद दोबारा से यह यात्रा फरवरी महीने से शुरू हो जाती है।
यदि आप भी बाबा बर्फानी गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो बताना चाहेंगे कि बाबा बर्फानी की है उसका चमोली जिले के अंतिम गांव नीति से लगभग 700 मीटर की दूरी पर मौजूद है।
बाबा बर्फानी का इतिहास. Barfani Baba Ka Itihas
बाबा बर्फानी का इतिहास के बारे में बात करें । हमें देखने को मिलता है कि भारत में बाबा बर्फानी के दो पवित्र स्थल मौजूद है। एक अमरनाथ यात्रा पर पड़ने वाला बाबा बर्फानी की गुफा और एक उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा। किवदंती है कि इस स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग उत्पन्न होता है। जिसकी ऊंचाई लगभग 2 फिट होती है। जिस स्थान पर यह प्राकृतिक रूप से शिवलिंग उत्पन्न होता है उस जगह को स्थानीय लोगों द्वारा बाबुक उडियार कहा जाता है।
यात्रियों के द्वारा फरवरी माह के बाद बाबा बर्फानी गुफा के दर्शन किए जाते हैं जिसके बाद यह प्राकृतिक रूप से बना शिवलिंग दिखाई देता है। फरवरी माह से पहले यहां पर काफी बर्फ होती है इसलिए उत्तराखंड के पर्यटन विभाग द्वारा यहां पर श्रद्धालुओं का आना वर्जित किया जाता है।

तिमरसैन बाबा बर्फानी दर्शन करने का अच्छा समय. Barfani Baba Jane Ka Samay
तिमरसैन बाबा बर्फानी दर्शन करने का अच्छा समय फरवरी माह से अक्टूबर माह तक माना जाता है। इस बीच यहां का मौसम काफी अच्छा रहता है । इसलिए आप यहां के दर्शन फरवरी से अक्टूबर माह के बीच तय कर सकते हैं। अक्टूबर माह के बाद यहां का मौसम काफी ठंडा रहता है। रास्ते में पर्यटकों को बर्फीले रास्ते से गुजरना पड़ता है इसलिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा बाबा बर्फानी की यात्रा पर रोक लगा दी जाती है।
तिमरसैन महादेव मंदिर कैसे पहुंचे. Barfani Baba Kese pachuchen
बाबा बर्फानी महादेव मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है जहां पहुंचने के लिए सबसे अच्छा विकल्प सड़क मार्ग है। सड़क मार्ग के माध्यम से बाबा बर्फानी के दर्शन आराम से किए जा सकते हैं। बाबा का मंदिर पहुंचने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग से जोशीमठ तक बस एवं टैक्सी से पहुंच सकते हैं। नीति गांव तक पहुंचने के लिए आपको किराया की टैक्सी लेनी पड़ सकती है।
नीति गांव से महज 1 किलोमीटर पहले बाबा बर्फानी जी की गुफा विद्यमान है । बाबा बर्फानी जी की गुफा में पहुंचने के बाद आप गुफा के दर्शन करके नीति गांव में रहने का प्रबंध कर सकते हैं।
पूर्णागिरी मंदिर उत्तराखंड.Poornagiri Temple
दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में आज हम आप लोगों के साथ पूर्णागिरी मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं । जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूर्णागिरि का मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक हैं जो कि अपने भव्य मंदिर एवं पौराणिक महत्व के लिए जानी जाती है। हर कोई दर्शनार्थी इस मंदिर के बारे में जाने के लिए उत्सुक है तो चलिए आज हम आपको पूर्णागिरी मंदिर टनकपुर के बारे में जानकारी देते हैं।
पूर्णागिरी मंदिर उत्तराखंड. Poornagiri Temple
मां भगवती को समर्पित पूर्णागिरि का मंदिर उत्तराखंड राज्य राज्य के चंपावत जिले में स्थित एक भव्य एवं ऐतिहासिक मंदिर है जो कि काली नदी के किनारे पर बना हुआ है। यह प्रसिद्ध मंदिर तीन देश चीन, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से घिरा हुआ है। मां भगवती के 108 शक्तिपीठों में से यह मंदिर टनकपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अन्नपूर्णा चोटी के शिखर में 3000 फिट की ऊंचाई पर स्थित है।
आस्था एवं भक्ति का प्रसिद्ध है यह भव्य मंदिर अपनी ऐतिहासिक पहलुओं को संजोया हुआ है। हर साल हजारों दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और मां भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करके मां के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। स्थानीय मान्यता है कि जो भी भक्त यहां सच्चे मन से कामना करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है।
पूर्णागिरी मंदिर निर्माण कथा के अनुसार.Poornagiri Temple
किवदंती है कि जहां देवी के अंग गिरे वही स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। माना जाता है कि इस प्रकार से माता के कुल 108 शक्तिपीठ है और जहां पर माता सती का नाभि अंग गिरा वह चंपावत का पूर्ण गिरी पर्वत था। इसलिए यहां पर माता का भव्य मंदिर बनाया गया।
इसलिए इस मंदिर को मां भगवती के 108 सिद्ध गीतों में से एक माना जाता है जोकि पवित्र होने के साथ-साथ ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व को संजोया हुवा है।
पूर्णागिरी मंदिर पौराणिक मान्यता. Poornagiri Temple Pouranik Manyta
दोस्तों जिस तरह से पूर्णागिरी मंदिर आस्था और भक्ति से ओतप्रोत है ठीक इसी तरह से इसका पौराणिक महत्व अपने आप में विशेष मान्यता रखता है। पूर्णागिरी मंदिर के सिद्ध बाबा के बारे में कहा जाता है कि एक साधु ने व्यर्थ रूप से मां पूर्णागिरि के सबसे ऊंचे पर्वत पर पहुंचने की कोशिश की। तो मां ने क्रोध में आकर उस साधु को नदी के पार फेंक दिया। लेकिन मान्यताओं के आधार पर माना जाता है कि मां ने दयालुता की भाव में आकर सिद्ध बाबा के नाम से विख्यात होने का आशीर्वाद प्रदान किया। और कहा कि जो व्यक्ति मेरे दर्शन के लिए आएगा वह जरूर तुम्हारे दर्शन भी करेंगे। इस तरह से पूर्णागिरि का मंदिर अपने पौराणिक महत्व के लिए भी जाना जाता है।
पूर्णागिरी धाम के झूठे मंदिर की कथा. Poornagiri Temple History
पौराणिक मान्यताओं के आधार पर माना जाता है कि जो भी भक्त मां पूर्णागिरि के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। एक समय की बात है । एक सेट संतान विहीन थे। मां पूर्णागिरि ने उनके सपने में कहा कि मेरे दर्शन के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। सेठ माता के दर्शन के लिए मंदिर में गए और उन्होंने माता से मन्नत मांगी कि यदि उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह सोने का मंदिर बनाएंगे। मां पूर्णागिरि के आशीर्वाद से सेठ का पुत्र हो गया और उनका मनोकामना पूर्ण हो गई। इसके बाद सेठ की मंदिर बनाने की बारी आती है लेकिन वह लालच में आ जाते हैं और वह तांबे के मंदिर में सोने की पॉलिश करवा कर मां पूर्णागिरि को चढ़ाने चले जाते हैं। बताया जाता है कि तुन्यास नामक स्थान पर पहुंचने के बाद वह मंदिर को आगे नहीं ले जा सके और वह मंदिर वही जम गई। जो कि आज के समय में झूठे मंदिर के नाम से विख्यात है। स्थानीय लोगों द्वारा बच्चों के मुंडन संस्कार इसी मंदिर में किए जाते हैं।
वैसे तो पूर्णागिरी मंदिर में हर साल हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते रहते हैं लेकिन खासतौर पर चैत्र माह में पूर्णागिरि मेला आयोजन होने के कारण यहां पर लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आया करते हैं। चैत्र माह से यह पूर्णागिरि का मेला शुरू होता है और लगभग 90 दिनों तक चलता है।
पूर्णागिरी मंदिर कैसे पहुंचे. Poornagiri Temple Kese Pauchen
पूर्णागिरी मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। मंदिर सड़क मार्ग से जुड़े होने के कारण यहां सड़क मार्ग के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है साथ ही वायु मार्ग एवं रेल मार्ग के माध्यम से भी पूर्णागिरी मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं।
सड़क मार्ग द्वारा
मां पूर्णागिरि का मंदिर अन्नपूर्णा में पर्वत पर स्थित है जो की समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। मां पूर्णागिरि का मंदिर चंपावत से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और टनकपुर से यह मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
रेल मार्ग द्वारा
मां पूर्णागिरी मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन टनकपुर है टनकपुर से पूर्णागिरी मंदिर की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है यहां से प्राइवेट टैक्सी एवं बस के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली जैसे महानगर से पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस नामक ट्रेन शुरू की गई है।
हवाई मार्ग द्वारा
पूर्णागिरी मंदिर का नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है। पंतनगर से पूर्णागिरी मंदिर की दूरी 160 किलोमीटर है जहां से आपको बस एवं किराए की गाड़ी भी मिल जाएगी।
मां पूर्णागिरी मंदिर से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q-पूर्णागिरि का मंदिर कहां पर है
Ans – देवी भगवती को समर्पित मां पूर्णागिरि का मंदिर उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में टनकपुर नामक स्थान से 20 किलोमीटर की दूरी पर अन्नपूर्णा पर्वत पर स्थित है। आस्था एवं भक्ति का प्रतीक यह मंदिर अपने पौराणिक इतिहास को संजोया हुआ है।
Q -पूर्णागिरी मंदिर का इतिहास
Ans – किवदंती है कि जहां देवी के अंग गिरे वही स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। माना जाता है कि इस प्रकार से माता के कुल 108 शक्तिपीठ है और जहां पर माता सती का नाभि अंग गिरा वह चंपावत का पूर्ण गिरी पर्वत था। इसलिए यहां पर माता का भव्य मंदिर बनाया गया।
Q -पूर्णागिरी मंदिर दूरी
Ans – मां पूर्णागिरि का मंदिर टनकपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं इसका नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है जहां से मां पूर्णागिरी मंदिर की दूरी मात्र 160 किलोमीटर है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है।
Q – पूर्णागिरी मंदिर की फोटो
Ans –
Q -पूर्णागिरि से नैनीताल की दूरी
Ans – आस्था एवं भक्ति का प्रतीक मां पूर्णागिरि का मंदिर नैनीताल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहां से प्राइवेट टैक्सी एवं बस सेवा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आप चाहे तो टनकपुर तक बस के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं।
Q -टनकपुर से पूर्णागिरी मंदिर की दूरी
Ans -टनकपुर से मां पूर्णागिरि मंदिर की दूरी मात्र 20 किलोमीटर की है। मंदिर अन्नपूर्णा नामक शिखर पर स्थित है जहां के लिए टनकपुर से टैक्सी आसानी से मिल जाती है।
कोटेश्वर महादेव मंदिर. Koteshwar Mahadev Temple
नमस्ते दोस्तों जय देव भूमि उत्तराखंड. स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग के आज के नए लेख में। आज हम आप लोगों के साथ कोटेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड की प्रमुख मंदिरों में से एक है जो कि अपने पौराणिक तथा एवं मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। देवभूमि उत्तराखंड के इस लेख में हम आपको कोटेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी एवं उसके इतिहास की जानकारी साझा करेंगे।
कोटेश्वर महादेव मंदिर.Koteshwar Mahadev Temple
पवित्र कोटेश्वर महादेव मंदिर हिंदू धर्म के पवित्र मंदिरों में से एक है जोकि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित एक प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है। मंदिर शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थिति हम मंदिर एक गुफा के रूप में मौजूद हैं जोकि अपने ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व को संजोया हुआ यह मंदिर हर वर्ष लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है लेकिन खासतौर पर शिवरात्रि के दिन यहां पर दर्शनार्थियों की अत्यधिक संख्या देखने को मिलती है।
भगवान शिव जी के प्राचीन मंदिरों में से एक कोटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण लगभग 14वी शताब्दी का माना जाता है। लेकीन 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। इस प्राचीनतम मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि चार धाम यात्रा पर निकले ज्यादातर श्रद्धालु मंदिर को देखते ही दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं।
ऐतिहासिक कहानियों के आधार पर किवदंती है कि भगवान शिव जी ने केदारनाथ जाते समय इस पवित्र गुफा में साधना की थी। तभी से इस स्थान पर एक मूर्ति स्थित है जो कि प्राकृतिक रूप से निर्मित हो गई थी। गुफा के अंदर प्राचीन मूर्तियां एवं शिवलिंग के अलावा मां पार्वती और भगवान गणेश जी, हनुमान जी , और मां दुर्गा जी की मूर्ति विद्यमान है। कोटेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने से पहले यदि इस पवित्र गुफा के दर्शन किए जाते हैं तो दर्शनार्थियों को पाप से मुक्ति प्राप्त होती है।
कोटेश्वर मंदिर पौराणिक कहानी. Koteshwar Mahadev Temple Kahani
कोटेश्वर महादेव मंदिर जिसकी पौराणिक कहानी प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि भगवान शिव जी ने भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में कुछ समय व्यतीत किया। भस्मासुर ने शिवजी की आराधना करके एक विशेष वरदान प्राप्त किया था कि वह किसी के भी सर में हाथ रखकर उसे भस्म कर सकते हैं। और इसी वरदान आजमाने के लिए उन्होंने भगवान शिव जी को चुना। उसके बाद भगवान शिवजी जहां भी जाते भस्मासुर उनके पीछे-पीछे वहीं तक पहुंच जाते हैं। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव जी ने कोटेश्वर गुफा में प्रवेश किया और कुछ समय वहां पर विश्राम करने का निर्णय लिया। मान्यता है कि इस बीच भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर से संहार किया और पवन शिवजी की सहायता की जिसके पश्चात यहां पर भगवान शिव जी ध्यान अवस्था में रहे। इसलिए इस मंदिर का महत्व बड़ा ही खास माना जाता है।
कोटेश्वर महादेव मंदिर कैसे पहुंचे. Koteshwar Mahadev Mandir kese Pahuchen
दोस्तों कोटेश्वर महादेव मंदिर रुद्रप्रयाग शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं सड़क के समीप होने के कारण सड़क मार्ग से यहां आराम से पहुंचा जा सकता है। देश की किसी भी कोने से सड़क मार्ग के माध्यम से कोटेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंच सकते हैं।
रेल मार्ग द्वारा
कोटेश्वर महादेव मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है जो कि कोटेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश से आप टैक्सी एवं बस के माध्यम से आ सकते हैं।
हवाई मार्ग द्वारा
कोटेश्वर महादेव मंदिर का नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट है। यहां से पवित्र धाम की दूरी 160 किलोमीटर है जिसके लिए आप सड़क मार्ग के माध्यम से बस सेवा एवं टैक्सी के द्वारा भी आ सकते हैं।
कोटेश्वर मंदिर से जुड़ें पूछे जाने वाले सवाल
Q- कोटेश्वर महादेव मंदिर कहां है
Ans – प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव जी के पवित्र धामों में से एक हैं जो कि उत्तराखंड राज्य की रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। मंदिर की मुख्य मान्यता के बारे में उल्लेखित है कि केदारनाथ यात्रा से पहले कोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करके दर्शनार्थियों के सभी पाप शुद्ध हो जाते हैं।
Q -कोटेश्वर महादेव का इतिहास
Ans -कोटेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास प्राचीन होने के साथ-साथ पौराणिक भी है। मान्यता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव जी ने कोटेश्वर गुफा में शरण लिया था जिसके बाद उन्होंने इस स्थान पर ध्यान किया और आज के समय में यह स्थान पवित्र होने के साथ-साथ भगवान शिव जी के प्रमुख धामों में से एक है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में कोटेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक खास स्थान रखता है।
Q – कोटेश्वर महादेव मंदिर रुद्रप्रयाग
Ans – भगवान शिव जी की पवित्र मंदिरों में से एक कोटेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्राचीन गुफा है जोकि अपने पौराणिक महत्व के लिए जानी जाती है। कोटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण लगभग 14वी शताब्दी का माना जाता है। लेकीन 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था
दोस्तों यह था हमारा आज कल ही कोटेश्वर महादेव मंदिर के बारे में यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।
यदि आप भी अपना जानकारी युक्त लेख हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें गेस्ट पोस्ट के माध्यम से भेज सकते है। यह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्ञानवर्धक लेख प्राप्त करके हमें बहुत खुशी होगी।
बिनसर महादेव मंदिर. Binsar Mahadev Mandir Almora
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में. देवभूमि उत्तराखंड अपने प्राचीन मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के अलावा ऐतिहासिक इस महत्वों के लिए प्रसिद्ध है। उन्हीं प्राचीन मंदिरों में से एक है बिनसर महादेव मंदिर जोकि अपने ऐतिहासिक मान्यताओं के लिए पूरे देश भर में मशहूर है।
आज के इस लेख में हम आपको बिनसर महादेव मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किस तरीके से आप लोग बिनसर महादेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और बिनसर महादेव मंदिर की मान्यताएं क्या है। तो चलिए आज का लेख शुरू करते हैं।
भगवान शिव जी को समर्पित बिनसर महादेव मंदिर उत्तराखंड के रानीखेत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर कुंज नदी के खूबसूरत तट से लगभग 5500 फिट की ऊंचाई पर स्थित है। हरे भरे देवदार एवं विभिन्न प्रकार के सदाबहार पेड़ पौधों से गिरा हुआ यह मंदिर पहाड़ के मनमोहक हास्य प्रस्तुत करता है।
मंदिर में प्रवेश करने के दौरान आप देख पाएंगे कि मंदिर एक भव्य एवं बेहद खूबसूरत वास्तुकला से निर्मित है। मंदिर के अंदर महेश मर्दिनी और हर गौरी और गणेश के रूप में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल है। बिनसर महादेव मंदिर आस्था एवं भक्ति का प्रसिद्ध केंद्र है। यहां पर वर्ष भर में हजारों की संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन खासतौर पर शुभ रात्रि एवं बिनसर के दिन यहां पर श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ इकट्ठा होती है जिससे मंदिर का भव्य एवं आकर्षक दृश्य प्रदर्शित होता है।
बिनसर महादेव मंदिर का इतिहास. Binsar Mahadev Mandir Ka Itihas
दोस्तों जिस तरह से बिनसर महादेव मंदिर अपनी आस्था एवं भक्ति के लिए पूरे उत्तराखंड में जाना जाता है ठीक उसी प्रकार से बिनसर महादेव मंदिर का पौराणिक इतिहास भी अपने आप में खास महत्व रखता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस मंदिर के बारे में विभिन्न प्रकार के तथ्य एवं मित्र सामने आए हैं । जिन को मध्य नजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि बिनसर महादेव मंदिर अपने पुरातात्विक महत्व और वनस्पति के लिए काफी लोकप्रिय है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि बिनसर महादेव मंदिर के स्थापना पांडवों द्वारा किया गया था। और एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि यह मंदिर एक रात में बनकर तैयार हुआ जिसके बारे में यकीन कर पाना शायद ही मुश्किल होगा।
लेकिन इतिहास के कुछ पन्नों पर नजर डालने से एवं स्थानीय लोगों की सहायता से पता चलता है कि बिनसर महादेव मंदिर को राजा पृथु ने अपने पिता बिंदु की याद में बनवाया था। इसलिए इस मंदिर का नाम बिनसर महादेव पड़ा।
बिनसर महादेव से जुड़ी लोक कथा. Binsar Mahadev Mandir Lokkathayen
दोस्तों बिनसर महादेव मंदिर से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार बिनसर महादेव मंदिर से कुछ ही दूरी पर है सैनी नामक गांव में मनिहार जाति के लोग रहते थे। उन सभी लोगों की गाय चलने के लिए बिनसर के क्षेत्र में जाती थी। कहानी के आधार पर ज्ञात होता है कि उन्हें गायों मैं से एक गाय का दूध हमेशा निकला हुआ मिलता था। 1 दिन गाय के मालिक ने गाय पर नजर डालते हुए देखा कि वह अपना पूरा दूध एक शीला के ऊपर गिरा के आ जाती है मालिक ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी के उल्टे हिस्से से उस शिला पर वार किया इससे की उस शिला से खून की धार निकलना शुरू हुई गई जिसे देख गाय का मालिक हैरान हुआ और वह चुपचाप घर चला गया। उसी रात उस गाय के मालिक के सपनों में एक बाबा आता है और उन्हें पूरा गांव खाली करने का आदेश देते हैं। आदेश के अनुसार सभी लोग गांव को खाली कर देते हैं। कुछ वर्षों के पश्चात सैनी गांव के नजदीक एक निसंतान वृद्ध दंपत्ति रहते थे। एक रात उनके सपने में बाबा जी दर्शन दे गए और कहा कि कुंज नदी के तट पर एक शिवलिंग पड़ा है उस की प्राण प्रतिष्ठा करा कर मंदिर का निर्माण करो। आज्ञा के अनुसार उस वृद्ध दंपति ने वहां पर मंदिर का निर्माण किया जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई।
बिनसर महादेव मंदिर कैसे पहुंचे. Binsar Mahadev Mandir Kese Pahuchen
प्यारे पाठको बिनसर महादेव मंदिर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग के साथ-साथ वायु मार्ग एवं रेल मार्ग के विकल्प भी उपलब्ध है। सड़क मार्ग के माध्यम से बिनसर महादेव मंदिर पहुंचना काफी आसान है। बिनसर महादेव मंदिर सड़क मार्ग से पूरी तरह से जुड़ा हुआ।
सड़क मार्ग से बिनसर महादेव मंदिर
बिनसर महादेव मंदिर सड़क मार्ग से देश के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है । रानीखेत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिनसर महादेव पहुंचने के लिए आपको रानीखेत पहुंचना होगा इसके बाद खूबसूरत पहाड़ के चढ़ाई करने के बावजूद पहाड़ के शिखर पर भगवान भोले शंकर का खूबसूरत सा बिनसर महादेव मंदिर स्थित है।
रेल मार्ग द्वारा बिनसर महादेव
रेल मार्ग द्वारा बिनसर महादेव पहुंचना काफी आसान है क्योंकि बिनसर महादेव मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जहां से बिनसर महादेव मंदिर की दूरी मात्र 120 किलोमीटर की है। काठगोदाम से महादेव मंदिर के लिए टैक्सी एवं बस के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं।
हवाई जहाज से बिनसर महादेव मंदिर
हवाई जहाज के माध्यम से भी बिनसर महादेव मंदिर हो सकते है। बिनसर महादेव मंदिर का नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है। पंतनगर एयरपोर्ट से बिनसर महादेव मंदिर की दूरी लगभग 127 किलोमीटर है। यहां से सड़क मार्ग के माध्यम से बस और टैक्सी के द्वारा मंदिर तक पहुंचा जा सकता है।
शिव कालेश्वर मंदिर . Shiv Kaleshwar Mandir
नमस्ते दोस्तों को जय देव भूमि उत्तराखंड स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग के आज के नए लेख में। आज हम आप लोगों के साथ शिव कालेश्वर मंदिर उत्तराखंड के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड संपूर्ण आकर्षक का केंद्र है जहां पर मंदिर, धार्मिक स्थल एवं खूबसूरत पहाड़ियों के मंदिर में बसे गांव, शहर एवं कई ऐतिहासिक जगह देखने को मिल जाती है। उन्हीं जगहों में से एक है शिव कालेश्वर मंदिर (Shiv Kaleshwar Mandir )जोकि उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक हैं। आज हम शिव कालेश्वर मंदिर का इतिहास एवं हिंदी के बारे में जानकारी देने वाले हैं।
शिव कालेश्वर मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के लैंसडाउन के पास
स्थित एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो कि अपने पौराणिक इतिहास के लिए जाने
जाते हैं। लैंसडाउन उन जगहों में से एक हैं ब्रिटिश शासन काल के दौरान हिल
स्टेशन हुआ करते थे। और आज के समय में भी यह एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन हुआ
करता है जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक आया करते हैं।
इसी स्थान पर स्थित है भगवान शिव का एक सदियों पुराना मंदिर जिसे कालेश्वर महादेव
मंदिर लैंसडाउन (Shiv Kaleshwar Mahadev Temple) के नाम से जाना जाता है।
संपूर्ण लैंसडाउन का आकर्षक एवं आस्था का केंद्र यह मंदिर वर्ष भर में
हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह जगह अपने ऐतिहासिक महत्व के
साथ आज भी पौराणिक महत्व को जीवंत रखती है। वैसे तो इस मंदिर में श्रद्धालु
रोज आया करते हैं लेकिन खासतौर पर शिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहां पर
हजारों की संख्या में श्रद्धालु आया करते हैं। किवदंती है कि इस स्थान पर
ऋषि कालून जी ने ध्यान किया था। जिनके नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध हुआ। शिव
कालेश्वर मंदिर भगवान शिव जी के भक्तों की प्रमुख जगह है। जहां हर कोई
श्रद्धालु आना चाहता है।
शिव कालेश्वर मंदिर की मान्यता. Shiv Kaleshwar Mandir manyta
शिव कालेश्वर मंदिर की मान्यता है कि कालेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। बताया जाता है कि इसके नजदीकी गांव की गाय जब यहां चलने आती थी तो शिवलिंग के पास आते ही वह स्वयं दूध देने लगती थी। मान्यता है कि उस समय में जो भी श्रद्धालु यहां पर जो भी मन्नत मांगते थे उनकी मनोकामना में बातचीत जी जरूर पूर्ण करते हैं। इसी आस्था एवं मान्यता को देखते हुए गढ़वाल रेजीमेंट में 1901 मैं यहां पर एक छोटा सा मंदिर का निर्माण किया। धीरे-धीरे यह मंदिर आस्था का केंद्र बनता गया और 1926 में भक्तों की सहायता से इस मंदिर को एक विशाल रूप दिया गया। हालांकि 1995 के समय में मंदिर को और अधिक बढ़ाया गया जिसमें रेजीमेंट के साथ-साथ स्थानीय लोगों का योगदान भी है। वाकई में यह पवित्र जगह आस्था एवं भक्ति का केंद्र हैं। चरते हुएं गाय का यहां पर आकर अपने आप दूध देना एवं ऋषि कलून के ध्यान करने से यह जगह आस्था का एक पवित्र केंद्र हैं।

कालेश्वर महादेव कैसे पहुचें . Shiv Kaleshwar Kese Pahuchen
शिव कालेश्वर मंदिर उत्तराखंड (Shiv Kaleshwar Mahadev Temple)के पौड़ी गढ़वाल जिले के लैंसडाउन ब्लॉक में स्थित हैं यदि आप लोग वाकई में इस खूबसूरत एवं ऐतिहासिक जगह के दर्शन करना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ कालेश्वर महादेव मंदिर आने के लिए आप सड़क माध्यम एवं रेल मार्ग द्वारा भी आसानी से पहुंच सकते हैं हालांकि पहुंचने के लिए आप इस मंदिर में फ्लाइट के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं लेकिन एयरपोर्ट दूर होने के कारण आपको यात्रा में परेशानी आ सकती है।
सड़क मार्ग से – शिव कालेश्वर मंदिर उत्तराखंड पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया मार्ग सड़क मार्ग हैं यह जगह सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है एवं आप देश के किसी भी कोने से यहां आराम से आ सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से यह जगह मात्र लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है साथ ही देश की राजधानी दिल्ली से यह जगह लगभग 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग के माध्यम से आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं।
रेल मार्ग द्वारा -शिव कालेश्वर मंदिर उत्तराखंड में रेल मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। मंदिर लैंसडाउन में स्थित है एवं लैंसडाउन का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कोटद्वार में स्थित हैं । कोटद्वार से यह जगह मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहां से आप किसी लोकल टैक्सी एवं बस के माध्यम से भी आ सकते हैं।
हवाई मार्ग द्वारा – शिव कालेश्वर मंदिर उत्तराखंड (Shiv Kaleshwar Mahadev Temple)में वायु मार्ग द्वारा पहुंचना एक मुश्किल भरा काम है क्योंकि यहां का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित हैं जहां से यह जगह लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप फ्लाइट के माध्यम से लैंसडाउन की यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी एयरपोर्ट से फ्लाइट के माध्यम से देहरादून पहुंच सकते हैं और देहरादून से आप यहां किराए की टैक्सी एवं बस के माध्यम से आ सकते हैं।
दोस्तों यह तो हमारा आज का लेख शिव कालेश्वर मंदिर उत्तराखंड के बारे में आशा करते हैं कि आपको यह लेख पसंद आया होगा। आपको यह आलेख कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और यदि आप भी किसी जानकारी युक्त लेख हम तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी जानकारी साझा करना चाहते हैं तो आप भेज जख्म से संपर्क कर सकते हैं। आपका लेख हमारे लिए कीमती एवं जानकारी युक्त होगा। हम उसे अपने पाठकों के लिए जरूर प्रकाशित करेंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे देवभूमि उत्तराखंड को जरुरु फॉलो करें , आज हमसे से व्हाट्सअप और फेसबुक के माद्यम से भी संपर्क कर सकते है
घोड़ाखाल मंदिर. Ghodakhal Mandir Uttarakhand
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड की आज के नए लेख में। आज हम आप लोगों के साथ उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर घोड़ाखाल मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। घोड़ाखाल मंदिर उत्तराखंड के पवित्र एवं धार्मिक स्थलों में से एक है जो कि अपने इतिहास और पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है। आज के इस लेख में हम घोड़ाखाल मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं।
घोड़ाखाल मंदिर उत्तराखंड (Ghodakhal Mandir Uttarakhand) के पवित्र मंदिरों में से एक है जो कि जिला नैनीताल के भावली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। प्रसिद्ध घोड़ाखाल मंदिर न्याय देवता के रूप में गोलू देवता को समर्पित है। इस मंदिर को गोलज्यू महाराज के नाम से भी जाना जाता है।
आस्था और भक्ति का प्रतीक यह मंदिर हर वर्ष हजारों भक्तों को अपनी और आकर्षित करता है। मंदिर की मुख्य विशेषता है कि जो भी भक्त यहां सच्चे मन से कामना करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। घोड़ाखाल मंदिर एक रमणित शांत एवं धार्मिक स्थल के रूप में भी पहचाना जाता है। मंदिर के चारों दिशाओं में बंदी हजारों घंटियां गोलू देवता मंदिर की आस्था की ओर संकेत करते हैं।
घोड़ाखाल का शाब्दिक अर्थ. Ghodakhal Mandir Uttarakhand
दोस्तों घोड़ाखाल मंदिर नाम पड़ने के पीछे मान्यता है कि घोड़ाखाल एक छोटा सा गांव है ( Ghodakhal Village ) जो कि पहाड़ के सुरम्य घाटी के बीच स्थित है। यहां के निवासी आस्था और भक्ति से ओतप्रोत इसलिए उन लोगों ने पूजा की । और जिस स्थान पर उन लोगों ने पूजा की उसी स्थान पर गोलू देवता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता है कि मनोकामना पूर्ण होने पर हर वक्त यहां पर घंटी चढ़ाता है इसलिए इसलिए घंटियों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
आस्था और भक्ति का प्रतीक है गोलू देवता का मंदिर. Ghodakhal Mandir Uttarakhand
मंदिर के चारों दिशाओं में लकी घंटियां और भक्तों के द्वारा कागज पर लिखे मन्नत उसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह मंदिर आस्था और भक्ति का प्रतीक है। गोलू देवता अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि यहां पर भक्तों के द्वारा चिट्ठियों के रूप में अपनी मन्नतें लिखी जाती है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो भक्तों के माध्यम से मंदिर में घंटा चढ़ाई जाती है। मंदिर में मौजूद घंटियों की संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में गोलू देवता अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं।
वैसे तो इस मंदिर में वर्ष भर में हजारों की संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है लेकिन खासतौर पर नवरात्रि व श्रावण मास के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ इकट्ठा होती है।
घोड़ाखाल मंदिर की मान्यता. Ghodakhal Mandir Uttarakhand Manytayen
घोड़ाखाल मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो कि अपने पवित्र मान्यताओं के लिए भी पहचाना जाता है।
घोड़ाखाल
मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहां पर सभी भक्तों अपनी मुरादे
चिट्ठियों के माध्यम से गोलू देवता तक पहुंचाया करते हैं और न्याय के देवता
गोलू महाराज उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के
बावजूद भक्तों के माध्यम से मंदिर में घंटियां बेड स्वरूप चढ़ाई जाती है
वर्तमान में मौजूद घंटियों की संख्या के आधार पर आप मंदिर की पौराणिक महत्व
के बारे में जान सकते हैं।
गोलू देवता मंदिर के बारे में मान्यता है कि नवाब भाई जोड़ी इस मंदिर के दर्शन करते हैं तो उनका रिश्ता सात जन्मो तक बना रहता है। वाकई में उत्तराखंड का गोलू देवता मंदिर आस्था और भक्ति का प्रतीक है।
नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा. Nanda Devi Mandir Almora
नमस्ते दोस्तों देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस लेख के माध्यम से हम आप सभी लोगों के साथ नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मां नंदा देवी उत्तराखंड की कुलदेवी के रूप में भी जानी जाती है और इसके इतिहास और पौराणिक कहानी अपने आप में एक ऐतिहासिक पहलू बनी हुई है। अपनी धार्मिक छटा को प्रस्तुत कर दी मां नंदा देवी उत्तराखंड के सबसे पवित्र धामों में से एक है। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको मां नंदा देवी का इतिहास और पौराणिक कहानी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आशा करते हैं आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा। इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ना।
नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा. Nanda Devi Mandir Almora
कुमाऊं क्षेत्र के सबसे पवित्र धामों में से एक नंदा देवी का मंदिर अपने पौराणिक इतिहास और महत्व के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से 7816 मीटर की ऊंचाई पर इस पवित्र मंदिर में मां दुर्गा देवी का अवतार विराजमान है। प्रसिद्ध मां नंदा देवी का मंदिर चंद्रवंशी देवी के रूप में भी जानी जाती है। मंदिर में मां नंदा देवी और भगवान शंकर की पत्नी के रूप में पूजी जाती है।
मां नंदा देवी गढ़वाल की राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री है इसलिए सभी कुमाऊनी और गढ़वाली लोग उन्हें पर्वत पर्वतआंचल की पुत्री मानते हैं।
मां नंदा देवी का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है मां नंदा देवी का मंदिर शिव मंदिर की बाहरी ढलान पर स्थित है। पत्थर का मुकुट और दीवारों पर प्रतिमा बनाई गई इस मंदिर की कलाकृति की शोभा बढ़ाते हैं। मान्यता है कि नंदा देवी की उपासना प्राचीन काल से ही की जाती थी जिसके प्रमाण धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी मिलते हैं।
मां नंदा देवी मंदिर का पौराणिक इतिहास. Nanda Devi Mandir Ka Itihas
मां नंदा देवी मंदिर के पौराणिक इतिहास से संबंधित कई कहानियां एवं ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हुई है। इस स्थान में मां नंदा देवी को प्रदेश करने का श्रेय चंद्र शासकों को जाता है। किवदंती है कि 1670 में कुमाऊं के चंद शासक राजा बाज बहादुर चंद बधानकोट से मां नंदा देवी की सोने की मूर्ति लाए और मल्ला महल में स्थापित कर दिया।
बधाणकोट से विजय प्राप्त करने के बाद जब राजा जगत चंद्र को नंदा देवी की मूर्ति नहीं मिली तो उन्होंने खजाने में से अश्फियों को पिघलाकर मां नंदा देवी की भव्य मूर्ति बनाई। मोती बनाने के बाद राजा ने मूर्ती को मल्ला महल में स्थापित कर दिया। सन 1815 को कमिश्नर ट्रेल ने मां नंदा देवी की पूजनीय स्मृति को उधोत चंदेश्वर मंदिर में रखवा दिया।
मां नंदा देवी मंदिर की पौराणिक मान्यता. Nanda Devi Mandir Poranik Manyta
मां नंदा देवी मंदिर पौराणिक मान्यताओं के आधार पर प्रचलित है कि जब कमिश्नर ट्रेल नंदा देवी पर्वत की चोटी की ओर जा रहे थे तो अचानक कमिश्नर ट्रेल की रहस्यमय ढंग से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जिसके बाद वह स्थानीय लोगों से इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करने को कहते हैं। लोगों के द्वारा उन्हें अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर बनवा कर उसमें माता की पूजनीय स्मृति को स्थापित कराने के लिए कहा। इस ऐतिहासिक एवं रहस्यमई कार्य करने से उनकी कुदरती आंखों की रोशनी अपने आप ही वापस आ गए।
किवदंती यह भी है कि जब राजा बहादुर प्रताप को गढ़वाल पर आक्रमण करने के दौरान उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने प्रण किया कि उन्हें युद्ध में यदि विजय मिल जाती है तो वह नंदा देवी को अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजा करेंगे। और तब से मां नंदा देवी को इष्ट देवी और कुलदेवी के रूप में भी पूजा जाता है।
मां नंदा देवी मंदिर कैसे जाएं. Nanda Devi Mandir Kese Jaye
प्यारे पाठको यदि आप भी मां नंदा देवी के दर्शन करना चाहते हैं। मां नंदा देवी के पावन धाम यात्रा करना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मां नंदा देवी मंदिर कैसे पहुंचे।
दोस्तों मां नंदा देवी मंदिर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग के साथ-साथ रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विकल्प भी उपलब्ध है लेकिन सड़क मार्ग से सरलतम माध्यम हम सभी लोग मां नंदा देवी के पावन धाम में पहुंच सकते हैं।
सड़क मार्ग से मां नंदा देवी
सड़क मार्ग से मां नंदा देवी का मंदिर की यात्रा आसानी से की जा सकती है। सड़क मार्ग के माध्यम से भीमताल भवाली होते हुए अल्मोड़ा के रास्ते माता के पावन धाम में पहुंचा जा सकता है।
रेल मार्ग के माध्यम से मां नंदा देवी मंदिर
प्यारे पाठक को रेल मारे के माध्यम से मां नंदा देवी की यात्रा करना थोड़ा कठिन हो सकता है लेकिन बताना चाहेंगे कि नंदा देवी मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है यहां से आप अल्मोड़ा पहुंचने के लिए प्राइवेट टैक्सी और बस के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं।
हवाई मार्ग से नंदा देवी मंदिर
वायु मार्ग के माध्यम से नंदा देवी मंदिर पहुंचने के लिए हम सभी को अपने नजदीकी एयरपोर्ट से पंतनगर हवाई अड्डा पहुंचने की जरूरत है। मां नंदा देवी मंदिर का नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है जहां से हल्द्वानी की दूरी 27 किलोमीटर है जबकि हल्द्वानी से अल्मोड़ा लगभग 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बचे हुए सफर को आप टैक्सी और बस के माध्यम से भी कर सकते हैं।
दोस्तों यह तो हमारा आज का लेख जिसने हमने मां नंदा देवी के मंदिर और मां नंदा देवी मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक पहलुओं को जाना। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आया होगा यदि आपको यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। यदि आप भी अपना लेख हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपने बहुमूल्य शब्दों को ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं।
मां नंदा देवी मंदिर F&Q
Q – नंदा देवी मंदिर कहां है
Ans – मां नंदा देवी का पवित्र पावन धाम मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा जिले में स्थित है। मां नंदा देवी उत्तराखंड की ईस्ट एवं कुलदेवी के रूप में भी पूजी जाती है।
Q – नंदा देवी की ऊंचाई
Ans – मां नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 7816 मीटर है। नंदा देवी पर्वत भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है जो कि सिक्किम राज्य और नेपाल के सीमा के बीच स्थित है।
Q – मां नंदा देवी मंत्र
Ans – ॐ शिवाये नम:। * ॐ उमाये नम:। * ॐ जगत्प्रतिष्ठायै नम:। * ॐ शांतिरूपिण्यै नम
पाताल भुवनेश्वर मंदिर. Patal Bhubaneswar Mandir
हेलो दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में । आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको पाताल भुवनेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और यहां पर पवित्र धामों और धार्मिक स्थलों के साथ विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्थल अपने महत्व को संजोए हुए हैं। आज भी इनकी रहस्य और मान्यताएं उनको बहुत खास बनाती है। स्थानों में से एक है पाताल भुवनेश्वर मंदिर ( Patal Bhubaneswar Mandir)जो कि अपनी पौराणिक इतिहास और मान्यताओं के लिए पहचाना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड का यह लेख पाताल भुवनेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी देने वाला है। आशा करते हैं कि आपको यह देख जरूर पसंद आएगा।
पाताल भुवनेश्वर मंदिर. Patal Bhubaneswar Mandir
प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर मंदिर भगवान शिव जी की पवित्र मंदिरों में से एक है जो कि अपने चमत्कारिक व ऐतिहासिक रहस्यों के लिए पहचानी जाती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के भुवनेश्वर गांव में स्थित यह मंदिर आस्था और भक्ति का प्रतीक है।
मंदिर समुद्र तल से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक गुफा जो कि पूरे वर्ष भर में हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गंगोलीहाट तहसील से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह चमत्कारी गुफा भगवान भोलेनाथ के भक्तों की पवित्र धाम है। यह गुफा प्रवेश द्वार से लगभग 160 मीटर लंबी है और 90 फीट गहरी है। श्रद्धालुओं को 90 फीट गहरे स्थान में जाकर पाताल भुवनेश्वर के दर्शन होते हैं।
पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज कब हुई. Patal Bhubaneswar Gufa Ki Khoj
पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज श्रेया राजा रितुपर्णा को जाता हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में राजा रितुपर्णा ने इस गुफा की खोज की थी जिसके बाद उन्हें नागों के राजा अधिशेष मिले थे। ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज करने वाले पहले मनुष्य में से राजा ऋतुराज पहले व्यक्ति हैं।
राजा अधिशेष के माध्यम से रितुपर्णा को इस गुफा के अंदर ले जाया गया और जहां उन्होंने सभी देवी देवताओं के साथ भगवान शिव जी के दर्शन किए। मान्यता है कि रितुपर्णा के बाद इस गुफा की चर्चा नहीं हुई। जबकि द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा को वापस ढूंढ लिया गया था।
पाताल भुवनेश्वर मंदिर की मान्यताएं. Patal Bhubaneswar Mandir Ki Manytaye
पाताल भुवनेश्वर मंदिर की ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर किवदंती है कि हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को पूजा जाता है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान सिंह जी ने क्रोध में गणेश जी का सिर अलग कर दिया था और बाद में माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव जी गणेश जी पर हाथी का मस्तक लगाया था। लेकिन गणेश जी का मस्तक जो अलग हुआ था उसे भगवान शिव जी द्वारा पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा गया था। इसलिए पाताल भुवनेश्वर मंदिर की मान्यताएं ( Patal Bhubaneswar Mandir) पौराणिक काल से जुड़ी हुई है। जो कि आज के समय में भी अपने महत्व को संजोए हुए हैं।
गुफा में भगवान गणेश के कटे हुए शिलारूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल के रूप में एक चट्टान है। इस ब्रह्म कमल रूपी चट्टान से भगवान गणेश जी के शिलारुपी मस्तक दिव्या रोटी पानी की अमृतवाणी पड़ती रहती है।
पाताल भुवनेश्वर क्यों प्रसिद्ध है. Patal Bhubaneswar Mandir Kyu Parashidh Hai
पाताल भुवनेश्वर गुफा अपने पौराणिक इतिहास के साथ-साथ भगवान शिव जी की प्रतिमा और सभी देवी देवताओं के प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। पाताल भुवनेश्वर चूना पत्थर की एक प्राकृतिक उपाय है जो उत्तराखंड राज्य की पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह गुफा भूमि से 90 फीट गहरे होने के कारण इसके राज और चमत्कारी रहस्य इसको बहुत खास बनाते हैं।
पाताल भुवनेश्वर गुफा वही स्थान है जहां पर भगवान शिव जी ने अपने पुत्र गणेश के कटे हुए सर को विराजमान किया था। गुफा में 108 पंखुड़ियों वाला पत्थर का ब्रह्म कमल है जिससे गणेश जी की मूर्ति के मस्तक पर पानी की अमृत बूंदें पड़ती हैं।
यह एक ऐतिहासिक गुफा है इसलिए पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन करना हर एक शिव भक्तों का सपना होता है। यह भगवान शिवजी से जुड़े प्रमुख स्थानों में से एक है।
पाताल भुवनेश्वर मंदिर कैसे पहुंचे. Patal Bhubaneswar Mandir Kese Pachuche
प्यारे पाठको पाताल भुवनेश्वर मंदिर के बारे में तो हम जान चुके हैं लेकिन यदि आप भी इस ऐतिहासिक पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो हम आपको इस गुफा तक पहुंचने के लिए मार्ग का विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।
पाताल भुवनेश्वर जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता सड़क मार्ग है क्योंकि पाताल गुफा जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे अच्छी अच्छा माध्यम है। पिथौरागढ़ जिले से पाताल गुफा 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
रेल मार्ग द्वारा
रेल मार्ग द्वारा पाताल भुवनेश्वर पहुंचने के लिए हमें अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से काठगोदाम आना है। काठगोदाम पाताल भुवनेश्वर ( Patal Bhubaneswar Mandir) का नजदीकी रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम से अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से भुवनेश्वर गांव तक सड़क मार्ग के माध्यम से आ सकते हैं।
वायु मार्ग द्वारा
यदि वायु मार्ग द्वारा पाताल भुवनेश्वर गुफा पहुंचने की बात की जाए तो इसका निकटतम हवाई अड्डा नैनी सैनी हवाई अड्डा है जोकि पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यहां से सड़क मार्ग के द्वारा बस और टैक्सी के माध्यम से भी पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन किए जा सकते हैं।
दोस्तों यह था हमारा आज का लेख जिसमें हमने आपको पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में जानकारी( Patal Bhubaneswar Mandir) दी। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह नहीं जरूर पसंद आया होगा यदि आपको यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं।
पाताल भुवनेश्वर गुफा F&Q
Q – पाताल भुवनेश्वर कहां है
Ans – पाताल भुवनेश्वर गुफा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित पिथौरागढ़ जिले के भुवनेश्वर गांव में स्थित यह प्राचीन गुफा अपने दिव्य इतिहास और पौराणिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऐतिहासिक महत्व होने के कारण हर कोई यहां आने के लिए बेताब रहता है।
Q – अल्मोड़ा से पाताल भुवनेश्वर की दूरी
Ans – अल्मोड़ा से पाताल भुवनेश्वर की दूरी 110 किलोमीटर है। जबकि पिथौरागढ़ जिले से यह 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा भगवान शिव जी और अन्य देवी देवताओं की रहस्यमई प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
Q – भुवनेश्वर मंदिर का इतिहास
Ans – भुवनेश्वर मंदिर का इतिहास भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जय भगवान शिव जी ने गुस्से में आकर गणेश जी का सर काटा था तो। कटे हुए सर को उनके द्वारा पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा गया था। पाताल भुवनेश्वर गुफा में भगवान शिवजी और पार्वती के अलावा विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा शामिल है।
मनिला देवी मंदिर. Manila Devi mandir Uttarakhand
नमस्ते दोस्तों देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में आपका स्वागत है आज हम आपको उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर मनिला देवी मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित मनिला देवी मंदिर आस्था और भक्ति का प्रतीक है। आज के इस लेख में हम मनिला देवी मंदिर और मनिला देवी मंदिर का इतिहास के साथ मनिला देवी मंदिर का पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा।
मनिला देवी मंदिर के बारे में. Manila Devi mandir Ke Baren Me
प्रसिद्ध मनिला देवी मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित सल्ट क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है। देवदार और चील की खूबसूरत वृक्षों से गिरा हुआ मनीला माता मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
मनीला न केवल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अभी तो यह एक उत्तराखंड का पर्यटन स्थल भी है। रामनगर से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित माता का यह भव्य मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहां पर हर साल हजारों की संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है।
मनीला में माता के दो भव्य मंदिर है एक मंदिर का नाम मल्ला मनीला है जबकि दूसरे मंदिर का नाम तल्ला मनीला है। मल्ला मनीला मंदिर से तात्पर्य गांव की ऊपरी ओर बसा हुआ मंदिर जबकि तल्ला मनिला मंदिर से तात्पर्य गांव के निचली ओर बना हुआ मंदिर से है।
मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली के अंतर्गत किया गया है और मंदिर में मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी की मूर्तियों के साथ काले पत्थर से बनी मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा मौजूद है।
मनिला मंदिर देवी का इतिहास. Manila Devi mandir Ka Itihas
दोस्तों जिस तरह से हर किसी मंदिर का अपना अस्तित्व और अपना महत्व होता है ठीक उसी तरह से मनिला देवी मंदिर का इतिहास भी अपने आप में एक खास स्थान रखता है। इतिहास के आधार पर मान्यता है कि मनिला देवी को कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी कहा जाता था। इसलिए मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी राजाओं को जाता है। मनिला देवी मंदिर का निर्माण 1488 में कचोरी राजा ब्रह्मदेव में किया था। इस मंदिर को खास बनाती है इसकी कत्यूरी निर्माण शैली इसे देखने के लिए हर वर्ष हजारों की संख्या में भक्तों का निहाया करते हैं।
मनीला माता मंदिर पौराणिक महत्व. Manila Devi mandir Mahatwa
आस्था और भक्ति का प्रतीक मनीला माता का मंदिर का पौराणिक महत्व अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। लोगों की मान्यता अनुसार जो भी श्रद्धालु यहां पर सच्चे मन से कामना करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इसीलिए मनीला माता पर श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास रहता है।
मंदिर के महत्व के बारे में बताया जाता है कि नवविवाहित जोड़ियों द्वारा जब मंदिर में मन्नते मांगी जाती है तो माता देवी मनीला उनके झुर्रियों को खुशियों से भर देती है।
मंदिर मुख्य रूप से एक पर्यटन का हिस्सा भी है। इसके आसपास देवदार और चीड़, बांज सदाबहार खूबसूरत से पेड़ स्थित है जो यहां आए श्रद्धालुओं को छांव प्रदान करते हैं।
मनीला माता मंदिर की कहानी. Manila Devi mandir Ki Kahani
मनिला देवी क्षेत्र के कुलदेवी के रूप में भी जानी जाती है। जो कि उन्हें हर समय सचेत रखती है। किसी भी प्रकार की अनहोनी का संकेत माता अपने भक्तों को पहले ही दे देती है। मनीला माता मंदिर की कहानी के बारे में बताया जाता है कि प्राचीन काल में दूर प्रदेश से बैलों की खरीदारी करने बाहरी लोग गांव में आए थे। मनीला क्षेत्र में उन्हें एक किसान के बैल बड़े पसंद आ जाते हैं लेकिन मोलभाव का तालमेल ना बैठ पाने के कारण बैलों का मालिक उन्हें देने से मना कर देता है।
इस तरह से बैलों को खरीदने आए व्यापारी उन्हें नहीं ले जा सके। लेकिन उन्हें बेल काफी पसंद थी इसलिए उन्होंने उन्हें चोरी करने की योजना बनाई। एक रात उन्होंने बालों को चोरी करने का फैसला किया और जैसे ही बाहर गांव में घुसे तो माता मनिला देवी द्वारा बैल की मालकिन को आवाज देकर उठाया गया जिससे वह चोरी करने में असफल हो गए।
व्यापारी बहनों को चुराने में असफल हो गए लेकिन उन्होंने मंदिर में स्थित देवी की प्रतिमा को चुराने की योजना बनाई। जैसे ही वह लोग चोरी के भाव से मंदिर में घुसे और देवी की प्रतिमा को हिलाना चाहा लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिली। इस कार्य को करने के दौरान माता की मूर्ती से हाथ अलग हो जाता है। व्यापारी उस हाथ को लेकर ही आगे बढ़ते हैं लेकिन रास्ते में पहुंचकर उस हाथ का वजन इतना भारी हो गया कि उसे उठाना उन व्यापारियों के वश में नहीं था। उन्होंने उस हाथ को वहीं पर छोड़ दिया। सुबह जब गांव वालों को इस घटना का पता चला तो उन्होंने जहां पर माता का हाथ रखा हुआ था वहां पर मंदिर बनाने का फैसला किया। इस तरह से मनीला में माता के दो भव्य मंदिर मल्ला और तल्ला नाम से प्रसिद्ध है।
मनीला माता मंदिर कैसे पहुंचे. Manila Devi mandir Kese Pahuchen
प्यारे पाठको अभी तक हम मनीला माता मंदिर के बारे में जान चुके हैं यदि आप भी मनीला माता मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो हम आपको मनीला माता मंदिर कैसे पहुंचे के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं।
मनीला माता मंदिर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग के साथ-साथ वायु मार्ग और रेल मार्ग का विकल्प भी उपलब्ध है। लेकिन सड़क मार्ग की अच्छी संपर्क ना होने के कारण सभी श्रद्धालु सड़क मार्ग के माध्यम से ही माता के दर्शन किया करते हैं। मनीला माता मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन रामनगर है जबकि इसका नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है। यहां से आप बस और टैक्सी के माध्यम से भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं।
प्रमुख जगहों से मनीला माता मंदिर की दूरी निम्न प्रकार से है
अल्मोड़ा से मनिला देवी मंदिर की दूरी 128 किलोमीटर है
रानीखेत से मनिला देवी मंदिर की दूरी 85 किलोमीटर है।
रामनगर से मनीला माता मंदिर की दूरी 80 किलोमीटर है
पंतनगर से मनीला माता मंदिर की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है
दोस्तों यह था हमारा आज का लेख जिसमें हमने मनिला मंदिर के बारें में
बात की है। आशा करते है की आपको हमारा यह लेख पसंद आएगा , आपको यह लेख कैसा
लगा हमें टिप्पणी के माध्यम से बातें।
ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे
देवभूमि उत्तराखंड को जरुरु फॉलो करें , आज हमसे से व्हाट्सअप और फेसबुक के
माद्यम से भी संपर्क कर सकते है
भैरव बाबा उत्तराखंड. Bhairabh Baba Uttarakhand
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड की आज के नए लेख में। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको भैरव बाबा उत्तराखंड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही दिव्य आत्माओं का निवास स्थान रही है। प्राचीन काल से ही इसके कण-कण में भगवान एवं देवी देवताओं का वास रहा है। उन्हीं दिव्य आत्माओं में से एक है भैरव बाबा जोकि उत्तराखंड में काफी प्रसिद्ध है। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको भैरव बाबा के बारे में जानकारी देने वाले हैं आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आएगा। इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ना।
भैरव बाबा उत्तराखंड के कुल देव के रूप में भी पूजे जाते है। काल भैरव कलयुग के जागृत देवता हैं। भैरव बाबा भगवान शिव जी के पूर्ण रूप माने जाते हैं। भगवान शिव जी के रूपों में से एक भैरव बाबा कहानी के आधार पर किवदंती है कि ।
एक ऋषि-मुनियों ने सभी देवी देवताओं से पूछा कि आप सभी में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। सभी देवी देवताओं के द्वारा एक ही ऊंचे स्वर में बताया गया कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ और ज्ञानी पूजनीय भगवान शिवजी है। यह बात सृष्टि की रचना सुनने वाले ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आई और वे भगवान भोलेनाथ की वेशभूषा के बारे में उल्टा सीधा कहने लगे।
ब्रह्मा जी के पांचवें सिर ने कहा की जिस व्यक्ति के पास अच्छे वस्त्र और धन वैभव नहीं है वह व्यक्ति सृष्टि में सबसे कैसे हो सकते हैं। इन सभी बातों को सुनकर देवी देवताओं को बहुत दुख हुआ । उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती के तेज से एक तेजपुंज पर प्रकट हुवा । वह तेज जोर-जोर से रुद्र कर रहे थे उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि यह उनके तेज से उत्पन्न हुआ है। इसलिए उन्होंने उसका नाम रूद्र रख दिया जोकि भैरव बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं।

भगवान शिव जी के बारे में ऐसे ऐसे प्रचंड शब्द उस बालक के द्वारा नहीं सुनी गए और उसने क्रोध में आकर अपने हाथ की कानी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के पांचवे में सर को काट दिया। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अपने पांचवे सिर से पांचवा वेद की रचना करने वाले थे।
इसी कारण से भैरव को ब्रह्मा जी की हत्या का पाप लग गया और उन्हें काल भैरव के नाम से जाना जाने लगा। इस शराब से बचने के लिए भगवान शिव जी ने भैरव जी से कहा कि तुम वर्मा जी के कटे हुए सिर को हाथ में लेकर भीख मांग कर अपने पापों और कष्टों को भुक्तोगे। और कहा कि जब तक तुम इस बात से मुक्त नहीं हो जाते तब तक आप लोग में घूमते रहो और तुम काशी में चले जाओ वही रहना।
जैसे ही भैरव जी काशी में पहुंचे और काशी में पहुंचने के बाद अचानक से ब्रह्मा जी का शीश स्वताः उनके हाथों से गिरकर काशी में गिर गया। और तभी भैरवनाथ अपने पाप से भी मुक्त हो गए। और माना जाता है कि जिस जगह पर ब्रह्मा जी का कपाल गिरा वह स्थान कपाल मोचन कहलाया।
दोस्तों यह भैरव बाबा उत्तराखंड के बारे में जानकारी। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया होगा। आपको यह लेख कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और यदि आपको यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। भैरवनाथ बाबा के बारे में अधिक जानकारी पाने वा पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।
दायरा बुग्याल ट्रैक. Daira Bugyal Uttarakashi
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज के इस लेख के माध्यम से हम आप लोगों के साथ दयारा बुग्याल उत्तरकाशी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देव भूमि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य का एक जगमगाता उदाहरण है। जो धार्मिक पर्यटन स्थल और प्रकृति की हसीन वादियों को अपने में समेटे हुआ है। उन्हीं खूबसूरत पर्यटन स्थलों मैं से एक है दायरा बुग्याल उत्तरकाशी जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं और हर वर्ष लाखों पर्यटकों को अपनी और आकर्षित करता है। आज के इस लेख में हम आपको दायरा बुग्याल एवं दायरा बुग्याल ट्रेक के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आएगा इसलिए इसे अंत तक जरूर पढ़ना।
प्रकृति का स्वर्ग कहे जाने वाले उत्तराखंड में घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ है। उन्हें खूबसूरत जगहों में से एक है दायरा बुग्याल। जोकि उत्तराखंड के प्रसिद्ध बुग्यालों में से एक है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित दायरा बुग्याल एक रमणीक और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करने वाले पर्यटन स्थलों में से एक हैं। दायरा बुग्याल ट्रैक उत्तराखंड में काफी प्रसिद्ध है । समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दायरा बुग्याल सर्दियों के समय में बर्फ से ढके खूबसूरत से हास्य प्रस्तुत कराता है। दरअसल अब आप यह सोच रहे होंगे कि दायरा बुग्याल या बुग्याल क्या होते हैं। चलिए हम पहले बुग्याल के बारे में जानते हैं।
बुग्याल क्या होते हैं. Bugyal Kya Hote Hai
बुग्याल मुख्य रूप से पहाड़ की चोटी पर स्थित वह जगह है जहां पर छोटी-छोटी घास होती है। इस इस क्षेत्र में पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। और दूर दूर तक यहां से खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत होते हैं इसलिए उन्हें बुग्याल कहा जाता है। पहाड़ की चोटी पर हल्की-फुल्की घास और पेड़ पौधों से वंचित जगह को बुग्याल कहते हैं।
दायरा बुग्याल उत्तरकाशी. Daira Bugyal Uttarakashi
दायरा बुग्याल भी उन्हीं प्रमुख बुग्यालों में से एक है जो पूरे वर्ष भर में लगभग हजारों आगंतुकों को आकर्षक करता है। दायरा बुग्याल मुख्य रूप से प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है जिसके कारण यह कैंपिंग और ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों को अंजाम देता है। यदि आप लोग प्रकृति प्रेमी हैं और पहाड़ों में यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं। तो दायरा बुग्याल आपके लिए एक अच्छा यात्रा विकल्प हो सकता है।

दायरा बुग्याल दोस्तों के साथ यात्रा करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। इस खूबसूरत से स्थान में आप कैंपिंग और ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। पहाड़ की खूबसूरत सी चोटी पर बने कैंप दोस्तों के साथ खूबसूरत से पल बिताने के लिए आपको मंजूर करने वाला है।
दायरा बुग्याल से आप आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ स्थानीय गांव के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सर्दियों के समय में दायरा बुग्याल की यात्रा का प्लान बनाते हैं तो आप को यहां पर बर्फ से ढकी खूबसूरत सी चोटिया भी देखने को मिल जाती है।
यदि आप शहर की तपती गर्मी से कुछ दिन की छुट्टियां लेकर पहाड़ी के लिए स्टेशन और पहाड़ के मनोरम दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं। जहां पर शुद्ध हवा पानी और शहर की तपती गर्मी से छुटकारा मिल सके। तो दायरा बुग्याल कहीं ना कहीं आपको अपनी और आकर्षित करने वाला है। इसके आसपास का खूबसूरत दृश्य वाकई में देखने लायक है। यदि आप भी वाकई में प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको जिंदगी में एक बार दायरा बुग्याल के दर्शन जरूर करने चाहिएं।
दायरा बुग्याल कैसे पहुंचे. Daira Bugyal Kese Pachuchen
दोस्तों यदि आप भी दायरा बुग्याल के दर्शन करना चाहते हैं और दयारा बुग्याल कैसे पहुंचे सवाल से परेशान हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड के माध्यम से आपको किसी भी विषय के ऊपर संपूर्ण जानकारी दी जाती है।
दायरा बुग्याल मुख्य रूप से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। इसका निकटवर्ती गांव बारसू गांव है। यहां से दायरा बुग्याल की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। बारसू गांव तक पहुंचने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बस एवं टैक्सिया उपलब्ध है। देहरादून से लगभग 186 किलोमीटर की दूरी तय करने पर दायरा बुग्याल के दर्शन होते हैं। आप अपने नजदीकी शहर, कस्बे, व गांव से दायरा बुग्याल के दर्शन कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से दयारा बुग्याल की दूरी लगभग देहरादून होते हुए 350 किलोमीटर है। सड़क मार्ग के माध्यम से आप यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
दोस्तों यह तो हमारा आज का लेख जिसमें हमने आपको दायरा बुग्याल के बारे में जानकारी साझा की। यह लेख पढ़ने के बाद आपको दायरा बुग्याल ट्रैक एवं दायरा बुग्याल उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आपको यह आलेख कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और यदि आपको यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।
यदि आप भी ऐसे ही उत्तराखंड से संबंधित जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमें फेसबुक एवं इस संग्राम के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।
तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड. Tungnath Temple Uttarakhand
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज के इस लेख के माध्यम से हम आप लोगों के साथ उत्तराखंड का पवित्र धाम तुंगनाथ मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भगवान भोलेनाथ की कई ऐसी पवित्र धाम है जो कि अपनी इतिहास और पौराणिक मान्यताओं को अपने में समेटे हुए हैं। उन्हीं स्थानों में से एक है तुंगनाथ मंदिर जोकि अपने भव्य इतिहास और मान्यताओं के अलावा यहां के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी पहचाना जाता है। आज के इस लेख में हम आपको तुंगनाथ मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आशा करते हैं कि दोस्तों आपको हमारे यह लेख पसंद आएगा इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ना।
भगवान शिव जी को समर्पित तुंगनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है । हिमालय की खूबसूरत प्राकृतिक वादियों के बीच में स्थिति भगवान भोलेनाथ का यह पावन धाम मंदिर 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
यहां भगवान शिव जी के पंच केदार रूप में से एक की पूजा की जाती है। ऐतिहासिक मान्यता है कि तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव जी के सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिरों में से एक है। जिसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से भव्य एवं आकर्षक तरीके से किया गया है। इसके आसपास का सुंदर सा वातावरण और हिमालय के शानदार दृश्य प्रस्तुत करते यहां के खूबसूरत से पर्वत शरद ऋतु में बर्फ की चादर ओढ़े दिखाई देते हैं। शायद यही कारण है कि पूरे वर्ष भर में यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आया करते हैं।
तुंगनाथ महादेव मंदिर की स्थापना. Tungnath Mandir Isthapna
पौराणिक कहानियों के आधार पर तुंगनाथ महादेव मंदिर की स्थापना आज से करीब 1000 वर्षों से भी पहले का माना जाता है। किवदंती है कि तुंगनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने संबंधियों के नरसंहार के पाप से बचने के लिए करवाया था। मान्यता है कि जब कुरुक्षेत्र में पांडवों की लड़ाई हुई थी तो उनके सगे संबंधी भी उनके द्वारा मारे गए थे जिसके कारण भगवान शिव जी उनसे नाराज हो गए थे और भगवान शिव जी को मनाने के लिए उन्होंने तुंगनाथ मंदिर की स्थापना की थी।

तुंगनाथ मंदिर की पौराणिक मान्यताएं. Tungnath Mandir Manyta
प्यारे पाठको तुंगनाथ मंदिर की पौराणिक मान्यताओं के बारे में किवदंती है कि यहां पर भगवान भोलेनाथ के हृदय और उनकी भुजाओं की पूजा होती है। मंदिर में पूजा कार्य का दायित्व स्थानीय लोगों का होता है। जबकि चार धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं द्वारा इस मंदिर के दर्शन बड़े आराम से किए जा सकते हैं।
तुंगनाथ मंदिर के कपाट मई के महीने में खुलते हैं और लगभग सर्दियों में यानी कि नवंबर माह में दीपावली के समय बंद कर दिए जाते हैं। इस बीच यहां पर काफी बर्फ पड़ती है इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए मंदिर के कपाट मई के महीने में खोले जाते हैं।
तुंगनाथ महादेव मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्षों से पुराना है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के कारण तुंगनाथ को भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। इसके निकटवर्ती दार्शनिक स्थल में चोपता है जहां से मंदिर की दूरी मात्र 3.30 किलोमीटर है ।

तुंगनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय. Tungnath Mandir Jane Ka Samay
प्यारे पाठको जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि तुम नाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मई से लेकर अक्टूबर माह तक होता है। क्योंकि इसके बाद यहां प अधिक बर्फ एवं ठंड होने के कारण मौसम ठंडा रहता है श्रद्धालुओं के आवागमन में परेशानियां देखने को मिलती है।
इसलिए तुंगनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मई माह से अक्टूबर माह के बीच माना जाता है। इस बीच यहां का मौसम अच्छे बने रहने के साथ-साथ गर्मी के मौसम से भी निजात दिलाता है।
तुंगनाथ मंदिर कैसे जाएं. Tungnath Mandir Kese Jayen
दोस्तों तुंगनाथ मंदिर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग के साथ-साथ वायु मार्ग एवं रेल मार्ग का विकल्प भी शामिल है। सड़क मार्ग के माध्यम से रघुनाथ मंदिर आराम से पहुंचा जा सकता है। सर्वप्रथम श्रद्धालु चोपता पहुंचते हैं जिसके बाद वह मंदिर परिसर तक आराम से पहुंच सकते हैं।
रेल मार्ग के माध्यम से चोपता पहुंचना काफी आसान है। तुंगनाथ मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और काठगोदाम है जोकि चोपता से लगभग 207 किलोमीटर एवं 276 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

हवाई जहाज के द्वारा तुंगनाथ मंदिर पहुंचने के लिए निकटतम एयरपोर्ट जौली ग्रांट है। यहां से चोपता की दूरी करीब 224 किलोमीटर है। आप अपने नजदीक एयरपोर्ट से जौलीग्रांट तक पहुंच सकते हैं और यहां से प्राइवेट टैक्सी एवं बस के माध्यम से भी तुंगनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं।
दोस्तों यह तो हमारा आजकल एक जिसमें हमने आपको तुंगनाथ मंदिर के बारे में जानकारी दी। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि आपको तुंगनाथ मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी । यदि आपको हमारा यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।
तुंगनाथ महादेव मंदिर F&Q
Q – तुंगनाथ की ऊंचाई
Ans – भगवान शिव जी को समर्पित तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां भगवान शिव जी के पंच केदार रूप में से एक की पूजा की जाती है।
Q – तुंगनाथ मंदिर कहां स्थित है।
Ans – तुंगनाथ मंदिर भारत के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित चोपता से लगभग 71 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ एक भव्य मंदिर है। जो कि पूरे वर्ष भर में लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।
Q – चोपता से तुंगनाथ की दूरी
Ans – चोपता से तुंगनाथ मंदिर की दूरी लगभग 71 किलोमीटर है। यहां से सभी श्रद्धालु सड़क मार्ग के माध्यम से बस एवं प्राइवेट टैक्सी के द्वारा भी तुंगनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। चार धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के द्वारा तुंगनाथ मंदिर के दर्शन किए जाते हैं
Q – ऋषिकेश से तुंगनाथ की दूरी
Ans – ऋषिकेश से तुंगनाथ मंदिर की दूरी 206 किलोमीटर है। ऋषिकेश तुंगनाथ मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन है। यहां से प्राइवेट टैक्सी एवं बस के माध्यम से अभी तक नाथ मंदिर पहुंचा जा सकता है। आमतौर पर श्रद्धालु चोपता होते हुए तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं।
Q – रुद्रप्रयाग से तुंगनाथ की दूरी
Ans – रुद्रप्रयाग से तुंगनाथ मंदिर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। यहां से प्राइवेट टैक्सी और बस के माध्यम से भी श्रद्धालु तुंगनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ऐतिहासिक मान्यता है कि तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव जी के सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिरों में से एक है।
छोटा कैलाश धाम उत्तराखंड. Chota Kailash Dhaam Mandir
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में। आज के इस लेख के माध्यम से हम आप लोगों के साथ छोटा कैलाश धाम के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों तीर्थ स्थल ऐसे हैं जो कि अपनी पौराणिक शक्तियों एवं स्थानीय मान्यताओं के लिए पहचानी जाती है। आज के समय में भी उन तीर्थ स्थलों के प्रति लोगों का अटूट विश्वास देखने को मिलता है। उन्हीं पवित्र धामों में से एक है छोटा कैलाश धाम। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको छोटा कैलाश धाम के बारे में छोटा कैलाश धाम के इतिहास और इसके बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि आपको हमारा यह देख जरूर पसंद आएगा। इसलिए इसे अंदर जरूर पढ़ना।
छोटा कैलाश धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में पिनरों गांव की एक छोटी सी चोटी में स्थित है। हल्द्वानी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटा कैलाश धाम मंदिर अपनी भव्य वास्तु कला एवं शिल्प कला के लिए भी पहचाना जाता है।
छोटा कैलाश धाम मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है वह आसपास के सभी ऊंचे पर्वतों में से एक है। इसलिए इसके आसपास कभी काफी खूबसूरत एवं मनमोहक लगता है जिसके कारण यहां पर पूरे वर्ष भर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु आया करते हैं।
छोटा कैलाश धाम पहुंचने का पैदल रास्ता काफी शांत वातावरण और सुंदर वादियों के बीच से होते हुए हैं। कैलाश धाम मंदिर के रास्ते में कई छोटे-बड़े घर दिखाई देते हैं जो कि स्थानीय वास्तुकला से निर्मित होते हैं और बेहद खूबसूरत लगते हैं।
छोटा कैलाश धाम की मान्यताएं. Chota Kailash Dhaam Ki Manytayen
प्यारे दोस्तों जिस तरह से छोटा कैलाश धाम अपने अलौकिक शक्तियों के लिए पहचाना जाता है ठीक उसी तरह से छोटा कैलाश धाम की मान्यताएं भी अपने आप में खास महत्व रखती है। छोटा कैलाश धाम के बारे में मान्यता है कि सतयुग में भगवान भोलेनाथ एक बार यहां आए थे और उन्होंने अपने हिमालय भ्रमण के दौरान भगवान शिव जी एवं मां पार्वती जी ने इसी पर्वत पर विश्राम किया था। और भगवान भोलेनाथ में छोटा कैलाश धाम पर ही धुन रमाई थी। तभी से यहां अखंड धूनी जुलाई जाती है।
छोटा कैलाश धाम की मान्यता है कि यहां पर स्थित शिवलिंग के दर्शन जो कोई भी भक्त करता है भगवान शिवजी उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। किवदंती है कि भक्तों की मन्नत पूरी होने पर इस मंदिर में घंटी और चांदी का छत्र चलाते हैं।

छोटा कैलाश धाम की दूसरी मान्यता यह भी है कि त्रेता युग में भगवान शिव जी ने राम और लक्ष्मण के बीच हुए युद्ध को इसी पर्वत से देखा था।
जब भगवान शिव जी ने ही छोटे कैलाश धाम में वास किया था तो उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों से यहां पर एक कुंड का निर्माण किया जिसे पार्वती कुंड कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि बाद में इस पवित्र कुंड को किसी व्यक्ति ने अपवित्र कर दिया था तो वह कुंड सो गया था और उस में बहने वाली तीन सतत जलधाराएं विभक्त होकर पहाड़ी के तीन कोणों प्थम गई थी।
छोटा कैलाश धाम शिवरात्रि का भव्य मेला. Chota Kailash Dhaam Mela
भगवान शिव जी का वास स्थान छोटा कैलाश धाम। वैसे तो श्रद्धालुओं के लिए हमेशा ही खास रहता है लेकिन खास तौर पर शिवरात्रि के दिन यहां पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पधार कर मेले का आनंद लिया करते हैं।
मेले में स्थानीय लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। साथ ही दूर-दूर से श्रद्धालु छोटा कैलाश धाम में शिवरात्रि के पावन अवसर पर आया करते हैं। मान्यता है कि चोटा कैलाश धाम के प्रति श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास रहता है इसलिए भगवान भोलेनाथ यहां आए श्रद्धालुओं की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं।

दोस्तों यह था हमारा आज का लेख। जिसमें हमने छोटा कैलाश धाम के बारे में जानकारी साझा की। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया होगा। यदि आपको यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। और यदि आप भी ऐसी ही अनमोल जानकारी हमारे पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें गेस्ट पोस्ट के माध्यम से भी लिख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।
कपिलेश्वर महादेव मंदिर पिथौरागढ़. Kapileshwar Mahadev Mandir
नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के आज के नए लेख में।
आज के इस ले के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड का प्रसिद्ध कपिलेश्वर महादेव
मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं।
देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन
काल से ही दिव्य आत्माओं का निवास स्थान रही है। यहां पर भगवान शिव जी को
समर्पित कई ऐसे तीर्थ स्थल है जिनकी कण-कण में भगवान शिव जी का वास है
उन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है कपिलेश्वर महादेव मंदिर जो कि अपने
इतिहास और पौराणिक महत्व के लिए पहचाना जाता है। आज की इसलिए के माध्यम से
हम आप लोगों के साथ कपिलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास एवं कपिलेश्वर महादेव
मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। आशा करते
हैं कि आपको हमारे यह लेख जरूर पसंद आएगा।
भगवान भोलेनाथ को समर्पित कपिलेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। प्रसिद्ध मंदिर टकोरा एवं टकारी गांव के ऊपर सोर घाटी में स्थित है। 10 मीटर गहरी गुफा हमें बना हुआ यह मंदिर अपने पौराणिक इतिहास स्थानीय लोगों के अटूट विश्वास के लिए प्रसिद्ध है।
मंदिर में प्रवेश करने के लिए मुख्य मंदिर पहुंचने के लिए लगभग 200 से अधिक सीढ़ियां बनाई गई है। मंदिर अपने प्राचीन भाषा और शिल्प कला का एक जगमगाता उदाहरण है। पुराने लोगों की कौशल को अपने में समेटे कपिलेश्वर महादेव मंदिर पूरे वर्ष भर में हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।
वैसे तो कपिलेश्वर महादेव मंदिर में हर दिन श्रद्धालु दर्शन के लिए आया करते हैं लेकिन खासतौर पर शिवरात्रि के दिन यहां पर हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आया करते हैं। स्थानीय मान्यता है कि जो भी भक्त यहां पर सच्चे मन से कामना करते हैं भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं।
कपिलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास. Kapileshwar Mahadev Mandir Ka Itihas
प्यारे पाठको वैसे तो कपिलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार इस मंदिर को सैकड़ों वर्षों से देखते आ रहे हैं।
पौराणिक कहानी के आधार पर किवदंती है कि कपिलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार महर्षि कपिल मुनि ने तपस्या की थी। शायद इसी कारण से इस मंदिर का नाम कपिलेश्वर महादेव रखा गया। मंदिर के भीतर एक चट्टान पर शिव सूर्य एवं शिवलिंग की आकृति मौजूद है। मंडी में प्रवेश करने के लिए दर्शनार्थियों को 200 से भी अधिक चिड़ियों को चढ़ना पड़ता है।
कपिलेश्वर मंदिर का निर्माण के विषय में माना जाता है कि भगवान शिव जी को समर्पित इस दिव्य मंदिर का निर्माण आठवीं और दसवीं शताब्दी के आसपास कत्यूरी राजाओं ने किया था। मंदिर में स्थित शिवलिंग प्राकृतिक तरीके से बना हुआ है। इसलिए स्थानीय इलाकों में इस मंदिर के प्रति अटूट विश्वास देखने को मिलता है।

कपिलेश्वर महादेव मंदिर कहानी. Kapileshwar Mahadev Mandir Kahani
दोस्तों पौराणिक कहानी के आधार पर कहा जाता है कि कपिलेश्वर महादेव मंदिर के सामने हैं ही मौन मंदिर भी शामिल है। कपिलेश्वर मंदिर में दो नाग रहते थे और एक समय की बात है जब उन दोनों नागों में शर्त लग जाती है कि कौन एक दूसरे के मंदिर को जल्दी तोड़ता है। इसी शर्त के अनुसार जब मौन कपिलेश्वर मंदिर को तोड़ने जाता है तो अखिलेश्वर मंदिर का नाम मौन के मंदिर को तोड़ने जाते हैं।
कपिलेश्वर महादेव मंदिर के नाग ने मौन के मंदिर को तहस-नहस कर दिया और जब वह और जब मौन कपिलेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ने वाले होते हैं तो तुरंत ही कपिलेश्वर मंदिर के नाम आ जाते हैं और उन्हें अपनी जीत के बारे में बताते हैं तो मौन मंदिर के नाम वापस चले जाते हैं। मैंने तो है कि इस मंदिर के सामने बहने वाली नदी के किनारे पत्थरों में आज भी सफेद रंग के निशान है। खूबसूरत पहाड़ियों के मध्य एवं नदी के आकर्षक दृश्यों को प्रस्तुतकर्ता कमलेश्वर महादेव मंदिर एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी जाना जाता है।
कपिलेश्वर महादेव मंदिर कैसे पहुंचे. Kapileshwar Mahadev Mandir Kese Pahuchen
कपिलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग के साथ-साथ वायु मार्ग का विकल्प भी उपलब्ध है। लेकिन कपिलेश्वर महादेव मंदिर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होने के कारण बस एवं टैक्सी के द्वारा कपिलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचना काफी आसान है।
कपिलेश्वर महादेव मंदिर पिथौरागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वही कपिलेश्वर महादेव मंदिर देश की राजधानी दिल्ली से लगभग सर 400 किलोमीटर की दूरी पर जहां से बस एवं प्राइवेट टैक्सी के द्वारा आराम से पहुंचा जा सकता है
दोस्तों यह तो हमारा आज का लेख जिसमें हमने आपको कपिलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया होगा। यदि आपको यह लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।



































































































































































































































































































































































































































.jpg)
